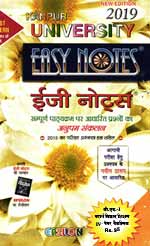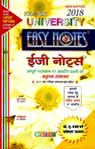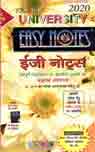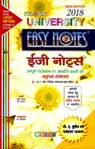|
शिक्षाशास्त्र >> ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षण ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षणईजी नोट्स
|
|
||||||
बी.एड.-I प्रश्नपत्र-4 (वैकल्पिक) पदार्थ विज्ञान शिक्षण के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
प्रश्न 1. पाठ्यक्रम संगठित करने की कौन-कौन-सी विधियाँ (उपागम) हैं?
अथवा
स्कूल पाठ्यक्रम निर्माण के लिये किसी एक विधि की विवेचना कीजिए।
उत्तर- विज्ञान का पाठ्यक्रम संगठन
(Organisation of Curriculum in Science)
पाठ्यक्रम संगठन निम्नलिखित पद्धतियों के आधार पर किया जाता है -
1. उप-विषय पद्धति (Topical Method) - पाठ्यक्रम संगठन की उप-विषय वह विधि है
जिसमें किसी विषय के एक प्रकरण को जिस कक्षा में आरम्भ किया जाता है उसे
पूर्णरूप से उसी कक्षा में समाप्त कर दिया जाता है। जैसे - हाईस्कूल कक्षाओं
में यदि गुणनखण्ड, संख्या-पद्धति और बैंक जमा पूंजी के प्रकरण प्रारम्भ किये
गये हैं तो इन प्रकरणों से सम्बन्धित सभी प्रकार की सरल एवं जटिल समस्याओं का
ज्ञान हाईस्कूल में ही पूरा करा दिया जाता है जिससे विद्यार्थी एक ही प्रकार की
समस्याएं एक लम्बे समय तक हल करता रहता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को नियम,
सूत्र और सिद्वान्तों का काफी अभ्यास हो जाता है जिससे उस पाठ्यक्रम के सारे
प्रकरण उसको समझ में आ जाते हैं लेकिन कुछ विषयों के विभिन्न प्रकरण एक दूसरे
से अलग होते हैं जिससे एक प्रकरण अन्य विषयों के प्रकरण से सह-सम्बन्धित नहीं
होता है जिससे विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई होती है।
2. चक्राकार पद्धति (Spiral Method) - चक्राकार पद्धति में किसी विषय के एक
प्रत्यय की थोड़ी-थोड़ी जानकारी प्रत्येक कक्षा में करायी जाती है। जैसे-जैसे
बच्चा आगे की कक्षा में पहुँचता है वैसे-वैसे पूर्व में पढ़ाये गये प्रत्ययों
का ज्ञान भी विस्तृत होता जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों के मानसिक विकास के
साथ-साथ उस प्रत्यय की कठिनता भी बढ़ती जाती है जिससे विद्यार्थी उन प्रकरणों
का ज्ञान सरलता एवं सुगमता से प्राप्त करता है। जैसे - किसी विद्यार्थी को
संख्या पद्धति, समीकरण आदि के सम्बन्ध के बारे में कक्षा 6 में सरल ज्ञान कराया
जाता है। इसके बाद कक्षा का स्तर बढ़ने के साथ-साथ उसका ज्ञान बढ़ता जाता है।
अत: इस पद्धति के अन्तर्गत किसी भी उप-विषय के प्रत्यय को किसी कक्षा में
पढ़ाकर पूर्णतया समाप्त नहीं कर दिया जाता बल्कि विद्यार्थियों की आयु और
मानसिक स्तर के अनुसार उस उप-विषय के केवल उतने ही कठिन प्रश्न हल करायें जाते
हैं जिन्हें विद्यार्थी आसानी से समझ सकें। इस प्रकार विद्यार्थी के मानसिक
स्तर के साथ-साथ उप-विषय कठिनाई स्तर बढ़ाई जाती है। प्रत्यय की पूरी जानकारी
प्रारम्भ में ही दे दी जाती है।
3. आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति (Organised and Incidental Method) - इस पद्धति
में एक किसी विषय को केन्द्र मानकर पढ़ाया जाता है। इस केन्द्रित विषय को
पढ़ाते समय जो अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं वे अकस्मात ही पढ़ाये जाते हैं,
पढ़ाने वाले ने इसको पढ़ाने की कोई विशेष योजना नहीं बनायी होती। जैसे - हमारा
केन्द्रीय विषय है, "भाखड़ा बाँध का भ्रमण" अब इस विषय का अध्ययन करते समय
पिछले अनुभवों का ज्ञान, स्थान कहाँ है, किधर है, ऊँचा है, नीचा है, भ्रमण आदि
पढ़ाने का विषय केवल भाखड़ा बाँध का भ्रमण है। इस प्रकार विज्ञान में पढ़ाने की
विधि को प्रासंगिक विधि कहा जाता है। इस विधि का सिद्धान्त यह है कि ज्ञान की
एक इकाई है, इसके भिन्न-भिन्न अंग नहीं होते हैं। ज्ञान इकाई के रूप में ही
देना चाहिये। इस विधि द्वारा विद्यार्थी ज्ञान अंगों से परिचित हो जाता है। इस
विधि के द्वारा प्रोजेक्ट विधि से प्राप्त प्रासंगिक होता है। प्रोजेक्ट
प्रणाली हरबर्ट के विषय संगठन का परिणाम है।
4. प्रक्रिया उपागम (Process Approach) - इस विधि के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के
प्रारूप को विकसित करने में पाठ्य-वस्तु के ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है।
अत: इससे पाठ्य-वस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया
जाता है।
5. सहसम्बन्ध उपागम (Correlation Approach)- पाठ्यक्रम संगठन के इस उपागम से
अभिप्राय विषयों के परगर समान आधारों पर सम्बन्धों से माना जाता है जिससे एक
विषय के शिक्षा में
दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। इसे पूर्ववर्ती ज्ञान का सिद्धान्त भी कहा
जाता है। इसके अनुसार पूर्व विचारों से नवीन विचारों को सम्बन्धित कर दिया जाता
है। जॉन डी.वी. ने इस प्रकार की सम्बद्धता को सामंजस्यीकरण का नाम दिया है।
6. संकेन्द्रित उपागम (Conceantric Approach) - संकेन्द्रित उपागम पर आधरित
पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर बालकों की सामान्य अवधारणाएँ विकसित करने पर बल
दिया जाता है जो मानव जीवन की दैनिक गतिविधियों पर आधारित उच्च कक्षाओं में
विद्यार्थी अधिक कठिन सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभवों का क्रमबद्ध
संगठन संयुक्त अधिगम प्रदान करता है। यह अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त सरल से
जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है।
7. इकाई उपागम (Unit Approach)-एक संगठित पाठ्यक्रम जैसे गृहकार्य का पाठ्य
सामग्री का उचित विभाजन आदि समान तत्वों को सामूहिक रूप से एकत्रित करके सीखना
आसान हो जाता है। यह सामान्यीकरण की ओर संकेत देता है। इससे सूझ-बूझ आसान हो
जाती है। सूचनाओं अधिगम अनुभवों तथा विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों,
शैक्षिक, रुचि, वृत्तियों को विकसित करने तथा कुछ निश्चित बोध तक पहुँचाने के
लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री का संग्रह इकाई है। इकाई का उद्देश्य
ही सामग्री को सम्मिलित करना या निश्चित करना है। इकाई में केवल वह सामग्री ही
सम्मिलित की जाती है जो उपयुक्त हो और उद्देश्य प्राप्ति पर बल देती हो।
|
|||||