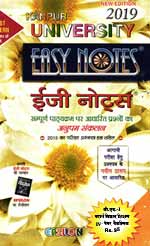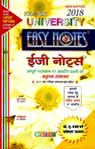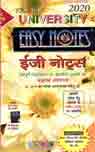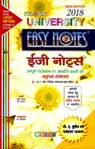|
शिक्षाशास्त्र >> ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षण ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षणईजी नोट्स
|
|
||||||
बी.एड.-I प्रश्नपत्र-4 (वैकल्पिक) पदार्थ विज्ञान शिक्षण के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
प्रश्न 1. पाठ्यक्रम (Curriculum) किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के
विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
अथवा
पाठ्यक्रम संगठन के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। पाठ्यक्रम संगठन के किस
उपागम को उपयुक्त मानते हैं तथा क्यों?
अथवा
पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिये। पाठ्यक्रम संगठन के विभिन्न सिद्धान्तों का
वर्णन कीजिये। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य झुकाव क्या होना चाहिये?
अथवा
पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। पदार्थ विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन
बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए।
अथवा
पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं? विस्तृत व्याख्या कीजिए।
1. पाठ्यक्रम की परिभाषा बताइये।
2. पाठ्यक्रम के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
3. पाठ्यक्रम संगठन के उपागमों को बताइये।
उत्तर-पाठ्यक्रम की परिभाषाएँ
(Definition of Curriculum)
पाठ्यक्रम लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कैयूटर Currer शब्द से हुई है।
इसका अर्थ है 'दौड़ का मैदान' अत: पाठ्यक्रम शब्द दौड़ के मैदान का पर्याय है।
जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी एक निश्चित लेन में दौड़कर अपनी गन्तव्य दूरी को
प्राप्त करता है। उसी प्रकार विद्यार्थी एक-एक निश्चित पाठ्य-वस्तु का अध्ययन
करके शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। यह एक त्रिकोणकारी प्रक्रिया
हैं जिसमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। यथार्थ रूप
में पाठ्यक्रम ही स्कूली शिक्षा का आधारभूत स्तम्भ हैं। इसी के द्वारा शिक्षा
के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पाठ्यक्रम ही छात्रों
और अध्यापकों के मध्य समन्वय का कार्य करता है तथा दोनों के बीच शिक्षण
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित मार्ग का गठन होता है। वहीं दूसरी ओर
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पाठ्यक्रम महत्त्वपूर्ण है। इसके
द्वारा कार्य की निश्चितता होने के कारण उसकी सफल समाप्ति पर सन्तोष और आनन्द
की अनुभूति होती है। प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा पाठ्यक्रम की निम्नलिखित
परिभाषाएँ दी गई हैं।
मुनरो के अनुसार-"पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा
के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है।"
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार- "पाठ्यक्रम, पाठ्य-वस्तु का सुव्यवस्थित रूप
है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है।"
फ्रोबेल के अनुसार—“पाठ्यक्रम मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार
है।"
इस तरह उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यक्रम वृहद
रूपरेखा है जिसको छात्र कक्षा द्वारा, प्रयोगशाला द्वारा, खेल द्वारा अपने
अध्यापकों में अनौपचारिक रूप से अर्जित किया जाता है। इस तरह मानव का जीवन भी
पाठ्यक्रम का एक अंग है।
पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त
(Principles of Curriculum Construction)
पाठ्यक्रम निर्माण में विशिष्ट सिद्धान्तों की अनदेखी करने के कारण पाठ्यक्रम
में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अत: इन दोषों को दूर करने के लिए
पाठ्यक्रम निर्माण के समय निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुपालन करना चाहिए।
(1) क्रियाशीलता का सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम का गठन इस
प्रकार करना चाहिए जिसमें यह बच्चों को भार के समान महसूस न हो अत: पाठ्यक्रम
में ऐसे सिद्धान्तों और बातों को भी शामिल करना चाहिए जिससे विद्यार्थी विज्ञान
के गूढ़ तथ्यों के अतिरिक्त पढ़ते समय आनन्द और क्रियाशीलता का अनुभव करे।
(2) उपयोगिता का सिद्धान्त विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।
अत: विज्ञान पाठ्यक्रम में उन बातों को शामिल करना चाहिए जो हमारे व्यावहारिक
जीवन में काम आती हो और वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी हो।
(3) सामाजिक आदर्शों का सिद्धान्त—पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामाजिक
आदर्शों और लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐसे
प्रकरणों को सम्मिलित करना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं के समाधान में लाभकारी
हों।
(4) लोच का सिद्धान्त पाठ्यक्रम लोचहीन नहीं होना चाहिए। इसमें समय, परिस्थिति
व आयु के अनुसार परिवर्तन की सम्भावना होनी चाहिए जिसमें बच्चों की विभिन्न
रुचियों के अनुसार अध्ययन की सुविधा का प्रावधान हो। हमें अपने ज्ञान के अनुसार
पाठ्यक्रम को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए।
(5) विविधता का सिद्धान्त—पाठ्यक्रम विषय-केन्द्रित न होकर बालक केन्द्रित होना
चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण स्थान, सभ्यता और सांस्कृतिक परिस्थितियों को
ध्यान में रखकर करना चाहिए।
(6) प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धान्त क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों,
शिक्षकों और पाठ्यक्रम से मिलकर होता है। अत: पाठ्यक्रम को छात्रों एवं
शिक्षकों की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए
जिसके द्वारा एक-दूसरे के समान की भावना जाग्रत हो तथा सामूहिक स्तर पर
समस्याओं के निवारण और अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध हो।
(7) सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त—पाठ्य-वस्तु एकांकी न होकर अन्य विषयों से भी
सम्बन्धित होना चाहिए। एक विषय का दूसरे विषय के साथ पारस्परिक समन्वय रहना
चाहिए।
(8) तर्क एवं मनोविज्ञान का सिद्धान्त - तर्क एवं मनोविज्ञान शिक्षा की दो
आधारभूत आवश्यकताएँ हैं। पाठ्यक्रम को बालक की रुचि, आयु, उत्साह, क्षमता के
अनुसार तथा उनमें तार्किक शक्ति को विकसित करने का लक्ष्य होना चाहिए। छोटी
अवस्था में बच्चों के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग होना लाभकारी है। वहीं बड़ी
कक्षाओं में तार्किक पाठ्य-वस्तु पर बल देना चाहिए।
पाठ्यक्रम संगठन के उपागम किसी भी विषय का पाठ्यक्रम कई विषय वस्तुओं का
संक्षिप्त रूप होता है। अत: पाठ्यविषयों को संगठित करने के लिए शिक्षा विदों ने
अलग-अलग दृष्टिकोणों के उपागमों का वर्णन किया हैं-
(1) सह-सम्बन्ध उपागम (Correlation Approach),
(2) समन्वित उपागम (Integrated Approach),
(3) केन्द्रित उपागम (Concentric Approach),
(4) चक्राकर उपागम (Spiral Approach),
(5) इकाई उपागम (Unit Approach),
(6) कालक्रम उपागम (Chargonological Approach)|
वैसे तो पाठ्यक्रम संगठन में प्रत्येक उपागम का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।
किन्तु विषय की प्रकृति, जटिलता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि देखा
जाये तो एकीकृत रूप समन्वित उपागम विशेष उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है।
समान्वित उपागम (Integrated Approach) - एकीकृत अथवा समन्वित उपागम का.
तात्पर्य पाठ्यवस्तु के विभिन्न खण्डों, इकाइयों या अंशों को समग्र रूप में
एकत्रित करने तथा निकट लाने की प्रक्रिया पाठ्यक्रम के इस एकीकृत रूप में इस
प्रकार से परिवर्तन कि छात्रों को नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके तथा
पाठ्यक्रम उनके जीवन की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकें।
यद्यपि यह एक अमेरिकी सम्प्रत्यय है किन्तु सर्वप्रथम भारत में कोठारी आयोग
(1964-66) ने इस उपागम की ओर संकेत किया था। समाज में अपव्यय अवरोधन की समस्या
को दूर करने के लिए इस उपागम पर बल दिया। इस उपागम में निम्नलिखित स्तरों पर
विशेष बल दिया गया है-
(1) छात्रों को स्वयं अनुभव के बल पर सीखने के लिए स्वतन्त्र रूप से प्रेरित
करना।
(2) ज्ञान की प्राप्ति में केवल विषयों को ही शिक्षा न देकर व्यावहारिक पक्ष पर
बल देना।
(3) छात्र की रुचि तथा अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
पाठ्यक्रम संगठन के इस उपागम में यह व्यवस्था होती है कि-
-पाठ्यक्रम को छोटी-छोटी इकाइयों में क्रमबद्धता के साथ विभाजित कर लिया जाता
है।
- विषयवस्तु को सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थल की ओर संगठित
किया जाता है।
-ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।
-छात्र अपनी रुचि सामर्थ्य तथा योग्यता के अनुरूप इन इकाइयों का अध्ययन करता
है।
-इसमें इकाइयों को पूरा करने के बाद दूसरी इकाई का अध्यापन किया जाता है।
-इसमें कमजोर तथा पिछड़े छात्र की सरलता एवं शीघ्रता से सीख सकते हैं तथा तेज
बुद्धि के छात्र कम समय में अधिक सीख सकते हैं।
इस प्रकार पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्याओं का सरलता से निराकरण इस उपागम के द्वारा
किया जा सकता है। साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली तथा बालकों की रुचि के अनुरूप
बनाया जा सकता है। विज्ञान विषयों के लिए यह उपागम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध
हुआ है।
|
|||||