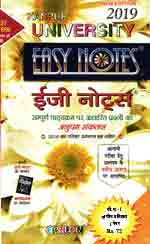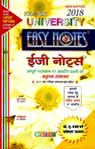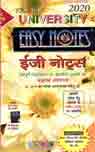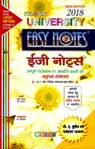|
इतिहास >> ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्रईजी नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
(3)
ईरानी आक्रमण (Persian Invasion)
दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. ईरानी आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी ? स्पष्ट कीजिए।
भारतवर्ष पर पारसी प्रभाव का वर्णन कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. ईरानी आक्रमण के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ?
2. क्षयार्षा (जरक्सीज) पर टिप्पणी लिखिए।
3. फारसी सम्पर्क के क्या परिणाम प्राप्त हुए ?
उत्तर -
ईरानी आक्रमण
छठी शती ई. के पूर्व उत्तरार्द्ध में भारत अनेक छोटे-छोटे राज्य में विभक्त
था। उनमें परस्पर द्वेष भी कुछ कम न था, उनकी पारस्परिक ईर्ष्या और कलह को
दबाकर रखने वाला कोई प्रबल राष्ट्र भी उनके समीप न था। इसी कारण फारस के हखमी
(Achaemenian) राजकुल के साम्राज्य की मनोरथों के लिए वह प्रबल आकर्षण सिद्ध
हुआ, हखमी साम्राज्य ठीक इसी काल कुरुष अथवा साइरस (Cyrus, लगभग ई. पूर्व
558-30) के नेतृत्व में प्रसार के लम्बे डग भर रहा था। उसने अपने साम्राज्य
की पश्चिमी सीमाएँ भूमध्य सागर तक फैला लीं और गन्धार पर भी अधिकार कर लिया
था, परन्तु भारतीय सीमा के भीतर वह प्रवेश नहीं पा सका था। उसके उत्तराधिकारी
काम्बुजीय प्रथम, कुरुष द्वितीय और काम्बुजीय द्वितीय (530-22 ई. पूर्व) तो
अपने शासनकाल में पश्चिम में इतना उलझे रहे कि उन्हें पूर्व के विषय में
सोचने का अवकाश ही नहीं मिला, परन्तु दारायवौष, प्रथम (Darius 522-486 ई.
पूर्व) ने निश्चय सिन्ध नदी की तटवर्ती भूमि का एक भाग जीत लिया था। यह
पर्सिपोलिस और नक्श-ए-रुस्तम के उसकी कब्र के अभिलेखों से प्रमाणित है। इनमें
हिन्दू अथवा सिन्धु (तट) के निवासियों को फारस की प्रजा कहा गया है। यह विजय
उस बेहिस्तुन अभिलेख (जिसमें फारसी प्रजाओं के परिगणन में हिन्दुओं का नाम
नहीं है।) की संभाव्य तिथि 518 ई. पूर्व के पश्चात् और दारायर्वोष प्रथम की
मृत्यु की तिथि 486 ई. पूर्व के बहुत पूर्व हुई होगी।
इतिहासकार हेरोडोट्स के वर्णन से उस प्रयत्न पर प्रकाश पड़ता है जो डेरियस
(दारायवौष) ने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के अर्थ में किया था। इससे विदित होता है
कि उसने 517 ई. पूर्व के कुछ बाद कार्यन्दा के स्काईलक्स (Skylax) को सिन्धु
के मार्ग से फारस तक सामुद्रिक जलमार्ग खोजने के अर्थ में भेजा । स्काईलक्स
सिन्धु नदी से समुद्र और वहां से फारस पहुंचा और उसने वह सारी जानकारी
प्राप्त कर ली जिसके लिए वह भेजा गया था और जिसका दारायवौष (डायरिस) अपनी
अर्थ-सिद्धि के हेतु सदुपयोग किया। हेरोडोट्स लिखता है कि यह विजित भारतीय
भाग, जिसमें पंजाब का केवल कुछ हिस्सा शामिल था, फारसी साम्राज्य का बीसवां
प्रान्त (क्षत्रपी) बना जहाँ से साम्राज्य को स्वर्णचूर्ण के रूप में
प्रतिवर्ष प्रायः दस लाख पौण्ड से अधिक की आय होती थी। इससे स्पष्ट है कि यह
भू-भाग उर्वर, जन-संकल्प और समृद्ध था।
क्षयार्षा (जरक्सीज Xerkes)
डायरिस प्रथम के उत्तराधिकारी क्षर्याषा अथवा जरक्सीज (486-65 ई. पूर्व) के
शासनकाल में उसकी जिस सेना ने ग्रीस पर आक्रमण किया था उसमें 'सूती वस्त्र
पहने और बेंत के धनुष तथा लौहफलक के बाण' धारण किये हुए भारतीय योद्धा भी
शामिल हुए थे। इससे सिद्ध होता है कि क्षर्याषा ने भारत के उत्तरी पश्चिमी
भाग पर अपना अधिकार बनाये रखा। सम्भवतः फारस का यह प्रभुत्व कुछ काल तक और
बना रहा, यद्यपि यह बताना कठिन है कि भारत और फारस का यह सम्बन्ध कब टूटा। इस
के फिर भी कुछ प्रमाण उपलब्ध हैं कि सिकन्दर के विरुद्ध लड़ने वाली डेरियस
तृतीय कोरोमनल की सेना में कुछ भारतीय वीर थे।
यह राजनैतिक सम्पर्क दोनों देशों के पारस्परिक लाभ का कारण हुआ, व्यापार को
प्रोत्साहन मिला और सम्भवतः संगठित फारसी साम्राज्य को देख भारतीयों में भी
उसी प्रकार के संगठित साम्राज्य की महत्वाकांक्षा जागी। फारसी लेखकों ने भारत
में अर्मई लिपि (Armaic) का प्रचार किया जिससे कालान्तर में खरोष्ठी विकसित
हुई। यह खरोष्टि लिपि अरबी की भांति दाहिनी ओर से बायीं को लिखी जाती है और
इसी लिपि में सदियों तक पश्चिमोत्तर सीमा में अभिलेख लिखे गये। विद्वानों ने
चन्द्रगुप्त मौर्य की सभा के आचारों पर भी फारसी प्रभाव का आभास पाया है। इसी
प्रकार यह प्रभाव संभवतः अशोक के अभिलेखों की प्रस्तावना तथा स्तम्भों आदि,
विशेषकर उनके शीर्षों की घंटानुमा आकृतियों पर भी बताया जाता है।
फारसी सम्पर्क के परिणाम
फारसी सम्पर्क के निम्नलिखित परिणाम हुए-
1. यह राजनीतिक सम्पर्क दोनों देशों के पारस्परिक लाभ का कारण हुआ।
2. इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला।
3. सम्भवतः फारसी साम्राज्य को देख भारतीयों में भी उसी प्रकार की संगठित
साम्राज्य की महत्वाकांक्षा जागी।
4. फारसी लेखकों ने भारत में अर्मई लिपि (Armaie) का प्रचार किया जिससे
कालान्तर में खरोष्ठी विकसित हुई। खरोष्ठी लिपि अरबी की भाँति दाहिनी ओर से
बायीं ओर को लिखी जाती है। इसी लिपि में सदियों तक पश्चिमोत्तर सीमा में
अभिलेख लिखे गये हैं।
5. कुछ इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त मौर्य की सभा के आचारों पर भी फारसी
प्रभाव का आभास पाया है।
इसी प्रकार यह प्रभाव सम्भवतः अशोक के अभिलेखों की प्रस्तावना तथा. स्तम्भों
आदि विशेषकर उनके शीर्षों की घण्टानुमा आकृतियों पर भी बताया जाता है।
इस प्रकार विजित देशों की जनता को फारसी सम्राट को भारी कर अदा करना और अपने
सम्राट की सेना में नौकरी के लिए भेजना पड़ता था। कर की उगाही के बाद ग्राम व
नगर ऐसे लगते थे कि जैसे कोई अभी-अभी इन्हें आकर लूट गया हो। उधर सरकारी
खजाना उत्तरोत्तर भरता ही जा रहा था । सम्राट के अनगिनत महल और तहखाने सोने
की गिन्नियों से अटे पड़े थे।
विजित देशों में जब विद्रोह फूट पड़ते थे तब सम्राट को उनकी सूचना तुरन्त मिल
जाती थी। मार्गों पर फारसियों ने घुडसवारों की चौकियां कायम की हुई थीं।
सारसों जैसे तीव्रगामी घुड़सवार स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त रपटें राजधानी
तक और सम्राट के आदेश स्थानीय अधिकारियों तक पहुँचा देते थे। विद्रोहियों के
विरुद्ध भेजी गयी सेनाएं निर्ममतापूर्वक उन्हें कुचल डालती थीं। फिर भी फारसी
सम्राट विजित देशों की जनता को जो विजेताओं से घोर नफरत करती थी, बड़ी कठिनाई
से अपने वश में रख पाते थे।
|
|||||