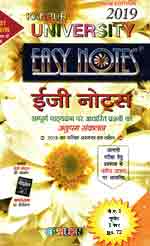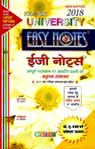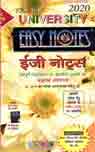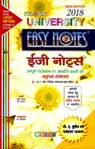13
भूमिगत जल के द्वारा स्थलाकृतियों का विकास
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में
स्थित जल को भूमिगत जल की संज्ञा प्रदान की जाती है। वर्षा का जल विभिन्न
रूपों में धरातल की ऊपरी सतह से रिस करके नीचे चला जाता है तथा पारगम्य
चट्टानों के रिक्त स्थानों में एकत्र होकर भूमिगत जल का रुप धारण करता है।
भूमिगत जल कार्य सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों स्थानों पर होता है, क्योंकि ऊपरी
सतह पर भी जल रिसते समय कुछ अपरदन का कार्य (धोलीकरण Solution) करता है,
जिससे छोटे-छोटे गर्त तथा कटक का निर्माण होता है। ऊपरी सतह के नीचे जब
पारगम्य शैल की स्थिति होती है तो ऊपरी जल का रिस कर नीचे चला जाता है जहाँ
पर अपरदन तथा निक्षेप द्वारा स्थलरुपों का सृजन तथा विकास करता है। भूमिगत जल
के अन्तर्गत जब तक गति नहीं होती है तब तक उसका भूगर्भशास्त्र एवं
भूआकृतिविज्ञान की दृष्टि से महत्व नहीं होता है, क्योंकि इस परिस्थिति में
भूमिगत जल स्थलरूप के निर्माण में निष्क्रिय होता है। गतिशील भूमिगत जल का ही
सम्बन्ध भूगोल तथा भूगर्भशास्त्र के विधार्थियों
से होता है। भूमिगत जल की समस्त मात्रा का ठीक पता लगाना कठिन है क्योंकि यह
अदृश्य तथा अलभ्य स्थान पर होता है। प्रायः ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि
समस्त भूमिगत जल को धरातल की सतह पर ला दिया जाय तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर
सर्वत्र 500 फीट की ऊंचाई तक जल का विस्तार हो जायेगा।
भूमिगत जल द्वारा अपरदनात्मक कार्य (Erosional Work of groundwater) अपरदन के
अन्य कारकों के समान ही भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य भी कई रूपों में
सम्पन्न होता है। अपक्षय के साथ विघटित तथा वियोजित चट्टानों के सामूहिक
स्थानान्तरण (mass translocation) में भूमिगत जल का महत्व अत्यधिक होता है।
अपक्षय के कारण चट्टानें जब विघटित तथा वियोजित होकर ढीली पड़ जाती हैं तो
भूमिगत जल चट्टानों की भग्न राशि (rock waste) को सामूहिक रूप से खिसकने में
चिकनाहट या स्नेहन (lubrication) का कार्य करता है। जल से चट्टानें संतृप्त
(saturated) होकर ऊंचे ढालों से निचले भागों में सामूहिक रुप से सरकने लगती
हैं। इस क्रिया को 'भग्नराशि का सामूहिक स्थानान्तरण' (mass translocation of
rockwaste) कहते हैं। इसके अन्तर्गत भूमिस्खलन, मृदासपर्ण (solifluchion)
भूमि सर्पण, पंक वाह (mud flow) अवपात (slumping) आदि को सम्मिलित किया जाता
है। भूमिगत जल का वास्तविक अपरदनात्मक कार्य निम्न रूपों में सम्पन्न होता
है-
(i) घुलन क्रिया (solution)
(i) जलगति क्रिया (hydraulic action)
(iii) अपघर्षण (corrasion or abrasion)
(iv) सन्निघर्षण (attrition)
भूमिगत जल द्वारा निक्षेपात्मक कार्य (Depositional work of
Groundwater)-अपरदनात्मक कार्य में धोलीकरण के समान ही भूमिगत जल का निक्षेपण
कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। घुलनक्रिया के कारण भूमिगत जल में कई प्रकार
के रासायनिक खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। इस तरह एक निश्चित सीमा के बाद भूमिगत
जल अवसाद से परिपूर्ण हो जाता है तथा और अधिक पदार्थ को समाविष्ट करने की
सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाती है। परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदार्थ का निक्षेपण
प्रारंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त घोल में मिला हुआ बारीक पदार्थ निम्न
कारणों से निक्षेपित होने लगता है-
1. भूमिगत जल के मार्ग में थोड़ा भी अवरोध आने पर उसका वेग शिथिल हो जाता है,
जिससे घुलित पदार्थ नीचे बैठने लगता है।
2. जब किसी कारण से भूमिगत जल का ताप बढ़ जाता है तो उसका कुछ जल भाप बन जाता
है। इस कारण जल के कुछ आयतन में कमी के कारण जल की घोलन शक्ति कम हो जाती है।
फलस्वरूप शेष जल समस्त घुले हुए पदार्थ को धारण नहीं कर सकता है।
3. उपर्युक्त स्थिति के विपरीत यदि भूमिगत जल का ताप कम हो जाता है तो उस जल
की घुलन शक्ति भी कम हो जाती है। परिणामस्वरूप पहले से घुले हुए पदार्थ का
कुछ भाग निक्षेपित होने लगता है।
4. भूमिगत जल की घुलाने की सामर्थ्य अधिक दबाव के कारण बढ़ जाती है, परन्तु
जैसे ही दबाव कम होने लगता है, धुले हुए पदार्थ का निक्षेपण होने लगता है,
क्योंकि दबाव में कमी के कारण घोलन शक्ति में भी कमी आ जाती है।
5. भूमिगत जल की घोलन सामर्थ्य बहुत कुछ कार्बन डाई आक्साइड गैस की मात्रा पर
आधारित होती है। इसकी बढ़ती हुई मात्रा के साथ घुलन क्रिया बढ़ती जाती है।
परन्तु जब किसी कारण से भूमिगत जल में इस गैस की कमी हो जाती है तो घुलन
सामर्थ्य में कमी के कारण निक्षेपण होने लगता है।
6. जब भूमिगत जल के मार्ग में शैवाल (algae) आदि आ जाती हैं तो धुलित पदार्थ
इनके साथ एक जाग है तथा नीचे बैठने लगता है।
उपर्युक्त कारणों की व्यवस्था के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि जल की घोलन
सामर्थ्य में कमी के कारण निक्षेपण होता है। जल के घोलन सामर्थ्य में कमी,
उपर्युक्त विवरण के आधार पर ताप में कमी, वाष्पीकरण, दबाव में कमी, कार्बन
डाइ आक्साइड की मात्रा में कमी आदि कारणों से होती है।
स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
* पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भू-पटल के चट्टान के छिद्रों एवं दरारों में
संचित जल को भूमिगत जल कहा जाता है।
* भूमिगत जल अधिकतम 6 मील की गहराई तक पाया जाता है। इससे अधिक गहराई पर
अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों के छिद्र एवं दरारें बन्द हो जाती है। * धरातल
के अन्दर से जब जल प्राकृतिक रुप से बाहर निकलकर, बहने लगता है तो उसे 'सोता'
(Spring) कहा जाता है।
* 'सोते' सामान्यतः वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ मेघ
चट्टानों के नीचे अमेघ चट्टानों की परतें होती हैं।
* कुछ ऐसे कुएं हैं जिनसे पानी स्वयं सतह से ऊपर निकलता रहता है, ऐसे कुओं को
'आर्टिजन' या 'उत्स्त्रुत कुआं' (Artesian wells) कहा जाता है।
* संसार के सबसे विस्तृत आर्टिजन बेसिन आस्ट्रेलिया में पाये जाते है।
* वह स्तर, जिसके नीचे पारगम्य चट्टानें (Permeable Rocks) जल से संतृप्त
(Saturated) रहती हैं, भौम जल स्तर या जल तल (water table) कहलाता है। * भौम
जल स्तर संतृप्त मण्डल का ऊपरी तल होता है।
* भूमिगत जल का कार्य सतह से ऊपर एवं सतह के नीचे दोनों ही स्थानों पर होता
है।
* भूमिगत जल द्वारा रासायनिक ऋतुक्षरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके
अन्तर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मिश्रित जल, चूना पत्थर (Limestone), डोलोमाइट
(Dolomite) एवं खड़िया (Chalk) जैसे घुलनशील चट्टानों को तेजी से घुलाता है,
जिसके फलस्वरूप, ‘कार्ट स्थलाकृति' का विकास होता है।
* 'कार्स्ट' शब्द युगोस्लाविया से लिया गया है, जहां एड्रियाटिक सागर के तट
पर स्थित युगोस्लाविया एवं इससे सटे इटली में चूना पत्थर का पठार है, जिसे
काट प्रदेश कहा जाता है।
* जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि
के अंदर प्रवेश करता है तो सतह के ऊपर मिट्टी की एक पतली परत का विकास होता
है, जिसे टेरा-रोसा (Terra Rossa) कहा जाता है।
* टेरा-रोसा नामक मिट्टी में क्ले, चूना एवं लोहा की प्रधानता होती है।
* जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ एवं असमान हो
जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को 'लैपीज' (Lapies) कहा जाता है। [कानपुर
2019]
* 'लैपीज' को इंग्लैण्ड में क्लिन्ट (Clint), जर्मनी में कैरेन (Karren),
साइबेरिया में बोगाज के नाम से जाना जाता है।
* चूना पत्थर प्रदेशों में वर्षा का जल विलियन क्रिया द्वारा चट्टानों की
संधियों पर कई छोटे-छोटे छिद्रों का निर्माण करता है। इन छिद्रों को घोल
रंघ्र (Sinkholes) कहा जाता है।
* जब घुलन क्रिया के फलस्वरूप घोल रंध्र का विस्तार अधिक हो जाता है उसे
डोलाइन (Doline) कहा जाता है।
* जब मृत्तिका (Clay) द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है तो जल
रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। फलस्वरूप जल के जमा होने के कारण छोटी-छोटी
अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों को ‘कार्ट झील' कहा जाता है।
* जब भूमिगत नदियों के मार्ग में दो निकटवर्ती डोलाइन या विलयरंघ्र के बीच का
धरातल धवस्त होकर गिर जाता है, तो भूमिगत जल प्रवाह धरातल पर दृष्टिगोचर होने
लगता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को 'कार्ट खिड़की' (Carst windows) कहा जाता
है।
* कई डोलाइनों के मिलने से निर्मित वृहदाकार गर्न को 'युवाला' (uvalas) कहा
जाता है।
* युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्तों को पोल्जे (polje) कहा जाता है। पोल्जे
की तली समतल एवं दीवारें खड़ी होती है।
* कुन्दरा या गुफा (Care or Caverms) का निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया
एवं अपघर्षण के फलस्वरूप होता है। यह धरातल के नीचे एक खोखली आकृति होती है।
* भारत में देहरादून, बिहार के रोहतास (गुप्त धाम कंदरा), मध्य प्रदेश में
बस्तर (कुटुम्बसार), चित्रकूट आदि स्थानों में कन्दरा देखने को मिलते हैं।
* भौम कंदराओं को जो विलय छिद्र धरातल से मिलता है, उसे युगोस्लाविया में
पोनोर कहा जाता है।
* भूमिगत कन्दराओं में जल के वाष्पीकरण होने के फल-स्वरूप कन्दरा के तल एवं
छत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होने लगता है। यह निक्षेप लम्बे एवं
पतले स्तंभों के रूप में होता है, जो कंदरा के तल की ओर बढ़ते जाते हैं। इन
लटकते हुए स्तंभों को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। जब फर्श पर स्तंभ की आकृति
बनकर ऊपर की ओर विकसित होती है, तो उसे स्टैलेग्माइट (stalagmites) कहा जाता
है।
...Prev | Next...