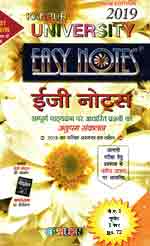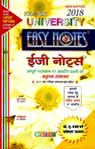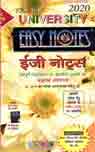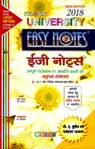|
भूगोल >> ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्रईजी नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
12.
हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विकास
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
अपरदन के अन्य कारकों (सरिता, पवन, भूमिगत जल, सागरीय तरंग) आदि के समान ही
हिमानी भी भूपृष्ठ पर समतल स्थापना के कार्य में तत्पर रहती है। हिमानी भी
अन्य कारकों के समान चट्टानों का अपरदन करती है, अपरदित पदार्थों का परिवहन
करती है तथा उनका निक्षेपण करती है। हिमानी द्वारा उत्पन्न स्थलरूप अपरदन के
अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थलरुपों से अधिक भिन्न होते हैं। इस कारण
हिमानी के विभिन्न कार्यों तथा उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन आवश्यक
हो जाता है। हिमानी के विभिन्न कार्यों के विश्लेषण के पहले उसके सामान्य
रुपों का उल्लेख करना अति आवश्यक है। हिमानी धरातल पर सरिताओं के समान ही
हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं, यद्यपि इनकी गति बहुत मंद होती है।
हिमानी वास्तव में हिम समूह होते हैं, जो हिम क्षेत्र (Snow fields) से
गुरुत्व के कारण प्रवाहित होते हैं। हिमानी का निर्माण एक सामान्य प्रक्रिया
के अन्तर्गत सम्पन्न होता है। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिमरेखा (snow
line) कहते हैं। यह वह रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण रहता है तथा
बर्फ पिघल नहीं पाती है। हिमरेखा की ऊँचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर समान न
होकर अलग-अलग होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिमरेखा की
ऊंचाई कम होती जाती है। ध्रुवों के पास हिमरेखा प्रायः सागर तल के बराबर होती
है।
इस तरह यह स्पष्ट है कि हिमरेखा पर जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस
हिमरेखा के ऊपर स्थित भाग जो कि सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं 'हिमक्षेत्र
कहे जाते हैं। ऋतुवत् परिवर्तन के साथ हिम क्षेत्रों के विस्तार में भी
परिवर्तन होता रहता है। परन्तु भूपृष्ठ कुछ ऐसी भी भाग हैं, जहाँ पर सदैव
बर्फ जमी रहती है।
सामान्य रुप से हिमानी, अपरदन के अन्य कारकों के समान मार्ग में आनेवाली शैली
का अपरदन करती है, उससे प्राप्त पदार्थों का परिवहन करती है तथा मलवा का
यथास्थान निक्षेपण भी
करती है। परन्तु हिमानी के अपरदनात्मक कार्य के विषय में विद्वानों में दो
प्रकार के मत प्रचलित हैं। ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। प्रथम वर्ग के
विद्वानों के अनुसार हिमानी शैल को संरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि यह ऊपर
से शैल को ढके रहती है। अतः हिमानी का अपरदनात्मक कार्य नगण्य होता है। इस
विचारधारा को संरक्षण संकल्पना (protection concept) तथा समर्थकों को
संरक्षणवादी कहा गया। इसके विपरीत विद्वानों का एक वृहद समूह हिमानी के
अपरदनात्मक सामर्थ्य में विश्वास करता है। रेमजे तथा टिण्डल नामक विद्वानों
के अनुसार हिमानी अपरदन का एक सक्रिय कारक होता है तथा इसके अपरदन द्वारा
विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों का आविर्भाव तथा विकास होता है। हिमानी न केवल
अपने अपरदन द्वारा पूर्वनिर्मित स्थरुप में परिवर्तन लाता है वरन् नवीन
स्थरुपों का सृजन करती है। हिमानी अपरदन का प्रभावशाली कारक होते हुए भी
शैलों का कुछ सीमा तक रक्षक भी है। हिमानी द्वारा परिवहन किये जाने वाले
पदार्थों में शिलाखण्ड, कंकड़-पत्थर, रेतकण, मिट्टी आदि सम्मिलित किये जाते
हैं। इन पदार्थों के सम्मिनित रुप से ग्लेसियल ड्रिफ्ट कहा जाता है। हिमोढ़
का प्रयोग हिमानी निक्षेप के लिए किया जाता है। इनका कुछ भाग हिमानी के
पार्श्व भागों से होकर स्थानान्तरित होता रहता है। हिमानी के पाश्र्यों के
सहारे हिमोढ़ प्रायः पंक्तिबद्ध रुप से चलता है। आगे बढ़ता हुआ हिमानी अपने
अग्रभाग (snout) द्वारा कुछ पदार्थों को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। हिमानी
द्वारा बारीक तथा मोटे कणों वाले पदार्थों का निक्षेप अलग-अलग न होकर मिश्रित
रूप में होता है। यही कारण है कि हिमानी द्वारा जमा किये गये पदार्थों में
स्तरीकरण (Stratification) नहीं होता है अर्थात स्तर (beds) या परतें
(Strata) नहीं मिलती हैं। हिमानी द्वारा जमा किये गये पदार्थों में
हिमाड्रिफ्ट (glacial drift) तथा उससे बने हिमोद (Moraines) अधिक महत्वपूर्ण
है। हिमानी द्वारा जमा किये गये अवर्गीकृत तलछट को सम्मिलित रूप से टिल कहते
हैं। टिल के कणों के आधार के अनुसार पदार्थों में श्रेणीकरण (assortment)
नहीं होता है। अतः छोटे बड़े सभी प्रकार के कण एक साथ मिश्रित रुप से
निक्षेपित होते हैं।
इस प्रकार उपरोक्त कार्यों के अनुसार हिमानी अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक
स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं।
|
|||||