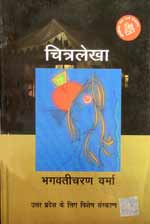|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
18
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
(Pre-Primary Education)
प्रश्न- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व
(Meaning and Importance of Pre-Primary Education)
पूर्व-प्राथमिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है - पूर्व तथा प्राथमिक। अतः पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education) का शाब्दिक अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा से पूर्व अर्थात् पहले की शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में बालक प्राथमिक स्कूल की शिक्षा में प्रवेश से पूर्व जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व- प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वास्तव में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा माता के गर्भधारण के साथ प्रारम्भ हो जाती है तथा बालक की आयु 5 या 6 वर्ष होने तक चलती है। इसे दो भागों, जन्मपूर्व शिक्षा तथा जन्मोत्तर शिक्षा में बाँटा जा सकता है। जन्मपूर्व शिक्षा के अन्तर्गत माता के गर्भ में भोजन, मनोस्थिति आदि पर ध्यान दिया जाता है जिससे गर्भ में स्थित बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से हो सके। जन्मोत्तर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत घर, परिवार व पड़ोस तथा पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में अर्जित ज्ञान आता है।
प्राचीन काल में परिवार ही बालक की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का केन्द्र हुआ करते थे। माता-पिता परिवार के अन्य सदस्य तथा इष्टमित्र, सम्बन्धी व पड़ोसी आदि व्यक्ति ही बालक के अध्यापक माने जाते थे। ये सभी अच्छे कार्यों को प्रेरणा देकर बालक को सदाचार का पाठ पढ़ाते थे, उसके भाषा- कौशल तथा गणित ज्ञान को बढ़ाते थे। उस समय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कोई औपचारिक शिक्षा न होकर सामाजिक आदान-प्रदान तथा अभिव्यक्ति को विकसित करने की प्रक्रिया मानी जाती थी। परन्तु बाद में घरेलू व्यावसायिक क्रियाकलापों में व्यस्तता के कारण माता-पिता के लिये यह असम्भव सा प्रतीत होने लगा कि वे अपने बच्चों को स्वयं ही पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दे सकें। इस स्थिति में शिशुओं की देखभाल तथा उनके व्यवहार शोधन के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान युग में इस आवश्यकता में वृद्धि उस समय महसूस की गई जब माताओं ने भी व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश किया तथा अशिक्षित अभिभावकों में भी अपने बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। इन सभी परिस्थितियों ने यह आवश्यक कर दिया कि सर्वाधिक पूर्व- प्राथमिक स्कूल खोले जायें तथा इस प्रकार से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए औपचारिक संस्थाओं का प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में सामान्यतः 2-3 वर्ष से लेकर 5-6 वर्ष तक के शिशुओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को इस आधार पर भी दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम, घर पर दी जाने वाली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा जो माता द्वारा गर्भधारण से लेकर बालक के 2-3 वर्ष तक के होने तक चलती है। द्वितीय, पूर्व-प्राथमिक स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा जो प्रायः बालक के 2-3 वर्ष के होने से 5-6 वर्ष के होने तक चलती है।
फ्रोबेल को आधुनिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सन् 1837 में जर्मनी के ब्लेकन्बर्ग नामक शहर में सबसे पहले पूर्व-प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी। मारग्रेट मैकमिलन तथा रचेल मैकमिलन नाम की दो बहनों तथा मारिया मॉन्टेसरी व आर्नोल्ड गसेल ने भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक युग में भारत में औपचारिक रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भ करने का श्रेय भी ईसाई मिशनरियों को दिया जाता है।
कोठारी आयोग ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य में एक-एक विकास केन्द्र खोलने तथा जिला स्तर पर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने का सुझाव दिया। आयोग ने व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति के द्वारा चलायी जा रही पूर्व-प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने, पूर्व- प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक साहित्य को तैयार करने तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने का सुझाव दिया। कोठारी आयोग ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने तथा पाठ्यक्रम को लचीला बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कोठारी आयोग की इन संस्तुतियों के बावजूद भी सन् 1968 में घोषित प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिया गया जिनके कारण कोठारी आयोग की संस्तुतियों के बावजूद भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की स्थिति दयनीय बनी रहीं। 1979 मंर जनता सरकार द्वारा तैयार किये गये शिक्षा नीति मसौदे में भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपेक्षणीय ही बनी रही। सन 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व-प्राथमिक को कम से कम सिद्धान्त रूप में अपना उचित स्थान मिला। इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खण्ड 5 के अनुच्छेद 1, 2, 3 व 4 में पूर्व बाल्यकाल परिचय तथा शिक्षा को विशेष महत्व देने तथा बालकों के पोषण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास के लिये पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा को यथासम्भव एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा के कार्यकम बाल केन्द्रित होंगे तथा इनमें खेलकूद व बालक की व्यक्तिगतता को ध्यान में रखा जायेगा। शिक्षण की औपचारिक विधियों तथा लिखने, पढने व गणित के ज्ञान को औपचारिक ढंग से सिखाने को इस स्तर पर हतोत्साहित करने की बात भी नवीन राष्ट्रीय नीति में कही गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा को अत्यन्त महत्व दिये जाने के कारण कार्यान्वयन कार्यक्रम में इस प्रकारण पर जोर दिया गया है। इसे मौन संसाधन विकास की व्यू रचना के प्रमुख अदा, प्राथमिक शिक्षा के पोषक व सहायक कार्यक्रम तथा समाज के सुविधाहीन वर्गों की कार्यरत महिलाओं के लिए सहायक सेवा के रूप में देखा जा सकता है। पूर्व बाल्यकाल, परिचर्या तथा शिक्षा में बालक का सम्पूर्ण विकास शारीरिक, गामक, बौद्धिक, भाषायी, संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक-समाहित रहता है। इसकी आयु अवधि गर्भाधान से लेकर लगभग छः वर्ष तक रहती है। इस अवधि की विकास प्रक्रिया में गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि में माता का आहार, सही स्तनपान, टीकाकरण, बाल परिचर्या से सम्बन्धित माता की शिक्षा आदि बातें सम्मिलित रहती हैं जिसके लिए एकीकृत तथा समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्यान्वयन कार्यक्रम में निम्न बातें कही गई हैं
1. एकीकृत बाल विकास सेवा के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
2. पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य व पोषण पक्षों को जोड़ा जायेगा, कर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा बच्चों को शैक्षिक सामग्री दी जायेगी।
3. स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे बाल विकास के सभी कार्यक्रमों में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।
4. राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं के द्वारा संचालित किए जाने वाले पूर्व प्राथमिक स्कूलों में स्वास्थ्य व पोषण के पक्षों को जोड़ा जायेगा तथा लिखना पढ़ना व गणित सिखाने की प्रक्रिया को बहुत जल्दी शुरू करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जायेगा।
5. क्रैश तथा दिवस परिचर्या केन्द्र योजना की समीक्षा करने तथा इसके सुदृढ़ीकरण की तत्काल आवश्यकता है।
6. सातवीं तथा आठवीं योजना में कम लागत के निर्देश विकसित करने के लिए किये जाने वाले प्रयोगों पर जोर दिया जायेगा।
7. पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा कार्यक्रम के सभी प्रारूपों में प्रशिक्षण पक्ष को सुदृढ़ किया जायेगा।
8. मॉनिटरिंग तथा मूल्याँकन प्रणाली को प्रबन्ध सूचना प्रणाली एवं वृत्तिक संस्थाओं के सहयोग से सुदृढ़ किया जायेगा।
इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अत्यन्त धीमी व असन्तोषजनक ही रही है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कुछ सीमा तक लोकप्रिय हुई है तथा अभिभावकों ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के प्रति अपनी माँग सम्मुख रखी है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूर्व- प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित है।
|
|||||