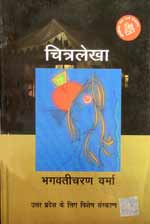|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किये गये विशेष प्रयत्न इस दिशा में कितने कारगर हैं? विश्लेषण कीजिए।
उत्तर-
मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किये गये विशेष प्रयत्न 1993
मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन पिछले लगभग एक दशक से भारत में कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'एमनेस्टी इण्टरनेशनल' तथा अन्य कुछ मानवीय अधिकार समर्थकों द्वारा यह कहा जा रहा था कि भारतीय संविधान में 'मूल अधिकारों का प्रावधान' होने के बावजूद व्यवहार में राजसत्ता से जुड़ी विविध एजेन्सियों (राज्य के पुलिस बल, अर्द्ध सैनिक बल, सेना और जेल-व्यवस्था आदि) द्वारा अनेक बार मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। अतः यह अनुभव किया गया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रसंग में पहले तो सितम्बर 93 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया तथा उसके बाद दिसम्बर 93 में मानवाधिकार आयोग व न्यायालय गठन सम्बन्धी विधेयक पारित किया गया।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)
यह एक 8 सदस्यीय आयोग होगा। आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। आयोग के अन्य सदस्य होंगे, सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हों, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का अध्यक्ष तथा महिला आयोग का अध्यक्ष। महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि आयोग को स्वशासी तथा वैधानिक स्तर प्राप्त हैं तथा इसे वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आयोग का मुख्यालय भारत की राजधानी में होगा तथा केन्द्र सरकार की अनुमति से अन्य स्थानों पर आयोग के कार्यालय स्थापित किये जा सकते हैं।
आयोग का कार्यक्षेत्र और कार्यविधि - आयोग को मानवीय अधिकारों (भारतीय संविधान से स्वीकृत अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं से मान्यता प्राप्त व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा आदि अधिकारों) के हनन, और मानवीय अधिकारों के हनन की रोकथाम में सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की सभी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा। आयोग अपनी प्रकृति के सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने पर तो आयोग अपने तरीके से जनमत को जाग्रत करने की चेष्टा कर सकता है। आयोग को सशस्त्र बलों या अन्य सैनिक बलों के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह केवल राज्य के पुलिस बलों के कार्यों की ही जाँच कर सकता है। आयोग आतंकवाद सहित, मानवीय अधिकारों के उपभोग में बाधक तत्वों पर विचार करेगा। आयोग को जेलों के निरीक्षण का अधिकार भी होगा। आयोग को राज्य या राजसत्ता की किसी एजेन्सी के कार्यों से मानवीय अधिकारों का हनन होने पर ही जाँच करने और मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है, व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों या निजी क्षेत्र के प्रसंग में उसे काम करने का अधिकार नहीं है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग को मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की स्वतन्त्र रूप से जाँच करने का अधिकार प्राप्त है। जाँच के लिए आयोग के अपने कर्मचारीगण होंगे तथा आयोग को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की जाँच एजेन्सियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। आयोग अपने जाँच कार्य में 'एमनेस्टी इण्टरनेशनल' अथवा अन्य किसी विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी को अथवा गैर सरकारी विशेषज्ञों को संयुक्त कर सकता है। आयोग को यह भी मताधिकार प्राप्त है कि वह मानवीय अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से विद्यमान कानूनों में संशोधन के लिए शासन को सुझाव दे सके।
आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा तथा सरकार आयोग को सूचित करेगी कि उसकी सिफारिशों परं क्या कार्यवाही की गई है। इसके बाद आयोग पीड़ित पक्ष को अपनी जाँच और इस प्रसंग में स्वयं द्वारा या शासन द्वारा उठाए गये कदमों की सूचना देगा। अत्यन्त जरूरी मामलों में आयोग अन्तरिम रिपोर्ट भी दे सकेगा।
राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना राज्य सरकार पर निर्भर करेगी और वे अपने मानव अधिकार आयोग की स्थापना से सम्बन्धित व्यवस्था में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकेगी।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगों, ने 1994 के प्रारम्भिक दिनों से ही अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 'टाडा' कानून की समाप्ति और बालश्रम का निषेध करने की बात पर बल देने में इस आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तथा अपने कार्यकाल के प्रथम आठ वर्षों में आयोग ने मानवीय अधिकारों की रक्षक संस्था के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। भविष्य में सरकार की किसी एजेन्सी के कारण जब नागरिकों के मौलिक अधिकार या अन्य अधिकार का हनन होगा तब नागरिक के सामने विकल्प होगा कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जाये अथवा मानव अधिकार आयोग और उससे जुड़े न्यायालयों में जायें।
|
|||||