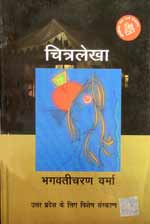|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का मूल्यांकन कीजिए।
अथवा
भारतीय संविधान द्वारा दिये गये स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए।
अथवा
संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार
भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12-35 में नागरिकों को छह प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। यद्यपि मूल संविधान में कुल अधिकारों की संख्या 7 थी, किन्तु 44 वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकारों से निकालकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार निम्न प्रकार है -
1. समता का अधिकार ( अनुच्छेद 14-18) - इस अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित पाच प्रकार के अधिकार शामिल किये गये हैं-
(I) भारतीय राज्य क्षेत्र में 'विधि के समक्ष समता' तथा 'विधियों का समान संरक्षण' (अनुच्छेद 14)- इसका तात्पर्य यह है कि देश की विधियों के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे किसी व्यक्ति की पद अथवा प्रतिष्ठा कुछ भी हो तथा सभी व्यक्तियों को विधि का समान रूप से संरक्षण प्राप्त रहेगा, चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर। इस अनुच्छेद का उद्देश्य 'स्तर एवं अवसर' की समानता स्थापित करना है।
(II) धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में समानता (अनुच्छेद 15) इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के आधार पर उपरोक्त किसी आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।
(III) लोक सेवाओं में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) - इस अनुच्छेद के आधार पर राज्य की लोक सेवाओं में सभी नागरिकों के समान अवसर उपलब्ध होंगे। यद्यपि समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु उन्हें आरक्षण के रूप में कुछ सुविधायें दी जा सकती हैं।
(IV) अस्पृश्यता का अन्त - (अनुच्छेद 17) - इस अनुच्छेद के आधार पर छुआ-छूत संबंधी किसी भी व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। समाज से अस्पृश्यता का अंत करने के लिए संसद द्वारा 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' 1955' पारित किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976' कहा गया। इस अध्याय का यही एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें गांधी जी के विचारों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
(V) उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सेना एवं विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि प्रदान नही करेगा तथा राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22 ) - नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार है। एम. पी पावली के अनुसार, यह अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है और मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय का मूल आधार है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्न छः स्वतंत्रतायें प्रदान की गयी हैं
(i) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(ii) सभा करने की स्वतंत्रता।
(iii) संघ बनाने की स्वतंत्रता।
(iv) अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता।
(v) आवास की स्वतंत्रता।
(vi) पेशा, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) - इस अनुच्छेद 23 के तहत मानव के व्यापार तथा उससे बेगार लेना अपराध घोषित किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम के आयु किसी भी बालक को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे उद्योगों में लगाना अपराध घोषित किया गया है।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना का परिचायक है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत के सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के अनुसार, लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी धार्मिक समुदायों को धार्मिक प्रयोजनों से संस्थाओं की स्थापना और पोषण, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबन्ध करने तथा कानूनी तौर पर अर्थोपाजन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के हितार्थ कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य की संचित निधि से संचालित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ( अनुच्छेद 29-30) - इन अनुच्छेदों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर देश की विविधता में एकता स्थापित करना है। अनुच्छेद 29 उपबंधित करता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत धर्म व भाषा आधारित अल्पसंख्यक कार्यों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्ध का पूर्ण अधिकार होगा।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) - डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 'संविधान की आत्मा' कहा था। वास्तव में अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जा सके और यदि उनका हनन हो तो उपचार किया जा सके। संविधान के अंतर्गत यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत पांच प्रकार के आदेश तथा प्रलेख जारी कर सकता है जो निम्न हैं-
(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - इस लेख द्वारा न्यायालय बंदी बनाये गये व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है तथा उसे बंदी बनाये जाने के कारणों की जांच करता है। यदि बंदी बनाये जाने के वैध कारण नहीं हैं तो उसे मुक्त करने का आदेश देता है। यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
(ii) परमादेश (Mandamus) - इसका आशय है- 'हम आदेश देते हैं इस लेख द्वारा न्यायालय किसी पदाधिकारी अथवा किसी सार्वजनिक संस्था को उसके कर्त्तव्य का पालन कराने के लिए आदेश देता है।
(iii) उत्प्रेषण (Certiorai) - यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों को इस आशय से दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले की कार्यविधियों अभिलेख उच्च न्यायालय के पास विचारार्थ भेजे।
(iv) प्रतिषेध (Prohibition) - प्रतिषेध द्वारा निम्न न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहकर कृत्यों के निर्वहन के लिए बाध्य किया जाता है। यह लेख केवल न्याययिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही निकाला जाता है।
(v) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto ) यह प्रलेख किसी व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान जहाँ नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है।
मूल्यांकन - इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय प्रजातंत्र के उदार स्वरूप को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' 1948 का भी समर्थन करता है।
हालांकि मौलिक अधिकारों की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है, किन्तु फिर भी इन्हें महत्वहीन नहीं माना जा सकता। वास्तव में मौलिक अधिकारों के साथ अनेक सीमायें लगाने का मुख्य उद्देश्य 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' एवं 'राज्य की सुरक्षा' के मध्य समन्वय स्थापित करना था। मौलिक अधिकारो के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है।
|
|||||