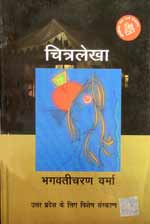|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- स्वतन्त्रता, न्याय, समता एवं बन्धुत्व की संवैधानिक वचनबद्धता के संदर्भ में शिक्षा की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
स्वतन्त्रता, न्याय, समता एवं बन्धुत्व की संवैधानिक वचनबद्धता के संदर्भ में शिक्षा -
प्राचीन काल से ही शिक्षा समाज का प्रमुख आधार रही है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही कोई भी देश अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप ही विकास कर सकता है।
स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में लोकतान्त्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप देश में लोकतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य पर ध्यान रखा गया, जिसके लिए स्वतन्त्रता न्याय, समता एवं बंधुत्व की संवैधानिक वचनबद्धता है। अतः देश की शिक्षा का उद्देश्य वर्गविहीन, जातिविहीन, धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी समाज की रचना करना है ताकि देश को कुशल, देशभक्त एवं निष्ठावान नागरिक मिलें, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत परिवर्तन एवं संशोधन की दृष्टि से विभिन्न आयोगों का गठन किया गया -
(A) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (University Education Commission 1948- 49) - स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में गठित प्रथम शिक्षा आयोग के रूप में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विशेष महत्व है। इसके सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है - "ज्ञान के प्रसार, नवीन ज्ञान के लिए सतत् खोज, जीवन के अर्थ को साधने के सतत् प्रयास, अपने समाज की व्यावसायिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं।' अतः आयोग ने उपयुक्त कार्यो को क्रियान्वित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख किया-
(1) इस शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय और वाणिज्य आदि में नेतृत्व प्रदान कर सकें।
(2) विश्वविद्यालय को छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए।
(3) विश्वविद्यालय शिक्षा का एक मुख्य कार्य छात्रों का चारित्रिक उत्थान होना चाहिए।
(4) विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा छात्रों में विश्व बन्धुत्व भावना का विकास करना चाहिए।
(5) संविधान में समानता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व के आदर्श का संरक्षण करना विश्वविद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए।
(B) माध्यमिक शिक्षा आयोग - इनके अनुसार, "शिक्षा व्यवस्था को आदतों, अभिवृत्तियों एवं चारित्रिक गुणों के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिससे यहाँ के नागरिक लोकतान्त्रिक नागरिकता के उत्तरदायित्वों को योग्यतापूर्वक वहन करने के सुयोग्य हो सकें और उन सभी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करे।
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तावित किए हैं -
(1) व्यक्तित्व का विकास - यह माध्यमिक शिक्षा का अन्य उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा को अपने छात्रों में रचनात्मक शक्ति के स्रोतों का विकास करना चाहिए जिससे कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का आनन्द लेने के लिए सुयोग्य बनेंगे।
(2) व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना माध्यमिक शिक्षकों को अपने छात्रों की उत्पादक, प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए जिससे वे राष्ट्र की समृद्धि में सहायता कर सकें।
(3) लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास करना - भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को अंगीकृत किया गया है। अतः माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों में बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए जिससे कि वे लोकतान्त्रिक नागरिकता के उत्तरदायित्वों को समझ सकें।
(4) नेतृत्व के लिए शिक्षा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना माध्यमिक शिक्षा का एक मुख्य कार्य होना चाहिए जो सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व के उत्तरदायित्व को वहन करने में समर्थ हों।
(C) शिक्षा आयोग - शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार यह है कि इसे परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में इसके सम्बन्ध को स्थापित किया जाए और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त साधन बनाया जाए, इस प्रकार शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया -
(i) शिक्षा के द्वारा समाज का आधुनिकीकरण।
(ii) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना।
(iii) शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाना।
(iv) सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का बिकास करना।
|
|||||