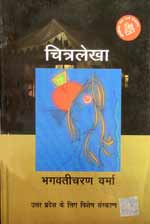|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- शिक्षा के उद्देश्यों से सम्बन्धित संवैधानिक मूल्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
शिक्षा के उद्देश्यों से सम्बन्धित संवैधानिक मूल्य
भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 ई. को स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। जिसके माध्यम से देश में एक सम्प्रभुतासम्पन्न समाजवादी, धर्मनिपरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ताकि देश में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष समाज की रचना की जा सके। तद्नुसार नवनिर्मित समाज के कल्याण हेतु शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके और शिक्षा की सम्यक् व्यवस्था के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
शिक्षा के उद्देश्यों को भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों जैसे कि स्वतन्त्रता, न्याय, समता एवं बंधुत्व पर आधारित करके सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है -
(1) स्वतन्त्रता (Freedom) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतन्त्रता (Liberty) जिसका अर्थ Freedom है, संवैधानिक मूल्य है जो भारत के नागरिकों को स्वतन्त्रता के अधिकार से रूबरू कराता है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतन्त्रता के अन्तर्गत विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना को रखा गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, संघ या समुदाय का गठन, देश के किसी भी भाग में निवास, कोई भी पेशा या धन्धा अपनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना विधि के अनुसार किसी को भी अपराधी सिद्ध करके दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत किसी को भी उसके जीवन और स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25-28 तक व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता का आश्वासन संविधान प्रदान करता है।
(2) न्याय (Justice) - न्याय के आदर्श को संविधान की प्रस्तावना में प्राथमिकता प्रदान की गई है। सविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की स्थापना करना है। संविधान में सामाजिक न्याय से जुड़ी कई सारी अनेक व्यवस्थायें की गईं। संविधान निर्माताओं के विचार के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना तभी तक सम्भव है जब तक समाज में सभी प्रकार की असमानताओं को हटाया जा सके। संविधान के अनेकों अनुच्छेदों के द्वारा सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राज्य किसी के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, धर्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। वहीं अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत छुआछूत परम्परा को समाप्त करके एक लम्बे समय से चले आ रहे सामाजिक अभिशाप को खत्म करने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 18 भारतीय नागरिकों पर यह प्रतिबन्ध लगाता है कि शिक्षा और सेना से सम्बन्धित उपाधियों को छोड़कर वह दूसरी कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के अन्य उपबन्धो द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत संविधान सरकार को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों, स्त्रियों, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और उनके किसी भी प्रकार के शोषण को रोकें। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत मानव व्यापार तथा बेकारी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने और उस पर आचरण कराने का अधिकार प्रदान करता है। 42 वें संशोधन ने एक तरफ बालकों तथा युवकों के विकास की बात को कहा तो वहीं पर दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की। 44 संशोधन में यह स्पष्ट हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न आय वर्ग तथा विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों के बीच भेदभाव को कम करने की दिशा में कदम उठाया जायेगा।
(3) समानता (Equality) - समानता संविधान की प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण आदर्श है। प्रस्तावना के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय राज्य का ध्येय व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना है। मूल अधिकारों की सूची में समानता का अधिकार प्रथम स्थान में रखा गया है। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को कानून के सम्मुख समानता और समान कानूनी संरक्षण देने की बात कही गयी। अनुच्छेद 15 राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, वहीं पर अनुच्छेद 16 सभी भारतीयों को सरकार के अन्तर्गत नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 ने शिक्षा और सेना छोड़कर अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया है।
(4) बंधुत्व (Fraternity) - इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विशेष महत्व दिया गया क्योंकि इससे व्यक्ति की गरिमा एव राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सन्निहित है। व्यक्ति की गरिमा इसी पर निर्भर है। इसके लिए संविधान के लिए संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रावधान दिए गए हैं -
अनुच्छेद 38 (2) राज्य विशिष्ट या आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा तथा न ही केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच की प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।
राष्ट्र की एकता व अखण्डता को मद्देनजर रखते हुए संविधान (42 वें संशोधन) अधिनियम 1976 भाग 4 (A) अनुच्छेद 51 A द्वारा भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करे।
अतः उपरोक्त दिए गए विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों से सम्बन्धित जो संवैधानिक मूल्य हैं उनसे शिक्षा के उद्देश्यों में स्वतन्त्रता, न्याय, समता एवं बन्धुत्व की संवैधानिक वचनबद्धता स्पष्ट झलकती है। इसलिए देश के सभी लोग शिक्षा के द्वारा अपने एवं देश के निर्माण में संलग्न है व जिसके परिणामस्वरूप देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
|
|||||