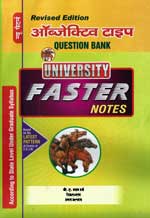|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
23
राष्ट्रीय स्तर (एन.सी.ई.आर.टी, एन.ए.ए.सी. (नैक), एन.यू.पी.ए., एन.आई.ओ.एस., ए.आई.सी.टी.ई.)
[National Level (NCERT, NAAC, NUPA, NIOS, AICTE)]
प्रश्न- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संगठन का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
अथवा
एन. सी. आर. टी. एवं डायट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एक सितम्बर उन्नीस सौ इकसठ को भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। प्रारम्भ में माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो, बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान, श्रव्य दृश्य राष्ट्रीय संस्थान जैसी अनेक संस्थाओं को मिलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। यह एक स्वायत्त तथा पूर्णरूप से केन्द्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार को सहयोग व परामर्श देना है जिससे शिक्षा सम्बन्धी नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण व क्रियान्वयन समुचित ढंग से हो सके। इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निम्न कार्यक्रम व गतिविधयों का संचालन करती है -
(i) शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कार्य में सहायता करना व अनुसंधान कार्य का समन्वय करना।
(ii) सेवारत व सेवा पूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण के उच्च स्तरीय कार्यक्रम चलाना
(iii) शैक्षिक पुननिर्माण के कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन करना। (iv) शिक्षण की उन्नत तकनीकों व नवाचारों को बढ़ावा देना।
(v) शैक्षिक सूचनाओं को संकलित व सम्पादित करना।
(vi) माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करने के कार्यक्रमों को लागू करने में शिक्षा संस्थाओं की सहायता करना।
(vii) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनेस्को व यूनिसेफ तथा अन्य राष्ट्रों की शिक्षा संस्थाओं से सम्पर्क रखना।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वास्तविक नियन्त्रण मुख्य रूप से इसके सामान्य निकाय व कार्यकारिणी समिति के अधीन रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परषिद का सामान्य निकाय वास्तव में इसका नीति निर्धारक निकाय है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री इस सामान्य निकाय के अध्यक्ष (President) होते हैं। सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री यू.जी.सी. के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के चार कुलपति, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संगठन आयुक्त, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत चार अध्यापक तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। यह निकाय नीति सम्बन्धी उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए सक्षम है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संचालन व शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के लिये एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष भी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं तथा इसके सदस्य केन्द्रीय राज्य शिक्षामंत्री, केन्द्रीय शिक्षा सचिव, यू.जी.सी के अध्यक्ष, एन.सी.आई.आर.टी. के निदेशक व संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय, संसाधन विकास मन्त्रालय व केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के एक-एक प्रतिनिधि, दो अध्यापक, परिषद के संकायों के तीन प्रतिनिधि तथा दो प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। परिषद के कार्यों से सम्बन्धित सभी मामलों पर कार्यकारिणी समिति निर्णय लेती है। एन. सी. ई. आर. टी. के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के नियम व संचालन का उत्तरदायित्व निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा सचिव विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की सहायता से सम्पादित करते हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अपने आठ संघटकों के माध्यम से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। इन आठ संघटकों के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने क्षेत्रीय सलाहकारों की भी नियुक्ति की थी। इन क्षेत्रीय सलाहकारों को राज्यों के साथ सम्पर्क करने का कार्य सौंपा गया था। प्रत्येक क्षेत्रीय सलाहकार का कार्य क्षेत्र निश्चित था। बड़े राज्यों में एक-एक क्षेत्रीय सलाहकार को रखा गया था। जबकि कई छोटे राज्यों का कार्यक्षेत्र एक क्षेत्रीय सलाहकार को दिया गया था। कार्यक्षेत्र के निर्धारण में भौगोलिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया था। क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालय को प्रायः राज्य की राजधानी में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के शैक्षिक केन्द्र होने के कारण क्षेत्रीय सलाहकार का कार्यालय इलाहाबाद शहर में खोला गया था। क्षेत्रीय सलाहकार अपने सम्बन्धित राज्यों। राज्यों के शिक्षा अधिकारियों के सम्पर्क में रहते थें तथा उन्हें परिषद के क्रिया-कलापों से अवगत कराकर राज्य के शैक्षिक विकास में परिषद के योगदान का लाभ उठाने की परिस्थितियों का निर्माण करते थे। इसके साथ-साथ राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचना परिषद को देते थे जिसमें तदनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास किया जा सके। इस प्रकार से क्षेत्रीय सलाहकार राज्यों के शैक्षिक विकास के मार्ग को प्रशस्त बनाने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्र सरकार के योगदान को सुगम बनाने का कार्य करते थे। परन्तु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कुछ समय पूर्व कतिपय कारणों से अपने क्षेत्रीय सलाहकार के कार्यालयों को बन्द कर दिया है। ऐसे संकेत हैं कि पुनः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इन्हें खोलने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आठ संघटक निम्नवत् हैं
(1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
(2) केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली
(3) पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
(4) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(5) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
(6) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
(7) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर
(8) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का मुख्य कार्य शिक्षा के शोध करना तथा अध्यापकों, शिक्षक-अध्यापकों तथा अन्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन करना है। यह अनुसंधान परिणामों, प्रसार क्रियाकलापों, सरकारी नीतियों तथा शैक्षिक विकास से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाओं के संकलन व प्रसार का कार्य भी करता है। ये सभी शैक्षिक, प्रशासनिक व अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाकलाप शिक्षा के क्षेत्र से कार्यरत या कार्य करने के इच्छुक प्रतिभागियों के वृत्तिक विकास में तथा पाठय-विषयक व अन्य शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास की दृष्टि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभाग प्रभाग एकक तथा प्रकोष्ठ - राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों, एककों तथा प्रकोष्ठों का गठन समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान अग्रांकित विभागों, प्रभागों, एककों तथा प्रकोष्ठों के माध्यम से अपने कार्य का निर्वाह कर रहा है।
विभाग -
(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (DEE)
(2) अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार विभाग (DTEE)
(3) भाषा विभाग (DOL)
(4) विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग (DESM)
(5) शैक्षिक, सर्वेक्षण एवं प्रदत्त प्रक्रियन विभाग (DES & DP)
(6) शैक्षिक अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग (DERPP)
(7) सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग (DESSH)
(8) कला एवं सौन्दर्यशास्त्र एवं शिक्षा के आधार विभाग (DEAA)
(9) शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा के आधार विभाग (DEPEE)
(10) विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा विभाग (DEGSN)
(11) कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहायता विभाग (DCETA)
(12) प्रकाशन विभाग (PD)
(13) महिला अध्ययन विभाग (DWS)
(14) शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन विभाग (DEME)
प्रभाग -
(1) योजना, कार्यक्रम, अनुवीक्षण मूल्यांकन प्रभाग (PPMED)
(2) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध प्रभाग (IRD)
(3) पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना प्रभाग (DLDI)
प्रकोष्ठ तथा एकक
(1) हिन्दी प्रकोष्ठ
(2) पठन प्रकोष्ठ
(3) गणित प्रकोष्ठ
(4) आन्तरिक कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ
(5) जनसम्पर्क एकक
(6) पाठ्यक्रम समूह
अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर व शिलांग में स्थित क्षेत्रीय संस्थान देश के विभिन्न भागों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शिक्षा केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त हैं तथा अध्यापक प्रशिक्षण के उन्नयन के कार्य में जुटे हुए हैं। ये क्षेत्रीय संस्थान एक वर्षीय बी. एड. पाठ्यक्रमों के अलावा चार वर्षीय समाकलित अध्यापक शिक्षा पाठयक्रम (B.A., B.Ed. व B.Sc., B.Ed.) तथा दो वर्षीय विज्ञान शिक्षा निष्णात (M.Sc. M.Ed.) पाठयक्रम भी चलाते हैं। संस्थान राज्यों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद जैसी संस्थाओं के द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिये विशेषज्ञता प्रदान करते हैं तथा विद्यालय शिक्षा व अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार व विकासात्मक कार्यकलापों में लगे हुये रहते हैं। ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान पहले क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के नाम से जाने जाते थे। अप्रैल 1995 में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में स्थित इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों का नाम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कर दिया गया एवं इनके उत्तरदायित्वों में कतिपय परिवर्तन करके अनुसंधान, विकास, प्रसार, तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया गया।
स्पष्ट है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की है। इसके लिये यह अनुसंधान व नवाचार को सहयोग देती है, बढ़ाती है तथा समन्वित करती है। पाठ्यक्रमों में सुधार तथा पाठ्य-पुस्तकों की रचना का कार्य भी यह करती है। यह परिषद् अध्यापक निर्देशिका, छात्र कार्य पुस्तिकायें, प्रयोगशाला सामग्री, शिक्षण सामग्री, शैक्षिक चलचित्र भी तैयार करती हैं। शैक्षिक सूचनाओं का संकलन प्रसार व फैलाव परिषद का एक प्रमुख कार्य है। यह परिषद शैक्षिक क्षेत्र में शोध व अन्य चिन्तन सम्बन्धी लेखों पर आधारित पाँच पत्रिकायें इंडियन
एजूकेशनल रिव्यू, जनरल ऑफ इंडियन एजूकेशन, स्कूल साइन्स द प्राइमरी टीचर (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में) तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रकाशन करती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की पहचान व पोषण के लिये परीक्षा का संचालन करती है तथा छात्रवृत्ति प्रदान करती है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना तथा इसकी प्रवेश परीक्षा के आयोजन में प्रारम्भिक सहयोग प्रदान करना भी एन.सी.ई.आर.टी. का एक विशिष्ट योगदान है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, जनसंख्या शिक्षा जागरूकता, कम्प्यूटर शिक्षा तथा मूल्य शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सक्रिय ढंग से सहयोग प्रदान करती है।
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।