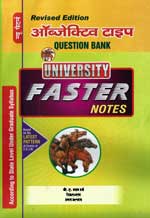|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
प्रश्न- सांस्कृतिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के अभिकरण बताइए।
उत्तर-
सांस्कृतिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के अभिकरण
(Agencies of Cultural Education andDevelopment of Cultural Values)
सामान्यतः सांस्कृतिक शिक्षा से तात्पर्य किसी समाज द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति अर्थात् रहन-सहन एवं खान-पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, रीति-रिवाज, कला-कौशल एवं संगीत-नृत्य में प्रशिक्षित करने और उन्हें अपने भाषा-साहित्य तथा धर्म-दर्शन का ज्ञान कराने और तदनुकूल आचरण करने की ओर प्रवृत्त करने से लिया जाता है परन्तु यह कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक आने वाली पीढी को इनके पीछे आदर्श, विश्वास और सिद्धान्तों से परिचित नहीं कराया जाता है और उनमें यथा मूल्यों का विकास नहीं किया जाता। लोकतंत्रीय भारत में तो अपने समाज की संस्कृति को ग्रहण करने के साथ-साथ दूसरे समाजों की संस्कृतियों के सामान्य तत्वों की जानकारी और उनके प्रति आदर भाव के विकास को भी आवश्यक समझा जाता है और यह कार्य तभी सम्भव है जब शिक्षा के अनौपचारिक और औपचारिक अभिकरण इसके लिए प्रयत्नशील हों।
परिवार और सांस्कृतिक शिक्षा
जहाँ तक स्वसंस्कृति की बात है इसका शुभारम्भ परिवार में ही हो जाता है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर रहन-सहन एवं खान-पान की विधियाँ एवं व्यवहार प्रतिमान सीखते हैं। परिवार में ही वे अपने रीति-रिवाजों को देखते-समझते और सीखते हैं। कला-कौशल और संगीत-नृत्य की शिक्षा का शुभारम्भ भी परिवारों में हो जाता है और धीरे-धीरे उनमें सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होने लगता है। बच्चों के प्रारम्भिक जीवन में पड़े ये संस्कार बड़े स्थायी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का तो यह मानना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का तीन चौथाई निर्माण इसी काल में हो जाता है।
और जहाँ तक दूसरी संस्कृतियों के ज्ञान और परसंस्कृति ग्रहण की बात है उसके लिए परिवारों में कोई अवसर नहीं मिलता। हाँ. दूसरी संस्कृतियों के ज्ञान और परसंस्कृति ग्रहण के लिए परिवारों की संस्कृति आवश्यक होती है। जब तक परिवार के बड़े सदस्यों में सांस्कृतिक उदारता नहीं होगी, वे दूसरी संस्कृतियों का आदर नहीं करेंगे, तब तक बच्चे में सांस्कृतिक उदारता का विकास नहीं किया जा सकता, उन्हें परसंस्कृति ग्रहण के लिए तैयार नहीं किया जा सकता।
जाति और सांस्कृतिक शिक्षा - परिवार में रहते हुए बच्चे अपनी जाति की सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, बड़े होने पर भी यह क्रम जारी रहता है। परिणामतः जाति की सामाजिक- सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हुए अपनी संस्कृति सीखते हैं, उसमें प्रशिक्षित होते हैं। इसी के साथ-साथ उनमें सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, वे सुदृढ़ होते हैं पर जाति की सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हुए बच्चे स्वसंस्कृति ग्रहण ही करते हैं। न उन्हें दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान होता है और न वे परसंस्कृति ग्रहण करते हैं फिर जाति के बीच बच्चों में प्रायः सांस्कृतिक संकीर्णता का ही विकास होता है जबकि आज प्रत्येक जाति को सांस्कृतिक उदारता का परिचय देने की आवश्यकता है।
प्रायः सांस्कृतिक सकीर्णता का ही विकास होता है जबकि आज प्रत्येक जाति को सांस्कृतिक उदारता का परिचय देने की आवश्यकता है।
समुदाय और सांस्कृतिक शिक्षा - समुदाय एक बृहत् सामाजिक समूह होता है। भारत के संदर्भ में इसमें भिन्न-भिन्न परिवार और जातियों के बच्चे एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक-दूसरे के आचार- विचार को प्रभावित करते हैं। जब एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों की सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तो वे एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं और जाने-अनजाने एक-दूसरे की संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण भी करते हैं और कालान्तर से ये तत्व एक-दूसरे की संस्कृति के अभिन्न अंग बन जाते हैं और इसे ही समाजशास्त्रीय भाषा में परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार भारत के संदर्भ में समुदाय परसस्कृत ग्रहण के मुख्य अभिकरण होते हैं पर तभी जब समुदाय की भिन्न-भिन्न जाति एव संस्कृति के लोगों में सांस्कृतिक संकीर्णता न हो, वे एक-दूसरे की संस्कृति का आदर करते हों।
विद्यालय और सांस्कृतिक शिक्षा यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को अपने समाज (परिवार, जाति और समुदाय) की सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाओं का अनुकरण करके और उनमें भाग लेकर स्वयं सीखता, उसे एक सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त करता है, उसे सुरक्षित रखता है उसमें विकास करता है और उसे आने वाली पीढी में हस्तान्तरित करता है, परन्तु उसे इसके मूल तत्वों का स्पष्ट ज्ञान विद्यालयों में ही कराया जाता है।
फिर हमारे देश में तो अनेक संस्कृतियाँ हैं और लोकतंत्र इस बात की मांग करता है कि सबको अपनी-अपनी संस्कृति सीखने और उसे सुरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और सबको एक-दूसरे की संस्कृति रखने का आदर करना चाहिए। आज तो अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है और अन्तर्राष्ट्रीयता देश-विदेश की सभी संस्कृतियों के संरक्षण और विकास में विश्वास रखती है। वह संसार की समस्त संस्कृतियों के प्रति आदर भाव विकसित करने के पक्षधर है और यह तभी सम्भव है। हो सकता है जब हमें अपनी संस्कृति के साथ-साथ देश-विदेश की अन्य संस्कृतियों का भी ज्ञान हो। यह कार्य परिवारें में किया जा सकता है, न जाति में और न समुदायों में यह कार्य विद्यालयों में ही संपन्न किया जा सकता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि विद्यालय अपने इस उत्तरदायित्व को कैसे पूरा कर सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश में विद्यालयों में भिन्न-भिन्न जातियों, धर्मो और संस्कृतियों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इससे उनमें जाति, धर्म और संस्कृति के बंधन ढीले पड़ते हैं और वे एक-दूसरे की संस्कृति को सीखने की मानसिकता बनती है और जैसे-जैसे वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, वैसे-वैसे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता जाता है. वे एक-दूसरे की संस्कृति के विषय में जानकारी करने के इच्छुक होते जाते हैं।
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।