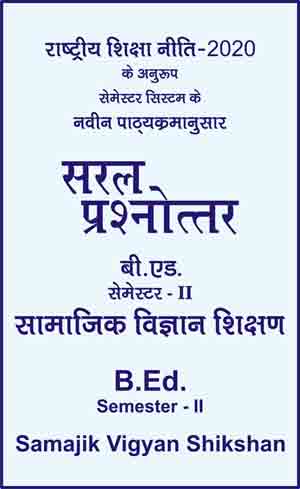|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 13 - उद्देश्य, प्रकार, विशेषताएँ, तकनीक एवं
मूल्यांकन के उपकरण एवं नैदानिक मूल्यांकन,
उपचारात्मक शिक्षण, सतत और व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई)
[Purpose, Types, Characteristics, Techniques and
Tools of Evaluation, Diagnostic Evaluation, Remedial
Teaching, Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE)]
प्रश्न- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन किसे कहते हैं ? इसकी प्रमुख प्रक्रिया और महत्त्व की विवेचना कीजिए।
अथवा
सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का क्या अर्थ है ? इसके महत्त्व तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
अथवा
मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके महत्त्व का विस्तृत वर्णन कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का क्या अर्थ है ? इसकी परिभाषाओं की विवेचना कीजिए।
- मूल्यांकन के उद्देश्यों एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
- सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के महत्त्व को व्याख्यायित कीजिए।
- मूल्यांकन का महत्त्व बताइए।
उत्तर -
मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Evaluation)
शिक्षण एवं परीक्षण के क्षेत्र में मूल्यांकन प्रणाली का अपना विशेष महत्त्व है। इन क्षेत्रों में नियतात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी सीमा तक हुई है, इसका ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा ही सम्भव हो पाता है। शिक्षण प्रणाली का नियतात्मक बिन्दु यह है कि निर्धारित उद्देश्यों सम्बन्धी व्यवहार किस हद तक प्राप्त हुआ है? इस दृष्टि से प्रत्येक शिक्षण कार्य प्रक्रिया में अर्थ, विकास, उद्देश्य, गतिविधि, परिणाम आदि में परिवर्तन को जानना आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत मूल्यांकन का विशेष महत्त्व है। इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है तथा कितना अभी शेष है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रभाव में शिक्षण का आयोजन नियोजन अन्त्ययन सम्भव है। यह एक व्यापक तथा सतत रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक है।
मूल्यांकन एक व्यापक व उद्देश्य केन्द्रित प्रक्रिया है। शिक्षक के लिए इसका सर्वप्रथम कार्य शिक्षण को उद्देश्य केन्द्रित बनाना है। व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की परख इस प्रक्रिया के आधार पर की जा सकती है। व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले इसे मूल्यवाचक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया के आधार को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने विचार निम्न प्रकार से दिए हैं -
डॉक्स के अनुसार - "मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया है।"
रेमर्स एवं गेज के शब्दों में - "मूल्यांकन के अन्तर्गत व्यक्ति या समाज, दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है, उसका ही प्रयत्न किया जाता है।"
किंबेल तथा मुनरो के अनुसार - "विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साधनों के संकलन तथा उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है।"
गाइबिन्स के अनुसार - "मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसके निर्देशन के अन्तर्गत कार्यों की जाँचने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा सम्पादित की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं।"
कोरी क्रोम्बैक के अनुसार - "अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, जोकि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न क्षेत्र है तथा इसके शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है।"
बेसेट के अनुसार - "मूल्यांकन एक सम्प्रेषणीय धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्त्व एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाणों तथा साधनों का प्रयोग करती है। यह बहुस्रोत प्रमाण तथा आत्ममूल्य निर्धारण कर शिक्षा है। यह एक आवश्यक एवं पूरक-प्रक्रिया है। वस्तुतः मूल्यांकन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अभाव में शिक्षण प्रणाली को सफलता प्रदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रक्रिया के आधार पर ही यह जाना जाता है कि किसी विशेष उद्देश्य के सन्दर्भ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी सीमा तक सफल रही है। इस जानकारी के आधार पर ही शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया को नियतात्मक उद्देश्यों की दिशा में गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। अतः इस दृष्टि से आयोग का यह कथन उचित है कि मूल्यांकन अनवरत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है।"
मूल्यांकन के उद्देश्य
(Aims of Evaluation)
मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रक्रिया विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इस आधार पर शिक्षा के कुछ प्रमुख पक्षों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है -
-
यह प्रक्रिया छात्रों को अध्ययन में परिश्रम करने तथा समुचित रीति से अधिगम करने की दिशा में प्रेरित करती है।
-
मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में निहित योग्यताओं के सम्बन्ध में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त होती है।
-
इस प्रक्रिया के आधार पर शिक्षार्थियों की भावी उपलब्धियों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की जा सकती है।
-
शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर प्रदत्त ज्ञान की सीमा भी इस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात की जा सकती है।
-
छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से निर्देशान प्रदान करने में भी यह प्रक्रिया सहायक है।
-
किस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसका विश्वसनीय ज्ञान भी मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा ही सम्भव है।
-
यह प्रक्रिया अधिगम की दिशा में छात्रों को प्रेरित करने में भी सहायक है।
-
इसके माध्यम से शिक्षण के विभिन्न अंगों की गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है।
मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान
(Steps of Evaluation Process)
मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन प्रमुख आधार हैं - उद्देश्य, अधिगम सम्बन्धी अनुभव तथा मूल्यांकन के उपकरण। ये तीनों आधार एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्ध रखते हैं। इनमें से किसी भी एक आधार के अभाव में मूल्यांकन की प्रक्रिया का सम्बन्ध ही प्राप्त पूर्णता असम्भव है। इन आधारों को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन की प्रक्रिया को तीन सोपानों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ये तीन सोपान निम्नलिखित हैं -
(1) शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से अधिगम के उपयुक्त अनुभव उत्पन्न करना - निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अधिगम अनुभवों का विशेष महत्त्व होता है। इन अनुभवों के आधार पर ही छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। शिक्षण के विभिन्न अंग अथवा शिक्षण प्रक्रिया से सम्बन्धित क्रियाकलापों के द्वारा ही अधिगम अनुभवों को प्रदत्त किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण भी इसके द्वारा ही सम्भव हो पाता है। वस्तुतः उद्देश्यों की प्राप्ति करने की दृष्टि से अधिगम अनुभव ही सर्वोत्तम सहायक होते हैं। किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार कई व्यवहार परिवर्तन आवश्यक होते हैं उसी प्रकार एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई अधिगम अनुभवों की आवश्यकता होती है। इन अधिगम अनुभवों के माध्यम से ही परिस्थितियों की पूर्ति तथा अधिगम अनुभवों के संयोजन की प्रक्रिया में अन्तर्निहित शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मूल्यांकन अधिगम अनुभवों के आधार पर ही सम्भव हो पाता है, अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम अनुभवों की व्यवस्था एवं उनका संयोजन जितने उपयुक्त ढंग से किया जायेगा उतना ही मूल्यांकन भी विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ सिद्ध होगा।
(2) शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण व परिसीमांकन - शिक्षण की प्रक्रिया के चार प्रमुख तत्त्व होते हैं। इनमें सबसे पहला सोपान शिक्षण का नियोजन करना है। इसी सोपान के अन्तर्गत शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। कौशल, ज्ञान, प्रवृत्ति, रुचियाँ आदि से सम्बन्धित इन उद्देश्यों के आधार पर ही बालकों के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। उद्देश्यों की उपयुक्त जानकारी का बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसके आधार पर ही यह ज्ञात हो पाता है कि किन-किन व्यवहार परिवर्तनों के आधार पर इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, अतः उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान व उनका सुनिश्चित निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण सोपान है। इसी सोपान के अन्तर्गत उद्देश्यों के परिसीमांकन की क्रिया भी सम्पन्न होती है। परिसीमांकन के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि किस उद्देश्य के सम्बन्ध में बालकों में कौन-से व्यवहार परिवर्तन होंगे।
(3) व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना - शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से जो अधिगम अनुभव प्रदत्त किए जाते हैं वे अधिगम अनुभव ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार परिवर्तनों में सहायक होते हैं। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् ब्लूम के द्वारा प्रत्येक उद्देश्य के सन्दर्भ में इन व्यवहार परिवर्तनों को निर्धारण किया जाता है। उदाहरणार्थ, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। ये छः उद्देश्य हैं- ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य के लिए कुछ व्यवहार परिवर्तन भी सुनिश्चित किए गये हैं जैसे- ज्ञान उद्देश्य से सम्बन्धित व्यवहार परिवर्तन हैं - नवीन सूचनाएँ, तथ्य, नियम, सिद्धान्त आदि का स्मरण करना तथा परीक्षा के आधार पर इन्हें यथायोग्य अभिव्यक्त कर देना। इसी प्रकार भावात्मक एवं क्रियात्मक स्तर से सम्बन्धित उद्देश्यों तथा उद्देश्यों से सम्बन्धित व्यवहार परिवर्तनों का निर्धारण भी ब्लूम के द्वारा किया गया है। वस्तुतः इन व्यवहार परिवर्तनों के निर्धारण एवं मूल्यांकन के अभाव में यह जानना असम्भव है कि किस उद्देश्य की प्राप्ति कितनी सीमा तक हो चुकी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी उद्देश्य की प्राप्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को एक मापदण्ड के आधार बनाया जाता है।
मूल्यांकन के उपर्युक्त सोपानों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है। छात्रों की योग्यताओं के सम्बन्ध में शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता के प्रति पर्याप्त सावधानी रखी जाये।
मूल्यांकन का महत्त्व
(Importance of Evaluation)
इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षण की प्रक्रिया के सतत संचालन में मूल्यांकन का अत्यधिक महत्त्व है। यदि सार रूप में कहा जाए तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया का निरन्तर सम्पादन हो पाना न केवल कठिन है, वरन् असम्भव भी है। मूल्यांकन के महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है -
(1) छात्रों में निहित योग्यताओं के सम्बन्ध में जानकारी - शिक्षा का महत्त्वपूर्ण पक्ष बालकों का सर्वांगीण रूप से विकास करना है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है कि मानसिक, भावात्मक एवं शारीरिक पक्ष का विकास करते से है। इन तीनों प्रकार के स्तरों पर छात्रों के विकास के लिए अनेक विशिष्ट शक्तियों का विकास करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, छात्रों के मानसिक पक्ष का विकास करने के लिए उनमें बोध, विश्लेषण, ज्ञान, संश्लेषण आदि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास करना आवश्यक होता है। इन विशेष योग्यताओं का विकास किए बिना छात्रों का मानसिक विकास नहीं किया जा सकता है।
यह छात्रों में निहित विशेष योग्यताओं अथवा शक्तियों ही हैं, जिनके आधार पर छात्र का समस्त व्यवहार संचालित होता है। छात्रों के इस व्यवहार तथा विशेष शक्तियों के विकास का प्रमुख माध्यम, अधिगम के अनुभव होते हैं जो नियमित पाठ्यक्रम का अंग होते हैं। इन अधिगम अनुभवों की प्राप्ति करते ही, छात्र विविध प्रकार के व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं। व्यवहार का यह रूप प्रदर्शन ही छात्र में निहित, अन्तर्निहित शक्तियों की जानकारी में सहायक होता है। परन्तु तब तभी सम्भव हो पाता है जब मूल्यांकन के द्वारा इन व्यवहार परिवर्तनों की सीमा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो जाये।
(2) छात्र को प्रेरित करने एवं निर्देश प्रदान करने के लिए - छात्र को प्रेरणा प्रदान करने एवं अध्ययन की दिशा में अग्रसरण हेतु निर्देश देने की दृष्टि से भी मूल्यांकन का विशेष महत्त्व होता है। यदि मूल्यांकन के आधार पर किसी शिक्षार्थी (Student) को सफल घोषित कर दिया जाता है तो उस शिक्षार्थी की सर्वत्र सराहना होती है तथा उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत यदि वह असफल/अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है अथवा वांछित स्तर तक उपलब्धि प्राप्त करने में असफल रहता है तो मूल्यांकन के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह किन कोशलों में कमजोर है तथा किन क्षेत्रों में प्रगति की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह निर्देश भी प्रदान किया जा सकता है कि वह सफलता प्राप्त करने के लिए क्या और किस प्रकार कार्य करे ?
(3) उद्देश्य प्राप्ति हेतु जानकारी - उद्देश्य प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने का एकमात्र माध्यम मूल्यांकन ही है। शिक्षण की प्रक्रिया के संचालन से पूर्व जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, यह केवल मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अभाव में यह जानकारी प्राप्त कर पाना नितान्त असम्भव है। यह छात्रों में निहित योग्यताओं, क्षमताओं, कौशलों आदि के सम्बन्ध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने का एकमात्र माध्यम है।
(4) छात्रों की उपलब्धि के स्वरूप में जानकारी - छात्रों की उपलब्धि का ज्ञान अनेक दृष्टियों से आवश्यक होता है। सम्पूर्णता के आधार पर जो ज्ञान छात्रों को प्रदत्त किया जाता है, उस ज्ञान को अधिग्रहण करने के लिए परीक्षण का आयोजन किया जाता है। परीक्षा के द्वारा ही यह स्पष्ट प्रमाण होता है कि छात्रों को बताया पारस्थितियों में अधिग्रहण करें। यह अधिग्रहण, लिखित एवं मौखिक दोनों ही रूप में की जा सकती है। इस अधिग्रहण को ही मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार बनाया जाता है। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र ने किसी विशिष्ट विषय में कितनी उपलब्धि की है। उपलब्धि के सम्बन्ध में प्राप्त यह जानकारी छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाने, कठिनाइयों का निवारण करने तथा छात्रों के भविष्य के सम्बन्ध में क़दम उठाने की दृष्टि से विशेष सहायक होती है।
(5) शिक्षण में परिवर्तन एवं बाह्य सुधार हेतु - छात्रों में निहित शक्तियों के विकास करने हेतु निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षण प्रक्रिया का विशेष महत्त्व होता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता व सम्यकता में जानकारी प्राप्त होती है। यदि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है तो इसी के आधार पर यह भी मान लिया जाता है कि शिक्षण के विभिन्न अंग प्रभावपूर्ण हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत यदि यह ज्ञात होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति satisfactorily नहीं हो सकी है तो शिक्षण के समस्त अन्य आंगों में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं तथा उन्हें पुनः नियोजित, व्यवस्थित एवं सम्पन्न किया जाता है।
इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में बाह्य सुधार करके इस प्रक्रिया को उद्देश्य केन्द्रित बनाने की दृष्टि से भी मूल्यांकन का अत्यन्त महत्त्व होता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत जितना महत्त्व अन्य सोपानों का है उतना ही महत्त्व मूल्यांकन का भी है।
|
|||||