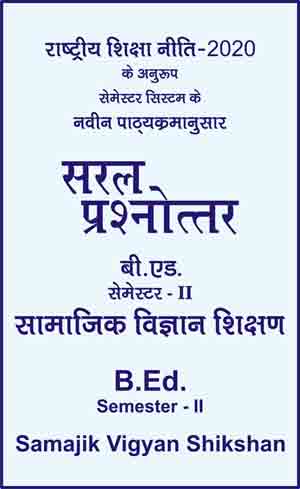|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 15 - पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में एक सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण
(Critical Analysis of a Social Science Textbook with reference to Syllabus)
प्रश्न- पाठ्य-पुस्तक का क्या अर्थ है ? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली कसौटियों का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए।
अथवा
पाठ्य-पुस्तक से क्या आशय है ? सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक के प्रमुख लक्षण लिखिए।
अथवा
पाठ्यक्रम एवं छात्रों के परिवेश के सन्दर्भ में सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य-पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
अथवा
पाठ्य-पुस्तकों के आलोचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए तथा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर -
पाठ्य-पुस्तक का अर्थ
(Meaning of Text-Book)
पाठ्य-पुस्तक सीखने वाला एक साधन है, जिसका प्रयोग विद्यालय तथा कॉलेजों में अनुशासन कार्यक्रम को परिचालित करने हेतु किया जाता है। सामान्य अर्थ में, पाठ्य-पुस्तक मुद्रित होती है जिसकी जिल्द मजबूत होती है, यह अनुशासन अधिगम में प्रयुक्त की जाती है और सीखने वालों के हाथों में सौंपी जाती है। पाठ्य-पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने परिभाषा के रूप में अपने विचार व्यक्त किये हैं, जो निम्नलिखित हैं -
"पाठ्य-पुस्तक अनुशासन अधिगमों के लिए व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया एक प्रामाणिक चिन्तन का अधिग्रह है"
"पाठ्य-पुस्तक कक्षा-कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है।"
सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन का मापदण्ड
(Scale for Evaluating Text-Books of Social Studies)
A. प्रकाशन सामग्री –
(1) पुस्तक का नाम,
(2) लेखक या लेखकों का,
(3) प्रकाशक,
(4) पृष्ठों की संख्या,
(5) पुस्तक का मूल्य।
B. भौतिक तत्व –
(1) पुस्तक का आकार,
(2) जिल्द की सुदृढ़ता,
(3) काग़ज़,
(4) छपाई
(5) मार्जिन की चौड़ाई।
C. संगठन –
(1) पाठों की सामान्य योजना,
(2) पाठों का तर्कसंगत विभाजन,
(3) पाठों की पूर्णता,
(4) सारांश।
D. प्रस्तुतीकरण –
(1) शैली,
(2) भाषा,
(3) सुसंगति,
(4) निष्पक्षता,
(5) प्रयोगिक शब्द।
E. उद्धरण –
(1) उदाहरणों की सुसंगति,
(2) पुनरुच्चारण,
(3) छात्रों के लिए उपयुक्त उदाहरण।
F. चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ तथा चार्ट –
(1) संख्या,
(2) शुद्धता,
(3) सुसंगति,
(4) आकार,
(5) उपयुक्तता तथा महत्व,
(6) स्पष्टता।
G. प्रश्न –
(1) पाठ्य-वस्तु से सम्बन्ध,
(2) उनकी विविधता,
(3) शिक्षक तथा छात्रों की दृष्टि से महत्व,
(4) उनकी प्रेरणा-शक्ति।
H. परिशिष्ट तथा अनुक्रमणिका –
(1) व्यवस्थापन,
(2) विषय-सूची,
(3) व्यावहारिकता,
(4) पूर्णता,
(5) महत्व।
सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक के लक्षण
(Criteria of Social Studies Text-Book)
सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक में निम्नलिखित लक्षणों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है –
(1) पाठ्य-वस्तु का चयन एवं व्यवस्था – इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –
(i) छात्रों की दृष्टि से पाठ्य-वस्तु का चयन उनकी रुचि, अवस्था, योग्यता, मानसिक स्तर, प्रौढ़ता, अनुभवों तथा समझबूझ स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
(ii) छात्रों की दृष्टि से पाठ्य-वस्तु का स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए जिससे पाठ्य-पुस्तक समान तथा आर्थिक विकास एवं उन्नति के लिए देश के नागरिकों में नवाचारों का संचार कर सके।
(iii) पाठ्य-वस्तु की व्यवस्था छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए।
(iv) समस्याओं एवं शिक्षण-विधियों के अनुकूल व्यवस्था की जाये।
(v) पाठ्य-वस्तु में मनोवैज्ञानिक क्रम स्थापित किया जाये।
(2) पाठ्य-वस्तु की बाह्य आकृति –
टाइटल, जिल्द, काग़ज़, चित्रों की संख्या, शब्दों के बीच की दूरी, आकार, मार्जिन की चौड़ाई आदि की उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाये।
(3) विषय-सूची – उनकी ग्रहणता, महत्व तथा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए।
(4) प्रस्तुतीकरण –
पाठ्य-पुस्तक की पाठ्य-वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए जो –
(i) छात्रों में व्याख्यान की आदतों का निर्माण एवं कुशलताओं का विकास कर सके।
(ii) प्रत्येक विषय की पाठ्य-वस्तु में सहसम्बन्ध स्थापित कर सके एवं सहायक हो।
(iii) वर्ग तथा वैयक्तिक विभेदताओं की सन्तुष्टि करती हो।
(iv) सीखने के नियमों के अनुकूल हो।
(v) निर्देशित अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करने वाली हो।
(vi) सुसंगति के अनुसार हो।
(vii) छात्रों में विषय के प्रति रुचि जाग्रत करे।
(viii) छात्रों के मानसिक विकास में सहायक हो।
(5) शैक्षिक साधन – अध्ययन के लिए प्रश्न, निर्देश, सहायक पुस्तकों की सूची, अनुक्रमणिका, प्रस्तारण आदि की यथायोग्यता तथा उनकी उपयुक्तता।
(6) उदाहरण – शाब्दिक तथा प्रदर्शनात्मक उदाहरण जैसे, सूची-पत्र, तालिकाएँ, ग्राफ, रेखाचित्र एवं रेखाचित्रित, मानचित्र आँकड़े, उद्धरण एवं सन्दर्भ की शुद्धता, उपयुक्तता तथा पर्याप्त संख्या।
(7) लेखक – उनके विचारों की स्पष्टता, मौलिकता एवं निष्पक्षता, अनुभव एवं प्रतिष्ठा, योग्यता तथा प्रकाशन और मनोविज्ञान का ज्ञान।
|
|||||