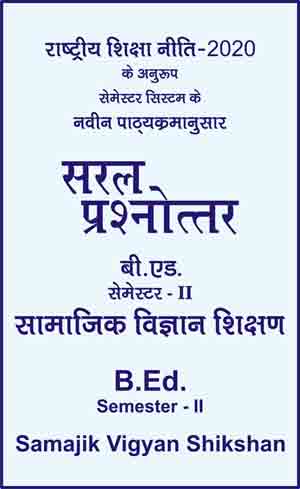|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 14 - परीक्षण अनुभूति और परीक्षण
प्रदर्शन, ग्रेडिंग सिस्टम, सी.बी.सी.एस,
उपलब्धि परीक्षण का निर्माण
(Testing Cognition and Testing Performance,
Grading System, CBCS, Construction of Achievement test)
प्रश्न- वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विज्ञान अध्ययन में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिए।
अथवा
सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
सामान्य लघु उत्तरीय प्रश्न
- वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अर्थ बताइए।
- वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुणों की विवेचना कीजिए।
- वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष बताइए।
- वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर -
वस्तुनिष्ठ परीक्षा का अर्थ
(Meaning of Objective Type Test)
वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ उन परीक्षाओं को कहते हैं जिनका निर्माण निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रणाली के अन्तर्गत बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता तथा बुद्धि आदि की जाँच अनेक प्रकार प्रश्नों के माध्यम से होती है। यह परीक्षा प्रायः 100 या कभी-कभी 200 तक छोटे-छोटे तथा कठिन प्रश्नों के लिखित उत्तर द्वारा थोड़े ही समय में कर ली जाती है। इन परीक्षाओं के उत्तर निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। अतः इनमें वस्तुनिष्ठता होती है। इनके मूल्यांकन में किसी प्रकार की पक्षपात नहीं दिखाया जाता और न ही शिक्षक की परीक्षा में मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। कोई भी परीक्षक उन्हें जाँचने जाये मूल्यांकन द्वारा किये गये उत्तरों में भिन्नता नहीं होगी।
अर्थात् एक ही परिणाम रहेगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षा का साहित्य सन् में "होरेस मैन" (Horace Mann) ने सन् 1845 ई० में किया था इसके उपरान्त जॉर्ज फिशर (Jeorge Fisher), जे० एम० राइस (J.M. Rice) तथा स्टॉर्च (Starch) एवं थॉर्न डाइक (Thorndike) आदि विद्वानों ने शैक्षिक निष्पत्ति (Educational Achievement) के मूल्यांकन हेतु बैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा बनायी और इनसे ही बालकों के व्यवहार के अध्ययन व विकास के मापदण्ड के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग किया जा रहा है।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण
(Merits of Objective Type Test)
वस्तुनिष्ठ परीक्षा के निम्नलिखित गुण होते हैं –
(1) वस्तुनिष्ठता (Objectivity) - ये परीक्षाएँ निरपेक्ष (Objective) होती हैं। इन पर परीक्षा की आत्मनिष्ठता (Subjectivity) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(2) विश्वसनीयता (Reliability) - ये परीक्षाएँ विश्वसनीय होती हैं। इन परीक्षाओं की किसी बालक अथवा बालकों के समूह को जितनी बार दिया जाता है उतने ही बार प्रत्येक परीक्षाओं में सत्य पाया जाता है।
(3) सरल अंकन (Easy Scoring) - निबंधात्मक परीक्षाओं में उत्तर-पुस्तिकाओं के जाँचने में काफी समय लगता है। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अंकन कार्य कुछ ही घण्टों में समाप्त हो जाता है।
(4) वैधता (Validity) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ उसी वस्तु का मानक करती हैं जिसके मापन के लिए इनका निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये परीक्षाएँ वैध होती हैं।
(5) भविष्यवाणी निश्चित करता (Definite Predicatability) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणामों को देखकर निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इन परीक्षाओं के परिणामों के आधार मानकर बालकों को उचित दिशा में मार्ग-प्रदर्शन किया जा सकता है।
(6) व्यावहारिकता (Practicability) - इन परीक्षाओं को देने में कम समय लगता है। इन्हें बालक तथा शिक्षक दोनों ही पसन्द करते हैं। अतः ये परीक्षाएँ व्यावहारिक भी हैं।
(7) व्यापकता (Comprehensiveness) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ सम्पूर्ण विषय-क्षेत्र का मापन करती है। अतः ये परीक्षाएँ विद्यालयीय परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं।
(8) लेखन तथा शैली का प्रभाव नहीं (No Effect of Writting and Style) - निबंधात्मक परीक्षाओं में बालकों के परीक्षण पर लेख तथा शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में बालकों के लेख, शैली विवेचन, व्याख्या तथा तर्क आदि शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष
(Demerits of Objective Type Test)
वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष प्रमुखतः निम्न प्रकार से हैं –
(1) कठिन निर्माण (Difficult Construction) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रश्न की संख्या ही से कई गुना से भी अधिक होती है। इन प्रश्नों का निर्माण केवल योग्य, अनुभवी तथा कुशल व्यक्ति ही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का निर्माण बहुत कठिन होता है।
(2) मानसिक योग्यताओं के मूल्यांकन की कठिनाई (Difficulty of Measuring Mental Abilities) - निबंधात्मक परीक्षाओं में बालकों के तर्क, अभिव्यक्ति, विचार तथा आलोचना आदि मानसिक योग्यताओं की जाँच आसानी से की जा सकती है परन्तु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में उत्तर मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
(3) अधूरी सूचना (Partial Information) - इन परीक्षाओं में प्रश्न बहुत छोटे होते हैं। इनके उत्तरों को या तो चिन्हों में दिया जाता है अथवा एक दो शब्दों में। इससे परीक्षा की बालकों के विषय में पूरी जानकारी नहीं हो पाती।
(4) अनुमान तथा धोखा (Guessing and Cheating) - इन परीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर देते समय बालक अधिकतर अनुमान से कार्य करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वे शिक्षक को धोखा देकर दूसरों बालकों की उत्तर-पुस्तकों से नक़ल भी कर लेते हैं।
(5) आवश्यकता से अधिक सरल (Over Simplification) - कभी-कभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ इतनी सरल होती हैं कि कमज़ोर-से-कमज़ोर बालक भी इनके प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर लिख देते हैं। इससे बालकों के भविष्य का उचित पथ-प्रदर्शन नहीं हो पाता है।
(6) विचार संगठन का अभाव (Lack of Organization of Thought) - इन परीक्षाओं में बालक प्रश्नों के छोटे-छोटे उत्तर देते हैं। इससे उनमें न तो कल्पना तथा मौलिकता चिन्तन का विकास होता है और न ही वे अपने विचार को क्रमबद्ध रूप से संगठित कर पाते हैं।
वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएँ
(Characteristics of Objective Type Tests)
अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं -
(1) विश्वसनीयता (Reliability) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की प्रथम विशेषता उनकी विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि किसी अमुक परीक्षा का बालकों पर तथा बालकों का परीक्षा पर सदैव एक-सा प्रभाव रहे। दूसरे शब्दों में, जब कोई परीक्षा किसी बालक अथवा बालकों के समूह को बार-बार दिए जाने पर भी एक ही अंक दें तो ऐसी परीक्षा को विश्वसनीय परीक्षा कहा जाता है।
(2) वैधता (Validity) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की दूसरी विशेषता उनकी वैधता है। यदि कोई परीक्षा अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती तो उसे वैध परीक्षा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत यदि कोई परीक्षा केवल उसी गुण का मापन करती है जिसके मापनार्थ उसका निर्माण किया गया है तो निस्सन्देह वह परीक्षा वैध मानी जायेगी।
(3) वस्तुनिष्ठता (Objectivity) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की तीसरी विशेषता यह है कि इनके फलस्वरूप न तो परीक्षक की आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव पड़ता है और न ही बालकों की मानसिक स्थिति का। अतः यदि कोई परीक्षा बालकों की निष्पक्षता का निर्धारण तथा मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाती है वह वस्तुनिष्ठ है। यदि किसी परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का अभाव है तो वह विश्वसनीय तथा वैध भी नहीं हो सकती।
(4) व्यापकता (Comprehensiveness) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की चौथी विशेषता उनकी व्यापकता है। दूसरे शब्दों में, इनके अन्तर्गत पाठ्यक्रम का पूर्ण प्रतिनिधित्व होता है। जिन परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्न न पूछकर केवल सीमित क्षेत्र से ही प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसी परीक्षाओं को व्यापक परीक्षाएँ नहीं कहा जा सकता है। इनमें बालकों का सम्पूर्ण ज्ञान असन्तुलित होना बालकों के भाग्य पर निर्भर करता है।
(5) विवेचन (Discrimination) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की पाँचवीं विशेषता विवेचन करता है। इसके अन्तर्गत ऐसे प्रश्नों को चुना जाता है जो मंद, औसत तथा प्रखर बुद्धि वाले बालकों में आसानी से विवेध कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नपत्र में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो कुछ हद तक औसत बुद्धि वाला बालक ही कर सके, मंद बुद्धि वाले बच्चे न करे एवं प्रखर प्रश्न भी होने चाहिए ताकि उत्तर ठीक प्रश्न प्रखर बुद्धि वाला बालक ही दे सके। इस प्रकार ये परीक्षाएँ विवेचक होती हैं।
(6) व्यावहारिकता (Practicability) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की छठी विशेषता उनका व्यावहारिक होना है। इन परीक्षाओं में समय की बचत होती है और निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा खर्च भी कम छप होता है। बालक भी इन्हें पसन्द करते हैं तथा शिक्षकों को भी अंक प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस दृष्टि से ये परीक्षाएँ व्यावहारिक होती हैं।
(7) उपयोगिता (Utility) - वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की सातवीं विशेषता उनकी उपयोगिता है। चूँकि इन परीक्षाओं का निर्माण किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसलिए उद्देश्य ज्ञात हो जाने पर इनके परिणामों को आधार मानते हुए बच्चों को भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शन किया जा सकता है। अतः वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ निबंधात्मक परीक्षाओं की तुलना में अधिक उपयोगी होती हैं।
प्रश्न- निबंधात्मक परीक्षाओं से क्या तात्पर्य है? निबंधात्मक परीक्षा के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए इसके गुण व दोष लिखिए।
अथवा
निबंधात्मक परीक्षा क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निबंधात्मक प्रश्नों के गुण तथा दोष स्पष्ट कीजिए।
अथवा
निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। (कानपुर 2008)
सामान्य लघु उत्तरीय प्रश्न
- निबंधात्मक परीक्षण से क्या आशय है?
- निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रकार बताइए।
- निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- निबंधात्मक प्रश्नों के दोषों को समझाइए।
- निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर -
निबंधात्मक परीक्षा
(Essay Type Examination)
हमारे देश में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का अधिक प्रचलन है। इस परीक्षा प्रणाली में परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर विस्तार से देता है, उत्तर की कोई सीमा निश्चित नहीं की जाती है तथा विद्यार्थी अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण स्वतन्त्र होता है। वास्तव में इन परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षार्थी की विभिन्न मानसिक योग्यताओं, जैसे- विश्लेषण, चिन्तन, कल्पना, आलोचना, मूल्यांकन की उचित मूल्यांकन सम्भव है, फिर भी ये परीक्षाएँ सुलझन इसलिये बन गई हैं कि कई बार परीक्षक केवल सुन्दर लेख एवं भाषा-शैली के आधार पर उत्तर को पुनः किसी कुशलता के साथ प्रस्तुत कर पाता है।
निबंधात्मक परीक्षाओं के रूप/प्रकार (Forms/Types of Essay Type Examination)
निबंधात्मक परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है -
1. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions) - इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में दिये जाते हैं जिनकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं होती, जैसे -
(अ) सुभाषचन्द्र बोस के भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान का विस्तृत विवेचन कीजिए।
(ब) राज्यसभा के संगठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
(स) भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के प्रभावों को लिखे गये कदमों का उल्लेख कीजिए।
2. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions) - इस प्रकार के प्रश्नों के परीक्षार्थी के निर्धारित शब्द-सीमा अथवा 9-10 पंक्तियों में देने होते हैं, जैसे -
(a) हिमालय को नवम बल्ति पर्वत क्यों कहा जाता है?
(b) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
(c) भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व बताइए।
3. अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions) - ऐसे प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थी को मात्र एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना होता है, जैसे -
(a) स्वतंत्रता संग्राम का आरम्भ किस स्थान से हुआ?
(b) भारत में वर्ष में कितना जल प्राप्त होता है?
(c) भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता है?
निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण
(Merits of Essay Type Examination)
निबंधात्मक परीक्षाओं में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं -
(1) उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन - केवल निबंधात्मक परीक्षाएँ विचारों के समाधान करती हैं जिनके उत्तर देने के लिए उच्च मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। मौलिकता का मापन केवल निबंधात्मक परीक्षाओं से ही सम्भव है।
(2) व्यक्तित्व एवं चिन्तन विधि पर प्रकाश - यदि एक अध्ययन पूर्ण गहराई से निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करे तो उसे बालकों के व्यक्तित्व व चिन्तन विधि के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को स्पष्ट एवं प्रभावशाली विधि से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है।
(3) भावों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति सम्भव - इसमें विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने में स्वतन्त्र होता है। किसी उत्तर में वह जिन तथ्यों को देना चाहे उन्हें दे सकता है। इसमें सम्बन्धित सूचना का संगठन वह स्वयं कर सकता है। उसके दृष्टिकोण, रुचि भावों की अभिव्यक्ति का पथ बन जाता है।
(4) विभिन्न अध्ययन विधियों के विकास में सहयोग - निबंधात्मक मूल्यांकन प्रणाली में विद्यार्थी की अध्ययन विधियों पर प्रभाव स्पष्ट पड़ता है। जब विद्यार्थियों को पता रहता है कि निबंधात्मक प्रणाली में उत्तर देने होंगे तो वे श्रवण, संज्ञान, संश्लेषण, सर्जन, प्रवृत्ति व ‘मूल्यांकन’ की जानकारी आदि विधियाँ अपनाते हैं जिनका प्रयोग वह अन्य परीक्षाओं हेतु नहीं करता है। इस प्रकार निबंधात्मक परीक्षा से विशिष्ट अध्ययन विधि के विकास में सहायता मिलती है।
(5) विश्वसनीयता एवं वैधता में वृद्धि की सम्भावना - यदि निबंधात्मक प्रश्नों की रचना, उनके प्रश्नावली एवं मूल्यांकन में सुधार हो जाए तो ये परीक्षाएँ भी उतनी ही विश्वसनीय एवं वैध हो सकती हैं जितनी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ। टाइलर के अनुसार, यह परीक्षा चार प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने में अधिक उपयोगी है-
-
सूचना, 2. चिन्तन, 3. अध्ययन दक्षता, 4. कार्य करने की आदतें
(6) उचित अध्ययन-विधि को प्रोत्साहन - ये परीक्षाएँ बालकों को अध्ययन में अच्छे ढंग से सीखने के लिए अधिक प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि ये केवल सूचना को अपेक्षा प्रयत्नशील, तथ्यों एवं उनके सम्बन्धों की अभिव्यक्ति एवं उनके प्रयोग पर अधिक बल देती हैं।
(7) कम समय में रचना अत्यधिक सरल - निबंधात्मक प्रश्नों की रचना अत्यधिक सरल है। केवल थोड़े से प्रश्नों की सहायता से विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित ज्ञान का मापन किया जा सकता है। यदि परीक्षा में कम समय रहे तो प्रश्नों की रचना को समय से पहले समय में मिलते ही बहुत कम समय में प्रश्नों की रचना की जा सकती है।
(8) नक़ल की कम सम्भावना - निबंधात्मक प्रश्न अत्यधिक लम्बे तथा उनमें भाषा-शैली एवं विषय-वस्तु का प्रभाव होता है के कारण इन प्रश्नों में नक़ल करने की कम सम्भावना होती है।
निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष/सीमाएँ
(Demerits /Limitations of Essay Type Examination)
निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष अथवा सीमाओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है -
(1) प्रतिनिधित्व की कमी - पूरे प्रश्नपत्र में कुल मिलाकर 10-11 प्रश्न होते हैं और विद्यार्थी को इनमें से ही 4-5 प्रश्न करने होते हैं। ये थोड़े से प्रश्न सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पाठ्यक्रम के अन्दर महत्वपूर्ण अंश बिल्कुल छूट जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप छात्र इसमें 33% या 36% या किसी अन्य स्तर पर फ्लाफ प्राप्त कर ले तो उसे उत्तीर्ण समझा जाता है। अतः इसमें प्रतिनिधित्व की कमी रहती है।
(2) दुर्बल छात्रों के लिये अनुपयुक्त - कुछ दुर्बल परीक्षार्थी परीक्षा की कला में निपुण होते हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार उत्तर लिखें, अनुमान लगाएँ एवं परीक्षक को प्रभावित करें। अतः ज्ञान न होने पर भी अन्य परीक्षार्थियों की अपेक्षा वे अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं जिससे उनकी प्राप्ति का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता।
(3) एकरूपता की कमी - निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षा का स्तर सन्देह-एकरूपता नहीं रखा जा सकता। कुछ परीक्षक अत्यन्त कठिन प्रश्नपत्र बनाते हैं जबकि कुछ अत्यन्त सरल प्रश्नपत्र बनाते हैं। प्रश्नपत्र एक वर्ग से दूसरे वर्ग एवं एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भिन्न होते हैं। इसी कारण द्वितीय श्रेणी में पास होने वाला विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी से श्रेष्ठ माना जाता है।
(4) अपूर्ण न्यायार्थ - इसमें सफलता संयम पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम के एक भाग से प्रश्न पूछे गये और अगर बालक ने वह भाग पढ़ा है तभी वह उत्तर दे सकता है अन्यथा असफल हो जाता है। इसी कारण कम योग्य विद्यार्थी सफल हो जाते हैं तथा योग्य विद्यार्थी असफल हो जाते हैं।
(5) आनियमित फलांक व्यवस्था - निबंधात्मक परीक्षाओं में फलांकों की व्यवस्था वास्तविक होती है किन्तु उत्तरों को अलग-अलग व्यक्तियों से जाँच कराने पर अलग-अलग फलांक प्राप्त होते हैं। इसी कारण इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है।
(6) रटने पर बल - वास्तव में, निबंधात्मक परीक्षाएँ ज्ञानोपाजन का मापन नहीं करती हैं। ये केवल स्मरण-शक्ति या रटने की योग्यता का मूल्यांकन करती हैं। उनके विद्यार्थी जो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम न पढ़कर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लेते हैं, इससे वे विद्यार्थी जो रटने में कुशल होते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं।
|
|||||