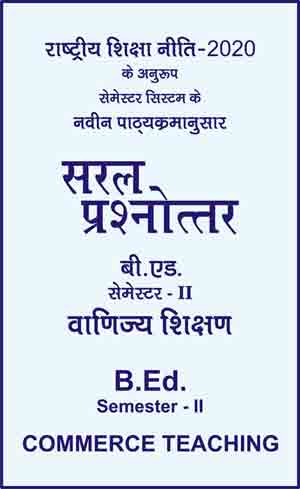|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 2 - वाणिज्य का अन्य विद्यालयी विषयों से सह-सम्बन्ध
(Correlation of Commerce with Other School Subjects)
प्रश्न- वाणिज्य शिक्षण में शिक्षा के सह-सम्बन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
शिक्षा के सह-सम्बन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
शिक्षा के समन्वय पुरातन काल से चला आ रहा है। पुरातन काल में शिक्षा जीवन-केन्द्रित थी, परन्तु सह-सम्बन्ध का आधुनिक रूप 150 वर्ष पूर्व यूरोप में विकसित हुआ। यह रूप विख्यात शिक्षाशास्त्री हरबर्ट के दार्शनिक सिद्धान्तों से प्रारम्भ हुआ। हरबर्ट के अनुसार-शिक्षा का मुख्य ध्येय चरित्र निर्माण करना है। उसने कहा है कि यह उद्देश्य निर्देशनात्मक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निर्देश द्वारा विचार चक्र निर्मित किया जाएगा और शिक्षा चरित्र का निर्माण करेगी। वह शिक्षा द्वारा रुचियों की वृद्धि, विकास तथा प्रयोग पर बल देता है। रुचियों का विकास ज्ञान द्वारा किया जा सकता है। इसलिए उसने ज्ञान की प्राप्ति पर अधिक बल दिया। इसके लिए उसने विविध विषयों का ज्ञान देने के लिए कहा, जिससे छात्रों के विचारों में वृद्धि हो। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। इस प्रकार उसका विचार चक्र पूर्ण होता है, जो कि चरित्र निर्माण करने में सहायक हैं। हरबर्ट ने सर्वप्रथम स्कूल के पाठ्य विषयों में सह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कहा। उसका कथन है कि पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषयों का ज्ञान महायक हो सके। इसको उसने 'सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त' के नाम से पुकारा! इसका आधार उसका 'पूर्वानुवतीं ज्ञान का सिद्धान्त' था। इस सिद्धान्त के अनुसार-सभी नवीन विचार तभी ग्राह्य हो सकते हैं, जब उनका सम्बन्ध हमारी चेतना में विद्यमान विचारों से स्थापित किया जाता है अर्थात् हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमारे पूर्वानुवर्ती विचारों से नवीन विचारों को सम्बन्धित कर दिया जायेगा तभी नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसी पूर्व - ज्ञान के सहारे अध्यापक को नवीन ज्ञान में छात्रों की रुचि तथा ध्यान को केन्द्रित करना चाहिए, तभी नवीन ज्ञान स्थायी हो सकेगा। उसकी पंचपद प्रणाली में प्रथम पद प्रस्तावना है जो पूर्व-ज्ञान पर आधारित है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान के लिए छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर तैयार करना है। उसका कथन है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को इस प्रकार सम्बन्धित करके पढ़ाया जाए जिससे बालकों के मस्तिष्क पर . उनका समवेत प्रभाव पड़े।
हरबर्ट के शिष्य जिलर ने इस सिद्धान्त को और अधिक विस्तृत करके केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त निरूपित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार-किसी एक विषय को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बनाकर अन्य विषयों का उसी के आधार पर शिक्षण किया जाए। उसने सभी विषयों को शिक्षा देने के लिए 'इतिहास' को केन्द्रीय विषय माना, परन्तु कर्नल पार्कर ने 'प्राकृतिक अध्ययन' को केन्द्रीय विषय बनाया जिसके माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। डी. गार्मो ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक कुशलता बताया। इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने 'भूगोल तथा अर्थशास्त्र' को केन्द्रीय विषय माना। डीवी के अनुसार-शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने शिक्षालय को जीवन की ठोस परिस्थितियों से सम्बन्धित करने के लिए कहा अर्थात् शिक्षालय में उन क्रियाओं को व्यवस्थित किया जाय जो जीवन से सम्बन्धित हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा शिक्षालय व समाज के जीवन को केन्द्रीय विषय माना गया है। डीवी ने इस प्रकार की सम्बद्धता को सामंजस्यीकरण के नाम से पुकारा। डीवी के सामंजस्यीकरण में बालक स्वयं अनुभवों से सम्बन्ध स्थापित करता है, परन्तु हरबर्ट के सह - सम्बन्ध के सिद्धान्त में शिक्षक द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। गाँधी जी की बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्त्व का सम्पूर्ण विकास तथा आत्म-निर्भरता का विकास करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 'हस्तकला' को केन्द्रीय विषय माना।
|
|||||