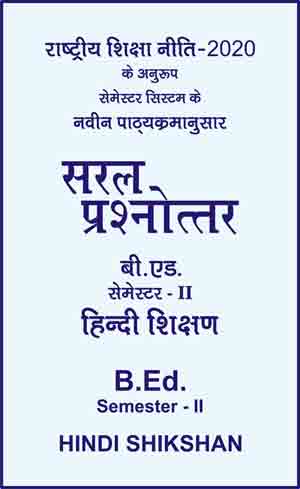|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 7- हिन्दी शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ एवं शिक्षण युक्तियाँ
प्रश्न- हिन्दी शिक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन-सी हैं? किसी एक विधि का वर्णन कीजिये।
अथवा
मातृभाषा शिक्षण की विधियों को बताइये तथा आगमन व निगमन विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
उत्तर-
भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम तथा साधन होता है। भाषा की प्रमुख क्रियाएँ - बोलना, लिखना, पढ़ना तथा सुनना हैं। भाषा की शुद्धता से तात्पर्य शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध सुनने से होता है। इन क्रियाओं की शुद्धता व्याकरण पर आधारित होती है। अर्थात् व्याकरण से इनमें शुद्धता आती है। भाषा का अमूल्य वरदान मनुष्य को ही प्राप्त है। भाषा ईश्वरीय व प्रकृति की देन है परन्तु भाषा का निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया है। हिन्दी / मातृभाषा की शिक्षण विधियों का वर्णन निम्नलिखित है-
1. लेखन कला के द्वारा - लेखन कला के द्वारा विद्यार्थियों को विचार अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है और उन्हें स्वयं वाक्य विन्यास करने का शिक्षण दिया जाता है। पद्य अथवा गद्य पढ़ाने के पश्चात् विद्यार्थियों को गृहकार्य प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी घर पर अपने-आप बगैर किसी के सहयोग के अपना गृहकार्य पूरा करते हैं तथा शिक्षकं उनके दोष निकालते हैं। निबन्ध-रचना तथा लेख- प्रतियोगिताओं द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। भाषा तथा शैली के विकास के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की रचनाओं का अभ्यास कराना अत्यन्त आवश्यक है।
2. प्रश्नों के द्वारा - शिक्षक विद्यार्थियों से उनके बोध- ज्ञान का पता लगाने के लिए परिस्थिति के अनुरूप प्रश्न करता है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से उनके बोध- ज्ञान का पता लगाने के अतिरिक्त उनके शुद्ध बोलने की शक्ति का भी पता लगता है। शिक्षक विद्यार्थियों के शुद्ध उत्तरों को ही स्वीकारता है जिसके कारण विद्यार्थी शुद्ध बोलना सीखते हैं।
3. काव्य-शिक्षण के द्वारा - विद्यार्थियों में सौन्दर्यानुभूति को उत्पन्न करने तथा विकसित करने में काव्य-शिक्षण का अत्यधिक महत्त्व है। शिक्षक कक्षा में स्वयं काव्य-पाठ करके वातावरण को सौन्दर्यमय तथा सरस बनाता है। एक विद्वान ने लिखा है कि, "कविता का बोध होने के पश्चात् विद्यार्थियों को भावों की गहराई में उतारने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ प्रश्नों की सहायता से विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति में लाया जाता है कि वे स्वयं भावों की गहराई में पहुँचकर डुबकियाँ लगाने लगते हैं। समान भाव की कविताओं अथवा पंक्तियों को सुनाने एवं सुनने से इस ओर बहुत सहायता मिलती है।"
4. वाचन द्वारा - विद्यार्थियों को वाचन कला में कुशलता प्रदान करने हेतु सस्वर वाचन कराया जाता है। काव्य-पाठ में विद्यार्थियों से आरोह-अवरोह का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है।
5. मौन - पाठ द्वारा - विद्यार्थियों में बोध शक्ति का विकास करने के लिए मौन-पाठ का अभ्यास कराया जाता हैं।
6. व्याकरण - शिक्षा द्वारा - भाषा की शुद्धता तथा अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है।
7. विभिन्न क्रियाओं के द्वारा - वाद-विवाद, नाटक, भाषण तथा सुलेख प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी छात्रों की सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास किया जाता है। इन क्रियाओं में भाग लेने से बालक शुद्ध बोलना तथा मनन करना सीखते हैं। उन्हें आत्म-अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं।
मातृभाषा शिक्षण की अन्य विधियाँ-
1. अनुकरण विधि - वाचन तथा लेखन।
2. आगमन तथा निगमन विधि- व्याकरण विधि।
3. प्रत्यक्ष शिक्षण विधि।
4. अभ्यास विधि - सामूहिक वाचन प्रविधि |
5. व्यवस्थित शिक्षण विधि।
6. वेस्ट की शिक्षण विधि।
आगमन विधि (Inductive Method) - आगमन तथा निगमन विधियाँ अधिक प्राचीन हैं। आज भी इनका उपयोग शिक्षा में किया जाता है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षण की स्वाभाविक विधि है क्योंकि छात्र का ज्ञान वस्तुओं के निरीक्षण पर आधारित होता है। जिन वस्तुओं को वह देखता है उनके सम्बन्ध में क्या, क्यों, कैसे? प्रश्न पूछता है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर- से नियम तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। मातृभाषा शिक्षण में इसका विशेष महत्त्व है। इस विधि में ' सीखने' को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इस विधि से छात्रों की 'सृजनात्मक' योग्यता का विकास होता है। इस विधि को उदाहरण विधि भी कहते हैं। इसके कई उदाहरण देकर उनसे नियम का प्रतिपादन किया जाता है। निगमन विधि में संज्ञा के दो उदाहरण दिए गए थे। इन्हें पहले दिया जायेगा तथा छात्रों से पूछा जाएगा कि यह पढ़ने में क्यों अच्छे लगते हैं? इस कविता की सुन्दरता कैसे बढ़ गई? शब्दों तथा अक्षरों से आरम्भ होने की पुनरावृत्ति हुई है। शिक्षक को बताना होगा कि जिन शब्दों या अक्षरों से कविता या काव्य की सुन्दरता / शोभा बढ़ती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। आगमन विधि के दो प्रकार हैं-
1. प्रयोग प्रणाली - इस प्रणाली के अनुसार-, व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सम्मुख पहले उदाहरण रखे जाते हैं। अनेक उदाहरणों में समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण छात्रों से कहलाये जाते हैं। अन्त में उन्हीं के द्वारा कही हुई बातों के आधार पर सिद्धान्त या नियम निकलवाये जाते हैं और फिर उन्हीं से उनका प्रयोग तथा अभ्यास कराया जाता है। अतः इस प्रणाली में निम्नांकित सोपानों अथवा पदों का अनुसरण करना पड़ता है-
(i) उदाहरण- प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित अनेक उदाहरण बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना।
(ii) तुलना एवं विश्लेषण - उन उदाहरणों की परस्पर तुलना करना, विश्लेषण करना और उनसे व्यक्त समान लक्षणों एवं विशेषताओं को समझाना।
(iii) नियमीकरण या निष्कर्ष - लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर नियम, निष्कर्ष या परिभाषा निकालना।
(iv) प्रयोग और अभ्यास - निकाले गए निष्कर्ष या नियमों की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोग करना और उनका अच्छी तरह अभ्यास करना।
2. सह-सम्बन्ध विधि - इस विधि में व्याकरण के नियमों को अधिक बोधगम्य कराया जाता है. क्योंकि इस विधि में उनकी सार्थकता एवं उपयोगिता का अनुभव कराया जाता है। यह आगमन विधि का ही एक रूप है। गद्य-शिक्षण एवं रचना-शिक्षण के साथ व्याकरण के नियमों का बोध कराया जाता है। सूक्ष्म तथा अमूर्त नियमों का ज्ञान उदाहरणों से दिया जाता है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण - सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
निगमन विधि (Deductive Method) - इस विधि को "नियम उदाहरण" विधि भी कहते हैं। इसमें छात्रों को पहले नियम समझा दिए जाते हैं। उसके बाद उदाहरण से उस विषय का प्रयोग करके दिखाया जाता है। इस नियम को पूर्णरूप में प्रस्तुत करके उदाहरण को अपूर्ण रूप में रखकर छात्रों से पूर्ति कराते हैं या उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। संज्ञा के शिक्षण हेतु नियम के अन्तर्गत परिभाषा सिखाते हैं-
नियम - "संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है।" इसके बाद छात्रों को वाक्यों में संज्ञा पहचानने को कहा जाता है।
उदाहरण- "छात्र व्याकरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। " इस वाक्य में 'छात्र' तथा 'पुस्तक' संज्ञा प्रयुक्त की गयी हैं।
परम्परागत व्याकरण-शिक्षण प्रणाली को सिद्धान्त अथवा निगमन प्रणाली कहा गया है। इस प्रणाली में नियम या परिभाषा बताकर उसके उदाहरण दे दिए जाते हैं।
इस प्रणाली के दो रूप हैं-
1. सूत्र प्रणाली - इसके अनुसार- व्याकरण के नियम सूत्र में रटा दिए जाते हैं और उनके लक्षण तथा उदाहरण बता दिए जाते हैं। यह प्रणाली अमनोवैज्ञानिक और परम्परागत संस्कृत व्याकरण-शिक्षण की ही नकल है जहाँ बालक संस्कृत भाषा में कुछ बोलने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही लघु कौमुदी के सूत्रों को रटना प्रारम्भ कर देता है। इस प्रणाली से भाषा के प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता।
2. पाठ्य-पुस्तक प्रणाली - इस प्रणाली में भी व्याकरण की पुस्तकों में दी गई परिभाषाएँ और सिद्धान्त रटा दिए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण आदि की परिभाषा और भेद छात्रों को बता दिए जाते हैं। इस प्रणाली से भी भाषा का प्रयोग और अभ्यास नहीं होता और बालक केवल व्याकरणीय नामों को याद करके सन्तोष कर लेता है।
अतः उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि निगमन या सिद्धान्त प्रणाली दोषपूर्ण प्रणाली है। अत- उसकी जगह आगमन प्रणाली का प्रयोग वैज्ञानिक और उपयोगी माना जाता है।
|
|||||