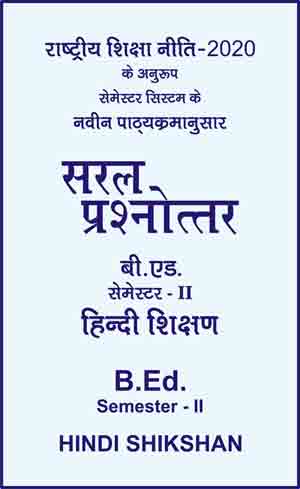|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 4 - हिन्दी में कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त, सूत्र एवं भाषा शिक्षण के सिद्धान्त
प्रश्न- मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त बताइये।
अथवा
हिन्दी भाषा शिक्षण के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
अथवा
हिन्दी में कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त कौन-कौन से हैं? किसी एक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
मातृभाषा (हिन्दी भाषा) शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त
सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण सिद्धान्त लगभग समान होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय पर बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान दिया जाना आवश्यक है, किन्तु मातृभाषा के साथ यह एक और विशेषता जुड़ी है कि बालक स्वयं ही अनुकरण द्वारा वातावरण से सीखना प्रारम्भ कर देता है। अतएव उसको मातृभाषा का अनुकरण उसी क्रम से कराना आवश्यक है जिस क्रम से बालक स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। मातृभाषा शिक्षण में जिन सामान्य सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं-
1. अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धान्त - प्रायः यह देखा गया है कि बालक उसी विषय या क्रिया में रुचि लेते हैं। जो उनकी जन्मजात इच्छाओं को सन्तुष्ट करती हैं। मातृभाषा का शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अतएव हिन्दी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। हिन्दी भाषा के शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक अनेक उपाय कर सकता है। किसी वस्तु, उसकी मॉडल या चित्र को दिखाकर वह बच्चों में उसके बारे में जानकारी या जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। बच्चों को अन्ताक्षरी प्रतियोगिता द्वारा ही भाषा सीखने की प्रेरणा दी जा सकती है।
2. क्रियाशीलता का सिद्धान्त - बालक क्रियाशील होता है। उसे करके सीखने (Learning by doing) में आनन्द का अनुभव होता है। प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियों ने जिनमें फ्रोबेल, डीवी, गाँधी, पार्क, मॉन्टेसरी, ईश्ट आदि प्रमुख हैं, ने इस सिद्धान्त पर बल दिया है। भाषा की शिक्षा के समय क्रियाशील के सिद्धान्त को अपनाना आवश्यक है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत् क्रियाशीलता रखने के लिए प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य अपनाये जा सकते हैं। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है।
3. अभ्यास का सिद्धान्त - मनोविज्ञान का यह मानना है कि पाठ जितनी तेजी से बालक याद करते हैं उससे तीव्रतर गति से विस्मृत करते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धान्त आवश्यक है। इससे विस्मृति रुकती है तथा छात्रों का ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित होता है। भाषा में कलात्मक पक्ष के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है।
थॉर्नडाइक ने कहा है- “भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है।"
4. जीवन-समन्वय का सिद्धान्त - प्रत्येक स्तर पर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे-वैसे ही अपने ढंग से एक नये संसार की कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होती हैं। अत- अध्यापक को चाहिए कि जो वह बच्चों को पढ़ाने के लिये पाठ्य सामग्री उसका सम्बन्ध उनके जीवन से हो। पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री का सम्बन्ध उनके जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए, अन्यथा वे सीखने में रुचि नहीं लेंगे। साहित्य के दो पक्ष होते हैं-गद्य एवं पद्य। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को गद्य-शिक्षण के समय व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान एवं पद्य शिक्षण के समय शब्द- शक्ति, शब्द- योजना, छन्द, अलंकार एवं रसों का ज्ञान अवश्य करायें।
5. निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धान्त - हिन्दी भाषा-शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना अथवा किसी को बिल्कुल ही छोड़ देना ठीक नहीं है। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना आवश्यक है। पाठ्य सामग्री की एक रूपरेखा होनी चाहिए, उसे स्थूल रूप देना शिक्षक का कार्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णनात्मक निबन्ध लिखना सिखाया जाये और उन निबन्धों का क्या स्तर हो, यह अध्यापक को स्वयं निश्चित करना चाहिए। हिन्दी शिक्षण द्वारा अध्यापक को बच्चों में सौन्दर्यानुभूति को जागृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। अत- यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक को शिक्षा देने पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए।
6. वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धान्त - मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण देना चाहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षाशास्त्रियों ने वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धान्त पर बल दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता, तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता। किसी का वाचन ठीक नहीं होता, तो किसी का लेख अशुद्ध है। कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सबकी वैयक्तिक भिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना चाहिए।
7. अनुपात और क्रम का सिद्धान्त - अध्यापक भाषा सिखाने के लिये पाठ्य-पुस्तकों के एक-दो पृष्ठ पढ़ाने, व्याकरण के नियम बताने और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्त्तव्य और कुछ भी नहीं समझता। परिणामतः भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रहती है। भाषा सिखाने के केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिये भी बोलकर समझाने, लिखकर समझाने और सुनकर समझाने तथा पढ़कर समझाने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण के दो अंग हैं-ग्रहण और अभिव्यक्ति। दूसरों के विचार ग्रहण करने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है-
1. पढ़ने से,
2. सुनने से।
8. जीवन एवं अनुभवों से सम्बन्ध - जिस विषय-वस्तु का बच्चे अपने निजी अनुभवों एवं दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं और जो उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन में उनके अनुभव में आती रहती है, उनसे यदि शिक्षण का सम्बन्ध जोड़कर अध्यापन कार्य किया जाए तो बच्चे सरलता से सीखेंगे और रुचि भी लेंगे। अतः बच्चों को उनके खेल-खिलौने, पशु-पक्षी, कथा-कहानी से शिक्षण का सम्बन्ध बताते हुए पढ़ाना चाहिए।
9. अनुकरण सिद्धान्त - बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं। इसलिये बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसा ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। यदि माता-पिता और विद्यालय में शिक्षक के बोलने के ढंग में अन्तर हो, तो बच्चे शिक्षक के बोलने के ढंग का अनुकरण करेंगे। यही कारण है कि बच्चों को विद्यालय में भेजने से उनके बोलने तथा भाषा - ज्ञान आदि में विकास होता है और वे सुधरी, सँवरी शुद्ध भाषा बोलना सीख जाते हैं।
10. चयन का सिद्धान्त - भाषा-शिक्षण के लिये कब किस सिद्धान्त का या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी सटीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिये अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए, जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें।
11. बाल केन्द्रित होने का सिद्धान्त - भाषा शिक्षण के समय इस बात का पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केन्द्र बालक है। अध्यापक इस समय इतना भाव-विभोर होना चाहिए कि बालक विस्तृत हो जाए, इसलिये भाषा-शिक्षण का केन्द्र बालक हो। बालक का स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए।
12. शिक्षण-सूत्रों का सिद्धान्त - शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके अनुसार-, शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे "सरल से कठिन की और", "ज्ञात से अज्ञात की ओर", "मूर्त से अमूर्त की ओर", "विशिष्ट से सामान्य की ओर", "आगमन से निगमन की ओर", "विश्लेषण से संश्लेषण की ओर" आदि। शिक्षण में इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षा अधिक प्रभावकारी होती हैं।
13. साहचर्य सिद्धान्त - बच्चे दूसरों को सुनकर तो सीखते ही रहते हैं परन्तु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिये साहचर्य का होना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकता है, जब शब्द 'माँ' के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या 'पापा' के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ-साथ अर्थात् साहचर्य होने से ही बच्चों को उस शब्द की समझ और पहचान हो सकेगी।
|
|||||