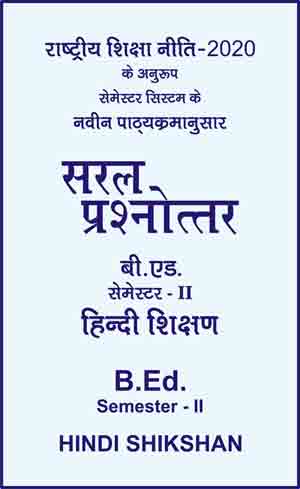|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- हिन्दी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति - 'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति का कारण फारसी प्रभाव बताया जाता है। सिन्धु-प्रदेश वासियों को ईरानी 'हिन्दी' नाम से पुकारते रहे। इसका कारण यह है कि फारसी में संस्कृत की 'स' ध्वनि 'ह' हो जाती है। इसी प्रकार संस्कृत का 'सप्ताह' फारसी प्रभाव के कारण हप्ताह हो गया। कालान्तर में यही 'हिन्दू' शब्द का समस्त भारतीय भाषाओं के लिए व्यहृत होने लगा और हिन्दुओं की भाषा को हिन्दी कहा जाने लगा। यह सही है कि हिन्दी शब्द प्राचीन आर्यभाषा-संस्कृत, प्राकृत अथवा अपभ्रंश में नहीं मिलता है। अरबी साहित्य में हिन्दी का अर्थ हिन्दी की भाषा है। हिन्दी शब्द से बने हिन्दी शब्द का एक अर्थ हिन्दुस्तान का निवासी भी होता है। प्राचीन कवि इकबाल ने इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है- 'हिन्दी हैं, हम वतन हैं, हिन्दोस्ताँ हमारा। परन्तु आज हिन्दी का जो अर्थ और रूप मिलता है, वह मध्य देश की भाषा से है। मुसलमानों को जब अनुभव हुआ कि हिन्दी सम्पूर्ण देश की भाषा नहीं है तो विशिष्ट अर्थ में वे मध्यदेश की भाषा को हिन्दी कहने लगे। हो सकता है उन्हें लगा हो कि वास्तव में मध्यदेश की भाषा ही हिन्दी देश की भाषा है, वरना कोई कारण नहीं है कि अर्थ का वैशिष्ट्य करते हुए पंजाबी, बंगला या गुजराती आदि को हिन्दी की भाषा (हिन्दी) नहीं कहा। बात भी ठीक है कि मध्ययुग के आरम्भ में सिंधी, लाहौरी, बंगला, गुजराती आदि मात्र बोलियाँ थीं और इनको उन्होंने गिनाया ही है बोलियों में। किन्तु, हिन्दी सार्वदेशिक 'भाषा' थी। सिन्धी, पंजाबी, बंगला, गुजराती आदि का जो साहित्य तब था, वह वस्तुतः लोग साहित्य था। तभी तो महाराष्ट्र के नामदेव, तुकाराम आदि, गुजरात के नरसी मेहता और दूसरी भक्तकवि, पंजाब के नानक और अन्य सिख गुरु सार्वदेशिक भाषा में लिखते थे- भले ही क्षेत्रीय जनता के लिए उन्होंने अपनी रचनाएँ लोक भाषाओं में भी कीं।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास तृतीय प्राकृत अर्थात् अपभ्रंश से हुआ है। इन भाषाओं में सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमी तथा हिन्दी आदि भाषाएँ हैं। यहाँ पर हिन्दी के विकास पर चर्चा की जा रही है।
हिन्दी का इतिहास - लगभग सन् 1000 ई. के पश्चात् अपभ्रंश भाषा शनै-शनैः हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। मध्यदेश अर्थात् गंगा की घाटी में बोली जाने वाली शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों ने हिन्दी भाषा के समस्त रूपों को जन्म दिया है। पिछले सहस्र वर्षों के विकास को तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है-
आदिकाल - हिन्दी के प्रारम्भिक रूप आठवीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को संक्रांति काल या संधिकाल कहा जा सकता है। यह काल हिन्दी का प्रारम्भिक युग है। इस युग की प्राप्त सामग्री संदिग्ध है। हिन्दी का प्रथम कवि 'पुष्य' माना जाता है, ये भोज के दरबारी कवि थे। 11वीं शती के आते-आते हिन्दी साहित्यिक भाषा के रूप में पदासीन हो गई। इस समय की हिन्दी पर प्राकृत अपभ्रंशों का प्रभाव था। इस संक्रांति काल में हिन्दी 'एक ओर अपने प्राचीन रूप अवहट्ठ की केंचुली उतार रही थी, दूसरी ओर प्रारम्भिक हिन्दी का नवीन रूप निखर रहा था।
इस काल के साहित्य को प्रामाणिकता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। शिलालेख तथा ताम्रपत्र जिन्हें अध्ययन के आधार के लिए प्रामाणिक माना गया है, सर्वथा अभाव है। इस समय विदेशी आधिपत्य के आधार के लिए प्रामाणिक माना गया है, सर्वथा अभाव है। इस समय विदेशी आधिपत्य के भी हो चुका था। केवल धार्मिक आंदोलनों ने कुछ संप्रदायों को जन्म देकर हिन्दी भाषा के विकास में सहायता की। गोरखनाथ, रामानन्द और कबीर ने अपने संप्रदायों के माध्यम से हिन्दी के प्रचार और प्रसार में योगदान दिया। इन संतों ने जनता का मार्ग-दर्शक बनकर उन्हीं की भाषा (जनभाषा) में रचनाएँ कीं। इस युग के प्रतिभासम्पन्न कवि अमीर खुसरों हुए। खुसरों की भाषा आज की खड़ी बोली के निकट है। यह भाषा उस समय की दिल्ली, मेरठ आदि की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर विद्यापति की 'कीर्तिलता' में अवहट्ठ (अथवा परवर्ती अपभ्रंश) के रूप में मिलते हैं।
इसके अतिरिक्त इस काल की भाषा के दो अन्य रूप भी मिलती हैं, जिन्हें डिंगल और पिंगल के नाम से पुकारते हैं। इनके सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है-
"प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक साहित्यिक भाषा की स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में 'पिंगल' भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह 'डिंगल' कहलाता था।" इस परम्परा के प्रसिद्ध काव्य बीसल देव रासो' और 'पृथ्वीराज रासो' आदि हैं।
इस प्रकार हिन्दी के उद्भव काल में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। धीरे-धीरे हिन्दी इस प्रभाव से मुक्त होती गई।
मध्यकाल - साहित्यिक दृष्टि से मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर- मध्यकाल दो भागों में विभाजित किया जाता है परन्तु भाषा के विकास की दृष्टि से यह काल पूर्ण रूप से ब्रजभाषा के उत्कर्ष एवं विकास से जुड़ा है। मध्यकाल के आरम्भ में ही हिन्दी की डिंगल और पिंगल बोलियों का स्थान ब्रज, अवधी और खड़ी बोली ने ले लिया। हिन्दी भाषा के मध्यकाल का आरम्भ से 1375 से 1900 तक माना जाता था। इस काल का आरम्भ राजनीतिक दृष्टि से उथल-पुथल था किन्तु मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो गयी और एक सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता का उदय हुआ। इसके बाद से ही राष्ट्र में कला, साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के विकास एवं परिष्कार का कार्य प्रारम्भ हो गया। मध्यकाल में केन्द्रीय सत्ता का केन्द्र दिल्ली थी किन्तु शासक विदेशी थे, जिनकी भाषा फारसी थी। अतः उनका दृष्टिकोण हिन्दी के प्रति इतना सहज नहीं था, फिर भी जन चेतना के प्रवाह एवं कालान्तर में साम्राज्य की स्थिरता के कारण लोगों ने भारतीय भाषाओं को प्रश्रय देना प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण है कि इस काल में हिन्दी की अनेक प्रमुख बोलियों ने साहित्यिक वैशिष्ट्य प्राप्त कर लिया। ऐसी बोलियों में अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली प्रमुख हैं।
'अवधी' का साहित्यिक विकास मध्यकाल में हुआ, यद्यपि, अवधी अवध क्षेत्र की भाषा थी परन्तु इस भाषा में जो कृतियां प्रणीत हुई उनको भारतीय समाज में इतना सम्मान मिला कि ये क्षेत्रीय बोली भाषा के रूप में स्थापित हो गयी। अवधी की अमरकृति गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस ने तो भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दिया। इसके अतिरिक्त सूफी कवि जायसीकृत-'पद्मावत' लोक-मानस में हिन्दू-मुसलमान एकता का पथ प्रदर्शन करता है।
इस काल की दूसरी प्रमुख भाषा ब्रजभाषा रही साहित्यिक दृष्टि से मध्यकाल के दोनों भाग-भक्तिकाल और रीतिकाल में विपुल साहित्य रचना ब्रजभाषा में प्राप्त होती है।
सूर, रसखान, बिहारी, घनानन्द, पद्माकर आदि कवियों ने ब्रजभाषा में लिखकर इस युग की श्रेष्ठ भाषा के रूप में घनानन्द, पद्माकर को स्थापित करने में योग दिया।
इस काल की तीसरी प्रमुख भाषा खड़ी बोली थी। यद्यपि इस युग में खड़ी बोली को विशेष साहित्यिक प्रतिष्ठा नहीं मिली, फिर भी आधुनिक मानक भाषा का प्रारम्भिक रूप इस काल की भाषा में देखा जा सकता है। अमीर खुसरो इस खड़ी बोली के सर्वप्रथम प्रयोक्ता थे जिनकी भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है-
चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुँ देश।।
खुसरो तो आदिकाल के कवि हैं। मध्यकाल में रहीम के काल में खड़ी बोली का पर्याप्त प्रयोग मिलता है।
ध्वनियों की दृष्टि से इस काल की विशेषता यह है कि इस काल में संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों का हिन्दी रचनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा और हिन्दी में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ गया। अपभ्रंश का द्वित्व रूप भी इस काल में कम हो गया। इस प्रकार इस काल तक आते-आते हिन्दी का स्वरूप तो निखरा ही, उसका शब्द भण्डार भी बढ़ गया, क्योंकि एक ओर तत्सम शब्दावली का बाहुल्य था तो दूसरी ओर अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का भी हिन्दी के साथ सामंजस्य हुआ। इसी कारण हिन्दी भाषा के विकास में मध्यकाल को ब्रजभाषा का 'स्वर्णयुग' कहा जाता है।
आधुनिककाल (1800 से अब तक) - हिन्दी का आधुनिक काल अंग्रेजी शासन की स्थापना से प्रारम्भ होता है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य के लिए प्रयत्न शुरू हुये। गद्य के विकास में मुद्रण-कला ने विशेष योग दिया। अवधी और ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप भी जन-भाषा से पूर्णतः अलग हो गया। अंग्रेजी शासकों ने सरकारी कर्मचारियों के दैनिक व्यवहार के लिए खड़ी बोली को ही स्वीकार किया, और इसे हिन्दुस्तानी नाम दिया। फल यह हुआ कि खड़ी बोली एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकृत हो गई। आधुनिक काल में काव्य रचना के रूप में खड़ी बोली को अपना लिया गया। संस्कृत की तत्सम शब्दावली से इसके अपने साहित्यिक रूप का श्रृंगार किया। साथ ही खड़ी बोली की नई शैली का भाषा एवं साहित्य दोनों दृष्टियों से विकास हुआ। इसी समय हिन्दी, अंग्रेजी तथा देशी व विदेशी भाषाओं के सम्पर्क में आई।
खड़ी बोली में साहित्य-रचना करने वाले प्रारम्भिक साहित्यकारों में लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्ला खाँ तथा सुदासुखलाल नियाज का नाम उल्लेखनीय है। भारतेन्दु-मुण्डल के लेखकों (विशेषकर स्वयं भारतेन्दु जी, पं. बालकृष्ण भट्ट, पं. प्रतापनारायण मिश्र आदि) ने इसे परिमार्जित और विकसित किया। द्विवेदी युग के आते-आते खड़ी बोली ही साहित्य की एक आम भाषा रह गई, तब लेकर आज तक खड़ी बोली का परिष्कार तथा परिमार्जन हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचन्द्रं शक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. रामकुमार वर्मा प्रभृति लेखको तथा कवियों ने आधुनिक काल में हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया।
|
|||||