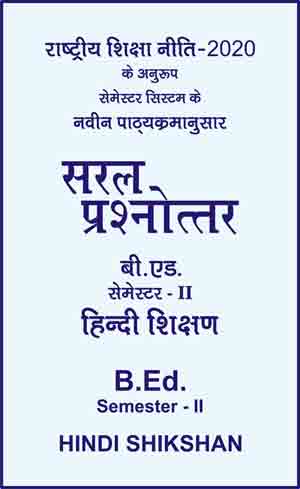|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 2 - हिन्दी : ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान
प्रश्न- हिन्दी भाषा में ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि-ग्रामों का अर्थ बताइए। ध्वनि-विज्ञान के सभी प्रकरणों का विवेचन कीजिए।
अथवा
"ध्वनि गठन" का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हिन्दी के स्वरों का वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1- हिन्दी भाषा में ध्वनि-विज्ञान तथा ध्वनि-ग्रामों का अर्थ बताइए।
उत्तर-
हिन्दी भाषा में ध्वनि-विज्ञान
ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध वर्णमाला से होता है। हिन्दी की वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। हिन्दी में दस स्वरों का प्रयोग होता है और बयालीस व्यंजन होते हैं। ध्वनियों का सम्बन्ध वर्णमाला के स्वर अक्षरों से होता है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण से वायुमार्ग में किसी भी प्रकार का पूर्ण या अपूर्ण अवरोध नहीं होता है।"
स्वरों की संख्या ग्यारह मानी जा सकती है। "भाषा-ध्वनि का सम्पूर्ण अध्ययन ध्वनि-विज्ञान है।"
भोलानाथ तिवारी ने ध्वनि-विज्ञान की तीन शाखाओं का उल्लेख किया है-
1. औच्चाराणिक ध्वनि-विज्ञान - बोलना
2. श्रोतिक ध्वनि-विज्ञान - सुनना
3. तरंगीय ध्वनि-विज्ञान - ध्वनि वेग।
इन शाखाओं का सम्बन्ध बोलने, ध्वनियों को सुनने तथा ध्वनि के प्रकार अथवा ध्वनि लहरों सम्बन्धी प्रक्रिया तथा यन्त्रों के अध्ययन से होता है। ध्वनि-विज्ञान का विकास, वर्गीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
1. ध्वनि-ग्राम-विज्ञान,
2. ऐतिहासिक ध्वनि-विज्ञान,
3. शारीरिक ध्वनि-विज्ञान,
4. वेग अथवा तरंगी ध्वनि-विज्ञान
5. हिन्दी भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण।
ध्वनि-ग्राम विज्ञान
ध्वनि इकाई मात्र है। ध्वनियों के परिवर्तन से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। भाषा विभिन्न ध्वनियों का निरन्तर प्रवाह है। ध्वनियाँ भाषा में शब्द के निर्माण में उपयोग की जाती हैं। सीमित ध्वनियों से असीमित शब्दों की संरचना की जाती है। प्रत्येक भाषा के ध्वनि-ग्राम अन्य भाषाओं के ध्वनि-ग्रामों से भिन्न होती है।
"ऐसी ध्वनियों के समूह को जिन्हें हमारे कान एक ध्वनि के रूप में स्वीकार करते हैं उसे ध्वनि-ग्राम कहते हैं। इस समूह निर्मित करने वाले ध्वनि के विभिन्न रूपों को ' सध्वनि' कहते हैं। '
भोलानाथ तिवारी के अनुसार- “किसी भाषा में किसी भी ध्वनि के यह विभिन्न रूप ही "संध्वनि" कहलाते हैं और उनका सामूहिक रूप से सबको समावेश करने वाला ध्वनि-ग्राम कहलाता है।"
रोबर्ट लाडो के अनुसार- "ध्वनि-विज्ञान में भाषा के ध्वनि-ग्राम और उनकी विभिन्न सध्वनियों का वर्णन होता है। यह सध्वनियाँ उच्चारण की दृष्टि से एक ही ध्वनि ग्राम की अनेक विविध ध्वनियाँ हैं। "
ध्वनि-ग्राम तथा सध्वनि
सम्पूर्ण भाषा विभिन्न ध्वनियों का निरन्तर प्रवाह है। मात्र 50-60 ध्वनियों से कई लाख शब्दों का निर्माण हो जाता है। वास्तव में उच्चारित भाषा का नियंत्रण ही उसकी भाषा विज्ञान है। बोलने और लिखने में अन्तर होता है क्योंकि एक ही ध्वनि की उच्चरित भाषा में कई सध्वनियाँ हैं। यद्यपि लिखते समय कोई भेद नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम क्रम से कागज, कलम, कपड़ा, कमान, केला शब्दों का उच्चारण करें तो अनुभव होगा कि उत्तरोत्तर पश्चगामी होता चला जा रहा है। इसी प्रकार हिन्दी में दो सध्वनियाँ स्फोटित 'प' व अस्फोटित 'प' वितरण में एक-दूसरे के पूरक हैं। अस्फोटित 'प' शब्दान्त में आता है। जैसे धूप, रूप, आप व स्फोटित 'प' अन्यत्र जैसे- पलंग, अपना, अटपटा आदि।
ध्वनि-ग्रामों में सध्वनियों का अस्तित्त्व किसी भाषा विशेष के सन्दर्भ में ही होता है। इंग्लिश में W तथा V दो ध्वनि-ग्राम हैं जबकि हिन्दी में इन दो ध्वनि-ग्रामों के लिये " व" ध्वनि-ग्राम हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाये तो कोई भी व्यक्ति एक ध्वनि को दो बार से अधिक पूर्ववत् उच्चारण नहीं करता। एक ही ध्वनि-ग्राम समूह को जिन्हें हमारे कान एक ध्वनि के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें ध्वनि-ग्राम कहते हैं।
ध्वनि-गठन का स्वरूप
प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनि-गठन होता है जो अन्य भाषाओं से भिन्न प्रकार होता है। हिन्दी भाषा के ध्वनि-ग्राम दो प्रकार के होते हैं-
1. खण्ड ध्वनि-ग्राम।
2. खण्डेत्तर ध्वनि-ग्राम।
स्वर तथा व्यंजनों का पता खण्ड ध्वनि-ग्राम के अन्तर्गत लगाया जाता है। खण्डेत्तर ध्वनि-ग्राम खण्ड-ग्राम पर आधारित होते हैं। इनमें बलाघात, सुरलहर, संगम अनुनासिकता और दीर्घता का अध्ययन किया जाता है।
हिन्दी में स्वरों की संख्या (आँ) से मिलाकर ग्यारह मानी जाती है। हिन्दी स्वरों का वर्गीकरण छः आधार पर किया जाता है-
(1) मात्राओं के आधार पर - हृस्व उच्चारण में कम समय और दीर्घ में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ह्रस्व अ, इ, उ, दीर्घ- आ, ई, ऊ, ऐ, ओ हैं।
(2) जीभ के भाग के आधार पर - अग्र स्वर- इ, ई, ए, ऐ, मध्य स्वर अ तथा पिछला स्वर उ, ऊ, ओ, औ, आँ।
(3) मुख के मार्ग से निकलने के आधार पर - जिन स्वर के उच्चारण में वायु मुख से निकलती है, जैसे- अ, आ, ओ, इ, ई, उ, ए, ऐ, औ। इस प्रकार के स्वर, जिनमें वायु नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं जैसे- अं, आँ, ई, ॐ, ऐं, औं आदि।
(4) ओठों की स्थिति के आधार पर - ओठ वृतमुखी - उ, ऊ, ओ, औँ तथा ओठ अवृतामुखी अ, आ, इ, ई, ए, ऐ।
(5) जीभ के उठने के आधार पर - जीभ ऊपर उठती है तो उसे संवृत तथा नीचे को होने को विवृत कहते हैं तथा मध्य में रहने को अर्धविवृत कहते हैं। संवृत जैसे- इ, ई, उ, ऊ, अर्धसंवृत जैसे- ऐ, ओ; अर्धविवृत ऐ, अ, आँ; विवृत - आ।
(6) प्रकृति के आधार पर - स्वर मूल तथा संयुक्त दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर में जीभ स्थिर रहती है जैसे- अ, ओ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर में जीभ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है जैसे- ऐ, औ संयुक्त स्वर हैं।
हिन्दी के व्यंजनों की संख्या बयालीस होती है और इनका वर्गीकरण निम्नांकित चार आधार पर किया जाता है-
(1) स्थान के आधार पर - व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। जैसे ओठ, दाँत, मसूड़े, तालव्य (तालु), जीभ तथा गले व मुख से उच्चारण किये जाते हैं।
1. ओठों से - प, फ, ब, भ, म, व
2. दाँतों से - त, थ, द, ध
3. तालु से - च, छ, ज, झ, ञ
4. पूर्व तालव्य से - ट, ठ, ड, ढ, ण
5. कोमल तालु से - क, ख, ग, घ, ङ
6. गले से - ह, क, ख, ज आदि।
(2) प्रयत्न के आधार पर - व्यंजन के आधार पर जो प्रयत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहा जाता है। इसमें एक अंग का दूसरे अंग से स्पर्श होता है जैसे- क, ख, ग, घ, ट, ठ, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, व भ, म स्पर्श व्यंजन हैं।
(3) प्राणत्म के आधार पर - प्राण का अर्थ है वायु जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है अल्पप्राण, यदि अधिक वायु निकलती है तो महाप्राण व्यंजन- क, ग, च, ज, ट, ड, ण, त, द, न, थ, ब, य, र, ल, व आदि।
महाप्राण व्यंजन - ख, घ, छ, झ, ठ, द, थ, ध, फ, भ आदि।
(4) घोषत्व के आधार पर - गले में स्थित स्वर-यन्त्र में घर्षण के साथ जो ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं और जिनमें यह यन्त्र प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। घोष ध्वनि - ग, घ, ज, झ, ड, द, ण, क्ष, ध, न, भ, म, र, ल, व, ह, ज, ग, ड सभी स्वर घोष हैं। अघोष ध्वनि क, ख, च, छ, ट, ठ, व, त, प, फ, स, श, फ अघोष स्वर हैं।
|
|||||