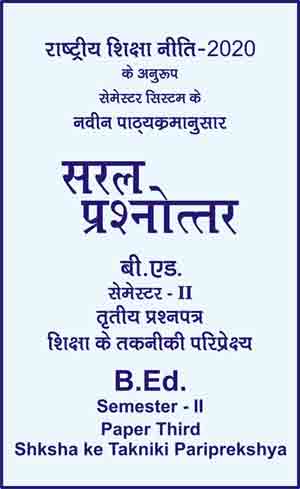|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्यसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय-9 शिक्षण तथा अधिगम में तकनीकी
(Technology in Teaching and Learning)
प्रश्न- अधिगम का क्या अर्थ है? मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गयी इसकी परिभाषाओं एवं अधिगम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
अधिगम का अर्थ
अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चलने वाली सतत् एवं निरन्तर प्रक्रिया है। जीवन के साथ-साथ अधिगम प्रक्रिया भी चलती रहती है। अधिगम का अर्थ है 'सीखना' अथवा व्यवहार परिवर्तन। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। बालक वातावरण में रहकर सीखता है। इस वातावरण में जो क्रियाएँ घटित होती हैं उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अधिगम है।
अधिगम की परिभाषाएँ-
(1) ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है - "व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है।"
(2) मार्गन और गिलीलैण्ड के अनुसार - "अधिगम, अनुभव के परिणामस्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन होते हैं, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है।"
क्रो और क्रो के अनुसार - "अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है।"
(3) थार्नडाइक के अनुसार - "अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है।"
गेट्स तथा अन्य के अनुसार - "अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होने वाले व्यावहारिक परिवर्तन को अधिगम (सीखना) कहते हैं।"
(4) क्रोनबैक के अनुसार - "अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम को व्यक्त करता है।"
(5) जे. पी. गिलफोर्ड के अनुसार - "व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।"
(6) वुडवर्थ के अनुसार - "अधिगम किसी नवीन क्रिया के करने में इस प्रतिबन्ध के साथ निहित है कि ऐसी नयी क्रिया पुनर्जीवित हों तथा बाद में घटित होने वाली क्रियाओं में प्रकट होती है।"
अधिगम की प्रक्रिया - अधिगम की क्रिया चेतन या अचेतन रूप में जीवन पर्यन्त चलती रहती है। व्यक्ति का विकास अधिगम प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इसका आधार है - परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना आवश्यक है।
गुथरी के अनुसार - "अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है।"
पील महोदय के अनुसार - "अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है।" पील महोदय ने अधिगम की प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया है-
(1) अधिगम द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं।
(2) अधिगम व्यक्ति की सहज स्वाभाविक क्रियाओं जैसे पलकें झपकाना, हाथ खींच लेना आदि से भिन्न है।
(3) अधिगम सामाजिक और जैविक अनुकूलन या चेतन उद्देश्य से हो सकता है।
(4) अधिगम व्यक्ति में सामाजिक या असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है।
(5) अधिगम त्रुटिरहित या त्रुटिपूर्ण हो सकता है।
मनोवैज्ञानिक बोआज ने कहा है - "अधिगम एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण, सामान्य जीवन की माँगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है।"
अधिगम प्रक्रिया की विशिष्टताएँ - अधिगम की परिभाषाओं में अधिगम को एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का स्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। यदि अधिगम की विशिष्ट प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाय तो अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित विशिष्टताएँ प्रकाशित होती हैं-
(1) अधिगम सार्वभौमिक है - अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सभी समयों और स्थानों में तथा सभी जीवों के द्वारा घटित होती रहती है। जहाँ प्राणी है, स्थान है व समय है वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्राणी प्रत्येक समय कुछ-न-कुछ क्रिया करता ही रहता है।
(2) अधिगम परिवर्तन है - बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अधिगम वह प्रक्रिया है, जिससे बालक में परिवर्तन परिलक्षित होंगे। अधिगम द्वारा परिवर्तन और पुनर्परिवर्तन की शृंखला चलती रहती है, जिससे बालक परिवर्तनों का परिणाम बन जाता है।
(3) अधिगम विकास है - बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील और संशोधन के रूप में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होता है। विकास के रूप में 'अधिगम दृष्टिगोचर होता है।
(4) अधिगम अनुकूलन है - अधिगम प्रक्रिया द्वारा बालक समाज व वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से इतनी सन्निकट हो जाती है कि हम अधिगम को अनुकूलन समझ लेते हैं। वास्तव में प्राणी को जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करना ही होता है। अतः जीवति रहने के लिए उसे अधिगम की प्रक्रिया करनी पड़ती है। गेट्स तथा अन्य ने अधिगम को अनुकूलन के रूप में स्वीकार किया है।
(5) अधिगम प्रयोजन पूर्ण है - अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजनपूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है।
(6) अधिगम निरन्तर है - अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता और न ही किसी काल विशेष तक सीमित रहता है, अपितु यह सतत आजीवन चलता रहता है।
(7) अधिगम रचनात्मक है - मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है, जिसे वह विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को स्वक्रिया के द्वारा अधिगम की ओर उन्मुख करती है।
(8) अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है - व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को पूर्णता के आधार पर परखकर उसके साथ समायोजन स्थापित करता है। व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए सही अनुक्रियाओं को सीखता रहता है। अतः अधिगम व्यक्ति की पूर्ण परिस्थिति के प्रति सही अनुक्रियाओं का प्रतिपादन है।
(9) अधिगम स्थानान्तरणीय है - व्यक्ति एक प्रकार की परिस्थिति में सीखे गये कौशलों अथवा समस्या के समाधानों का उपयोग मिलती-जुलती दूसरी परिस्थितियों में कर लेता है, अर्थात् अधिगम का स्थानान्तरण हो जाता है। इस प्रकार अधिगम स्थानान्तरणीय है।
(10) अधिगम प्रक्रिया है - मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिगम एक प्रक्रिया है, जो जीव और वातावरण के मध्य चलती रहती है। यह प्रक्रिया उत्तेजक-अनुक्रिया की दशाओं में आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, समायोजन में सफलता की प्राप्ति, व्यावहारिक परिवर्तन तथा सही व्यवहारों के स्थायीकरण में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में चार प्रमुख चरण होते है-
(i) आवश्यकता अथवा प्रयोजन - अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता अथवा प्रयोजन या प्रेरक उत्पन्न होता है। आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है, जो व्यक्ति को उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील बना देती है।
(ii) लक्ष्य - आवश्यकता लक्ष्य-उन्मुखी होती है जो व्यक्ति को एक लक्ष्य प्राप्त कर लेने तक क्रियाशील बनाये रखती है। लक्ष्य बोध के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती।
(iii) समायोजन - व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। वह बाधा भेदने के लिए अनेक प्रयास करता है, जिसमें बाधा भेदकर लक्ष्य प्राप्त कराने वाले प्रयास सफल प्रयास कहलाते हैं, शेष असफल प्रयास।
(iv) परिवर्तन - अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जो पहले के व्यवहार से भिन्न होता है या पहले से उसके व्यवहार में नहीं होता। यह परिवर्तन स्थायी होकर व्यक्ति के अर्जित व्यवहार का एक भाग बन जाता है यद्यपि इसमें भी परिवर्तन सम्भावित होता है। इसे सबलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं।
|
|||||