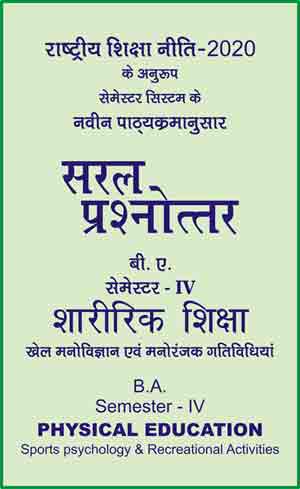|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 3
शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में मानव व्यवहार के मनो-सामाजिक पहलू
(Psycho-Sociological Aspects of Human Behaviour in Relation to Physical Education)
प्रश्न- मनो-सामाजिक पहलू का क्या अर्थ है? इसका मानव व्यवहार तथा शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए।
अथवा
एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त मनो-सामाजिक विकास की अवस्थाएँ बताइये।
उत्तर-
बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक एरिक एरिक्सन ने मनो-सामाजिक विकास सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। एरिक्सन के मनो-सामाजिक विकास सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन में विकास के आठ चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का सामना करना आवश्यक होता है। एरिक्सन का मानना था कि समस्या कोई संकट नहीं होती है बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला कारक होती है, व्यक्ति समस्या का जितनी सफलता से समाधान खोजता है। उसका उतना ही अधिक विकास होता है। एरिक्सन ने बचपन से वृद्धावस्था तक विकास के आठ चरण बताये हैं, जो निम्नलिखित हैं-
1. विश्वास बनाम अविश्वास - यह मनो-सामाजिक विकास का पहला चरण है। बालक इसका अनुभव एक वर्ष की आयु तक करता है। इसमें बच्चा अपने माता-पिता को देखकर स्नेह व प्रेम का अनुभव करता है जिससे उसमें विश्वास का भाव विकसित होता है। जब बच्चा अपने माता-पिता को अपने पास नहीं देखता है तो वह रोने लगता है इससे उसमें अविश्वास की भावना विकसित होती है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों का होना आवश्यक है। यदि बालक बचपन में विश्वास का अनुभव करता है तो उसमें संसार के प्रति अच्छे व सकारात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। जैसे- संसार रहने के लिए अच्छी जगह है आदि।
2. स्वायत्तता बनाम शर्म - एरिक एरिक्सन ने बताया कि विकास की यह अवस्था शैशवावस्था और बाल्यावस्था (1 से 3) के बीच की होती है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहना नहीं। चाहते हैं, वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य करना चाहते हैं। परन्तु बहुत से माता-पिता बालक को छोटे मोटे कार्य भी करने नहीं देते हैं उन्हें सदेह होता है कि बालक शायद यह न कर सके। कई बार तो वह बालक को डाँट तक देते हैं इससे बालक खुद अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है और लज्जा या संदेह की भावना का विकास बालक में होने लगता है।
3. पहल बनाम अपराध बोध - एरिक्सन के अनुसार, यह चरण बालक के विद्यालय जाने के प्रारम्भिक वर्ष में आता है इसमें बालक को प्रारम्भिक शैशवास्था की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में परिवार के सदस्य उसे छोटी-मोटी जिम्मेदारी जैसे- शारीरिक साफ-सफाई, खिलौनों को व्यवस्थित करना, पालतू पशुओं की देखरेख करने को कहते हैं। बालक यदि इन कार्यों को करने में असफल रहता है और परिवार के सदस्य बार-बार आदेश देते हैं तो वह असहज हो जाता है और उसमें अपराध बोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। एरिक्सन का मानना है कि, इस अपराध बोध की भावना को उपलब्धि बोध की भावना से समाप्त किया जा सकता है।
4. परिश्रम / उद्यम बनाम हीनभावना - एरिक्सन के अनुसार, विकास का यह चरण बाल्यावस्था के मध्य के वर्षों में होता है इसमें बालक अपने द्वारा की गयी पहल से नए अनुभवों के सम्पर्क में आता है और धीरे-धीरे वह अपनी ऊर्जा को नवीन पहल के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में खर्च करने लगता है। ऐसा माना जाता है कि बाल्यावस्था के अंतिम चरण में बालक कल्पना जगत में गोते लगाने लगता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है। परन्तु यदि बालक कल्पना को वास्तविक जगत से जोड़ने लगे तो उसमें हीन भावना अर्थात् अपने को अयोग्य समझने की भावना विकसित होने की सम्भावना होती है।
5. पहचान बनाम पहचान भ्रान्ति - एरिक्सन के अनुसार, यह चरण किशोरावस्था में प्रारम्भ होता है। विकास की इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा उथल-पुथल होती है। वह यह. जानना चाहता है कि उसकी अपनी पहचान क्या है, उसका समाज व परिवार से वास्तविक सम्बन्ध क्या है तथा उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह अपने आपको कई भूमिकाओं में देखता है तथा समायोजित करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में अभिभावकों को किशोरों की उन विभिन्न भूमिकाओं का पता लगाकर एक भूमिका या आवश्यक भूमिकाओं की पहचान करनी चाहिए यदि किशोर को सकारात्मक रास्ते की जानकारी न मिले तब उसमें पहचान भ्रान्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
6. आत्मीयता बनाम अलगाव - आत्मीयता बनाम अलगाव को एरिक्सन ने छठवां चरण बताया है। एरिक्सन के अनुसार, आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और (व्यक्ति में) खोजना पड़ता है। जब व्यक्ति की किसी के साथ मित्रता हो जाती है और आत्मीय सम्बन्ध बन जाते हैं तब उसके अन्दर आत्मीयता की भावना आ जाती है ऐसा न होने पर उसमें अलगाव की भावना विकसित हो जाती है।
7. उत्पादकता बनाम स्थिरता - एरिक्सन ने सातवें चरण को उत्पादकता बनाम स्थिरता का चरण कहा है जिसे मध्यवयस्कावस्था (Middle Adulthood) भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी अगली पीढ़ी की चिन्ता सताने लगती है और वह उसके कल्याण के लिए प्रयास करने लगता है तथा विकास के इस चरण में व्यक्ति समाज के लिए जननात्मक उत्पादकता के प्रति चिंतित होता है परन्तु यदि व्यक्ति में जननात्मक उत्पादकता की चिन्ता न उत्पन्न हो तो उसमें स्थिरता उत्पन्न होने लगती है।
8. सम्पूर्णता बनाम निराशा - एरिक्सन का मानना था कि, यह चरण मनो-सामाजिक विकास का अन्तिम चरण होता है जो वृद्धावस्था में आता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत की यादों को एक-दूसरे से जोड़ता है और सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है। दूसरी स्थिति में वह अपनी असफलताओं के कारण नकारात्मक सोच विकसित कर लेता है। सकारात्मक विचारों के पनपने से खुशी तथा नकारात्मक विचारों के पनपने से निराशा का भाव व्यक्ति में उत्पन्न होता है। यह सब उसकी अतीत की यादों तथा उपलब्धियों और असफलताओं के प्रति दृष्टिकोण की वजह से होता है।
शारीरिक शिक्षा का मनो-सामाजिक विकास की अवस्थाओं से सम्बन्ध
एरिक्सन का पहला मनो-सामाजिक चरण विश्वास बनाम अविश्वास है इस चरण में यदि माता-पिता बालक की उचित देखभाल करें तो बालक में परिवार तथा समाज के प्रति सकारात्मक दष्टिकोण विकसित हो सकता है। दूसरे चरण में बालक अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से स्वयं करना चाहता है वह अपने आप कपड़े पहनना, भोजन, करना, हाथ-पैर धोना आदि का प्रयास करता है। माता-पिता सकारात्मक सोच. के साथ यदि यह सब करने देते हैं और बालक को सहयोग देते हैं तो बालक छोटे-मोटे कार्यों को स्वयं करना सीख जाता है। बालक किसी कार्य को करने में अपने को असहज महसूस न करे इसके लिए उसे शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक नये अनुभवों के सम्पर्क में आता है। बालक नये अनुभवों को उचित प्रकार से सीख सके इसके लिए उसे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास में योगदान करती है। यदि बालक को उचित शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, व्यायाम, मनोरंजन का अवसर प्राप्त हो तो वह अपने जीवन के विभिन्न चरणों में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर पायेंगे। बालक में अविश्वास, शर्म, अपराध बोध, हीन-भावना, पहचान भ्रान्ति, अलगाव, स्थिरता तथा निराशा के स्थान पर विश्वास, स्वायत्तता, पहल, परिश्रम, पहचान, आत्मीयता, उत्पादकता तथा सम्पूर्णता का भाव उत्पन्न होगा जो उसे सफल जीवन व्यतीत करने में मदद करेगा।
|
|||||