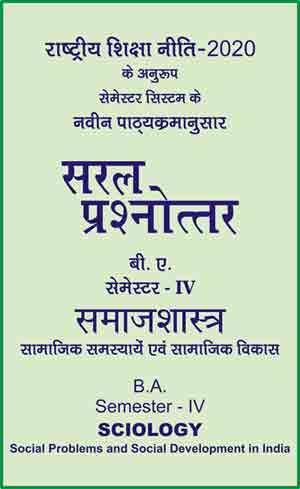|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 समाजशास्त्र बीए सेमेस्टर-4 समाजशास्त्रसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 समाजशास्त्र - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 22
विकास के सिद्धान्त
(Theories of Development)
विकास निरन्तरता का नियम है, यह नियम बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रारम्भ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यन्त निरन्तर चलती ही रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारम्भ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का सम्पूर्ण विकास इसी निरन्तरता के कारण भली-भाँति सम्पन्न होता रहता है। यद्यपि विकास तो बराबर होता रहता है, परन्तु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परन्तु बाद के वर्षों में यह मन्द पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारम्भ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है परन्तु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती।
इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं, वह सदा एकसमान नहीं रह पाती है। अर्थात् किसी भी अवस्था में एक जैसी नहीं रह पाती है।
इस नियम के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है।
विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अन्तर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में कुछ एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों में वृद्धि सिर की ओर से प्रारम्भ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
विकास की दिशा के नियम के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पूस्वामी के अनुसार क्रम से विकास लम्बवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियन्त्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टाँगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। क्रम के अनुसार विकास का क्रम केन्द्र से प्रारम्भ होता है, फिर बाहरी विकास होता है और इसके बाद सम्पूर्ण विकास। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों का तथा तत्पश्चात् इन सबका पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। बालक का विकास लम्बवत् सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालकों के इस विकास को मनोविज्ञान के अनुसार सिरापुछिय दिशा कहा जाता है। जिसके अनुसार पहले बालकों के सिर का उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। विकास व्यक्तिगत रूप से भी भिन्न-भिन्न होता है। दो व्यक्तियों में एकसमान विकास प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। जो व्यक्ति जन्म के समय लम्बा होता है, वह आगे जाकर भी लम्बा व्यक्ति ही बनेगा। एक ही उम्र के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएँ स्पष्ट देखी जा सकती हैं। व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, अर्थात् बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्तियों के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करने लगता है। उदाहरणार्थ- बालक पहले स्मृति स्तर में सीखता है फिर बोध स्तर पर और फिर अन्त में क्रिया करके सीखता है।
समान प्रतिमान के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति का विकास किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति या पशुओं का विकास अपनी - अपनी कुछ विशेषताओं के अनुसार होता है। इसी के अतिरिक्त व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुरूप भी होता है। अर्थात् जो भी गुण बालक के पिता या दादा में होते हैं, वही गुण उनके शिशुओं को भी मिलते हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लम्बाई ज्यादा होती है तो होने वाला बच्चा भी लम्बा ही होता है। इसके साथ ही व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है, अर्थात् पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी दिशा की ओर ही होगा। अतः यह बात इस प्रकार समझें कि बालक की शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे उनके सोचने, समझने, सीखने तथा पढ़ने का दायरा भी बढ़ता जाता है। इसी सिद्धान्त के अनुरूप बाल्यावस्था में शिशु की सीखने वाली चीजों के अध्ययनकर्ता तथा पुनर्बलन सिद्धान्त को देने वाले विचारक डोलार्ड और मिलर के अनुसार नवजात शिशु को स्तनपान कराकर उसकी भोजन आवश्यकता को हर बार पूरा नहीं किया जा सकता। बच्चे को अपनी भोजन व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक स्तनपान करने की आवश्यकता है जिसके लिए उसे अत्यधिक
संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। परिपक्वता एक ऐसा विकास सिद्धान्त है जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों को प्रभावित करता है।
|
|||||