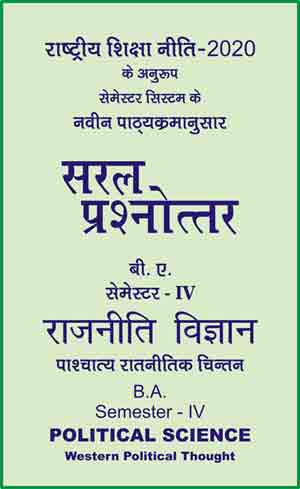|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 राजनीति विज्ञान बीए सेमेस्टर-4 राजनीति विज्ञानसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 राजनीति विज्ञान - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 11
जॉन ऑस्टिन
(John Austin)
जॉन ऑस्टिन - (परिचय)
जन्म 3 मार्च सन् 1990 ई० को इंग्लैंड के इप्सविच मानक स्थान में; माता-पिता के ज्येष्ठ पुत्र। जॉन सेना में भर्ती हुए और सन् 1812 ई० तक वहाँ रहे। फिर सन् 1818 ई० में वकील हुए और नारफोक सरकिट में प्रवेश किया।
जॉन ने सन् 1825 ई० में वकालत छोड़ दी, उसके बाद लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर वह न्यायशास्त्र के शिक्षक नियुक्त हुए। विधिशिक्षा की जर्मन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए वह जर्मन गए। वह अपने समय के बड़े ड़े विचारकों के संपर्क में आए जिनमें सविग्नी, मिटरमायर एवं श्लेगल भी थे। आस्टिन के विख्यात शिष्यों में जॉन स्टुअर्ट मिल थे। सन् 1832 ई० में उन्होंने अपनी पुस्तक 'प्राविस ऑव जरिसप्रूडेन्स डिटरमिंड' प्रकाशित की। सन् 1834 ई० में आसिटन ने इनर टेंपिल में न्यायशास्त्र के साधारण सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर व्याख्यान दिए। दिसम्बर, सन् 1659 ई० में अपने निवास स्थान बेब्रिज में मरे।
ऑस्टिन ने एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना की जो बाद में विश्लेषणीय संप्रदाय कहा जाने लगा। उनकी विधि संबंधी धारणा को कोई भी नाम दिया जाए, वह निस्संदेह विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान् व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित रहती है। उनका विचार था कि सम्पत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते। ऑस्टिन के मूल प्रकाशित व्याख्यान प्रायः भूले जा चुके थे जब सर हेनरी मेन ने, इनर टेंपिल में न्यायशास्त्र पर दिए गए अपने व्याख्यानों से उनके प्रति पुनः अभिरुचि पैदा की। मेन इस विचार के पोषक थे कि ऑस्टिन की देन के ही फलस्वरूप विधि का दार्शनिक रूप प्रकट हुआ, क्योंकि ऑसिटन ने विधि तथा नीति के भेद को पहचाना था और उन मनोभावों को समझाने का प्रयास किया था जिन पर कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, क्षति, दंड और प्रतिकार की धारणाएँ आधारित थी। ऑस्टिन ने राजसत्ता के सिद्धांत को भी जन्म दिया तथा स्वत्वधिकार के अंतर को समझाया।
संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का अर्थ
प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कलपना ही नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। राज्य के 4 अंगों में से सरकार और संप्रभुता को राज्य का आध्यात्मिक आधार माना जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता के विचार का यह अर्थ है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। सभी लोग तथा उनके संघ, राज्य के नियंत्रण के अधीन है। बाह्य क्षेत्र में संप्रभुता के विचार का अर्थ है कि राज्य का किसी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होना है। अधिनस्थ जातियों को राज्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें किसी अन्य राज्य की इच्छा के अनुसार रहना एवं कार्य करना पड़ता है। परंतु यदि कोई राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संधिया, समझौते का पालन करते हुए अपने कार्य की स्वतंत्रता पर सीमाओं को स्वीकार करें तो इसे उसकी संप्रभुता की क्षति या विनाश नहीं मानना चाहिए। उन्हें स्वारोपित प्रतिबंध समझाना चाहिए। चूंकि प्रभुसत्ता की संकल्पना प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता देती है, इसलिए प्रभुसत्ता एक असीम और स्थाई शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभुसत्ता का प्रयोग करते समय विवेक से काम नहीं लिया जाता या प्रचलित रीति-रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, न्याय या सामान्य हित के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसका अर्थ केवल यह है कि इन सब बातों का अर्थ लगाते समय प्रभु सत्ताधारी को किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह नहीं लेनी पड़ती। प्रभु सत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं यह निर्णय करता है कि न्याय क्या है, वह उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं। प्रभुसत्ता को 'निरंकुश शक्ति' (Arbitrary) मानना युक्ति संगत नहीं होगा।JW Garnar की Introduction to Political Science (राजनीति विज्ञान की रूपरेखा) के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। अन्य किसी की इच्छा से नहीं, कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। प्रभुसत्ताधारी Sovereign चाहे कोई मुकुट धारी नरेश ( crowned prince) हो, मुख्य कार्यकारी हो या कोई सभा (Assembly), वह केवल अपनी इच्छा से कानून की घोषणा कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और राजनीतिक निर्णय कर सकता है। ये कानून, आदेश और निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों या समूह और संगठनों के लिए बाध्यकर होते हैं। वास्तव में राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता (Supreme legal authority) के इस विचार को प्रभुसत्ता की संकल्पना के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के " Superanus" से हुई है जिसका अर्थ है 'सर्वोच्च सत्ता।' अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है।
संप्रभुता का सिद्धांत
ऑस्टिन की परिभाषा
यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का आदतन पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा पालन करने का आदी ना हो तो उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वह समाज राज्य है।
ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत मुख्य रूप से कानून की प्रकृति पर उनके विचार पर निर्भर करता है। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के निम्नानुसार हैं-
हर राजनीतिक समाज में सार्वभौमिक शक्ति जरूरी है। संप्रभुता व्यक्तियों का व्यक्ति या शरीर है। यह जरूरी नहीं है कि संप्रभु एक व्यक्ति होना चाहिए। कई लोगों में भी संप्रभुता रह सकती है। ऑस्टिन बताते हैं कि आधुनिक पश्चिमी दुनिया में एक व्यक्ति जरूरी नहीं है, वह शायद ही कभी है लेकिन उसके पास एक व्यक्ति के गुणों का निर्धारण करने के लिए बहुत अधिक गुण होने चाहिए। ऑस्टिन राज्य के लिए एक कानूनी आदेश है, जिसमें एक सर्वोच्च प्राधिकरण है, जो सभी शक्तियों का स्रोत है। संप्रभुता मनुष्य से चिंतित है, और प्रत्येक राज्य में मानव श्रेष्ठ होना चाहिए जो आदेश जारी कर सकता है और कानून बना सकता है।
सार्वभौमिक शक्ति अविभाज्य है। संप्रभुता का विज्ञान इसके विनाश की ओर जाता है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है।
संप्रभुता का आदेश सभी व्यक्तियों और संघों से बेहतर है। संप्रभु किसी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी इच्छा सर्वोच्च है। सही या गलत, सिर्फ अन्यायपूर्ण या कोई प्रश्न नहीं है, उसके सभी आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।
ऑस्टिन का सिद्धांत कहता है कि प्रभुत्व की आज्ञाकारिता आदत होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आज्ञाकारिता निरंतर होनी चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि आज्ञाकारिता पूरे समाज से आनी चाहिए। यह पर्याप्त है, अगर यह लोगों के बहुमत से आता है। आज्ञाकारिता समाज के थोक से आनी चाहिए अन्यथा कोई संप्रभुत नहीं है।
|
|||||