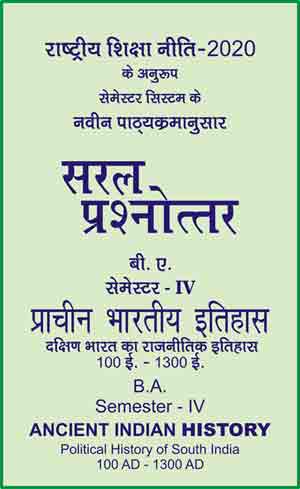|
प्राचीन भारतीय और पुरातत्व इतिहास >> बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृतिसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- पल्लवकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था तथा कला एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. कांची के पल्लव राजवंश के शासन प्रबन्ध का वर्णन कीजिए।
2. पल्लवों के शासन के समय में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति पर प्रकाश डालिए।
3. पल्लवों के शासनकाल में सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए।
4. पल्लव काल में वास्तुकला की शैलियों को बताइए।
5. पल्लव कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
पल्लवों का शासन प्रबन्ध
पल्लवों का शासन प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। उसकी शासन-प्रणाली मौर्यो और गुप्तों की शासन- प्रणाली के तत्वों से भरी पड़ी थी। प्रसिद्ध विद्वान ग्रोपालन ने अपनी पुस्तक 'काँची के पल्लवों का इतिहास' में बड़े ही सुन्दर लेख में लिखा है-
"वहाँ प्रशासन का एक ऐसा ढाँचा था जिसमें शीर्ष पर राजा तथा प्रान्तीय गवर्नर और विभिन्न विभागीय मंत्री, जो पार्कों, विभिन्न सार्वजनिक स्थान-गृहों, जंगलों आदि के अधिकारी होते थे, जो विस्तृत रूप से हमें मौर्य प्रशासन और कुछ मायनों में गुप्त प्रशासन की याद दिलाते थे।'
राजा - शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता था। राजा ही कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्यक्ष कहलाता था। राजा के अधीन ही अनेक मन्दिरों और विभागाध्यक्षों को नियुक्त करने का कार्य था। अपनी शक्ति और महत्ता को प्रदर्शित करता हुआ राजा अनेक उपाधियाँ धारण करता था। राजा ही युवराज की नियुक्ति करता था। राजा द्वारा नियुक्त युवराज राजा को प्रशासकीय कार्यों में मदद पहुँचाता था। इस काल के राजा और शासन प्रबन्ध के विषय में श्री नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है, "तथापि हम कह सकते हैं कि इस समय पल्लव प्रशासन ने और अधिक प्रगति की थी। राजा 'भटटारक' की अतिरिक्त पदवी धारण करता था। उत्तराधिकारी की 'युवरमहाराज' के रूप में मान्यता प्राप्त स्थिति थी और दूसरे राजकुमारों को भी राजकार्य में लगाये रखा जाता था।"
मंत्री - मंत्रियों का काम राजा को विशेष सलाह देना होता था जिसे 'रहस्यादिक' कहा जाता था। राजा मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य न था लेकिन अधिकांश पल्लव राजा मंत्रियों के परामर्श का सम्मान करते थे।
साम्राज्य विभाजन एवं विभिन्न क्षेत्रों का प्रशासन - सम्पूर्ण राज्य को राष्ट्रों में बाँटा गया था और 'राष्ट्र' में अनेक 'विषय' होते थे। एक विषय में बहुत से 'कोट्टम' और 'ग्राम' होते थे। राष्ट्रों में सामन्त शासन करते थे। 'विषय' के शासक को विषयिक कहा जाता था। 'कोट्टम' में 'देशान्तिक' का शासन होता था और ग्राम 'पिवत्र' के अधीन होता था।
स्वायत्त शासन - इस काल में स्वायत्त शासन-प्रणाली थी। ग्रामों में सभाएँ होती थीं। ग्राम सभाओं का कार्य भूमि की नाप करवाना, मुकदमों का निर्णय करना तथा सार्वजनिक कार्यों को पूर्ण करना होता था।
विभिन्न पदाधिकारी - हर जगह पर अनेक कर्मचारी नियुक्त किये गये थे। इन कर्मचारियों का अलग-अलग कार्य था। मण्डली नामक कर्मचारी राज्य-कर की वसूली करते थे। 'भूमिक' वन विभाग का अध्यक्ष होता था। 'तीर्थक' तालाबों और जलाशयों की देख-रेख करते थे।
सैन्य व्यवस्था - पल्लव राजा सदैव युद्ध करते रहते थे। इसलिए उन्होंने एक अच्छी सैन्य व्यवस्था की थी।
श्री नीलकान्त शास्त्री के अनुसार - "शक्तिशाली सैन्य और पुलिस संगठन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और मजदूरों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा सकता था।"
सामाजिक और आर्थिक स्थिति
पल्लव राज्य में वर्ण-व्यवस्था का सुचारु रूप से पालन किया जाता था। ब्राह्मणों का आदर- सम्मान किया जाता था लेकिन शूद्रों पर अत्याचार नहीं किया जाता था। साधारण लोग एक विवाह करते थे लेकिन बड़े-बड़े सामन्त एक से अधिक पत्नी भी रखते थे। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी ।
पल्लव राज्य में आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये गये। कृषि ही आय का मुख्य साधन था। व्यापार उन्नत दशा में था। कुछ उद्योग राज्य के अधिकार में थे।
श्री नीलकान्त शास्त्री के अनुसार - "नमक और कभी-कभी शक्कर के उत्पादन पर राज्य का पूर्ण अधिकार था और गाँव के लोगों को राजा के अधिकारियों का, जब कभी वे दौरे पर जाते थे, खर्च सहन करना पड़ता था।"
इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से पल्लव राज्य सुसम्पन्न था और यही कारण है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य और कीर्तिवर्मन ने पल्लवों को पराजित करके काँची से बहुत अधिक धन- सम्पत्ति प्राप्त की थी।
धार्मिक व्यवस्था
पल्लव वंश में हिन्दू धर्म ने बहुत उन्नति की। दक्षिणी भारत में भक्ति सम्प्रदाय पनप रहा था और दक्षिण का अनुकरण हो रहा था क्योंकि पल्लव नरेश धर्मानुरागी तथा सहिष्णु थे।
यद्यपि पल्लवकाल में हिन्दू धर्म का उत्थान हुआ लेकिन पल्लव राजाओं ने बौद्धों और जैनियों पर अत्याचार नहीं किये। ह्वेनसांग का वर्णन इस बात का गवाह है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे। पल्लव नरेश को विद्या से अत्यधिक प्रेम था। पल्लव नरेश महेन्द्रवर्मन प्रथम स्वयं एक उच्चकोटि का विद्वान था और उसने 'मित्तविलासप्रहसन नामक ग्रन्थ की रचना की थी। श्री गोपाल ने अपनी पुस्तक 'काँची के पल्लवों का इतिहास' में लिखा है कि पल्लवों की राजसभा में भास और शूद्रक के नाटकों का अभिनय किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान और किरातार्जुनीयम का रचयिता भारवि पल्लव नरेश सिंहविष्णु के राज्याश्रय में रहता था। इस युग में कई अभिलेखों की प्राप्ति हुई जो संस्कृत भाषा में लिखे थे। उनमें उच्चकोटि की भाषा का प्रयोग किया गया है। अभिलेख में संस्कृत के साथ तमिल का भी विकास हुआ। इस काल में ही 'तमील 'कुरल' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की गयी।
कला एवं संस्कृति
स्थापत्य और शिल्प कला के क्षेत्र में इस युग में महान उन्नति हुई। श्री नीलकान्त शास्त्री के अनुसार, "उनका स्थापत्य और शिल्प दक्षिण भारतीय कला के इतिहास का अत्यन्त वैभवशाली अध्याय है।'
पल्लव काल में वास्तुकला शनैः-शनैः काष्ठ कला और कन्दरा कला के प्रभाव से मुक्त हुई। प्रसिद्ध विद्वान वाशम के अनुसार, "दोनों ही शैलियाँ यह प्रदर्शित करती हैं कि उनके स्थापत्य को काष्ठ कला और कन्दरा कला की रितियों से शनैः-शनैः मुक्ति प्राप्त हुई।'
पल्लव काल में वास्तुकला की निम्नलिखित चार प्रमुख शैलियों का विकास हुआ-
1. महेन्द्रवर्मन प्रथम शैली - इस शैली का विकास 610 ई. से 640 ई. तक हुआ। यह पल्लव कला की प्रारम्भिक शैली है। इस शैली में महेन्द्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में निर्मित स्तम्भयुक्त मण्डपों का निर्माण हुआ। महेन्द्रवर्मन प्रथम के पश्चात् भी इस शैली का धीरे-धीरे विकास होता रहा है।
2. मामल्ल शैली - मामल्लपुरम् में इस शैली का विकास हुआ। इसका काल 640 ई. से 674 ई. तक माना जाता है। मामल्लपुरम् नामक नगर जो समुद्र तट पर स्थित था, इसकी स्थापना पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। इस शैली में निर्मित रथों को सप्तपैगोडा के नाम से पुकारा जाता है। कुल आठ रथ प्राप्त हुए हैं, जो सभी सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के हैं। ये रथ निम्नलिखित हैं- (i) द्रौपीद रथ, (ii) धर्मराज रथ, (iii) अर्जुन रथ, (iv) भीम रथ, (v) सहदेव रथ, (vi) पिंडारि रथ, (vii) गनेश रथ, (viii) वलैयकुट्टैथ रथ ।
इन रथों के विभिन्न नामों में काष्ठ कला का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। ये सभी रथ स्थापत्य की दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय हैं।
3. राजसिंह शैली - इस शैली का विकास 674 ई. से लेकर 800 ई. तक हुआ। यह काष्ठ कला से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। मामल्लपुरम् में बना हुआ "शोर मन्दिर" इस शैली का अत्यन्त सुन्दर नमूना है।
काँची के कैलाश मन्दिर में राजसिंह शैली के विकसित रूप के दर्शन होते हैं। इसका निर्माण पल्लव राजा जयसिंह के काल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राजसिंह के शासनकाल में कुछ समय पश्चात् गर्भगृह और मण्डप को जोड़ने के लिए अन्तराल का निर्माण कर दिया गया था।
पल्लव कला की सभी विशेषताएँ तथा मण्डप के सुदृढ़ स्तम्भ शिखरं, चहारदीवारी, सिंह स्तम्भ, छोटे-छोटे अलंकृत कक्ष आदि इस मन्दिर में दिखाई देते हैं। नीलकान्त शास्त्री के अनुसार, "इस मन्दिर में पल्लव शैली की प्रमुख विशेषताएँ अत्यन्त मोहक रूप में एकत्रित की गयी हैं।'
इस शैली का विकसित रूप काँची में बने हुए 'बैकुण्ठ पेरुमल' के मन्दिर में देखने को मिलता है। इस मन्दिर का गर्भगृह, मण्डप, प्रवेश द्वार सभी एक-दूसरे से पूर्ण रूप से सम्बद्ध हैं।
4. नन्दिवर्मन शैली - इस शैली का विकास 800 से 900 ई. तक हुआ। इस शैली के अन्तर्गत अपेक्षाकृत छोटे मन्दिरों का निर्माण हुआ। इसके उदाहरण काञ्ची के मुक्तेश्वर एवं मातंगेश्वर मन्दिर, ओरगडम् का वङ्मल्लिश्वर मन्दिर, तिरुत्तैन का वीरट्टानेश्वर मन्दिर आदि हैं। इनके प्रवेश द्वार पर स्तम्भयुक्त मण्डप बनाये गये हैं।
|
|||||