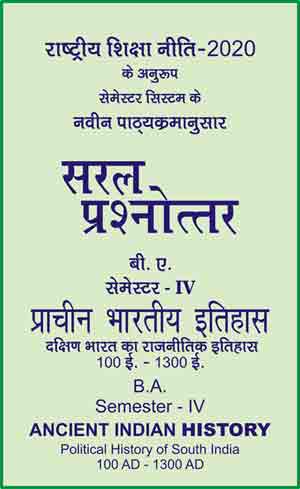|
प्राचीन भारतीय और पुरातत्व इतिहास >> बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृतिसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- दक्षिण-पूर्व एशिया की प्राग् भारतीय संस्कृति के बारे में आप क्या जानते है?
अथवा
दक्षिण-पूर्व एशिया की संस्कृति पाण्डुलिपियों की विषय-वस्तु के बारे में 'बताइए।
उत्तर-
प्रारम्भ में ऐसी धारणा थी कि दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रारम्भिक निवासी अत्यन्त अविकसित तथा बर्बर थे। फूनान के निवासियों को सर्वप्रथम वस्त्र धारण करने की शिक्षा कौण्डिण्य ने दी थी। किन्तु नित - नूतन आविष्कारों एवं अनुसंधानों के परिणामस्वरूप उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में परम्परित विचारों में परिवर्तन आवश्यक हो गया। पुनश्च, किसी देश अथवा जाति के इतिहास का अनुशीलन स्वतन्त्र रूप से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बाह्य प्रभावों के अलावा भी प्रत्येक देश के स्थानीय सांस्कृतिक तत्व अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया की प्राक् - हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति का परिज्ञान तीन साधनों से होता है। इस दृष्टि से प्रथमतः पुरातात्त्विक साक्ष्य विचारणीय हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न भागों से पुरा, मध्य एवं नवपाषाणकालीन मनुष्यों तथा उनके उपकरणों एवं उपभोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इस प्रसंग में बृहत्पाषाण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु इससे केवल उनके भौतिक पक्ष का ही ज्ञान हो पाता है। द्वितीय साक्ष्य भाषा सम्बन्धी हैं। इनकी उपादेयता पर कर्न आदि विद्वानों ने विशेष बल दिया है। इनके अनुसार इण्डोनेशिया की विभिन्न भाषाओं के अनेक उभयनिष्ठ शब्द दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रारम्भिक भाषा से उत्पन्न हैं। किन्तु मजूमदार आदि विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं। आपकी धारणा है कि ऐसे बहुत से शब्द, जिन्हें, प्रारम्भिक भाषा से सम्बन्धित किया जाता है, देशज न होकर विदेशी भी हो सकते हैं, क्योंकि भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान भाषा - विज्ञान की सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। तृतीय प्रमाण के रूप में आदिम जनजातियों की जीवन-पद्धति का उल्लेख किया जा सकता है, जो आज भी आदिम परम्पराओं को संजोए अर्द्धविकसित अवस्था में है। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया की आदिम संस्कृति स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होती है।
दक्षिण-पूर्व एशिया के प्राचीनतम मानव-प्राणी जावा मानव तथा पेंकिग मानव थे। दोनों मानव प्रजातियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया की ही नहीं, अपितु विश्व की प्राचीनतम मानव प्रजातियाँ हैं। इनसे थोड़ी विकसित मानव प्रजाति सोलो मानव थी, जिसके अवशेष न्गाण्डंग से सोलो नदी की उपत्यका से संगृहीत किये गये हैं। ये तीनों मानव प्रजातियाँ पूर्ण मानव प्रजातियाँ नहीं हैं। इन्हें मानवाभ वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है। इनका सम्बन्ध पुरापाषाकाल से था। दक्षिण-पूर्व एशिया का प्राचीनतम पूर्ण मानव वादजाक मानव है, जिसका सम्बन्ध परवर्ती प्लीस्टोसीन पीरियड अथवा उत्तर प्लीस्टोसीन पीरियड से था। इसी से मिलते-जुलते एक अन्य मानव के अवशेष आस्ट्रेलिया में मिले थे, जिसे कीलर मानव कहा गया। वादजाक कीलर मानव को दक्षिण-पूर्व एशिया की अनेक प्रजातियों का पूर्वज माना गया है। इनमें आस्ट्रोलायड, नेग्रिटो, मेलानेसायड तथा इण्डोनेशियन अथवा आस्ट्रो- नेशियन का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में सर्वप्रथम पूर्णतया प्रसार आस्ट्रोलायड प्रजाति का ही हुआ। इस वर्ग के मनुष्य आज भी सिनोई तथा सकाई की पर्वतीय जातियों में दिखायी पड़ते हैं। आस्ट्रोलायड से मिलती-जुलती एक अन्य प्रजाति का अस्तित्व भी मिलता है। इसे ' वेड्डायड नाम दिया गया है। इसके अस्तित्व आज भी सेलिबीज के दक्षिणी भाग इन्गानो तथा मेण्टाबाँयी प्रायद्वीपों में देखे जा सकते हैं। नेग्रिटो वर्ग के मनुष्य आज मलाया में सेमंग नामक संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। मेलानेसायड की प्रतिनिधि जाति अब नहीं मिलती। इन तीनों प्रजातियों का सम्बन्ध मध्यपाषाण काल से था। ये लघुपाषाणोपकरणों का प्रयोग करते थे। इनके प्रमुख उपकरण 'फिशिंग टैकिल' तथा 'डग आउट कैनो विद पैडिल' थे। उत्तरी वियतनाम की गुफाओं से एक विशेष प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिन्हें इनके प्राप्ति स्थल के आधार पर बैक्सोनियन तथा होवियन नाम दिया गया है। इनके एक ओर ही धार होती थी। इन उपकरणों के साथ कुछ अस्थि अवशेष तथा मृद्भाण्ड भी मिले हैं। मध्यपाषाणकालीन मनुष्यों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना तथा मछली मारना था।
वादजाक की वंश-परम्परा की चतुर्थ प्रजाति इण्डोनेशियन अथवा आस्ट्रोनेशियन था। इनके आगमन से दक्षिण-पूर्व एशिया में नवपाषाण युग का आविर्भाव हुआ। इस वर्ग के मनुष्य 2500 से 1500 ई. पू० के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में विद्यमान थे। इन्हें आद्य-मलय तथा ड्युटेरो - मलय नामक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। मलय प्रजाति की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसका सम्बन्ध भारत की आदिवासी मुण्डा, खस तथा संथाल प्रजातियों की भाषाओं से है। इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जर्मन विद्वान् पैंटर श्मिट ने किया था। श्मिट ने आगे चलकर आस्ट्रोनेशियन वर्ग को आस्ट्रोएशियाटिक वर्ग से सम्बन्धित कर आस्ट्रिक नामक एक बृहत् क्षेत्र की कल्पना की, जिसके अन्तर्गत इण्डोचीन तथा इण्डोनेशिया के आदि निवासियों के साथ-साथ भारत की आदिम खस, मुण्ड तथा संथाली जातियों को भी सम्मिलित किया गया। इस आधार पर श्मिट ने प्रस्तावित किया कि मलय प्रजाति का मूल निवास स्थान भारत था और यहीं से इस वर्ग के मनुष्य दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर बढ़े थे। जिस प्रकार ईसा की प्रथम एवं द्वितीय शती में उपनिवेशन के लिए भारतवासियों का प्रवाह दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व की ओर हुआ था, उसी प्रकार का एक प्रवाह सुदूर अतीत में भी हुआ था। श्मिट को प्रिज्युलुस्की, लेवी, ब्लाख इत्यादि विद्वानों के समर्थन से बड़ा बल मिला। श्मिट के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए फ्राँसीसी विद्वानों ने प्रस्तावित किया कि आर्यागमन के पूर्व भारत में रहने वाली उक्त मुण्ड खस तथा संथाल प्रजातियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न प्रदेशों में ही नहीं, अपितु दक्षिण में मेडागास्कर तक पहुँची। आर्यों के आगमन से इसे और बल मिला। क्योंकि उस स्थिति में इनके लिए अपनी मातृभूमि में रहना कठिन हो गया। किन्तु अनेक विद्वान् इस मत से सहमत नहीं हैं। डच विद्वान् क्रोम तो हार्नेल्स से सहमत होते हुए प्रस्तावित करते हैं कि सबसे पहले हिन्द- चीनियों ने भारत में उपनिवेश स्थापित किया उसके बाद आर्यों ने इस ओर प्रस्थान किया। मिड्ट के भाषाशास्त्रीय सिद्धान्त का निराकरण जी0 द हेव्से ने भी किया, जो आस्ट्रो-एशियाटिक भाषिक परिवार का अस्तित्व ही नहीं मानते।
इण्डोनेशियन वर्ग के मनुष्य कुठार, बसूल तथा सेल्ट जैसे उपकरणों का प्रयोग करते थे। इनमें चतुष्कोणीय बसूला, आयताकार कुठार तथा स्कन्धित कुठार का विशेष प्रचलन था। विद्वानों की धारणा है कि चतुष्कोणीय कुठार का केन्द्र जावा था। ये एक प्रकार के पालिशदार उपकरण थे, जिन पर उच्चकोटि की कलाकारिता प्रदर्शित थीं। उपकरणों के साथ-साथ इस युग में उत्तम कोटि के मृद्भाण्डों का निर्माण भी किया जाता था। दक्षिण-पूर्व एशिया में मृद्भाण्डों की लोकप्रियता सर्वप्रथम इसी युग में बढ़ी थी। नवपाषाण युग के आगमन के साथ-साथ यहाँ कृषि कर्म का भी पूर्णतया प्रचलन हुआ। चावल, गन्ना, नारियल तथा केले का उत्पादन किया जाने लगा। कृषि कर्म की दो विधियाँ थीं। प्रथम विधि को इण्डोनेशिया भाषा में लदंग विधि कहा गया है। यह एक प्रकार की अस्थायी कृषि थी, जिसमें एक स्थान पर एक बार फसल लेने के बाद उसे छोड़ दिया जाता था तथा खेती के लिए नयी भूमि खोज ली जाती थी। द्वितीय सवह विधि कही गयी है। इसमें उसी कृषि योग्य भूमि पर बार-बार कृषि की जाती थी। खाद्य के रूप में प्रयोग करने के साथ-साथ अन्न से एक प्रकार की मदिरा भी बनायी जाती थी। कृषि कर्म का विकास अवश्य हो गया था किन्तु शिकार करने तथा मछली मारने का धन्धा अभी भी प्रचलित था। कृषि के साथ-साथ पशुपालन का प्रचलन भी था। मुख्यतः भैंस तथा सुअर पालते थे। वस्त्र-निर्माण करना भी जान गये थे।
इन आविष्कारों के फलस्वरूप स्थायी जीवन को प्रोत्साहन मिला तथा सामाजिक संस्थाएँ अस्तित्त्व में आने लगीं। पारिवारिक गठन मातृसत्तात्कमक था तथा कुल का नामकरण माता के नाम के आधार पर किया जाता था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। बृहत्पाषाणों तथा उनके समीप प्राप्त अन्यान्य उपकरणों से उनकी धार्मिक मान्यताओं के विषय में भी कुछ जानकारी मिलती है। प्राचीन विश्व की अन्य जातियों के समान वे भी पारलौकिक जीवन के प्रति आस्थावान थे। वे आत्मतत्त्ववादी थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा विद्यमान रहती है। इसीलिए वे पर्वत, नदी, वृक्ष यहाँ तक कि चावल के पौधों की भी उपासना करते थे। पितृ - उपासना भी प्रचलित थी। समाज में पुरोहिती प्रथा का विकास हो चुका था। वे ही परम्परागत विधि-विधानों (आदत) तथा समाज के रक्षक थे। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें साधारण ज्योतिष, एक हजार तक की संख्या की - गणना तथा सामुद्रिक यात्राओं का ज्ञान था।
दक्षिण-पूर्व एशिया में नवपाषाणकालीन सभ्यता लगभग 1500 से 300 ई. पू0 तक विद्यमान रही। इसके बाद यहाँ धातु का आविष्कार हुआ यद्यपि पालिशदार उपकरणों का प्रयोग अभी भी जारी रहा। काँस्य एवं लौह मिश्रित यह संस्कृति 'डांगसोग संस्कृति' के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसके काँस्य उपकरण सर्वप्रथम टोंकिन में डांगसोग ग्राम से प्राप्त हुए थे। डांगसोग संस्कृति की प्रसिद्धि ताशा के निर्माण के कारण विशेष हैं। इसके निर्माण का उद्देश्य धार्मिक था। ताशा के साथ-साथ इस संस्कृति के लोग नौका-निर्माण तथा नौचालन में भी निष्णात थे। इन्हें ज्योतिष का भी कुछ ज्ञान था। इस युग में निर्मित वृहत्पाषाणों में मेनहिर तथा डालमेन विशेष प्रसिद्ध हैं।
उक्त समीक्षा से स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रारम्भिक निवासी कृषि, पशुपालन, नौका-निर्माण, वस्त्र-निर्माण तथा थोड़ा-बहुत ज्योतिष के ज्ञान को छोड़कर सामान्यतः अर्धविकसित अवस्था में ही थे। किन्तु, अधिकांश विद्वान् इससे सहमत नहीं है। सेद की धारण है कि भारतीयों के आगमन के पूर्व दक्षिण-पूर्व एशिया के निवासी कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर चुके थे। उदाहरणार्थ, भौतिक क्षेत्र में वे चावल की स्थायी कृषि करते थे, बैल तथा भैंस पालते थे, धातु के प्रयोग से परिचित थे तथा नौविद्या में निष्णात थे। उनमें सामाजिक संस्थाओं के विकास की प्रवृत्ति जागृत हो गयी थी। स्त्रियों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला था तथा वंश का निर्धारण मातृपक्ष के आधार पर किया जाता था। धार्मिक दृष्टि से वे सर्वचेतनवादी थे। ऊँचे स्थानों पर पूजागृहों की स्थापना तथा पूर्वजों एवं मृत्तिका देवताओं की उपासना करते थे। कलश में अस्थि अवशेष को रखकर समाधीकरण की विधि प्रचलित थी तथा एक प्रकार का द्वैतवाद विकसित था।
क्रोम की धारणा है कि भारतीयों के आगमन के पूर्व जावा के प्राचीन निवासी इनके साथ-साथ 'वयंग', जो एक प्रकार का छाया नाटक था, गैमलेन आस्केस्ट्रा तथा बटिक, जो एक विशेष प्रकार का वस्त्र था, से भी परिचित थे। कुछ विद्वान् इसके साथ-साथ कृत्रिम कृषि, माप-विद्या, मुद्रा - शास्त्र तथा राज्य-सिद्धान्त के अस्तित्व को जोड़कर प्राक् - हिन्दू जावानी सभ्यता की उत्कृष्टता की बात करते हैं। इस प्रकार की धारणा का बहुत कुछ आधार भाषाशास्त्र है। किन्तु ध्यातव्य है कि भाषाशास्त्र का आधार ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। वास्तव में अन्य साक्ष्यों से केवल धातु - ज्ञान, सामुद्रिक ज्ञान तथा ज्योतिष की जानकारी का ही समर्थन मिलता है, शेष का नहीं। उदाहरणार्थ, जावा में वयंग के अस्तित्व के प्रमाण 9वीं या 10वीं शती ई. के पूर्व नहीं मिलते, जबकि भारत में इससे बहुत पहले इसका प्रचलन था। अतः सम्भव है यह परम्परा भारत से ही गयी हो। इसी प्रकार प्राक - हिन्दू युग की एक भी मुद्रा यहाँ से नहीं मिली है। इसी प्रकार अन्य उपलब्धियों के समर्थन में भी अकाट्य प्रमाण नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जावा की उक्त सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्वीकार करना उचित नहीं हैं। वेल्स दक्षिण-पूर्व एशिया को सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में बाँटते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में वर्मा, मध्य स्याम, मलाया तथा सुमात्रा की गणना की जाती है, जिनकी प्रारम्भिक संस्कृति उन्नतशील नहीं थी और उस पर पूर्णतया भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ गया। इसके विपरीत पूर्वी क्षेत्र की, जिसमें जावा, कम्बुज तथा चम्पा को रखा गया है, प्रारम्भिक संस्कृति बहुत विकसित थी। फलतः भारतीयकरण के बावजूद भी उनके स्थानीय तत्त्व विनष्ट नहीं हुए। किन्तु वेल्स के क्षेत्रीय विभाजन के सिद्धान्त का आर. सी. मजूमदार ने यौक्तिक निराकरण किया है।
|
|||||