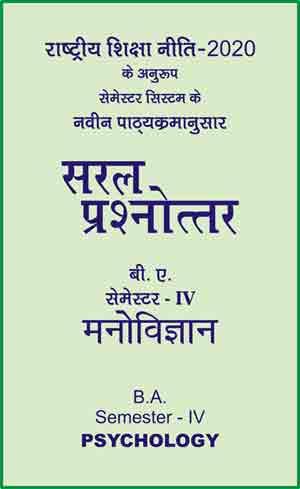|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञानसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 5
मनोविदलिता
(Schizophrenia)
प्रश्न- मनोविदलता से आप क्या समझते हैं? इसके लक्षणों और कारणों की विवेचना कीजिए।
अथवा
मनोविदलता से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य लक्षणों एवं कारणों का वर्णन करें।
अथवा
सीजोफ्रेनिया (मनोविदलता) के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसका उपचार कहाँ तक संभव है?
अथवा
मनोविदलता के लक्षणों एवं कारणों पर प्रकाश डालिए।
अथवा
मनोविदलता क्या है? मनोविदलता के कारणों पर प्रकाश डालिये।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. मनोविदलता के सामान्य लक्षण।
2. मनोविदलता के प्रमुख लक्षण बताइये।
3. व्यामोह (Delusion)।
4. विभ्रम (Hallucination)|
5. विभ्रम व्यामोह से किस प्रकार भिन्न है?
6. मनोपेशीय लक्षण (Psychomoter Symptoms) टिप्पणी लिखिए।
7. क्रियात्मक व्यवहार से सम्बन्धित लक्षणों को बताइये।
8. मनोविदलता के कारण तथा उपचार की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
मनोविदलता को लैटिन भाषा में Dementia Praecox कहते हैं। इस नाम का उपयोग जर्मन मनोचिकित्सक क्रेपलिन (Kraepelin) ने किया। क्रेपलिन के अनुसार यह रोग बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में होता है। क्रेपलिन का यह विचार भी था कि मनोविदलता में मानसिक शक्तियों का ह्रास स्थायी रूप से नहीं होता है।
कोलमैन (1964) के अनुसार - "मनोविदलता वह विवरणात्मक पद है जिसमें मनोविक्षिप्तता से सम्बन्धित कई विकारों का बोध होता है। इसमें बड़े पैमाने पर वास्तविकता की तोड़-मरोड दिखाई देती है। रोगी सामाजिक अन्तः क्रियाओं से पलायन करता है। व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण विचार और संवेग अपूर्ण और विघटित रूप में होते हैं।"
(Clinical Symptoms of Schizophrenia)
मनोविदलता के नैदानिक लक्षणों को निम्नलिखित तीन भागों में बाँट सकते हैं-
1. धनात्मक लक्षण (Positive Symptoms) - धनात्मक लक्षणों से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है जिसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक बहुलता दिखाता है। इसमें प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-
(i) व्यामोह (Delusion ) - व्यामोह से तात्पर्य एक ऐसे गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने के तथ्य उपस्थित होने के बावजूद भी व्यक्ति उन्हें गलत स्वीकार नहीं करता है। मनोविदलता के कुछ रोगियों में एक ही व्यामोह प्रबल होता है, परन्तु कुछ रोगियों में एक से अधिक व्यामोह स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं।
(ii) विभ्रम (Hallucination) - किसी बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाले प्रत्यक्षण को विभ्रम कहते हैं। मनोविदलता के रोगी में यह प्रायः पाया जाता है। मनोविदलता के रोगी में सबसे प्रमुख विभ्रम श्रवण का विभ्रम होता है।
(iii) विघटित चिंतन तथा संभाषण (Disorganized Thinking and Speech) - मनोविदलता के रोगी का चिंतन तथा संभाषण बहुत ही विघटित होता है। विघटित संभाषण से तात्पर्य ऐसे संभाषण से है जिसमें रोगी के विचारों के मध्य साहचर्य नहीं होता है तथा रोगी का विचार एक विषय से दूसरे विषय पर इतना तेजी से परिवर्तित होता है कि सुनने वाला व्यक्ति कोई अर्थ ही नहीं निकाल पाता है। रोगी में औपचारिक चिंतन विकृति भी होती है। वह इसकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से करता है-
(i) संतनन (Perseverating ) - इसमें रोगी अपने शब्दों तथा वाक्यों को बार-बार कहता है या दोहराता है।
(ii) तुकान्त ( Rhyme ) - कभी-कभी रोगी अपनी चिंतन की अभिव्यक्ति तुकान्त शब्दों तथा वाक्यों के माध्यम से करता है।
2. ऋणात्मक लक्षण (Negative Symptoms) - ऋणात्मक लक्षणों से तात्पर्य उन लक्षणों से है जिसमें रोग सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी से होता है, जो निम्नलिखित हैं-
(i) इच्छाशक्ति की क्षुब्धता (Disturbance in Volition) - मनोविदलता के रोगी की अपनी विकृत दुनिया होती है, इस कारण इनकी इच्छाशक्ति में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं।
(ii) संभाषण की कमी (Poverty of Speech) - संभाषण में कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं, जैसे रोगी किसी प्रश्न का उत्तर देने के पहले बहुत देर चुप रहता है या कम से कम शब्दों में उत्तर देता है या कभी-कभी वह उत्तर देता ही नहीं है।
3. मनोपेशीय लक्षण (Psychomotor Symptoms) - उनके द्वारा किये गये व्यवहार के हाव-भाव, गति तथा दिशा काफी मनोविदलता के रोगियों के मनोविदलता के रोगियों में विस्मयपूर्ण तथा हास्यास्पद होती है। ऐसे लक्षणों का स्वरूप पुनरावृत्तिक होता है। कभी-कभी मनोविदलता के मनोपेशीय लक्षण एक अन्य प्रारूप ले लेते हैं, जिसे कैटेटोनिया कहते हैं। इसमें निम्नलिखित श्रेणियों आती हैं-
(i) कैटेटोनिक दृढ़ता (Catatonic Rigidity) - कैटेटोनिक दृढ़ता में रोगी घंटों तक एक दृढ़ मुद्रा बनाये रखता है और वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नापसंद करता है।
(ii) कैटेटोनिक स्टूपर (Catatonic Stuper) - इसमें रोगी पर्यावरण के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञता तथा अनुक्रियाहीनता दिखाता है, जिस कारण वह लम्बे समय तक गतिहीन एवं खामोशी की अवस्था में रहता है।
(Causes of Schizophrenia)
1. जैविक कारक
(i) आनुवांशिकता
(ii) जैव-रासायनिक कारक
(iii) न्यूरोफिजियोलाजिकल कारक
2. मनोवैज्ञानिक कारक
(i) प्रारम्भिक जीवन में मनोघात
(ii) दोषपूर्ण संरक्षक-पुत्र तथा पारिवारिक अन्तः क्रियाएँ
(iii) सामाजिक भूमिका सम्बन्धी समस्याएँ
(iv) तीव्र प्रतिबल
(v) दोषपूर्ण सीखना।
3. सामाजिक-सांस्कृतिक कारक - व्यक्ति के सामाजिक वर्ग का भी प्रभाव मनोविदलता पर पड़ता है। अध्ययनों में पाया गया है कि जब उस व्यक्ति का सामाजिक वर्ग निम्न होता है तब मनोविदलता के उत्पन्न होने का प्रतिशत अधिक होता है। यह संबंध बड़े शहरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों के बीच यह सम्बन्ध अस्पष्ट होता है।
(Treatment of Schizophrenia)
आरम्भ में मनोविदलता का उपचार काफी कठिन तथा कुण्ठा से भरा हुआ था। पुरानी उपचार विधि अपने-आप अप्रभावी बन गयी और धीरे-धीरे कई नयी उपचार पद्धतियों ने उसकी जगह ले ली, जिनका वर्णन निम्नलिखित हैं-
1. मनोविक्षिप्ति विरोधी औषधि (Antipsychotic Drug) - ब्रेसलीन (1992) तथा विनवर्गन (1991) के अनुसार मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि का आविष्कार होने से मनोविदलता के उपचार में नयी क्रान्ति आयी। क्लोरप्रोमाजिन (Chlorpromazine) सबसे पहली औषधि है जो हिस्टामाइन विरोधी औषधि समूह की है। इसकी खोज के बाद कई अन्य प्रकार की औषधियों का आविष्कार हुआ, जिससे मनोविदलता का सफलतापूर्वक उपचार किया जाने लगा। इन्हें एक साथ न्यूरोलेपटिक औषधि (Neuroleptic drug) कहते हैं, क्योंकि इन्हें लेने से रोगी में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह तंत्रिका रोग के लक्षण के समान होता है। इस मानसिक रोग का उपचार करने के लिए निम्नलिखित औषधियों का व्यवहार किया जाता है-
(i) थियोरिडाजिन (Thioridazine)
(ii) मेसोरिडाजिन (Mesoridazine)
(iii) फ्लूफेनाजिन (Fluphenazine)
(iv) ट्रिफ्लूपेराजिन (Trifluoperazine)
2. मनश्चिकित्सा (Psychotheraphy) - इस रोग के उपचार में मनश्चिकित्सा के निम्नलिखित प्रकारों का प्रयोग करते हैं-
(i) सूझ चिकित्सा (Insight Theraphy ) - मनोविदलता के उपचार में विभिन्न प्रकार की सूझ चिकित्साओं का प्रयोग करते हैं। शोधों से स्पष्ट हुआ है कि सूझ चिकित्सक, जिन्हें मनोविदलता के रोगियों के उपचार का पर्याप्त अनुभव है, उन्हें सफलता अधिक मिलती है।
(ii) पारिवारिक चिकित्सा (Family Theraphy) - मनोविदलता के रोगी के सफल उपचार के बाद उसे मानसिक अस्पताल से निकलकर परिवार में पुनः जाना पड़ता है, जहाँ उसे परिवार के सदस्यों के साथ अन्तः क्रिया करनी पडती है।
3. सामुदायिक चिकित्सा (Community Approach) - सामुदायिक चिकित्सा के अन्तर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर अधिक बल डाला गया है-
(i) समन्वित सेवा (Coordinated Services) - इसके तहत 50,000 से 2,00,000 लाख की आबादी पर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करते हैं।
(ii) आंशिक अस्पतालीकरण (Partial Hospitalization) - इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरूआत मॉस्को (Moscow ) में 1944 में हुई तथा उसकी सफलता को देखकर फिर इसे अन्य देशों, जैसे इंग्लैण्ड, कनाडा, अमेरिका में भी अपनाया गया। अमेरिका में इसे सामुदायिक उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाया गया।
(iii) लघुकालीन अस्पतालीकरण (Short-term Hospitalization ) - जब किसी व्यक्ति में मनोविदलता के लक्षण विकसित हो जाते हैं तो उन्हें वर्तमान के चिकित्सक पहले मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि तथा मनश्चिकित्सा से दूर करने का प्रयास करते हैं।
(iv) अपूर्ण घर (Halfway Houses) - अपूर्ण घर से तात्पर्य ऐसे आवास से होता है जिसमें वैसे मानसिक रोगियों को रखते हैं जिन्हें अस्पतालीकरण की जरूरत नहीं होती है, परन्तु वे न तो अपने परिवार में रह पाते हैं तथा न ही अकेले रह सकते हैं।
(v) पेशेवर प्रशिक्षण (Occupational Training) - मनोविदलता के रोगियों को दिये जाने वाले सामुदायिक उपचार का महत्वपूर्ण पहलू पेशेवर प्रशिक्षण होता है। इसके पीछे पूर्वकल्पना यह है कि व्यक्ति रोजगार से न केवल अपने आप को समर्थन देता है, साथ ही साथ आत्म-सम्मान प्राप्त करता है।
|
|||||