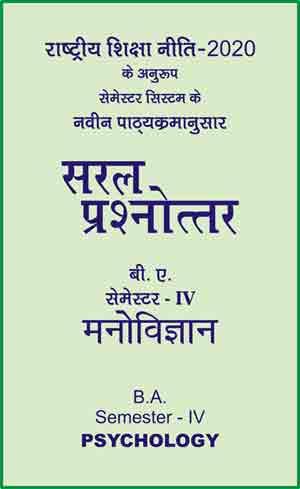|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञानसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- एकध्रुवीय तथा द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति में क्या अन्तर है?
उत्तर-
जीवन की परिस्थितियों एवं घटनाओं से व्यक्ति प्रभावित होता है और उसकी मनोदशा उन्हीं के अनुरूप बन जाती है। जैसेकि खुशी की बात हो अथवा खुशगवार माहौल हो तो व्यक्ति प्रसन्न होता है और जीवन की विपरीत एवं दुःखदायी घटनाओं से व्यक्ति उदास व दुःखी होता है। ये सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं । किन्तु यदि हर्ष अथवा विषाद की यह भावना बिना किसी वास्तविक कारण के उत्पन्न हो अथवा वास्तविक कारण के समाप्त हो जाने के बावजूद व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रसन्न अथवा दुःखी बना रहे तब यह मनोदशा विकार की श्रेणी में आती हैं।
आई. सी. डी. 10 के अनुसार - "मनोदशा विकारों का मूल व्यक्तिक्रम, मनोदशा अथवा भाव में परिवर्तन है, जोकि अधिकतर अवसाद या उत्साह होता है। यह भावात्मक परिवर्तन व्यक्ति के सम्पूर्ण कार्य व्यवहार को प्रभावित एवं संचालित करता है। अतः इन परिवर्तनों के आधार पर रोग के अन्य लक्षण आसानी से समझे जा सकते हैं। अधिकांश मनोदशा विकार पुनरावर्तक होते हैं एवं जीवन में अत्याधिक तनाव या अप्रिय घटना से आरम्भ हो सकते हैं।
एकधुवीय विकृति - एकध्रुवीय विकृति को विषादी विकृति भी कहते हैं। इसका प्रमुख लक्षण व्यक्ति में विषाद तथा उदासी का होना है। इसके अलावा इसमें भूख तथा शारीरिक वजन में कमी हो जाती है। व्यक्ति का संक्रियता स्तर कम हो जाता है।
द्विध्रुवीय विकृति या उन्माद विषाद विकृति - द्विध्रुवीयविकृति ऐसी विकृति को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति में बारी-बारी से विषाद तथा उन्माद दोनों प्रकार की अवस्थायें होती हैं।
एकधुवीय भावात्मक विकृति तथा द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति में अन्तर
| क्र.सं. | एकध्रुवीय भावात्मक विकृति | द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति |
|---|---|---|
| 1. | इसमें व्यक्ति में उदासी तथा विवाद होता है। | इसमें रोगी को बारी-बारी से विवाद तथा उन्माद दोनों के लक्षण होते हैं। |
| 2. | एकध्रुवीय विकृति को प्रमुख दो भागों में बाँटा गया है - (i) डायस्थाइमिक विकृति (ii) बड़ा विपरीत मनोविकृति |
द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा गया है - (i) साइकलोथाइमिक विकृति (ii) द्विध्रुव-एक मनोविकृति (iii) द्विध्रुव-दो मनोविकृति |
| 3. | एकध्रुवीय भावात्मक विकृति आनुवांशिक भी हो सकती है। | द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति का जननिक कारण भी हो सकता है। |
| 4. | इसमें रोगी का आत्म-सम्मान निम्न स्तर का हो जाता है। | इसमें रोगी का आत्म-सम्मान का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। |
| 5. | रोगी में नकारात्मक चिंतन बढ़ जाता है। उसकी विपरीत मनोदशा में बढ़ोतरी हो जाती है। रोगी उदास रहने लगता है। | रोगी पहले की तुलना में अत्यधिक बोलने लगता है। वह अधिक बातूनी हो जाता है। |
| 6. | क्रिया स्तर में परिवर्तन होने लगता है, जैसे - सुस्ती का अनुभव करना या उत्तेजना का अनुभव करना। इसलिए साधारण तथा सामान्य क्रियाओं में अभिरुचि तथा आनंद में कमी होने लगती है। | रोगी का ध्यान जल्दी-जल्दी भंग होने लगता है अर्थात उसमें ध्यान भंगता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं तथा व्यक्ति तुच्छ एवं महत्त्वहीन चीजों के प्रति जल्दी ध्यान आकर्षित करने लगता है। |
| 7. | एकध्रुवीय भावात्मक विकृति के रोगी के लिए जैविक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा चिकित्सा, व्यवहारस्थ चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा तथा संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। | द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति के रोगी के लिए मुख्यतः लीथियम चिकित्सा तथा योजना मनोचिकित्सा का उपयोग किया जाता है। |
| 8. | विपरीत विकृति के मुख्य: कारण, मनोवैज्ञानिक व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तथा जैविक होते हैं। साथ ही न्यूरोसायनस कारण तथा न्यूरोसामाजिक कारण भी विपरीत विकृति को प्रभावित करते हैं। | द्विध्रुवीय भावात्मक विकृति का मुख्य कारण न्यूरोट्रांसमीटर, सोडियम आयन क्रिया, तनाव तथा जननिक कारण होते हैं। |
अतः कह सकते हैं कि विषादी भावात्मक विकृति तथा द्विध्रुवीय भावात्मक विकृत ऐसी मानसिक विकृति है जिसमें व्यक्ति के भाव, संवेग तथा सम्बन्धित मानसिक दशाओं में इतना उतार-चढाव होता है कि व्यक्ति अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में समायोजन नहीं रख पाता है। जिस कारण उसे सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
|
|||||