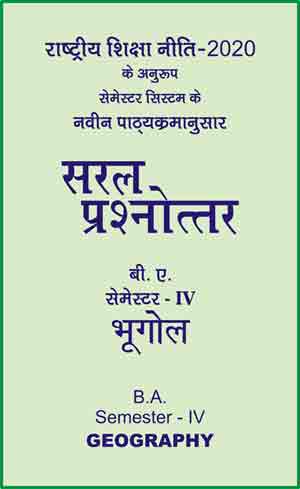|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 भूगोल बीए सेमेस्टर-4 भूगोलसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 भूगोल - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 14
विकासशील देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव
(Effect of Globalization on
Developing Countries)
वैश्वीकरण
वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है।
वैश्वीकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ विद्वान् मानते हैं कि वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। उपनिवेशवाद के आरम्भ होने के साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई थी। इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे देशों ने एशिया एवं दुनिया के अन्य देशों से कच्चा माल उपनिवेशवादी देशों को भेजकर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण किया तथा पुनः उन वस्तुओं को उन्हीं देशों के बाजारों में विक्रय हेतु भेजा। परन्तु इस प्रकार का वैश्वीकरण व्यवसाय अथवा व्यापारिक लाभ से ओत प्रोत था और आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का अर्थ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक एकरूपता तथा आदान-प्रदान से लगाया जाता है।
वैश्वीकरण की विशेषताएँ
वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ वैश्विक मुद्दों को संसार की दृष्टि से देखा जाता है एवं उन मुद्दों को समझने व समझाने के लिए विश्वव्यापी सहयोग व सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। वैश्वीकरण राज्यों के मध्य वस्तुओं, मानवीय संसाधनों, सूचनाओं, तकनीकों, पूँजी आदि का खुला आदान-प्रदान है।
वैश्वीकरण विचार में निहित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका स्वरूप बहुमुखी है, जैसे- सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी आदि।
(2) वैश्वीकरण राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को निकट लाने की प्रक्रिया है। यह विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर प्रदान करता है।
(3) वैश्वीकरण दूरियों को कम करने की एक प्रक्रिया है। यह संस्कृतियों के आदान-प्रदान, जीवन शैली को एक-दूसरे से जोड़ने और विश्व सभ्यता के निर्माण का कार्य करती है।
(4) वैश्वीकरण विश्व की समस्याओं को विश्व के सहयोग से सुलझाने का प्रयास है। यह वीभत्स बीमारी, सुनामी एवं आतंकवाद जैसी घटनाओं को विश्व स्तर पर राज्य के सहयोग से समाधान करती है।
(5) वैश्वीकरण सहयोग, पारस्परिक निर्भरता तथा पारस्परिक सम्बन्धों को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया है।
वैश्वीकरण की आवश्यकता तथा महत्व
वर्तमान समय में वैश्वीकरण सभी देशों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। कोई भी देश पूर्णरूप से विकसित नहीं है। प्रत्येक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस परस्पर निर्भरता को वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता निम्नलिखित रूप में कही जा सकती है-
(1) विश्व स्तर पर व्यापार करना - प्रत्येक देश विकसित तथा विकासशील होते हुए भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे देश पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता को सकारात्मक रूप प्रदान करते हुए वैश्वीकरण का अनुसरण किया गया है। वैश्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यापार को राष्ट्रीयता से निकालकर अन्तर्राष्ट्रीयता के स्तर तक पहुँचाया जाता है जिसमें प्रतिस्पर्धा व संसाधनों का पूर्ण प्रयोग सम्भव है। इस वैश्वीकरण को खुली अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जा सकता है।
(2) विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए - वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। सभी देशों को संसाधनों के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार प्रत्येक देश की अपनी अनेक समस्याएँ भी होती हैं जिनकी समाप्ति वैश्वीकरण के द्वारा की जा सकती है।
(3) राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता - विश्व के सभी देश अपनी सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के प्रति चिन्तित हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास समस्त समस्याओं का हल है। आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र अपना विकास अच्छी तरह से कर सकता है।
(4) विश्व नागरिकता के लिए - वर्तमान समय की आवश्यकता है कि लोगों के मन में ऐसा विचार डाला जाए जिससे वे अपने व्यापक दृष्टिकोण को सदुपयोगी कार्यों में लगा सकें तथा स्वार्थी बनकर केवल अपने राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विकास के विषय में सोच सकें। अतः भारतीय सभ्यता के अनुसार वसुधैव कुटुम्बकम् का सपना साकार हो सकेगा। इस धारणा को प्रत्येक राष्ट्र एवं व्यक्ति के मन में जगाने के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है क्योंकि आज विज्ञान व तकनीकी ने पूरे विश्व को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने देश की तरफ ध्यान न देकर विश्व की नागरिकता के बारे में ध्यान देना चाहिए।
(5) जनसंचार के साधनों द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होना - विश्व का प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान समय में अपने आधार को मजबूत करना चाहता है। सभी राष्ट्र आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं। इसलिए भूमण्डलीकरण के प्रसार को बढ़ाने के लिए जनसंचार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। इन संचार माध्यमों के द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र अपने संसाधनों की कमी का अनुमान लगाता है। इसी आधार पर वह दूसरे राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करता है। वैश्वीकरण में जन संचार के माध्यमों को अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है।
वैश्वीकरण के प्रभाव
विकासशील देशों की दृष्टि से भूमंडलीकरण के कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं-
(1) आर्थिक प्रभाव - भूमंडलीकरण से अन्य देशों से पूँजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। उदाहरण के लिए भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों और दूरसंचार यन्त्रों का प्रयोग करता है। भारत में संस्थानों के इंजीनियर स्नातकों की अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुत माँग है।
(2) राजनीतिक प्रभाव - भूमंडलीकरण सभी प्रकार की गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति सरकार के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों को देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। उदाहरण के लिए एक देश किसी अन्य देश की व्यापारिक गतिविधियों के साथ जुड़ा होता है तो उस देश की सरकार उन देशों के साथ अलग-अलग समझौते करती है। अब अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए नियमावली बनाता है और सभी सरकारों को ये नियम अपने-अपने देश में लागू करने होते हैं।
(3) सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव - भूमंडलीकरण पारिवारिक संरचना को भी बल देता है। अतीत में संयुक्त परिवार का चलन था। अब इसका स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया है। हमारे खान-पान की आदतें, त्यौहार, समारोह भी काफी बदल गए हैं। जन्मदिन, महिला दिवस, मई दिवस समारोह, फास्ट-फूड रेस्तरांओं की बढ़ती संख्या और कई अन्तर्राष्ट्रीय त्यौहार भूमंडलीकरण के प्रतीक हैं। भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पहनावे में देखा जा सकता है। समुदायों के अपने संस्कार, परम्पराएँ और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं।
|
|||||