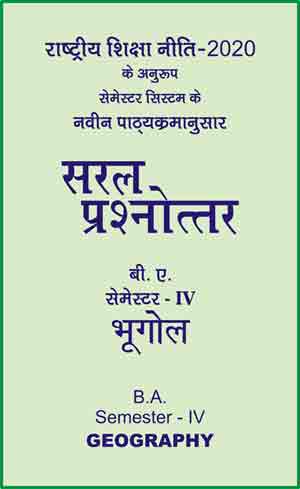|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 भूगोल बीए सेमेस्टर-4 भूगोलसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 भूगोल - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 8
खनन
(Mining)
खनन से आशय ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे - रासायनिक क्रिया तथा कोयला, रेल, तेल या प्राकृतिक गैस आदि जैसे गैर-खनिज पदार्थों को उत्खनित किया जाता है। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिकर्म या खनन (mining) है।
खनिकर्म को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है-
(1 ) तलीयखनन - इस प्रकार के खनन में धरातल के ऊपर जो पहाड़ आदि हैं उनको तोड़कर खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जैसे चूने का पत्थर, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, लौह अयस्क आदि। इस विधि में मुख्य कार्य पत्थर को तोड़ा ही है।
(2) जलोढ़ खनन - कुछ प्राचीन नदियों में जो अवसाद एकत्रित हुए हैं उनमें कभी-कभी बहुमूल्य धातुएँ भी निक्षिप्त हो जाती हैं। इन अवसादों को तोड़कर धातुओं की प्राप्ति करना इस प्रकार के खनन के अन्तर्गत आता है।
(3) भूमिगत खनन - उन अनेक प्रकार के खनिजों तथा अयस्कों के उत्खनन में भूमिगत खनन का सहारा लेना पड़ता है जिनका खुली हुई खानों के रूप में खनन, गहराई पर स्थित होने के कारण, आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त अथवा असंभव होता है। यद्यपि भूमिगत खनन में भी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, तथापि इन निक्षेपों के खनन के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं है। भूमिगत निक्षेप दो प्रकार के हो सकते हैं-
(1) जो स्तर रूप में मिलते हैं, जैसे कोयला
(2) धात्विक पट्टिकाएँ।
इन दोनों प्रकार के निक्षेपों की प्रकृति नितांत भिन्न होती है, इसलिये इनके खनन की विधियाँ भी सुविधानुसार अलग-अलग होती हैं।
भारत में खनन गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक
(i) खनिजों की मांग - स्वर्ण, हीरा, तांबा, यूरेनियम आदि की अत्यधिक मांग के कारण ये प्रायः उच्च लागत पर उत्खनित किए जाते हैं।
(ii) तंत्र तकनीक और उसका उपयोग - प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण संसाधनों के दोहन के तरीकों में भी परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए, सुदूर संवेदन तकनीकों (रिमोट सेंसिंग तकनीकों) की सहायता से, किसी क्षेत्र में संसाधनों के भंडार का अनुमान लगाया जा सकता है।
(iii) परिवहन लागत - कार्य लागत के संदर्भ में, तटीय क्षेत्र या औद्योगिक स्थानों के निकट स्थित निक्षेपों से दूर स्थित अंतर्देशीय निक्षेपों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है।
(iv) अन्य कारक - इसके अन्तर्गत श्रम लागत, अवसंरचना की विकास पूंजी देयता, प्रलेखधारकों में शामिल हैं।
खनन के हानिकारक प्रभाव
खनन से हमारे पर्यावरण पर बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है। खदानों में दिन-रात होने वाले खनन की वजह से रेत के कण वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। इससे इंसानों और अन्य पशु-पक्षियों को सांस लेने में परेशानी होती है। इस प्रदूषित वायु में सांस लेने से इंसानों के फेफड़ों और आंखों को भारी नुकसान पहुंचता है और वे कई घातक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।
खनन में प्रयोग किया जाने वाला बारूद और अन्य रसायन भी वायु को प्रदूषित करते हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खनन के कारण खोखली हो रही है। वहीं, कई जगहों पर खनन से पहाड़ों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जिससे वन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं।
खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले घातक प्रभाव
अंधाधुंध होने वाले खनन ने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे दिया है। इससे भूमि का कटाव, धूल और नमक से भूमि की उपज में परिवर्तन, जल का खारा होना आदि नुकसान होते हैं। खनन से वन्य क्षेत्रों में जल प्रदूषण भी बढ़ता है। खनन के कुछ घातक प्रभाव नीचे दिए जा रहे हैं-
(i) खनिज संपन्न क्षेत्रों में, उच्च कणों वाले पदार्थ के साथ दूषित हवा एक गंभीर समस्या
(ii) राजस्थान में मकराना मार्बल खदानों ने पर्यावरण को प्रदूषित किया है।
(iii) कर्नाटक में ग्रेनाइट की खानों ने धरती में एक बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है और कोयले के खनन ने दामोदर नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है।
(iv) खनन कार्यों के परिणामस्वरूप जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान हुआ है।
(v) धाराओं और नदियों का पानी अम्लीय हो जाता है और पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है।
(vi) अभ्रक आदि जैसे कुछ खनिजों के खनन से श्रमिकों और निवासियों दोनों में फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनिओसिस और सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा रहता है।
|
|||||