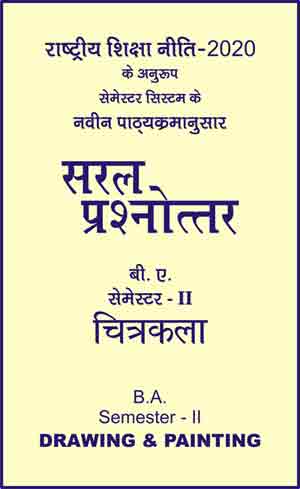|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-2 चित्रकला - कला के मूल तत्व बीए सेमेस्टर-2 चित्रकला - कला के मूल तत्वसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-2 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 8
षडंग
( Shadang )
प्रश्न- षडंग का विश्लेषण कीजिए।
अथवा
चित्रकला के छह अंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में समझाइए।
उत्तर -
चित्रकला के छह अंग जयपुर नरेश जयसिंह प्रथम की सभी के राजपुरोहितों पंडित यशोधर ने ग्यारहवीं शताब्दी में 'कामसूत्र' की टीका 'जयमंगला' नाम से प्रस्तुत की। 'कामसूत्र' के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य या शिल्प (चित्रकला) के छः अंग षडंग बताए हैं-
1. रूपभेद - प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए कि जिससे अमुक व्यक्ति की आकृति को पहचाना जासके। जिस विशेषता या गुण के द्वारा आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति हो उसी गुण का नाम 'रूप' है। जैसे माता के रूप से माता और धाया के रूप में धाया का आभास हो तब ही रूप रचना सार्थक और सत्य होगी। रूप साक्षात्कार आत्मा तथा आँखों दोनों के द्वारा किया जा सकता है।
2. प्रमाण - प्रमाण का अर्थ आकृतियों के अनुपात का ठीक ज्ञान करना है। प्रमाण के अन्तर्गत आकृतियों के माप, लम्बाई-चौड़ाई, सीमा, रचना, कद, कौड़ा आदि आकृति का विवरण आ जाता है। प्रमाण के द्वारा मूल वस्तु का ज्ञान चित्र में भरा जा सकता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को 'प्रमा' के नाम से सम्बोधित किया गया है। किसी विशाल पर्वतमाला या सागर-तट को किसी दीवार के धरातल पर अंकित करने से पहले पर्वत, आकाश, वृक्ष या सागर, नौका तट आदि के लिए अनुपातानुसार छोटा करके यथा स्थान अनुपात में रखना होगा। यही हमारी प्रमा शक्ति का कार्य माना गया है। प्रमा इस अनन्त दृष्टि या सीमित जगत को मापने, देखने, समझने - के लिए हमारे अन्तःकरण का मापदण्ड है। प्रमा से न केवल निकट या दूरी का ज्ञात होता है बल्कि किसी वस्तु का कितना भाग चित्र में प्रस्तुत करें जिससे चित्र आकर्षक लगे इसका भी प्रमा ही निर्धारण करती है। प्रमा के द्वारा ही हम पुरुष तथा स्त्री अनुपात की विभिन्नता, पशु-पक्षी आदि की भिन्नता तथा भेदों को ग्रहण करते हैं। पुरुष तथा स्त्री की लम्बाई-चौड़ाई में भेद, उनके अंगों की रचना किस क्रम में होनी चाहिए आदि देवताओं, राजाओं और साधारण मनुष्य के चित्रों के कद का क्या अनुपात है ये तत्त्व प्रमा के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। चित्राकार्यों में प्रमाण के आधार पर पाँच प्रकार के रूपों का वर्णन दिया है जो इस प्रकार हैं-
(1) मानव - दस ताल (जैसे पांडव, राम, कृष्ण, शिव आदि),
(2) भयानक- - बारह ताल (जैसे भैरव, बाराह, हयग्रीव)
(3) राक्षस - सोलह ताल (जैसे कंस, रावण)
(4) कुमार - आठ ताल (जैसे वामन),
(5) बाल -पाँच ताल (जैसे बाल गोपाल )
इस नाम - तोल में ताल को एक इकाई माना गया है। इसी आधार पर विभिन्न आकृतियों के अनेक प्रमाण बताइए गए हैं।
3. भाव - भाव का प्रदर्शन आकृति की भंगिमा से होता है। भारतीय काव्यशास्त्र में भाव के लिए काव्य रचना का मूल आधार माना गया है और भावों की महत्ता का सूक्ष्मता से विचार किया गया है - भाव के उदय से ही शरीर और इन्द्रियों में विकार की स्थिति उत्पन्न होती है। भाव दो प्रकार से प्रकट होता है-
(1) प्रकट
(2) प्रच्छन
भाव के प्रकट रूप का दर्शन हम नेत्रों के द्वारा कर सकते हैं परन्तु प्रच्छन्न रूप का अनुभव केवल मन के द्वारा कर सकते हैं। वर्षकाल के बाले बादलों तथा हरियाली का सौन्दर्य, माथे पर हाथों को रखकर बैठने में, आँखों को दबाकर रोने में अस्त-व्यस्त केशों के लहराने में, अंधेरों और नयनों की फड़कन में, झुकी झुकी पलकों में, जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रकट रूप से आँखों में देख सकते हैं। किन्तु भाव के प्रच्छन्न रूप का आँखों को आभास नहीं होता, इसका ज्ञान अनुभव के द्वारा होता है। चित्र की ये अचित्रित बातें, जो नेत्रों के द्वारा नहीं देखी जाती, व्यंजन के द्वारा पहचानी जा सकती हैं। बाहर के रूप को रेखा, रंगों तथा आकारों के द्वारा प्रकट रूप से अंकित किया जा सकता है परन्तु भाव के व्यंग्य पक्ष को या उसके आन्तरिक रूप को कलाकार रूप की ओट में अभिव्यक्त करता है। आकृति के शरीर की विभिन्न स्थितियों में परिवर्तन के द्वारा कलाकार अपने हृदय के भावों को प्रदर्शित करता आया है। परन्तु मन के अव्यक्त भावों को दिखाना बहुत कठिन होता है।
4. लावण्ययोजना - रूप, प्रमाण तथा भाव के साथ चित्र में लावण्य का होना परम आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक दिशा देता है उसी प्रकार लावण्य को उत्कर्ष प्रदान करता है भाव आन्तरिक सौन्दर्य का बोधक है और लावण्य बाह्य सौन्दर्य का प्रतीक है। भाव द्वारा कभी-कभी चित्र में कर्कशता का आभास होने लगता है किन्तु लावण्ययोजना से वह आकर्षक बन जाता है। चित्र में रूप और प्रमाण की यथोचित उपयुक्त व्यवस्था होने पर भी लावण्य का समावेश किए बिना चित्र से सौन्दर्य की अभिव्यंजना नहीं होती है। दूसरी ओर लावण्य का उदय मुख्तया रूप, प्रमाण तथा भाव से ही होता है। जिस प्रकार एक कान्ति (लावण्य) रहित मोती की भंगिमा निष्प्रभ है उसी प्रकार रूप प्रमाण तथा भाव से युक्त चित्र भी 'लावण्य' के बिना आकर्षक रहित है। लावण्य का ठीक सन्तुलन भी आवश्यक है।
5. सादृश्य - मूल पदार्थ या भाव को उसकी प्रतिकृति में मूल जैसी समानता के साथ दर्शित करना 'सादृश्य' है। चित्र पर आधारित हो या कल्पना पर इसमें चित्रित व्यक्ति या आकृति को दर्शक तुरन्त पहचान जाए तो सादृश्य ठीक है। जिस वस्तु को हम चित्र में अंकित करते हैं, उसके गुण अथवा दोष चित्र में समाविष्ट होना चाहिए। उदाहरणार्थ बुद्ध के चित्र में उनकी दया तथा अहिंसा की वे विशेषताएँ होनी चाहिए जो उनमें सारे संसार ने देखीं। यदि वे विशेषताएँ चित्र में नहीं हैं तो चित्र को महावीर स्वामी का भी समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही तपस्या की और दोनों का योगी रूप है। परन्तु इसके लिए बुद्ध को कटे केश, अहिंसा का सन्देश देती मुद्रा में तथा हाथ में भिक्षापात्र लिए अंकित करना होगा। महावीर के चित्र में ये विशेषताएँ उपयुक्त नहीं है।
चित्र की शुद्धताराहनीय है, जो सादृश्य के द्वारा ही प्राप्त है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अन्तर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना गया है। "चित्रे सादृश्करणम् प्रधानं परिकीर्तिनम्।' (चित्रसूत्र)
6. वर्णिका भंग - वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तूलिका का प्रयाग किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन-सा रंग आना चाहिए ये सभी समस्याएँ वर्णिकाभंग के अन्तर्गत आती हैं। रंग की भिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता बल्कि उनका अन्तर भी अभिव्यक्त होता है। बिना वर्ण साधना के उपरोक्त प्रथम पाँच अंगों का कोई दृष्टव्य अस्तित्व नहीं रहता बल्कि उनका स्थान केवल मन तक सीमित रह जाता है। इस प्रकार उपरोक्त पाँच कला अंगों को वर्ण विधि तथा तूलिका ही साकार रूप प्रदान करती है। यद्यपि वर्ण पाँच माने गए हैं परन्तु इनके सम्मिश्रण से सैकड़ों सम्मिश्रित वर्ण उत्पन्न होते हैं। पशु, पक्षी, मानवाकृति आदि में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किए जाए चित्रकार के लिए यह जानना परमावश्यक है।
वर्ण ज्ञानं नास्ति किं तस्य जपपूजनेः।
वर्णिका भंग की पूर्णता प्राप्त करने के लिए लघुता, क्षिप्रता और हस्तलाघव और वर्ण के कौशल की आवश्यकता है। यदि किसी पुष्प का चित्र बनाना है तो उससे फूलों का रंग ही नहीं सुगन्ध की भावना का उदय भी होना चाहिए। वात्स्यायन ने यह भी उल्लेख किया है कि नागर के आवास कक्ष में पलंग (सेज) के सिरहाने खूंटी पर वीणा तथा चित्र - रचना का सामान टंगा होना 'चाहिए। प्रेमिका को वश में करने का एक उपाय बताते हुए यह भी कहा गया है कि जहाँ उसका घूमना- -फिरना हो वहाँ उसके चित्रों के साथ नायक का चित्र बनाकर रख देना चाहिए।
चित्रकर्म के जिन छ: अंगों का ऊपर विवेचन किया गया, वस्ततः वे 'भारतीय शिल्प' के छः अंग हैं। शिल्प शब्द का अर्थ व्यापक है और चित्रकला भी एक शिल्प है। बाद में 'शिल्प' शब्द का अर्थ 'कला' से लिया जाने लगा। अन्ततः शिल्प, स्थापत्य और चित्र, ये कला के तीन भेद माने जाने लगे।
|
|||||