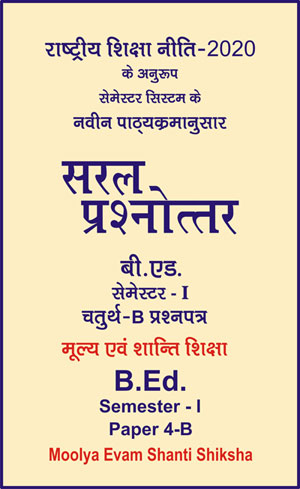|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा
प्रश्न- विश्व में शांति की सार्थकता को सिद्ध कीजिए एवं इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर -
मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आधारों की स्थापना हेतु विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के पांच आधारभूत सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं -
- एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करना।
- एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही न करना।
- एक दूसरे के आंतरिक विश्वास में हस्तक्षेप न करना।
- समानता एवं परस्पर लाभ की नीति का पालन करना।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना।
इसे माना जाता है यदि विश्व युद्ध उपर्युक्त पांच बिंदुओं पर अमल करे तो हर तरफ चैन एवं अमन का ही वास होगा। पंचशील नीति सिद्धांत को सर्वप्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विश्व में शांति एवं अमन स्थापित करने के लिए दिए थे।
‘विश्वशांति दिवस’ के उपलक्ष्य में प्रत्येक देश में जगह-जगह सफेद कबूतरों के उड़ाया जाता है, जो कहीं न कहीं पंचशील के सिद्धांतों को दुनिया तक पहुँचाते हैं। ‘विश्व शांति दिवस’ के अवसर पर कबूतर उड़ाने की परंपरा अत्यंत पुरानी है। इस कबूतर की उड़ान के पीछे एक शायर की पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं-
“तू नफरत की दुनिया में मोहब्बत के फूल खिला,
ताकि व्यर्थ युद्ध न हो किसी वतन के रखवाले का।”
वर्ष 1982 से शुरू होकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय शांति 'दिवस' या 'विश्वशान्ति दिवस' के लिए चुना गया था, लेकिन वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितम्बर का दिन घोषित कर दिया गया जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
उद्देश्य - सम्पूर्ण विश्व में शांति कायम करना आज संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि, अन्तर्राष्ट्रीय संघ के प्रमुख उद्देश्य में शांति की संस्कृति विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रयत्न करना होगा, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
अतएव इस उद्देश्य के प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र की भी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी तमाम संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, विविध सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरकारें प्रतिवर्ष 21 सितम्बर को 'अन्तर्राष्ट्रीय शांति दिवस' का आयोजन करती हैं। शांति का संदेश दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और राष्ट्रीय द्वेष के कारण जब राष्ट्र पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो यह दिन बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तत्क्षण इसे स्वीकार कर इसे दिन सभी देशों एवं उनके निवासियों में शांतिपूर्ण विचारों के सृजन करने के लिए समर्पित किया था।
वर्तमान परिवेश में शांति की सार्थकता - आज विश्व के देशों में सामरिक होड़ बढ़ रही है, एवं शस्त्रों की बिक्री तथा व्यापार राजनीतिक स्वार्थों के लिए जारी है। यदि इसे रोका न गया तो इसका परिणाम एक और विश्वयुद्ध हो सकता है।
प्रो. कोहन का मत है कि, "शस्त्रीकरण के द्वारा कोई समस्या हल नहीं हो सकती, केवल अहिंसात्मक उपायों से ही विश्व शांति की स्थापना संभव हो सकती है।"
आइंस्टाइन क्लब ने कहा है कि "शस्त्र सज्जा से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।" अतः सैन्यकरण के आह्वान से ही शांति स्थापना की ओर ले जाया जा सकता है।
अमेरिकी मित्र सेवा समिति का भी मत था कि, "सशस्त्रीकरण देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं करता, बल्कि यह पूरे देश को तथा विश्व को असुरक्षित बनाता है।" इस प्रकार सशस्त्रीकरण से युद्ध को बढ़ावा मिलता तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, अतः शासनतंत्र पर प्रतिबंध ही शांति स्थापना का एक मात्र साधन है।
विभिन्न विचारकों एवं विद्वानों का मत है कि शांति शिक्षा को विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्व विद्यालयों में एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रतिपादित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
इसके अंतर्गत शिक्षा के पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, क्रियाओं तथा कार्यक्रमों को एक अभिन्न अंग बनाया जाए। इसके माध्यम से छात्र स्वयं ही विश्व का एक अभिन्न अंग मानने सीख जाएंगे। पाठ्यक्रम में निहित शांति विषयों का अध्ययन अनिवार्य ढंग से किया जाना चाहिए।
इसकी ऐतिहासिक परंपरा को विश्व शांति, विश्व-बंधुत्व, श्रमपूज्य भावना आदि के प्रति रुझान बढ़ाने हेतु जनसंचार साधनों - रेडियो, टी.वी., आईटीआई, कैसेट्स, टेलीविजन, समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।
जनसंवर्धन व शांति संदेश प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक संगठनों की प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न देशों के मध्य संपर्क एवं संगठन में मजबूती, शांति-शिक्षा एवं नीति की व्यवस्था की जा सके। इसके संबंध में संबंधों एवं तनावों को दूर करने के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
|
|||||