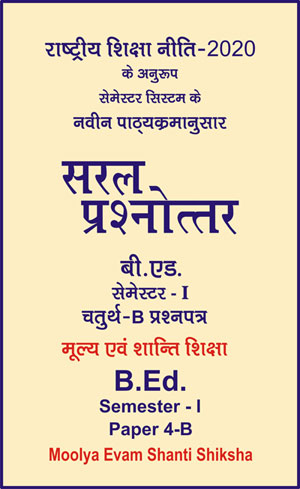|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा
अध्याय 4 - शान्ति शिक्षा
(Peace Education)
प्रश्न- वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म समभाव की व्याख्या कीजिए।
अथवा
भारतीय संदर्भ में विश्वशांति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।
उत्तर–
भारतीय संदर्भ में विश्वशांति की अवधारणा - भारतीय संस्कृति व सभ्यता ने विश्वशांति को प्राचीन काल से ही महत्व प्रदान किया। वेदों में विश्व शांति की सुन्दर झलक मिलती है। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने इस संदर्भ में धम्म नीति का अनुसरण किया। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने विश्व शांति की दिशा में प्रयास किया। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय मूल्यों से विश्व को परिचित कराया। उनके अनुसार, मूल्यों एवं आध्यात्मिक विकास की शिक्षा को दी जाए तो व्यक्ति का दृष्टिकोण समन्वित रूप में कार्य करेगा, वह नैतिकता के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग देगा तथा मानवता हित की भी ध्यान रखेगा। भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार समाज को सम्पूर्ण विश्व के समान एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर स्वीकार किया जाए तो विश्व के विभिन्न देशों में प्रेम बढ़ेगा तथा वे हिंगसा मुक्त समाज की स्थापना करेंगे। इसलिए छात्रों को प्राथमिक स्तर से भारतीय जीवन मूल्यों के माध्यम से सामाजिक शांति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को वर्णन निम्न रूप में किया जा सकता है –
(1) आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा - छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह सत्य आचरण कर सके तथा हिंसा से दूर रह सके। इससे समाज में शांति का माहौल सुगम होगा।
(2) मानवता की शिक्षा - सामान्य रूप से समाज में हिंसा की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाया करती हैं। अतः शिक्षा के माध्यम से छात्रों में मानवता की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोगी समझें तथा मानवता के आधार पर कार्य करें। इससे समाज में शांति व्यवस्था उत्पन्न हो सकेगी।
(3) नैतिकता की शिक्षा - आध्यात्मिक विकास हेतु नैतिक शिक्षा भी ज्ञान परमावश्यक है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में प्राथमिक स्तर से नैतिक शिक्षा का सम्पादन वैश्विक स्तर पर दिया जाता है तो सम्पूर्ण विश्व के छात्र नैतिकता का आचरण करने लगेंगे तथा समाज में शांति स्थापित हो जाएगी।
(4) प्रकृति प्रेम की शिक्षा - सामान्य रूप से प्रकृति के प्रति प्रेम तथा प्राकृतिक संसाधनों को अपने स्वार्थ के लिए विघटन न बनाना भी आध्यात्मिक विकास के लिए माना जाता है। जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करें, पेड़ नहीं काटें तथा नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करें। इस प्रकार समाज को पर्यावरणीय आपदाओं से बचाया जा सकता है। इससे समाज में शांति की व्यवस्था वैदिक काल से प्रचलित होती है।
(5) भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना - विश्व स्तर पर आध्यात्मिक विकास की स्थिति छात्रों एवं समाज में उच्चतम करती है। इसका सबसे सरल उपाय यही है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव हो। व्यक्ति बंधन मुक्त हो तथा सद्भाव सुखदान की भावना से परिणीत हो जाए। इससे सम्पूर्ण मानव समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मिक सुख की शांति के लिए दूसरों को सुख प्रदान करेगा। भौतिक सुख हेतु दूसरों को दुःख नहीं देगा।
(6) पशु प्रेम की शिक्षा - भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में पशुओं की पूजा की जाती है। अनेक जीव-जन्तुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। बालकों में पशुओं के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न किए जाने अनिवार्यक हैं।
(7) सार्वजानिक हित की शिक्षा - भारतीय संस्कृति एवं समाज में प्राचीन काल से ही मानव हित एवं सार्वजानिक हित के महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय समाज में किसी एक व्यक्ति का ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, किंतु प्राण बचाने के लिए सर्वस्व समर्पण करने की भावना को सर्वोपरि रखा गया। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो बचाने हेतु कोई प्राणी अपनी जान न्यौछावर कर देता था। ऐसा कार्य महाभारत में अपनी प्राण रक्षा करके सार्वजानिक हित के लिए रक्षा की थी।
(8) त्याग की भावना का विकास - सामान्य रूप से भारतीय संस्कृति में त्याग को खुली मानसिक मानव प्रवृत्ति के रूप में उद्धरण के लिए मानव हित के लिए व्यक्तियों ने सुख एवं विलासी जीवन को ठोकर मार दी। जैसे - महात्मा बुद्ध, भगवान राम, भरत आदि के नाम अग्रणीय हैं। अतः त्याग की भावना सम्पूर्ण विश्व में शांति की स्थापना करती है।
(9) ईश्वर में विश्वास - वर्तमान मानव में ईश्वर के प्रति आस्था के भाव में कमी आ रही है। मानव ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। इससे समाज में नैतिकता एवं पारस्परिक सौहार्द्र में गिरावट हो रही है। अतः हमें ईश्वर के मूलतत्व एवं उसे परमसत्ता मानते हुए धर्म के आचरण पर चलना चाहिए। ईश्वरीय आदर्शों जैसे – हमें किसी व्यक्ति के मन, वचन एवं कर्म से कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जिससे समाज में स्नेह उत्पन्न हो सके तथा शांति व्यवस्था बनी रहे।
(10) पुण्य को परिभाषित करना - भारतीय संस्कृति में पुण्य-पाप की अवधारणा रही है। यह पुण्य समाज एवं मानव दोनों के लिए हितकारी होता है। वही पुण्य मानव एवं समाज दोनों के लिए हित में होता है। पाप-पुण्य के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है –
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।
इससे सिध्द होता है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए, एवं दूसरों को कष्ट, पीड़ा आदि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार मूल्यों की शिक्षा द्वारा समाज एवं सम्पूर्ण विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है।
(11) वसुधैव कुटुंबकम - यह भारतीय सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा महाउपनिषद सहित कई अन्य ग्रंथों में उपलब्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ है – "धरती ही परिवार है।"
(12) सर्व-धर्म समभाव - भारतीय धर्मानुसार धर्म की प्राथमिकता एवं प्रेरणाएं शीलता, शांति, व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, प्रगति एवं विकास से सम्बंधित समाज में उपयोगिता के निर्माण में निहित हैं। क्योंकि भारतीय ही धर्म ही जो धारण करने योग्य है, अर्थात वह धर्म जो आचरण में उतरे वही धर्म होता है। अतः सभी धर्म अनुशीलन की करने की सलाह कोई नहीं देता है। धार्मिक शिक्षाएं एक स्वस्थ मानव को प्रगति की ओर, विश्व शांति में सहयोगी होती हैं।
|
|||||