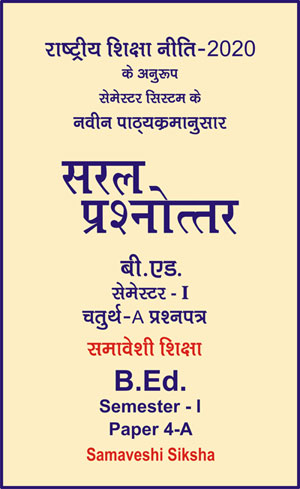|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- बाल अपराध का अर्थ क्या है? बाल अपराध का सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। बाल अपराध को रोकने के उपाय भी बताइए।
अथवा
बाल अपराध क्या है? इसे किस प्रकार रोका जा सकता है?
उत्तर-
बाल अपराध का अर्थ व परिभाषा
सामाजिक व्यवस्था तथा समाज के नियमों का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य है। जो व्यक्ति इन सामाजिक नियमों की विरुद्ध कार्य करता है, उसे सामाजिक दृष्टि से अपराधी माना जाता है। समाज के नियमों का उल्लंघन या समाज विरोधी व्यवहार जब बालक के द्वारा किया जाता है तो वह अपराध और जब बालकों या किशोरों के द्वारा किया जाता है तो बाल अपराध या किशोर अपराध कहलाता है।इस प्रकार जो बालक असामाजिक तथा अवैधानिक व्यवहार करते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा शांति भंग करते हैं, अपराधी बालक कहलाते हैं।
बाल-अपराध और बाल-अपराधी के सम्बन्ध में दो मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-
मेरेस- "जो जान-बूझकर इरादे के साथ समाज के हितों की उपेक्षा करता है, जिससे समाज अस्थिर हो, उसे ही अपराधी बालक कहते हैं।"
न्यूमर- "जो समाज विरोधी व्यवहार व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है, बाल-अपराध कहलाता है।"
स्किनर- "बाल-अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी बालक द्वारा किया गया हो अपराध होता है।"
बाल-अपराधियों के प्रकार
बाल अपराधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है-
(क) आक्रामक आधार
-
बच्चों के प्रति आक्रामकता।
-
वस्तुओं के प्रति आक्रामकता।
-
पशुओं के प्रति आक्रामकता।
-
बड़े तथा स्वयं के प्रति आक्रामकता।
-
संस्था के प्रति आक्रामकता।
(ख) स्थिति का आधार
-
संस्थागत - इस प्रकार के बाल-अपराधियों को पकड़कर संस्था के अंदर डाल देते हैं।
-
स्वतंत्र - इस प्रकार के अपराधी बालकों में वे बालक आते हैं जो अभी तक अपराध करते हुए पकड़े नहीं गये।
(ग) व्यक्ति-स्थिति का आधार
-
व्यक्तिगत - जो बालक अकेले में अपराध करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत अपराधी कहा जाता है।
-
सामूहिक - जो समूह में अपराध करते हैं, उन्हें सामूहिक अपराधी कहा जाता है।
आदत का आधार
-
पहली बार का अपराधी - वह व्यक्ति जो पहली बार अपराध करता है।
-
आदतन अपराधी - ऐसे बालक अपराध करने के आदी हो जाते हैं।
बाल अपराध को एक प्रकार से और वर्गीकृत कर सकते हैं-
1. यौन-संबंधी अपराध- इस प्रकार के अपराधों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-
(अ) विभिन्न लिंगों अपराध- इसे भी दो भागों में बाँटा जा सकता है-
-
पुरुष रखने वाले छोटी आयु के सदस्य के साथ।
-
स्त्रियाँ रखने वाली समान आयु के सदस्य के साथ।
(ब) विश्वास- इनको निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है-
-
सामान्य अपराध।
-
असामाजिक एवं निरंकुश प्रदर्शन।
2. बाल अपराधियों की प्रवृत्तियाँ
-
झूठ बोलना।
-
चोरी करना।
-
बिना उद्देश्य के घूमना।
-
मार-पीट करना।
-
स्कूल की वस्तुएँ नष्ट करना।
-
झगड़ालू होना।
-
दीवारों पर गंदी बातें लिखना।
-
कटु बोलना।
-
पलायनशीलता।
बाल अपराध सम्बन्धी विभिन्न मत
बाल अपराध के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। बालक अपराध क्यों करता है? किसी की वस्तु क्यों चुराता है? इसका एकमात्र यह कारण है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। यदि हम किसी को सही वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो बालक को सजा दिया जायेगा। किसी-किसी वर्ग में बाल-अपराध को बढ़ाने के लिये प्रेरणा दी जाती है। बाल अपराध के बारे में निम्न दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं—
-
अध्यापक के दृष्टिकोण में बाल अपराध- अध्यापक इस तथ्य को भली-भांति जानते हैं कि बालक क्यों अपराधी होते हैं? अध्यापक की जानकारी में वे तत्व होते हैं जिनके द्वारा बालकों के व्यवहार को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। यदि अध्यापक सदैव सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं तथा अपराधी बालकों से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। यही कारण है कि हम अपराधी बालकों के व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया परिवर्तन कर सकते हैं। उनके व्यवहार को सामान्य समाज के अनुकूल बनाने में अध्यापक का दृष्टिकोण बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
-
बाल अपराध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में- एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में अपराध भी एक तरह से "अधिगम प्रक्रिया" है। उनका कहना है कि बाल अच्छी हो या बुरी सभी सीखी जाती हैं। इसलिए कोई भी बालक दुबारा नहीं आता जाता है जिन फूलों की शिक्षा निर्देश है। इस प्रकार अपराधी बालक अपराध को अपने साथ स्कूल के बदलते हुए व्यवहार के मिलान पर सीखते हैं लेकिन इन अपराधी कार्यों से बालक अपराधी बन जाते हैं।
-
स्वयं बालापाशी की दृष्टि में बाल अपराध- यदि मनोवैज्ञानिक अपराधी बालकों के किसी भी अपराध का पता लगाए तो उसके पीछे कोई-न-कोई कारण अवश्य मिलेगा। इसके बाद हम अपने को यह कह सकते हैं कि अगर हमने ये अपराध किया तो हमारे सामने बालकों के अपराध का समाधान तुरन्त हो जायेगा।
-
मनोविश्लेषक की दृष्टि से बाल अपराध- मनोविश्लेषक की दृष्टि में बालक अपने अंदर उत्पन्न हुये दुख को मिटाने के लिए ही अपराध करता है। इसलिए अपराध का आधार मनोविश्लेषक संवेगात्मक हड़बों को माना है। उसके अनुसार, बालक इन हड़बों के कारण समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए वह इससे क्षण भर में छुटकारा पाने के लिये अपराध कर बैठता है।
-
बाल अपराध से दुखी व्यक्ति की दृष्टि में बाल अपराध- जब कोई व्यक्ति किसी बालक के द्वारा किये गए अपराध से दुखी होता है तो वह सोचता है कि बालक को इस अपराध का दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।
इन धारणाओं तथा दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि बाल अपराध एक जटिल व्यवहार है तथा हर व्यक्ति इस सम्बन्ध में विभिन्न मत रखता है। इसलिए जब कभी भी हम स्कूल और बाल अपराध के सम्बन्धों का अध्ययन करें तो इन धारणाओं को संगान में लाना जरूरी होगा। ऐसा करने से ही हम इसका निवारण निकाल सकते हैं।
विद्यालय में अपराध-प्रवृत्ति को रोकने के उपाय
बढ़ते हुए बाल अपराधों को रोकने के लिये विद्यालय में निम्न प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं—
-
विद्यालय के द्वारा बालकों के स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के लिये उत्तम वातावरण का निर्माण करना चाहिए।
-
विद्यालय में योग्य, प्रशिक्षित, प्रतिभाशाली और बाल मनोविज्ञान से परिचित अध्यापक को नियुक्त किया जाना चाहिए।
-
बालकों को उनकी रुचि एवं स्तर व योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
-
बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करके उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
-
विद्यालय में बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए।
-
बालकों में नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण के लिये धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
-
यौन अपराधों की रोकथाम के लिए किशोर एवं किशोरियों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए।
-
शिक्षा में रचनात्मक कार्य और स्वानुभव द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
-
शिक्षकों द्वारा बालकों के अनुकूल प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
-
बालकों में सामाजिक संबंधों के विकास और उनके अवकाश का सही प्रयोग करने के लिये विद्यालय में विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
-
बालकों के स्वास्थ्य मनोरंजन के लिये विद्यालय में खेल, सस्तरीय यात्राएँ, रेडियो, टेलीविजन आदि नवीन साधनों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
-
बालकों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिये स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए।
-
विद्यालय और बालक के मध्य निकट सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अभिभावक अध्यापक परिवार का निर्माण किया जाना चाहिए।
-
विद्यालयों में बालकों के चरित्र का लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए जिससे शिक्षक और उनके माता-पिता को उनके व्यक्तित्व की प्रवृत्तियों के बारे में पता लगता रहे।
-
बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए।
|
|||||