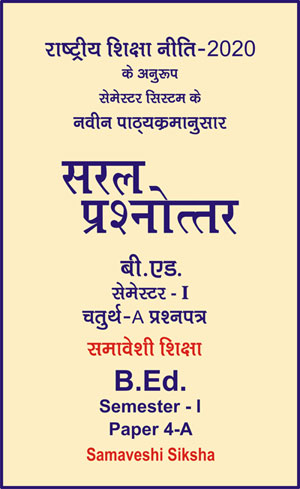|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- हड्डियों के रोगों से ग्रस्त या विकलांग बालकों को शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है? विवेचना कीजिए।
अथवा
हड्डियों से ग्रस्त विकलांग बालकों की शिक्षा पर एक लेख लिखिए।
अथवा
अधीर बधिर बालकों के शैक्षिक प्रावधान क्या हैं?
उत्तर-
शारीरिक रूप से अपंग बालक भी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतः यह सब का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें ताकि वह भी आत्मनिर्भर हो कर समाज में समान्यपूर्वक जीवन जी सके। हम अपंग बालकों को निम्न प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं—
(1) समायोजन - शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या समायोजन की होती है, विद्यालय तथा समाज में अपने को समायोजित करना पड़ता है। अगर हम उन बालकों की दृष्टि से देखें तो उनमें हीन भावना पनपने लगेगी। हमें उनकी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उनमें आत्म-विश्वास की भावना जागृत हो तथा वे अपने अपंग को अकेलापन न समझें। हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि वे भी सामान्य बालकों की भाँति हैं। उन्हें अन्य बालकों के साथ घुलमिल करने की प्रेरणा देनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक व योग्यताओं के अनुसार उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आत्म-निर्भर होकर समान्यपूर्वक जीवन जी सकें। जब उन्हें घर, विद्यालय तथा समाज से सहायता मिलेगी तो वे और ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे।
(2) देखभाल - शारीरिक रूप से अपंग बालकों को कई समस्याओं में विशेष पर ध्यान देना पड़ता है। अतः में हमेशा यह कहा जाता है कि इन बच्चों की देख-रेख से उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए उनको उचित इलाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कृत्रिम अंग लगाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। उनकी मानसिक योग्यताओं व शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए।
(3) उपचार सुविधा - कुछ अपंग या विकलांग बालकों को समय-समय पर अपने आप को चेक-अप करवाना पड़ता है। इसके लिए उसे अवसरों की आवश्यकता होती है तथा उसका विद्यालय से अनुपस्थित भी रहना पड़ता है। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। अध्यापक व दूसरे छात्रों को ऐसे बालकों के साथ सहयोग करना चाहिए तथा विद्यालय के नियम इन बालकों के लिए लचीले होने चाहिए। इनकी हर प्रकार की संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए।
(4) विशेष कक्षा- शिक्षा-शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करना चाहिए लेकिन कभी-कभी उनकी शारीरिक आवश्यकताएँ सामान्य बालकों से अलग होती हैं और वह साधारण कक्षा में लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
(5) विशेष कक्षाएँ- कुछ बालकों को अपनी बीमारी के कारण स्कूल से कई दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। इससे उनका शैक्षिक नुकसान होता है और वह पढ़ाई में सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए विशेष कक्षाएँ लगाकर उनकी शैक्षिक क्षति-पूर्ति करनी चाहिए।
(6) प्रशिक्षित अध्यापक- एक साधारण अध्यापक जब सामान्य कक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को पढ़ाता है तो वह विकलांग बालकों के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता। अतः ऐसे बालकों के लिए एक प्रशिक्षित व विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए जो इनके सामाजिक, व्यक्तिगत संपर्कों व शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर उनके विकास में अपनी योगदान दे। ऐसे बालकों के लिए हम किसी विशेष प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार विद्यालयों की स्थापना विकलांग बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा निर्देशों में इन बालकों को शिक्षा प्रदान करें।
(7) विशेष विद्यालय- कुछ बालक जो शारीरिक रूप से अधिक अपंग या विकलांग होते हैं वह सामान्य बालकों के साथ शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते तथा न ही वह विशेष या अतिरिक्त श्रेणी में पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ाने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इन विद्यालयों में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तथा एक डॉक्टर का प्रबन्ध होना चाहिए।
इन विद्यालयों में निम्नलिखित सुविधाएँ अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए।
(i) जाँच के लिए शारीरिक उपचार कक्ष के साथ-साथ डॉक्टर व दवाओं का प्रबन्ध होना चाहिए।
(ii) व्यायामशाला कक्ष, के साथ-साथ एक मनोरंजन कक्ष की स्थापना होना चाहिए ताकि इलाज के साथ-साथ मनोरंजन भी होता रहे।
(iii) विद्यालय के दरवाजे ऊँचे व अधिक चौड़े होने चाहिए। घुमावदार सीढ़ियों के साथ-साथ लिफ्ट का भी प्रबन्ध होना चाहिए।
(iv) कुर्सी, मेज तथा दूसरा फर्नीचर बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनवाना चाहिए।
(v) पीने के पानी की टंकी की ऊँचाई सभी बालकों के कद के अनुसार रखनी चाहिए ताकि उन्हें पानी पीने में कठिनाई न हो।
(vi) विद्यालय में एक आराम कक्ष अवश्य होना चाहिए ताकि बालक खाली समय में वहाँ पर आराम कर सकें।
(vii) छात्रावास का प्रबन्ध विद्यालय के साथ ही होना चाहिए ताकि उन्हें आने-जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
(viii) विकलांग बालकों की शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए योग्य, कुशल व अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
(ix) विद्यालयों में एक पुस्तकालय की भी स्थापना होनी चाहिए ताकि बालक वहाँ जाकर ज्ञान अर्जित कर सकें।
(8) विशेष पाठ्यक्रम- आमतौर पर विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाया जाता है तथा उनको वहीं पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है जो दूसरे सामान्य बालक पढ़ते हैं। कुछ बालकों की शारीरिक अपंगता इतनी अधिक होती है कि वह उस सामान्य पाठ्यक्रम का लाभ नहीं उठा सकते। अतः यह आवश्यक बन जाता है कि उनकी आवश्यकताओं व मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्यक्रम के साथ-साथ उनकी परीक्षा भी लचीली होनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव न हो।
(9) व्यावसायिक प्रशिक्षण- शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उनके मानसिक स्तर व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वह अपने भविष्य के लिए निपुण होकर अपनी योग्यता अनुसार अच्छी रोजगार कर सके या फिर कोई नौकरी कर सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा और उनमें सकारात्मक सोच व संचार होगा।
(10) समाजीकरण- समाज में प्रायः विकलांग बालकों के हीन दृष्टि से देखा जाता है। इससे उनमें हीनभावना का विकास होता है और उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है। अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हें पूरा समाज दें न कि समाज से उन्हें दूर रखें। घर, विद्यालय व समाज में समाजीकरण के लिए उनका पूरा सहयोग हो ताकि वे खुद समझ सकें कि वे भी अपने आप को समाज का अंग समझें। उनकी शारीरिक अपंगता को ध्यान में रखकर उनके लिए व्यायामशाला, विशेष कार्यक्रम, खेल-कूद, गोष्ठियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। उनकी इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
(11) नौकरी- विकलांग बालकों की शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा देने के पश्चात् उनके लिए सम्मानजनक नौकरी का प्रबन्ध करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। ये केंद्र अपंग या विकलांग बालकों को उनकी योग्यता, रुचि व अभिरुचि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा इनको रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं। विकलांगों की भलाई हेतु राज्य, राष्ट्र स्तर ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं। 20 सितंबर, 1959 को ज्यूरिख सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रति वर्ष मार्च महीने के तृतीय रविवार को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। सरकारी नौकरियों एवं विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए तीन प्रतिशत सीटें विकलांगों के लिए रखी गई हैं। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है।
|
|||||