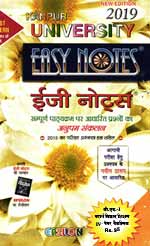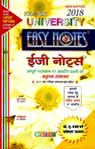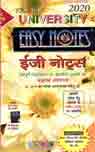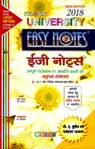|
शिक्षाशास्त्र >> ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षण ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षणईजी नोट्स
|
|
||||||
बी.एड.-I प्रश्नपत्र-4 (वैकल्पिक) पदार्थ विज्ञान शिक्षण के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
प्रश्न 6. सम्प्राप्ति परीक्षण क्या है? इसके उद्देश्यों को बताते हुये
इनकी विशेषताओं को बताइये एवं इनके कार्यों का वर्णन कीजिए।
अथवा
सम्प्राप्ति परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुये इसके उद्देश्यों को बताइये एवं
इसकी विशेषताओं व कायों को समझाइये।
1. सम्प्राप्ति परीक्षण की परिभाषा को बताइये।
2. सम्प्राप्ति परीक्षण के उद्देश्य बताइये।
3. सम्प्राप्ति परीक्षण की विशेषतायें बताइये।
4. सम्प्राप्ति परीक्षण के कार्य बताइये।
उत्तर-सम्प्राप्ति परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Achievement Test)
सम्प्राप्ति से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध,
कौशल आदि का मापन करते हैं। विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों
में विद्यार्थियों ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए सम्प्राप्ति
परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि किसी निश्चित
समयावधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा किसी एक या अनेक विषयों में
विद्यार्थी के ज्ञान व समझ में हुए परिवर्तन का मापन करने वाले उपकरणों को
सम्प्राप्ति परीक्षण अथवा उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। सम्प्राप्ति परीक्षण
प्राय: शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं तथा इनसे उद्देश्यों की
प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है। सम्प्राप्ति परीक्षण के अर्थ
को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का अवलोकन करना आवश्यक है -
गैरिसन एवं अन्य के अनुसार - "सम्प्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या
किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं।"
लिंडक्विस्ट एवं मन के अनुसार - "एक सामान्य सम्प्राप्ति परीक्षण वह है जो एक
ही फलांक द्वारा सम्प्राप्ति के किसी दिये हुए क्षेत्र में बालक के सापेक्षिक
ज्ञान का बोध कराये।"
एफ. एस. फ्रीमैन के अनुसार - “शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक
विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल
का मापन करता है।"
डी.ई. सुपर के अनुसार - "एक सम्प्राप्ति परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग
किया जाता है कि बालक ने क्या तथा कितना? सीख लिया है, अथवा वह कोई कार्य कितनी
अच्छी तरह से कर सकता है?
आर. एल. इबले के अनुसार - "सम्प्राप्ति परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों
के द्वारा ग्रहण किये गये ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है।"
हेनरी चोनसी के अनुसार - "प्रत्येक सम्प्राप्ति परीक्षण में विद्यार्थियों को
किसी न किसी रूप में अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का इस प्रकार प्रदर्शन करना
पड़ता है जिससे कि उसका अवलोकन तथा मूल्यांकन किया जा सके।"
सम्प्राप्ति परीक्षण के उद्देश्य
(Aims of Achievement Test)
सम्प्राप्ति परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं -
1. उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना।
2. विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना।
3. अध्ययन कार्य में सुधार लाना।
4. विद्यार्थियों को शैक्षिक मार्गदर्शन व परामर्श देना।
5. प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करना।
6. विद्यार्थियों के वर्गीकरण व प्रोन्नति में सहायता करना।
7. ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिये गये प्रशिक्षण के परिणामों का
मूल्यांकन करना। 8. शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का निर्धारण करना।
9. बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
10. शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाना।
11. विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता लगाना।
एक उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण की विशेषताएँ
(Characteristics of a Good Achievement Test)
एक उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण में लगभग वही विशेषताएँ निहित होनी चाहिए जो एक
उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए आवश्यक हैं। ये निम्नलिखित हैं -
1. उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण का निश्चित उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए।
2. उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण की पाठ्यवस्तु विद्यार्थियों के स्तर, रुचियों
एवं क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए जिससे वह उचित रूप से उपलब्धि कर सके।
3. उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी तथा धन, समय एवं
व्यक्ति के दृष्टिकोण से मितव्ययी होना चाहिए।
4. इसके प्रशासन, फलांकन एवं विवेचन की विधि सुगम, स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होनी
चाहिए जिससे एक मामूली अध्यापक भी इसका उपयुक्त प्रयोग कर सके।
5. इसकी विषय-सामग्री व्यापक होनी चाहिए अर्थात् जब किसी विषय पर सम्प्राप्ति
परीक्षण की रचना करनी हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय के समस्त क्षेत्रों
से पदों को परीक्षण में स्थान मिल रहा है या नहीं। उदाहरणार्थ, गणित के
सम्प्राप्ति परीक्षण में हमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी एवं
त्रिकोणमिति के समस्त क्षेत्रों से प्रश्नों को सम्मिलित करना होता है, तभी
हमारा परीक्षण व्यापक कहलायेगा।
6. उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि यह विभेदकारी होना
चाहिए जो किसी कक्षा के श्रेष्ठ एवं निम्न बालकों में विभेद कर सके।
7. उत्तम सम्प्राप्ति परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता से आशय है कि
आज वह जिस अमुक विद्यार्थी की उपलब्धि के विषय में इंगित करे, एक सप्ताह बाद भी
लगभग वही बात कहे।
8. इन सबके अतिरिक्त उसे वैध भी होना चाहिए अर्थात् अपने उद्देश्यों की पूर्ति
करने वाला होना चाहिए।
सम्प्राप्ति परीक्षण के कार्य
(Functions of Achievement Test)
सम्प्राप्ति परीक्षण को कई कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है इनमें कुछ
निम्नलिखित हैं -
1. सूचना स्रोत के रूप में (As a Source of Information) - सम्प्राप्ति
परीक्षणों के परिणाम विद्यालय के अभिलेख में प्रविष्ट किये जा सकते हैं तथा आगे
शिक्षा प्रदान करने तथा भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसर प्रदान
करने में मदद करते हैं।
2. अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना (Motivation and Direction for
Learning) - इनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित और
निर्देशित करना है। लगभग सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के अनुभव इस बात का
समर्थन करते हैं कि विद्यार्थी तब अधिक अध्ययन करते हैं जबकि वे एक परीक्षण की
आशा करते हैं अन्यथा नहीं। वे उन बातों को अध्ययन पर जोर देते हैं जिन्हें वे
समझते हैं कि परीक्षण में आयेंगे।
3. निर्देशकों या अध्यापक को लक्ष्य के समक्ष लाना (Bringing Instructors or
Teachers before Goal) - यह परीक्षण कार्य के प्रकार के रूप में उन उद्देश्यों
को क्रियान्वित रूप में परिभाषित करने में मदद करता है जिन्हें कि यह अध्यापक
या निर्देशक विद्यार्थी को लक्ष्यों को उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित करने में
सक्षम बनायेगा। विद्यार्थियों के अनुसार कक्षा परीक्षण लेना व इसके बाद उसके
प्राप्तांकों पर विचार-विमर्श उनके लिए एक बहुत पुरस्कृत अधिगम अनुभव हो सकता
है।
4. शैक्षिक स्तर पर बनाये रखना (Maintaining Educational Level) - शैक्षिक स्तर
बनाना उन्हें क्रियान्वित करना और भविष्य में उन स्तरों को तुलना का आधार बनाना
शिक्षाविदों का मुख्य उद्देश्य रहा है। अत: स्तर बनाये रखने का आधार स्कूल की
पढ़ाई और शैक्षिक अभियोग्यता है। परन्तु एक समान सामान्यीकृत स्तर लागू होने पर
उद्देश्य की पूर्ति न होकर हानि हुई। अनेक विद्यार्थी स्तर के समकक्ष न आने से
असफल एवं निराश हुए। इस अवस्था में सुधार हेतु हमें एक समान स्तरों के स्थान पर
ध्यानपूर्वक क्रमित विभेदकारी स्तर बनाना चाहिए जिससे निष्पत्ति स्तर अधिक
समन्वित हो सके।
5. शिक्षण विधि के चयन में सहायता देना (Providing Help in the Selection of
Teaching Method) - परीक्षाएँ विद्यार्थी को एक लम्बी अवधि में एकत्र सामग्री
को संगठित करने ' का अवसर प्रदान करती हैं। यदि उत्तर-पुस्तिकाओं को जाँच कर
उन्हें फिर वापस कर दिया जाए तो वे अपनी त्रुटियाँ जान जायेंगे। अध्यापक भी यह
जान जायेगा कि विद्यार्थी क्या बात नहीं समझ पाये हैं और तद्नुसार अध्यापन विधि
अपना लेंगे।
6. अध्यापक एवं विभागों का मूल्यांकन करना (Evaluation of Teachers and
Departments) - परीक्षा परिणामों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न
शिक्षा केन्द्रों में अध्यापन कितना प्रभावशाली है एवं विभिन्न विभागों की
स्थिति कैसी है। इस प्रकार शिक्षकों की कार्य कुशलता का तुलनात्मक अध्ययन किया
जा सकता है। अध्यापकों की कार्य कुशलता के आधार पर ही उनका चयन एवं पदोन्नति की
जा सकती है। स्वयं अध्यापक परीक्षा परिणामों का प्रयोग अपनी कमजोरियों का पता
लगाने और अपने अध्यापन का मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं।
7. शैक्षिक मार्गदर्शन करना (Educational Guidance) - जब तक हम विद्यार्थी की
योग्यता, अभिरुचियों, व्यक्तित्व, निष्पत्ति पृष्ठभूमि परिस्थितियाँ आदि के
बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम ठीक से नहीं बता सकते कि उसके लिए
कौन-सा विषय उपयुक्त है? अत: इस उद्देश्य हेतु परीक्षण की आवश्यकता होती है।
8. विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करना (Providing Opportunity to Discuss)
- परीक्षाओं में विद्यार्थी तीव्र गति से कार्य करता है। अत्यन्त अल्प समय में
उसे सभी सम्बन्धित तथ्यों को सोचना पड़ता है और उन्हें व्यक्त करना पड़ता है।
अत: अभ्यास के कारण उसकी विचार-शक्ति प्रबल होती है।
9. विभेदन शक्ति बढ़ाना (Increasing Differentiation Power) - अत्यधिक सामग्री
का संकलन होने पर परीक्षा प्रश्न के अनुरूप परीक्षार्थियों को उसमें काट-छाँट
करनी पड़ती है। अत: यह अधिक आवश्यक तथ्यों को लेता है और कम आवश्यक सामग्री का
परित्याग करता है। उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि कौन-से तथ्य आवश्यक हैं और
कौन से नहीं, इस प्रकार उसकी विभेदकारी शक्ति बढ़ती है।
10. पाठ्यवस्तु में संशोधन करना (Modification in Subject Matter) - पाठ्यवस्तु
के संशोधन में भी पूर्व परीक्षाओं के परिणाम सहायक होते हैं।
11. कक्षा-कक्ष की कठिनाइयों को जानने हेतु (For Knowing the Difficulties of
Classroom)- कक्षा-कक्ष में उत्पन्न विभिन्न स्तरों के बालकों की समस्याओं का
निदान उनका परीक्षण द्वारा विभेदीकरण करके किया जा सकता है।
|
|||||