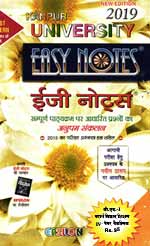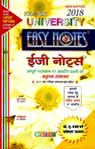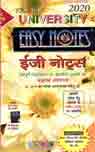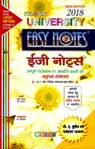प्रश्न 1. पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? पाठ योजना की निर्माण विधि
को बताते हुये इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा महत्व का वर्णन कीजिए।
अथवा
पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुये इसकी प्रमुख विशेषताओं व महत्व का उल्लेख
कीजिए।
1. पाठ योजना का अर्थ बताइए।
2. पाठ योजना की निर्माण विधि का वर्णन कीजिए।
3. एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएँ लिखिए।
4. पाठ योजना का महत्व लिखिए।
उत्तर-पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Lesson Plan)
'पाठ योजना' में दो शब्द - पाठ और योजना शामिल हैं। पाठ योजना का अभिप्राय उस
पूर्व निर्धारित योजना से है जिसके अनुसार शिक्षक नये ज्ञान को रीतियों एवं
सहायक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने एक निश्चित अवधि के अन्दर
प्रस्तुत करता है। पाठ योजना एक आलेख है जिसमें शिक्षक एक निश्चित समय में
पाठ्यवस्तु के बारे में निर्धारित लक्ष्यों के रूप में विद्यार्थियों को
जानकारी देता है।
"पाठ योजना वह एक ब्लू प्रिन्ट है जिसमें शिक्षक सृजनात्मक कार्य करता है।"
"शिक्षण-अधिगम व्यवस्था में विभिन्न शिक्षण क्रियाओं के क्रमबद्ध उपागम को पाठ
योजना कहते हैं।"
दैनिक पाठ योजना वर्तमान में उप-इकाई के कक्षा शिक्षण की योजना है। आज की दैनिक
पाठ योजना का आधार इकाई योजना ही है। अत: कहा जा सकता है कि इकाई योजना का
क्रियान्वयन दैनिक पाठ योजना द्वारा होता है। पाठ योजना एवं इकाई योजना से ही
शिक्षण सम्बन्धी विषयवस्तु, उद्देश्य, विधियाँ, प्रविधियाँ, उपक्रम आदि उपलब्ध
होते हैं।
पाठ योजना का आविर्भाव गैस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा माना जाता है। अधिगम के
अन्तर्गत गैस्टाल्ट अधिगम सिद्धान्त का प्रयोग अधिक प्रभावशाली माना जाता है।
इसमें सम्पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण के नियम को ध्यान में रखा जाता है। इसी के
आधार पर छात्र सम्पूर्ण को समझने के लिए इकाई लेता है क्योंकि यह पूर्व से अंश
की ओर के नियम को भी मानता है अतः पाठ योजना में सम्पूर्ण का सम्प्रेषण इकाईयों
में बाँटकर किया जाता है। जैक्सन महोदय ने इसे पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से
पुकारा है, अर्थात् इसमें शिक्षक की वह सब तैयारी सम्मिलित हैं जो वह कक्षा में
जाने से पूर्व सम्बन्धित पाठ योजना के विषय में करता है। पाठ योजना में वस्तुत:
'क्या पढ़ाना है', कैसे पढ़ाना है', तथा उसके मूल्यांकन' को पूर्ण रूप से
उल्लेखित किया जाता है।
इसी प्रकार आई. के. डेवीस ने अपने प्रथम सोपान में पाठ योजना की रचना को विशेष
बल दिया है। -"शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यावहारिक रूप से आलेख ही पाठ
योजना है।"
एन.एल.बोसिंग (N.L. Bossing) के अनुसार - "पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें
शिक्षक कक्षा के अन्तर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के
द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है।"
एल. बी. सैन्ड्स (L.B.Sands) के अनुसार - "पाठ योजना वास्तव में किये जाने वाले
कार्य की एक योजना है। इसके अन्तर्गत शिक्षक के अपने कार्य करने के ढंग से
सम्बन्धित दर्शन, दर्शन सम्बन्धित उसके ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के सम्बन्ध
में उसकी जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों से सम्बन्धित उसकी समझ, विषयवस्तु
सम्बन्धी उसके ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों को प्रयोग में लाने सम्बन्धी उसकी
योग्यता आदि सभी बातों का समावेश होता है।"
जोसेफ लैन्डन (Joseph Landon) के अनुसार - “पाठ योजना को हम कागज पर स्पष्ट रूप
से अंकित की जाने वाली पाठ की रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं जिसमें पाठ से
सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से आ जाते हैं, चाहे उनका सम्बन्ध
विषय-सामग्री से हो या विधि से।"
उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर पाठ योजना की निम्नलिखित परिभाषा
दी जा सकती है-
"पाठ योजना एक अभिकल्प है जो कक्षा में क्रियान्वित होती है। यह एक रूपरेखा है,
मार्गदर्शक नक्शा है, निकट भविष्य में प्रयोग में आने वाली कार्ययोजना है,
सृजनात्मक कार्य की एक भाषा है तथा कक्षा में एक कालांश शिक्षण के लिए व्यापक
योजना है।"
पाठयोजना का निर्माण
(Construction of Lesson Plan)
जे. एफ. हरबर्ट ने पाठ-योजना के निम्नलिखित पाँच चरणों का उल्लेख किया है-
(1) तैयारी (Preparation)- छात्रों में पाठ्य-वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने
के उद्देश्य से एक आकर्षक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसमें चार्ट्स व मॉडल आदि
का प्रयोग करना चाहिए।
(2) प्रस्तुतीकरण (Presentation) - इसके अन्तर्गत नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने
की विधियाँ आती हैं। यह एक प्रमुख अंग है क्योंकि इसमें छात्रों को पाठ्य-वस्तु
से परिचित कराया जाता है। अध्यापक को प्रभावी शिक्षण के लिए सहायक सामग्री जैसे
चार्ट व श्याम-पट आदि का प्रयोग करना चाहिए।
(3) तुलना (Comparison)- छात्रों को नवीन ज्ञान की तुलना पूर्व ज्ञान से करानी
चाहिए तभी ज्ञान उनके बौद्धिक परिवर्तन का स्थायी अंग बन सकता है।
(4) सामान्यीकरण (Generalization) - विज्ञान विषय के लिए यह आवश्यक अंग है।
विज्ञान के नियमों एवं सिद्धान्तों को विद्यार्थियों को समझाने के लिए उनका
सामान्यीकरण करना चाहिए।
(5) अनुप्रयोग (Application)- शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के उपरान्त उसके अभ्यास
प्रश्न छात्रों को कराने चाहिए। शिक्षक द्वारा सभी छात्रों द्वारा किए गए कार्य
का निरीक्षण करना चाहिए और उनकी गलतियों को ध्यान से देखकर उनका सुधार करना
चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छे कार्य के लिए छात्रों की प्रशंसा भी करनी चाहिए।
पाठ योजना की विशेषताएँ
(Characteristics of Lesson Plan)
पाठ योजना की विशेषताएँ अग्रवत हैं -
1. उद्देश्य पर आधारित (Objective Based) - पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर
आधारित होनी चाहिए। इसको लिखते समय उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लिखते समय
उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित भी कर देना चाहिए।
2. उत्पन्न सहायक सामग्री के सम्बन्ध में निर्णय (Decision about Appropriate
Material Aid) - आदर्श पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को चार्टी, ग्राफों,
चित्रों तथा रेखाचित्रों एवं मानचित्रों आदि उपयुक्त सहायक सामग्री के सम्बन्ध
में उचित निर्णय लेकर उसे यथास्थान अंकित करना चाहिए जिसे शिक्षण के समय प्रयोग
करना है।
3. पूर्व ज्ञान पर आधारित (Based on Previous Knowledge)- आदर्श पाठ योजना
विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों को
नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
4. पाठ योजना का सोपानों में विभाजन (Division of Lesson Plan into Units). पाठ
तीन प्रकार के होते हैं - (i) ज्ञान पाठ, (ii) कौशल पाठ, (iii) रसानुभूति के
पाठ। आदर्श पाठ योजना में उक्त तीनों प्रकार के पाठों के अनुकूल आवश्यक पद
निर्धारित करने चाहिए। प्रत्येक पाठ को उचित सोपानों में विभाजित कर देना चाहिए
जिससे पाठ थोड़ा-थोड़ा करके विद्यार्थियों की समझ में सरलतापूर्वक आ जाये।
5. भाषा की सरलता (Simplicity of Language)- आदर्श पाठ योजना में भाषा की सरलता
तथा भावों की स्पष्टता विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ
योजना, भाषा-प्रधान न होकर विषय-प्रधान होनी चाहिए।
6. क्रियाओं का निर्धारण (Determination of Activities) - आदर्श पाठ योजना में
यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि शिक्षण के प्रत्येक पद पर शिक्षक तथा
विद्यार्थियों को कौन-कौन सी क्रियाएँ करनी हैं। पाठ योजना के अन्तर्गत शिक्षक
तथा विद्यार्थी दोनों की क्रियाएँ पहले से ही निर्धारित कर देनी चाहिए।
7. विधियों अथवा नीतियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा उपकरणों का प्रयोग (Use of
Strategies, Tactics, Techniques and Teaching Aids) - आदर्श पाठ योजना तैयार
करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह मनोविज्ञान, शिक्षण सूत्रों तथा शिक्षण को
सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करे। तभी वह विभिन्न परिस्थितियों में
होने वाली घटनाओं तथा तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त विधियों अथवा
नीतियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा उपकरणों का उचित प्रयोग कर सकेगा।
8. समन्वय (Correlation) - आदर्श पाठ योजना में यथासम्भव समन्वय भी स्थापित
करना चाहिए जिससे विद्यार्थी ज्ञान को समग्र रूप से प्राप्त कर सके।
9. उदाहरणों का प्रयोग (Use of Illustrations) - आदर्श पाठ योजना में ऐसे
उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए जिनका सम्बन्ध विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से
हो।
10. व्यक्तिगत पथ-प्रदर्शन (Individual Guidance) - आदर्श पाठ योजना में इस बात
का संकेत मिलना चाहिए कि शिक्षक विद्यार्थियों का व्यक्तिगत पथ-प्रदर्शन कब और
कैसे करेगा।
11. स्मृति स्तर से चिन्तन स्तर तक शिक्षण (Teaching from Memory Level to
Reflective Level) - आदर्श पाठ योजना में विकासात्मक तथा विचारात्मक प्रश्नों
का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण कार्य को स्मृति स्तर से चिन्तन तक पहुँचाने का
प्रयास करना चाहिए।
12. समय का ध्यान (Time Sense) - आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के मानसिक स्तर
तथा कालांश की अवधि को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। उसमें यह बात भी स्पष्ट कर
देना चाहिए कि शिक्षण के किस पद पर कितना समय लगने की सम्भावना है।
13. श्यामपट का प्रयोग (Use of Blackboard) - आदर्श पाठ योजना में श्यामपट
सारांश का विकास साथ-साथ अथवा बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्मरण
रहे कि पाठ योजना को जितने सोपानों में विभाजित किया जायेगा, प्रत्येक सोपान को
पढ़ाने के तुरन्त पश्चात् श्यामपट सारांश श्यामपट पर संक्षिप्त किन्तु पूर्ण
वाक्यों में लिखना चाहिए।
14. मूल्यांकन (Evaluation) - आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों पर पड़े हुए
प्रभाव को जानने की विधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इससे शिक्षक द्वारा
उपयोग की गई विधियों का मूल्यांकन भी हो जायेगा तथा विद्यार्थी भी सीखने में
रुचि लेने लगेंगे।
15. गृहकार्य (Homework)- आदर्श पाठ योजना में गृहकार्य की व्यवस्था भी होनी
चाहिए। इससे विद्यार्थी अर्जित किये हुए ज्ञान का उचित प्रयोग करना सीख
जायेंगे।
पाठ-योजना का महत्व
(Importance of Lesson Plan)
पाठ योजना का महत्व निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है -
1. उपयुक्त वातावरण (Suitable Environment)- पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के
उद्देश्यों को निश्चित करते हुए शिक्षण की विधियाँ अथवा नीतियाँ , युक्तियाँ ,
प्रविधियाँ तथा सहायक सामग्री आदि सभी बातों पहले से ही निश्चित हो जाती है।
इससे विद्यार्थियों की पाठ में रुचि उत्पन्न होती है तथा विज्ञान के लिए
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायता मिलती है। जब उपयुक्त अथवा शैक्षिक
वातावरण तैयार हो जाता है तो शिक्षण बड़े नियोजित ढंग से चलता रहता है।
2. पूर्वज्ञान पर आधारित (Based on Previous Knowledge)- पाठ योजना बनाने में
शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता
है। इससे जहाँ एक ओर विद्यार्थी ज्ञान को सहज ही में ग्रहण कर लेते हैं वहीं
दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है।
3. मनोवैज्ञानिक शिक्षण (Psychological Teaching) - पाठ योजना बनाकर शिक्षक
विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं,
क्षमताओं तथा योग्यताओं को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण-नीतियों,
प्रविधियों, युक्तियों तथा उपकरणों का उपयोग करता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक
हो जाता है।
4. विषय-सामग्री का सीमित होना (Limited of Subject-matter) - पाठ योजना में
विषय-सामग्री परिमित एवं सीमित हो जाती है। इससे जहाँ तक ओर शिक्षक को अनावश्यक
बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित तथा सीमित बातों को याद करने तथा उन्हें
विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है वहीं दूसरी ओर
विद्यार्थियों को भी ज्ञान क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में प्राप्त हो जाता है।
5. क्रियाओं का निश्चित होना (Determination of Activities) - पाठ योजना में
शिक्षक तथा विद्यार्थियों की क्रियायें कक्षा स्तर के अनुसार पहले से ही
निश्चित हो जाती हैं। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पहले से ही निश्चित कर लेता
है कि उसे तथा कक्षा के विद्यार्थियों को क्या-क्या करना है। इससे शिक्षण की
क्रियाएँ सार्थक तथा सोद्देश्य बन जाती हैं। परिणामस्वरूप शिक्षक तथा
विद्यार्थी दोनों ही पक्ष पाठ को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने
लगते हैं।
6. सहायक सामग्री की तैयारी (Preparation of Material Aids) - पाठ योजना बनाते
समय शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि वह कौन-कौन से तथ्यों को कौन-कौन सी
विधियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए
किस-किस सहायक सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। इसमें आवश्यक एवं
प्रभावोत्पादक सहायक सामग्री शिक्षण आरम्भ होने से पहले ही तैयार हो जाती है।
7. शिक्षण कौशल का विकास (Development of Teaching Skill) - पाठ योजना
छात्र-शिक्षकों के अन्दर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षक-शिक्षा में
महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है।
8. शिक्षण में सैद्धान्तिक ज्ञान का प्रयोग (Use of Theoretical Knowledge in
Teaching)- छात्र-शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में जो कुछ तथा जितना सैद्धान्तिक
ज्ञान दिया जाता है उसको कक्षा शिक्षण में केवल पाठ योजना की सहायता से ही
प्रयोग किया जा सकता है। पाठ योजना सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप प्रदान
करने में सहायता प्रदान करती है।
9. चिन्तन में क्रमबद्धता तथा विकास (Orderliness and Development in
Thinking)- पाठ योजना तैयार करने से शिक्षक की चिन्तन प्रणाली में क्रमबद्धता
विकसित हो जाती है। इससे वह शिक्षण के समय पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप में
प्रस्तुत करते हुए शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है।
10. शक्ति तथा समय की बचत (Economy of Energy and Time) - जो शिक्षक पाठ योजना
बनाये बिना ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर देता है वह सदैव इधर-उधर भटकता फिरता
है। उसे विषय-वस्तु प्रस्तुत करने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है तथा समय भी
व्यर्थ नष्ट होता है। इसके विपरीत जो शिक्षक शिक्षण से पहले पाठ योजना बना लेता
है, वह नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करके विद्यार्थियों की शंकाओं
का समाधान भी उन्हीं की सहायता से सरलतापूर्वक कर देता है।
11. आत्मविश्वास के साथ शिक्षण (Teaching with Confidence) - पाठ योजना बनाने
में शिक्षक को अपने विषय तथा उससे सम्बन्धित सभी विषयों का स्पष्ट ज्ञान हो
जाता है। इससे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अब वह विद्याथियों के
सामने नवीन ज्ञान को उत्साह तथा स्वाभाविकता के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत
करता है।
12. कक्षा में अनुशासन (Discipline in Class)- पाठ योजना बनाने से शिक्षक को इस
बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में क्या, कितना और कब-कब करना है।
इससे सभी विद्यार्थी अपने-अपने कार्य में लगे रहते हैं जिससे कक्षा में
प्रशंसनीय अनुशासन बना रहता है।
13. ज्ञान का स्थायित्व (Fixation of Knowledge) - पाठ योजना में शिक्षक पाठ का
सारांश भी लिखता है। पाठ के सारांश को पढ़ने से विद्यार्थियों को पाठ दोहराने
में सहायता मिलती है और ज्ञान भी स्थाई हो जाता है।
14. मूल्यांकन सम्भव (Evaluation Possible) - पाठ योजना में मूल्यांकन का विधान
भी, होता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को इस बात का पता आसानी से लग जाता है कि
उसके शिक्षण का विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इससे शिक्षक द्वारा
प्रयोग की गई विधियों एवं नीतियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का
मूल्यांकन भी एक साथ हो जाता है। यदि शिक्षक यह देखता है कि उसके द्वारा प्रयोग
की गई शिक्षण नीतियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा उपकरणों का विद्यार्थियों पर
वांछनीय प्रभाव नहीं पड़ा तो वह इनमें आवश्यक सुधार कर सकता है। इस प्रकार पाठ
योजना द्वारा शिक्षक की शिक्षण नीतियों, प्रविधियों तथा उपकरणों एवं उनके
प्रभावों का मूल्यांकन सम्भव है।
...Prev | Next...