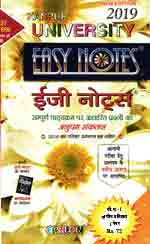|
इतिहास >> ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्रईजी नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
प्रश्न 3. प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख
कीजिए।
अथवा
समुद्रगुप्त की दक्षिणी-भारत की विजयों का वर्णन कीजिए।
अथवा
समुद्रगुप्त की उत्तरी-दक्षिणी भारत की विजयों का वर्णन कीजिए।
अथवा
दक्षिण विजय में समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन कीजिए।
अथवा
गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त के आर्यावर्त की विजय का उल्लेख कीजिए।
अथवा
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
अथवा
समुद्रगुप्त के आर्यावर्त /उत्तरापथ अभियान के विषय में आप क्या जानते हैं ?
अथवा
समुद्रगुप्त के अभियान की चर्चा कीजिए और समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का
उल्लेख कीजिए।
अथवा
समुद्रगुप्त के आर्यावर्त अभियान का विवरण दीजिए।
अथवा
समुद्रगुप्त के जीवन तथा उसके दक्षिणापथ अभियान का उल्लेख कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय
प्रश्न 1. समुद्रगुप्त का काल निर्णय बताइए।
2. समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन कीजिए।
3. पूर्व के प्रत्यन्त राज्यों का वर्णन कीजिए।
4. पश्चिम राज्य का वर्णन कीजिए।
5. समद्रगुप्त की उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
6. समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय पर प्रकाश डालिए।
7. प्रयाग प्रशस्ति के विषय में बताइए।
8. प्रयाग प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं ?
9. समुद्रगुप्त के उत्तरापथ अभियान के राजाओं का उल्लेख कीजिए।
10. प्रयाग प्रशस्ति से किस राजा के जीवन तथा व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है।
उत्तर-समुद्रगुप्त
चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा।
समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त के अनेक बेटों में से एक था। जैसाकि पूर्व
वृतान्तों से ज्ञात होता है कि उसे उसके पिता ने भरी सभा में अपना
उत्तराधिकारी शासक मनोनीत किया था, किन्तु आरम्भ में उसे अपने भाइयों के
विद्रोह का, जिसका नेतृत्व सम्भवतः काच ने किया था, सामना करना पड़ा था। अपने
विद्रोही भाई काच को परास्त कर चुकने के बाद समुद्रगुप्त ने तत्कालीन उत्तर
भारत में बिखरे हुए छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति सुदृढ़ करने की ओर
ध्यान दिया और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित कर एकराष्ट्र बनाने का प्रयत्न
किया। विजय अभियान की उसने जो विशाल योजना बनायी थी उसका विशद उल्लेख प्रयाग
प्रशस्ति में प्राप्त होता है।
प्रयाग, प्रशस्ति के रचनाकार - प्रयाग प्रशस्ति (लोहरसभा) पर उत्कीर्ण
प्रशस्ति को महादण्डनायक ध्रुभूति के पुत्र महाकवि हरिवेण ने रचा था। वह
स्वयं महामात्य था और खाद्यतपादिक, सन्धिविग्राहक, महादण्डनायक के पदों पर
आसीन था। सम्भवतः वह राजा के साथ विजय अभियान में गया था। इस प्रकार तत्कालीन
घटनाओं से उसका निकट का परिचय था। उसने न केवल सामान्य ढंग से शत समर में
सम्राट की योग्यता का, जिसके कारण उसके शरीर में घावों के निशान थे, सामान्य
रूप से उल्लेख किया है वरन् एक-एक शत्रु का भी नामोल्लेख भी किया है जिनसे
उन्हें लड़ना पड़ा था। उसके इस लेख को इतिहास के प्रामाणिक साधन के रूप में
ग्रहण किया और उसके विवरण को सत्य कहा जा सकता है।
यह अभिलेख प्रयाग (इलाहाबाद) के कौशाम्बी के लौह स्तम्भ पर उत्कीर्ण किया गया
है। कौशाम्बी के बाद में इसे इलाहाबाद के किले में गाड़ दिया गया था। इसी
स्तम्भ के दूसरी ओर सम्राट अशोक का शान्ति सन्देश भी उत्कीर्ण है। फ्लीट
महोदय ने इसे समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् लिखा गया माना है। परन्तु इस
अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा सम्पादित अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है जब
कि अन्य अभिलेखों तथा मुद्राओं पर अश्वमेध का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता
है कि इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय से लौटने तथा अश्वमेध
यज्ञ करने से पहले हुई थी।
प्रयाग प्रशस्ति - प्रयाग प्रशस्ति का प्रथम भाग पद्य में है तथा इसमें आठ
श्लोक हैं। इससे पहले के दो श्लोक नष्ट हो गये हैं। फिर भी उनसे पता चलता है
कि समुद्रगुप्त एक योग्य विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता तथा विद्वानों की
संगति में रहने वाला विद्वान और संगीतशास्त्र का ज्ञाता था। चौथे श्लोक में
उसके उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने पर कुछ व्यक्तियों के ईष्र्यावश चेहरे
पीले पड़ गये थे का उल्लेख है। सातवें तथा आठवें श्लोक में समुद्रगुप्त के
विजय अभियान का वर्णन है, 13वीं पंक्ति में उत्तरी भारत के तीन राज्यों को
परास्त करने का उल्लेख है। 19वीं तथा 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त की
दक्षिणी विजय का उल्लेख है। 21वीं तथा 13वीं पंक्ति में राजाओं के समर्पण का
उल्लेख है। 23वीं, 24वीं पंक्ति में उन अनेक विदेशी शासकों के नाम हैं
जिन्होंने समुद्रगुप्त को उपहार आदि दिये।
उत्तराधिकार का निर्णय - समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के सम्बन्ध में प्रयाग
प्रशस्ति से बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। प्रशस्ति की चौथी पंक्ति समुद्रगुप्त
प्रथम के दरबार के दृश्य का वर्णन करती है। प्रयाग प्रशस्ति से ऐसा आभास होता
है कि चन्द्रगुप्त ने खुले दरबार में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना।
इस प्रकार की आवश्यकता सम्भवतः इस कारण से हुई कि चन्द्रगुप्त के अन्य पुत्र
रहे होंगे और उनमें परस्पर युद्ध की सम्भावना को समाप्त करने के विचार से
चन्द्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को युवराज चुना, दूसरे समुद्रगुप्त के दरबार में
उत्तराधिकारी चुना जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राचीन गणराज्य
परम्परा में राजा का चुनाव होता था। इस प्रशस्ति की सातवीं पंक्ति में यह
बतलाया गया है कि -
आर्यो हीत्युपगुह्य भाव विशुनैः उत्कीणिति रोमभिः।
सभ्येष्वच्छवषु तुल्य कुलजग्लान नोद्वोक्षित।।
स्नेहव्याकुलितेन वाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुषा।
यः पिता भिहतो निरीक्ष्य निखिलां पाह्येव मूर्वीमिति॥
समुद्रगुप्त के समान पद वाले राजकुमारों के मुख म्लान हो गये और उसके विपरीत
सभासद हर्ष से उद्दवसित हो रहे थे। डा. अल्तेकर का कथन है कि प्राचीन भारत
में उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर किसी दूसरे
को चुना जाता था। चन्द्रगुप्त को यह आभास हो गया होगा कि दरबार में कुछ
व्यक्ति समुद्रगुप्त के विरोधी भी हो सकते हैं क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र नहीं
था। इसके साथ ही सम्भवतः उसे यह भी डर था कि समुद्रगुप्त लिच्छवि राजकुमारी
का पुत्र था जोकि ब्राह्मण ग्रन्थों के नियम के अनुसार व्रात्य क्षत्रिय थे।
यह व्रात्य क्षत्रिय बौद्ध तथा जैन जैसे विरोधी मतों को मानने वाले थे। इस
प्रकार समुद्रगुप्त के चुने जाने पर ब्राह्मण मतावलम्बियों के स्वाभाविक
विरोधी होने की सम्भावना थी।
डा. मजूमदार प्रयाग प्रशस्ति से सम्भवतः यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि
समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकार के निर्णय के पश्चात् सिंहासन भी त्याग दिया। इस
समुद्रगुप्त की अवस्था अवश्य ही परिपक्व थी और वह राज्यभार सम्भालने योग्य
थी। इस प्रकार शान्तिपूर्वक शक्ति हस्तान्तरण भी सम्पन्न हो सका।
समुद्रगुप्त का काल निर्णय - समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तिथि के विषय
में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। कृत्रिम नालन्दा पत्र के अनुसार
समुद्रगुप्त ने 325 ई. के पहले राज्य पद प्राप्त किया। कुछ विद्वान
समुद्रगुप्त को गुप्त सम्वत् का संस्थापक मानते हैं। इसलिए वे उसकी तिथि 320
ई. निर्धारित करते हैं। डा. आर. सी. मजूमदार उसकी तिथि 140 से 320 ई.
निर्धारित करते हैं। डा. वी. एन. स्मिथ 320 ई. से 375 ई. के बीच उसका समय
निर्धारित करते है। डा. आर. के. मुकर्जी उसकी तिथि 335 ई. मानते हैं।
उन्होंने लिखा है कि -
"His regime is roughly taken to begin from 335 A. D. otherwise it becomes
too long, its length also depends on his age, the date of his birth may be
taken to become to the throne at 25, the legal age of kingship in 335
A.D.'
नालन्दा और गया के तिथियुक्त दानपत्र शायद गुप्त सम्वत् के पंचवें तथा नवें
वर्ष अंकित किये गये थे। इस आधार पर समुद्रगुप्त का शासन प्रबन्ध 324-25 ई.
से आरम्भ हुआ माना जाना चाहिए। चन्द्रगुप्त द्वितीय की मथुरा प्रशस्ति उसकी
प्रारम्भिक प्रशस्ति है। उसका समय गुप्त सम्वत् के 16वें वर्ष माना जाता हैं।
इसलिए समुद्रगुप्त का शासनकाल (319 + 61) - 380 ई. तक अवश्य ही समाप्त हो गया
होगा।
समुद्रगुप्त की दिग्विजय - उत्तराधिकार युद्ध से निवृत होकर समुद्रगुप्त ने
अपनी शक्ति का संगठन किया और दिग्विजय का बीड़ा उठाया। उसने उत्तरी तथा
दक्षिणी भारत के राजाओं को पराजित करके अपनी सार्वभौम सत्ता की स्थापना की,
जो नरेश शेष रह गये उन्होंने उसके पराक्रम से आतंकित होकर या तो अपनी अधीनता
स्वीकार कर ली या उसके साथ मित्रता कर ली। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति
में हरिवेण द्वारा सम्पूर्ण दिग्विजय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।
प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजय नीति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो निम्न
प्रकार समझा जा सकता है -
1. राज्यग्रहण मोक्षानुग्रह - इससे तात्पर्य यह है कि राज्यों को जीतकर उनको
मुक्त करके अनुग्रहीत किया अर्थात् वहाँ पुराने शासकों को ही राज्य लौटा दिया
गया। इस विशिष्ट नीति का पालन दक्षिणापथ राज्यों के लिए किया गया।
2. राज्य प्रसमाद्दकरण - इसका तात्पर्य यह है कि समुद्रगुप्त ने नये राज्यों
को जीतकर बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लिया, यह नीति आर्यावर्त के राज्यों
के लिए प्रयोग में लायी गयी।
3. प्रचारकृत - इसका अर्थ है कि सेवक बनाना । यह नीति मध्य भारत के आटविक
राज्यों के के साथ अपनाई गयी थी।
4. करदानाज्ञाकरण प्रणामागमन - इसका अर्थ है कर एवं दान देना और आज्ञा का
पालन करना तथा सम्राट के अभिवादन हेतु आना। यह नीति सीमा स्थित राजाओं तथा
गणराज्यों के प्रति अपनायी गयी थी।
5. भ्रष्ट राज्योत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठा - हारे हुए राज्यों को पुनः
प्रतिष्ठापित करने की नीति का । प्रयोग भी दक्षिणापथ पर किया गया है।
6. आत्म-निवेदन कन्योपायनदान गरुड़ मद अङ्क स्व विषयमुक्ति शासन - इसका अर्थ
है कि कुछ राजाओं ने आत्मसमर्पण किया। कन्याओं का विवाह तथा अपने विषय तथा
मुक्ति में (जिला व प्रान्त) शासन के निमित्त गरुड़ की मुद्रा में अंकित
(गुप्तवंशीय चिन्ह) आज्ञापत्र की याचना की। इस नीति का पालन विदेशी राजाओं के
साथ किया था।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त ने दूरस्थ देशों के
राजाओं के साथ जिस नीति का अनुशीलन किया वह उसकी बुद्धिमत्ता एवं कूटनीति का
परिचायक थी।
समुद्रगुप्त की उत्तरापथ विजय अथवा आर्यावर्त विजय अभियान - समुद्रगुप्त ने
अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में उत्तर भारत में दो बार युद्ध किये। इंन
युद्धों को क्रमशः आर्यावर्त का 'प्रथम' तथा 'द्वितीय युद्ध कहा जाता है।
इनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के
राजाओं का विनाश कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रयाग
प्रशस्ति की इक्कीसवीं पंक्ति में आर्यावर्त के नौ राजाओं का उल्लेख हुआ है
जिनका विवरण निम्नवत् है -
1. रुद्रदेव - इस राजा को अब तक समस्त इतिहासकार रुद्रसेन (प्रथम) समझते रहे
हैं अथवा उसके प्रति अपनी अनभिज्ञता के भाव ही व्यक्त करते रहे हैं। इधर हाल
में दिनेश चन्द्र सरकार ने यह मत प्रतिपादित किया है कि रुद्रदेव की पहचान
पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदामन (द्वितीय) अथवा उसके पुत्र रुद्रसेन (तृतीय) से की
जानी चाहिए, किन्तु जैसाकि ऊपर इंगित किया जा चुका है कि वाकाटक रुद्रसेन (
प्रथम ) दक्षिण का राजा था। कौशाम्बी से रुद्रदेव की कुछ मुद्रायें प्राप्त
हुई हैं जिससे ज्ञात होता है कि रुद्रदेव वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम है।
परन्तु रुद्रदेव जो भी रहा हो यह सत्य है कि वह आर्यावर्त का शासक था तथा
समुद्रगुप्त ने इसे पराजित किया था।
2. मतिल - फ्लीट और ग्राउस का कहना है कि बुलन्दशहर से प्राप्त मिट्टी की
मुहर पर जो मतिल नाम है, वही यह मतिल है। उनके इस कथन को सभी इतिहासकारों ने
स्वीकार किया है किन्तु यह पहचान काफी संदिग्ध है। एलन ने उचित रूप से इस ओर
ध्यान आकृष्ट किया है कि इस मुहर में कोई उपाधि नहीं है जिससे कहा जाय कि
उसका स्वामी किसी रूप में सत्ताधारी था । उपाधि के अभाव में तो यह भी नहीं
कहा जा सकता है कि वह कोई छोटा-मोटा राजा रहा होगा। सम्प्रति मतिल और उसके
प्रदेश के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती।
3. नागदत्त - मथुरा के निकट बहुत-सी ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनमें
उत्कीर्ण नामों के अन्त में 'दत्त' शब्द आया है। नागदत्त के नाम के अन्त में
भी दत्त होने के कारण बहुत कुछ सम्भव है कि नागदत्त मथुरा के आसपास ही कहीं
राज्य करता होगा। परन्तु दत्त वंश के साथ उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ भी
ज्ञान नहीं हुआ। डा. जायसवाल इसे ई. 328-349 के लगभग नागवंश का शासक मानते
हैं। राजा महाराजा महेश्वर नाग का पिता तथा अन्य नागों का सरदार था । इसकी एक
मुहर नाग लच्छन के साथ लाहौर से प्राप्त हुई और फ्लीट ने उसका सम्पादन भी
किया।
4. चन्द्रवर्मा - पूर्वी बंगाल में बाकुड़ा जिले के सुसनियाँ पर्वत से
प्राप्त एक शिलालेख पर 'चन्द्रवर्मा' शब्द उत्कीर्ण है। इस आधार पर
चन्द्रवर्मा को बाँकुड़ा प्रदेश में स्थित पुष्कण का राजा माना जाता है। डा.
हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार पुपकरण मारवाड़ में स्थित था ।
डा. जायसवाल के अनुसार चन्द्रवर्मा पूर्वी पंजाब का राजा था। कपितय विद्वान
उसे महरौली स्तम्भ का 'चन्द्र' मानते हैं। मत वैभिन्य के कारण चन्द्रवर्मा के
विषय में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है।
5. गणपतिनाग- गणपतिनाग के नाम से ही पता चलता है कि यह कोई नागवंशीय नरेश था
। यह सम्भवतः नागों की राजधानी पद्मावती में ई. 310-344 तक शासन करता था। इस
राजा के सिक्के मारवाड़ तथा बेसनगर के समीप मिले हैं। डा. भण्डारकर का मत है
कि यह राजा नागों की विदिशाखा था। इसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है।
6. नागसेन - प्रयाग प्रशस्ति में नागों की सूची में पहले ही इसका उल्लेख हुआ
है । हर्षचरित में भी इसका उल्लेख इस प्रकार हुआ है।
"नागाकुल जन्मनः सारिका श्रवित मन्त्रस्थ अशीत नागों नाससेनस्य पद्मावत्याम्
॥'
विद्वानों का मत है कि गणपतिनाग के समय नागों की दूसरी शाखा पर राज्य कर रहा
है। रैप्सन महोदय भी प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित और हर्षचरित के नाम को एक ही
मानते हैं। परन्तु डा. जायसवाल नागसेन को मथुरा का नागवंशीय शासक बतलाते हैं।
7. अच्युत अच्युत कौन था और कहां का राजा था इस विषय में पर्याप्त मतभेद है।
अच्युत बरेली जिले में अहिछत्र नामक स्थान का शासक था । वहाँ से बहुत-सी ऐसी
मुद्राएं मिली हैं जिन पर अच्युत शब्द पढ़ने को मिला है। डा. भण्डारकर ने
उनकी बनावट के आधार पर पद्मावती की नाग मुद्राओं से समानता प्रकट की है।
8. नन्दि यह भी सम्भवत: नागवंशीय नरेश था। पुराणों में शिशुनन्दि और नन्दिशसू
को मध्य भारत का नागवंशीय नरेश बताया गया है। शिवनन्दि नामक एक राजा का वर्णन
हुआ है। इब्रील महोदय नन्दि तथा शिवनन्दि की एकता को सिद्ध करते हैं। यह
ध्यान देने का विषय है कि गुप्त राजाओं का राजकीय चिह्न गरुड़ था। गरुड़ को
नागों का शत्रु समझा जाता है। संभवतः इसी कारण गुप्त शासकों ने गरुड़ को
राजकीय चिह्न बनाया।
9. बलवर्मा- प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के शासकों में अन्तिम शासक
बलवर्मा था। कुछ विद्वान इसे कोट कुलज मानते हैं। यह सम्भवतः असम का राजा हो
सकता है जो हर्ष के समकालीन भास्करवर्मन से नौपीढ़ी पूर्व का था। इसे स्वीकार
करने में बड़ी कठिनाई है क्योंकि असम आर्यावर्त में सम्मिलित नहीं था, उसका
वर्णन पृथक रूप से आया है। डा. जायसवाल ने अच्युत तथा नन्दि एक ही शासक के दो
नाम बताये हैं अतः नन्दि को नागवंशीय शासक मानना ही उचित होगा।
आर्यावर्त विनय में इस बात का संकेत नहीं मिलता कि यहाँ के शासकों ने
समुद्रगुप्त के विरुद्ध किसी प्रकार के संघ का निर्माण किया हो। आगरा, देहली,
पंजाब आदि के कुछ भागों को छोड़कर उत्तरी भरत के सम्पूर्ण प्रदेश पर इस विजय
से गुप्त सत्ता की स्थापना हो गयी।
आटविक राज्य - आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध का वर्णन करने के पश्चात् हरिषेण
ने वन्य प्रदेश के राजाओं का उल्लेख किया है।
डा. चौधरी के अनुसार आटविक राज्य आलवक (गाजीपुर) और उभाल (जबलपुर प्रदेश) में
थे। इन आटविक राज्यों की स्थिति के सम्वत् में 199 गुप्त सम्वत् तथा 209
गुप्त सम्बन्ध के लेखों का सहारा लिया जाता है। इनके अनुसार हस्तिन डभाल तथा
18 अरबी राज्यों पर शासन कर रहा था। इस प्रकार यदि आटविक राज्यों को मध्य
भारत में मान लिया जाय तो यह अनुमान स्वाभाविक प्रतीत होता है कि प्रथम
आर्यावर्त युद्ध के पश्चात् दक्षिणी भारत की ओर अभियान करते समय समुद्र के
बीच में आटविक राज्यों की जीता था परन्तु हरिषेण ने आटविक राज्यों की विजय का
उल्लेख द्वितीय आर्यावर्त-युद्ध और पूर्वी भारत की विजय के बीच में किया है।
इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आटविक राज्य आर्यावर्त और पूर्वी सीमान्त
राज्यों के बीच में स्थित थे।
समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय - प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा
दक्षिण के 12 राजाओं की विजय का वर्णन मिलता है। इन राजाओं को पराजित करने के
पश्चात् बन्दी बना लिया जाता था परन्तु उन्हें मुक्त करके उनका राज्य लौटा
दिया जाता था। यह समुद्रगुप्त की धर्म विजय की नीति कहलाती है। यह नीति
समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता एवं परिपक्व कूटनीति का प्रमाण है क्योंकि दूरस्थ
प्रदेशों तक सत्ता बनाये रखने में आवागमन के साधनों के अभाव में कठिनाई होती।
दक्षिण भारतीय विजय प्रयाग में पराजित शासकों की सूची निम्न प्रकार है-
1. कोशल का महेन्द्र - यहाँ कोशल का अर्थ दक्षिण का कोशल से ही लगाना चाहिए।
इसकी राजधानी श्रीपुर थी। इसके अन्तर्गत विलासपुर, रायपुर सम्भलपुर के जिले
थे। इसका राजा महेन्द्र था। महेन्द्र के विषय में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा
जा सकता है, क्योंकि इस राजा का किसी प्रकार का लेख आदि नहीं मिलता है।
2. महाकान्तार का व्याघ्रराज - डॉ. राय चौधरी के अनुसार यह राज्य मध्य प्रदेश
का वन्य प्रदेश था। इसकी स्थिति बैनगड़ा और प्राक् कोशल के बीच थी। इसका राजा
व्याघ्रराज था। डॉ. जायसवाल महाकान्तार को वर्तमान कंकर एवं बस्तर प्रदेश
मानते थे। डॉ. भण्डारकर का विचार है कि महाकान्तार का व्याघ्रराज बुन्देलखण्ड
के जाने और अजयगढ़ प्रदेशों पर राज्य करता था। श्री रामदास महाकान्तार को
गंजाम और विशाखापट्टनम का झाड़ा खण्ड प्रदेश मानते हैं।
3. केरल का मन्तराज - कुछ विद्वान केरल को कुशल पढ़ते हैं। डॉ. वर्निट ने
इसका समीकरण. दक्षिण भारत के गंगा कोराड (गंजाम जिला) से किया है। ऐहोल
अभिलेख में कोलैर को कुनाल कहा गया. है। पवनदूत नामक ग्रंथ में केरलों को
ययातिनगर का निवासी बताया गया है। यह ययातिनगर मध्य प्रदेश के सोनपुर जिले
में था। कुछ विद्वान यही मज्तरात का राज्य मानते हैं।
4. विपटपुर का महेन्द्रगिरि - विपटपुर का समीकरण गोदावरी जिले में स्थित
आधुनिक पिट्टापुर ही तत्कालीन विपटपुर था यहाँ का राजा महेन्द्रगिरि था।
5. कोटूर का स्वामीदत्त - यह आधुनिक गंजाम जिले में कोटूर था। परन्तु कुछ
विद्वान कोटूर की समता विजगापट्टम के कोटूरा से करते हैं। फ्लीट महोदय भी
कोटूर की समता कोटूर कौलैसी से करते है, जो कोयम्बटूर जिले में है। यहाँ के
शासक स्वामीदत्त के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती है।
6. एरण्डपल्ल का दमन - डॉ. फ्लीट ने इसका समीकरण खानदेश जिले में स्थित
एरण्डोल से किया है। टुब्रिया महोदय ने इसका विरोध करते हुए एरण्डपल्ल को
गंजाम जिले में स्थित एरंडपलि नामक नगर माना है जिसे रामदास विशाखापत्तनम
एंडीपल्लिया एल्लोर में स्थित एंडीपल्लि मानते हैं।
7. कांची का विष्णुगोप - इसका समीकरण आधुनिक मद्रास के कांजीवरम् के साथ किया
गया है। यहाँ का राजा विष्णुगोप पल्लववंशीय था। डॉ. कृष्णस्वामी ने इसे
संस्कृत तथा प्राकृत लेख वाला विष्णुगोप कहा है परन्तु यह मानना उपयुक्त नहीं
है। कांची आधुनिक कांजीवरम ही है।
8. अवयुक्त का नीलराज - नीलराज अवमुक्त का शासक था परन्तु अभी तक पूर्ण
सन्तोषजनक 'अमरकोष' से हमें ज्ञात होता है कि सामान्य और विशिष्ट दोनों
प्रकार के वस्त्रों के लिए विभिन्न प्रकार के नाम इस युग में प्रचलित थे। चार
प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख 'अमरकोष' ने किया है -