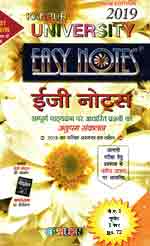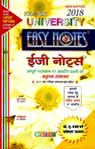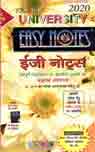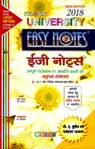|
भूगोल >> ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्रईजी नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
26
जैवमण्डल
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
जीव मण्डल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है
जिसके अन्तर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन (Protective
Device) के सम्भव होता है। कुछ लोग जीवमण्डल को जीवित वस्तुओं के मण्डल के
रूप में स्वीकार करते हैं। ए0एन0 स्ट्रालर (A.N. Strahler) एवं ए0एच0
स्ट्रालर के अनुसार पृथ्वी के सभी जीवित जीव (Living Organisms) तथा वे
पर्यावरण, जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया (interactions) होती है, मिलकर
जीवमण्डल की रचना करते हैं। जीवमण्डल के इस आवरण का संघटन सामान्य रूप से 30
किमी0 से मोटी वायु, जल, मिट्टी तथा शैल की पतली परत से होता है। यद्यपि
वायुमण्डल में 15किमी0 की ऊँचाई तक जीवाण्विक सक्रियता (Bacterial Activity)
का पता चला है परन्तु वायुमण्डल की मात्र उस निचले भाग में ही जीव अधिक पाये
जाते हैं जहाँ पर उनके विकास तथा संवर्धन के लिए पर्यावरणीय दशाएँ अधिक
अनुकूल होती हैं। जीवमण्डल की निचली सीमा (मृदा की गहराई तथा सागरीय गहराई)
आक्सीजन तथा प्रकाश की सुलभता तथा दबाव द्वारा निर्धारित होती है। ज्ञातव्य
है कि जीव के सामान्य रूप में पनपने के लिए पर्याप्त आक्सीजन तथा प्रकाश की
आवश्यकता होती है।
कुछ लोग वनस्पतियों तथा प्राणियों को ही जीवमण्डल के प्रमुख सहायक मानते हैं।
निश्चय ही यह अवधारणा संकुचित है। भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीव एक
दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से अन्तर्सम्बंधित (Interrelated) हैं कि उनको
एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप दासमैन के अनुसार,
जीवमण्डल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक
आवरण मण्डल के रूप में व्याप्त है तथा जिसके साथ जीवित जीव (Living
Organisms) सम्बंधित हैं तथा यह मण्डल जीवों की भरण पोषण करता है। इस प्रकार
जीवमण्डल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र (Basic Global System) है जिसके जैविक
(Biotic) एंव अजैविक (Abiotic) दो संघटक होते हैं। अजैविक संघटक भौतिक
पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अन्तर्गत मोटे तौर पर वायुमण्डल,
स्थलमण्डल तथा जलमण्डल को सम्मिलित किया जाता है। सामान्य रूप में इनको मृदा,
वायु तथा जल से सम्बोधित करते हैं। वायुमण्डल, जीवमण्डल में जीवों के लिए
आवश्यक आक्सीजन तथा अन्य गैस प्रदान करता है तथा प्रवेशी लघु तरंग सौर्यिक
विकिरण के लिए पारदर्शक बनकर तथा सौर्यिक ऊर्जा को छानकर भूतल पर आने में
सहायता करता है। इस सौर्यिक ऊर्जा को हरी पत्ती वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण
(Photosynthesis) विधि से अन्य ऊर्जा रूपों में परिवर्तित करते हैं जिसका
प्रयोग पौधे, जानवर तथा मनुष्य करते हैं। जलमण्डल के अन्तर्गत झीलों, नदियों
तथा महासागरों के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसी जलमण्डल से जीवमण्डल के लिए
जलवाष्प (Water Vapour) तथा जलीय घोल (Water Solution) प्राप्त होता है।
जलमण्डल जलीय जीवन (Aguatic Organism) को जीवन प्रदान करता है। स्थलमण्डल शैल
निर्मित क्रस्ट होता है जिसका विस्तार महाद्वीपों तथा महासागरों में होता है।
वास्तव में मृदा आवरण वायुमण्डल तथा स्थलमण्डल के मध्य आवान्तर मण्डल,
(Transition Zone) होता है। इस मृदा आवरण में सूक्ष्म जीवों के अलावा खनिज
तथा जैविक पदार्थ निहित होते हैं जो जीवों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
मृदातंत्र (Soil System) जीवमण्डल में ऊर्जा के स्थानान्तरण मार्ग तथा पोषक
आहार के जैविक चक्रण के लिए आवश्यक होता है। स्थलमण्डल पर वनस्पति आवरण तथा
अपक्षय से अप्रभावित आधार शैल के मध्य स्थित मृदा का पतला आवरण सर्वाधिक
महत्त्वपूर्ण जैविक मठ्ठी के रूप में होता है।
वास्तव में मृदा जीवों के लिए एक तरफ आवास प्रदान करती है तो दूसरी तरफ जीवों
के लिए पोषक आहार भण्डार (Nutrient Resservior) का कार्य करती है। जीवमण्डल
के जैविक संघटक का निर्माण तीन उपतंत्रों द्वारा होता है— (1) पादप तंत्र
(Plant System), (2) जन्तु तन्त्र (Animal System) तथा (3) सूक्ष्म जीवतंत्र
(Micro Organism System)। इन तीनों उपतंत्रों में से मात्र पौधे ही जैविक या
कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग पौधे स्वयं करते हैं,
साथ ही साथ मानव रहित जन्तु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
इन्हीं पौधों पर ही निर्भर करते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादक (Primary
Producers) होते हैं क्योंकि वे सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण
की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। कार्यात्मक आधार
(Functional Basis)पर जीवमण्डलीय पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख भागों में
विभक्त करते हैं- (1) स्वपोषित संघटक (Autotrophic Compoents) तथा (2)
परपोषित संघटक (Heterotrophic Components)। स्वपोषित संघटकों में सभी प्रकार
के हरे पौधे आते हैं। परपोषित संघटकों के अन्तर्गत उन जन्तुओं को सम्मिलित
करते हैं जो अपने आहार के लिए प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों पर निर्भर रहते
हैं। परपोषित जन्तुओं को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं— (1)
मृतजीवी (Saprophytes) (2)परजीवी (Parasites) तथा (3) प्राणिसमभोजी
(Holozonic)। सूक्ष्म जीव तन्त्र (MicroOrganism System) को वियोजक
(Decomposers) भी कहा जाता है क्योंकि ये मृत पौधों तथा जन्तुओं तथा जैविक
पदार्थों को विभिन्न रूपों में सड़ा-गलाकर वियोजित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव
जैविक पदार्थों के वियोजन के समय अपना आहार भी ग्रहण करते हैं।
|
|||||