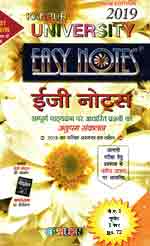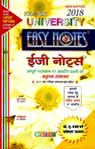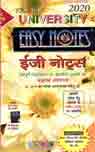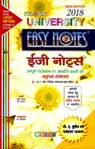25
महासागर : भविष्य के संसाधनों के स्थल भण्डार
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
महासागरीय जल तथा नितल (bottom) से सम्बन्धित जैविक तथा अजैविक संसाधनों के
सागरीय संसाधन कहते हैं। यह सागरीय संसाधन सागरीय जल, उसमें निहित ऊर्जा;
जैसे—तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि, उसमें रहने वाले जीव-जन्तु, पौधे,
सागरीय निक्षेप तथा उसमें निहित अजैविक तत्व, सागरीय तली के जैविक एवं अजैविक
पदार्थ, तलवासी जीव इत्यादि रूपों में हो सकता है। सागरीय जल में असंख्य
अतिसूक्ष्म पौधे (Microscopic Plants) मौजूद होते हैं। सागरीय जैविक संसाधनों
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे नवीनकरणीय (Renewable) हैं। प्रारम्भ से ही
सागर मानव के लिए आकर्षण का केन्द्र एवं उपयोगी रहा है। मनुष्य सागर की
विभिन्न रूपों में उपयोग करता रहा है; यथा यातायात एवं परिवहन, मत्स्यन
(Fishing) सेना एवं रक्षा, खनिज विदोहन (Mineral Extraction), मनोरंजन
(Recreation), दवा, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण (Waste disposal) आदि।
सागरीय जीवीय संसाधनों के परम्परागत विदोहन के अलावा मनुष्य अपने कौशल एवं
प्रौद्योगिकीय विकास के द्वारा उसमें संशोधन एवं परिमार्जन भी कर रहा है।
जैसे—सागर कृषि (Mariculture) जलकृषि (Aquaculture), सागर जन्तुवर्द्धन
(Oceah Ranching) आदि विधियों से सागरीय जीवों (पौधों एवं वनस्पतियों) की
उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने लगा है। सागरीय निक्षेपों तथा सागरीय
क्रस्ट में स्थित खनिज पदार्थों के विदोहन की होड़ लग गयी है। परिणामस्वरूप
सागरों का सामरिक महत्त्व भी बढ़ गया है। सागरीय जीवों के अध्ययन के लिए सागर
जीव विज्ञान (Marine Biology), सागरीय संसाधनों के विधिवत् अध्ययन के लिए
आर्थिक समुद्र विज्ञान (Economic Oceanography) या संसाधन समुद्र विज्ञान
(resource
Oceanography) को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है।
सागरीय क्षेत्रों में विविध प्रकार के जैविक तथा अजैविक संसाधन होते हैं। इन
संसाधनों के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रथम, नदियाँ स्थलीय भागों से बहाकर
नाना प्रकार के पदार्थों को सागर में पहुँचाती रहती है। इनमें खनिज तत्वों के
साथ जन्तु एवं पौधे भी होते हैं। द्वितीय, कुछ संसाधन पौधों द्वारा छिछले जल
में तैयार किये जाते हैं। स्पष्ट है कि महासागरों में जैविक संसाधनों का अपार
भण्डार निहित है। महासागरों में मोलस्का (घोंघा) तथा क्रस्टेसियन की लगभग
40,000 प्रजातियाँ तथा मछलियों की 25,000 प्रजातियाँ पायी जाती है। जैविक
संसाधनों के अलावा कई तरह के विटामिन एवं औषधियाँ भी सागरीय जल में निहित है।
सामान्यतया सागरीय संसाधनों को जैविक, अजैविक तथा वाणिज्यिक तीनों प्रकारों
में विभाजित किया जा सकता है। सागरीय संसाधनों को दूसरी तरह से तीन प्रकारों
में विभाजित किया जा सकता है-खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन तथा खाद्य संसाधन।
सागरीय क्षेत्रों में विभिन्न धात्विक एवं अधात्विक (metalic and
non-metalic) खनिज दो रूपों में मिलते हैं-
1. सागरीय जल में घोल के रूप में तथा 2. सागरीय तली के निक्षेप के रूप में।
सागरीय जल में धुले खनिजों में प्रमुख हैं-नमक, ब्रोमीन, मैग्नेशियम, सोना,
जस्ता, यूरेनियम, थोरियम आदि। एक अनुमान के अनुसार प्रति घन किलोमीटर सागरीय
जल में 41.25 मिलियन टन ठोस पदार्थ घुली अवस्था में रहता है। सागरीय जल में
घुले नमक की कुल मात्रा का 85 प्रतिशत भाग सोडियम तथा क्लोरीन का होता है।
सागरीय निक्षेपों के खनिजों को प्राप्ति के अनुसार दो वर्गों में विभाजित
किया जा सकता है-1. सतही निक्षेप (Surface Deposit) तथा 2. सागरीय तली के
नीचे स्थित खनिज (Subsurface minerals)। सागरीय ज्वार, सागरीय लहर एवं ऊपरी
गर्म जल तथा निचले ठंडे
जल के बीच तापमान में अन्तर बिजली उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। इस तरह
ज्वारीय ऊर्जा (Tidal energy) एवं लहर ऊर्जा (Wave Energy) का कुछ देशों के
तटीय भागों में विकास किया गया है। वर्तमान समय में औषधि विज्ञानियों का
ध्यान सागरीय जीवों (पौधों तथा जन्तुओं) से विटामिन तथा विभिन्न रोगों के
निवारण के लिए औषधि (Medicines) बनाने के लिए शोध की ओर लगा हुआ है। ज्ञातव्य
है कि अब ‘सागर औषधि विज्ञान' (Marine Pharmacology) का विकास हो चुका है।
सागरीय खाद्य संसाधनों को उपयोग की दृष्टि से दो प्रकारों में विभक्त किया जा
सकता है-1. मानव आहार के रूप में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ (जैसे—मछलियाँ)
तथा 2. जन्तुओं के लिए पुष्टाहार (खासकर पालतू पशुओं के लिए)। सागरीय
संसाधनों से होने वाली वार्षिक आय में मछलियों का योगदान दूसरे स्थान पर है।
सागरीय क्षेत्रों में मनुष्यों द्वारा कुछ खास विधियों द्वारा कतिपय मछलियों
को कैदी बनाकर पुष्टाहार का सेवन कराके उनके प्रजनन तथा उत्पादन में वृद्धि
करके बाजार में बेचने तक समस्त प्रक्रियाओं को सागर कृषि (Marine farming) जो
जलकृषि (Aquaculture) का ही एक रूप है, कहते हैं। सागर कृषि कोई नयी पद्धति
नहीं हैं वरन् यह कुछ देशों (यथा—जापान, चीन, जावा आदि) में प्राचीन काल से
चली आ रही है। इतना तो निश्चित है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि इस तरह होती रही
तो भविष्य में विश्व स्तर पर खाद्य आपूर्ति की मांग बढ़ती जायेगी। अतः सागरीय
संसाधनों के अधिकाधिक विदोहन की संभावना बढ़ती जायेगी। स्पष्ट है कि भविष्य
में सागरीय संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। अतः सागरीय संसाधनों के विदोहन
(Extraction), संरक्षण (Conservation) एवं परिरक्षण (Preservation) के लिए
समुचित कदम उठाना आवश्यक है।
...Prev | Next...