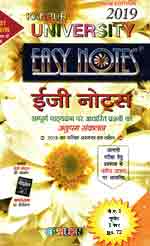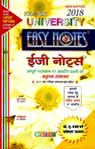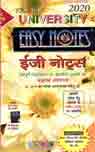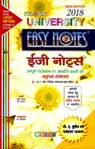|
भूगोल >> ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र ईजी नोट्स-2019 बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्रईजी नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
24
प्रवाल भित्तियाँ
अध्याय का संक्षिप्त परिचय
अन्तः सागरीय रूपों में प्रवाल भित्तियाँ तथा एटॉल अपना अलग ही स्थान रखते
हैं। इनका निर्माण सागरीय जीव मूंगे या केरल पालिप (Coral Polyps) के
अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। कोरल उष्ण कटिबंधीय
महासागरों में पाये जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। एक स्थान पर
असंख्य मूंगे एक साथ रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बना लेते हैं।
मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लगता है। इस
क्रिया के कारण एक लम्बे समय के अन्दर एक विस्तृत भित्ति (Reefs) बन जाते हैं
जिसे प्रवाल भित्ति (Coral Reerfs) कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण
25°N-25°S अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर
स्थित अन्तःसागरीय चबूतरों पर होता है। प्रवाल मूंगा जल के बाहर जीवित नहीं
रह सकता है। अतः प्रवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तल तक ही
पायी जाती है। उल्लेखनीय है कि उष्ण कटिबंधीय सदावहार वर्षा वनों की तुलना
में अधिक विविधता पायी जाती है क्योंकि प्रवालों की 1,000,000 प्रजातियाँ
हैं, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है।
प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन (Rainforsest of the Occeans) कहा जाता है।
जन्तु प्रवाल, जिसे पालिप कहते हैं, अपने द्वारा बनायी गयी चूने की खोल में
रहता है। इसके शरीर के बाहरी तन्तुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है
जिसे 'जुक्सान्थलाई अलगी (Zooxanthallae Algae) कहते हैं। यह शैवाल प्रकाश
संश्लेषण विधि से भोजन बनाती है जिससे अपना विकास करती है। सम्बन्धित प्रवाल
जिसके शरीर में वह वासित है, की शकल भोजन माँग के 60 प्रतिशत भाग की आपूर्ति
करती है। प्रवाल शेष 40 प्रतिशत आहार की अपने मुँह के टेण्टिकिल्स द्वारा
छोटे-छोटे जन्तुप्लैंकटन का शिकार करके आपूर्ति करते हैं। जब सागरीय तापमान
में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर
देता है, परिणामस्वरूप प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता है तथा वे मर जाते
हैं। शैवाल के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। इसे
प्रवाल विरंजन (Coral Bleakching) कहते हैं।
प्रवाल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाये जाते हैं क्योंकि इनको
जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम (20°C-21°C) आवश्यक होता है; परन्तु प्रवाल न
तो अति उष्ण जल में और न ही अति ठंडे जल में पनप पाते हैं। प्रवाल कम गहराई
तक पाये जाते हैं। 200-250 फीट से अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं क्योंकि
इसके बाद सूर्य प्रकाश प्रविष्ट नहीं हो पाता है और प्रवाल के लिए यथोचित
आक्सीजन नहीं मिल पाती है। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता
होती है क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बन्द हो जाता है और वह मर
जाता है। अत्यधिक सागरीय लवणता (Salimity) प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक
होती है क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना प्रवाल
का मुख्य भोजन है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27% से
30% होनी चाहिए। सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होते हैं
क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। प्रवाल के विकास के
लिए अन्तः सागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा
बनाते हैं। नगरीकरण, औद्योगिक विकास, वन विनाश इत्यादि मानवीय क्रिया-कलापों
द्वारा भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि होती है जिसका प्रवालों के विकास पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थलीय भागों से अत्यधिक मात्रा में अवसादों (वन
विनाश के कारण मृदा क्षरण के कारण अत्यधिक मात्रा में अवसाद नदियों द्वारा
सागरों में लाये जाते हैं।) का सागरों में पहुंचना, औद्योगिक क्षेत्रों के
कचरों एवं अपशिष्ट जल, नगरों से निकले कचरों तथा मल-मूत्र जल का सागरों में
विसर्जन एवं आवश्यकता से अधिक मछलियों का पकड़ना इत्यादि मानवीय क्रिया-कलाप
प्रवालों की मृत्यु का कारण बनते जा रहे हैं। वर्तमान समय में विश्व के 58
प्रतिशत प्रवाल संकटापन्न स्थिति (Thereatened Condition) में हैं।
प्रवाल भित्तियों को आकृति के आधार पर तीन वर्गों में रखा जा सकता है—(i)
तटीय प्रवाल भित्ति, (ii) अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा (iii) वलयाकार प्रवाल
भित्ति या एटॉल। स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को दो भागों में रखा जा
सकता है। (i) उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ तथा (ii) सीमान्त प्रदेशीय
प्रवाल भित्तियाँ।
प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए परस्पर
विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इन सिद्धान्तों का मन्थन किया
जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रतिपादन दो प्रमुख आधारों पर किया गया
है-प्लीस्टोसीन सागर तल में परिवर्तन तथा स्थलखण्ड में स्थिरता। इनकी
उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्तों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है-1.
अवतलन सिद्धान्त (Subsidence Theory) तथा 2. स्थिर स्थल सिद्धान्त
(Non-subsidence Theory)| प्रथम वर्ग के अन्तर्गत डार्विन का सिद्धान्त
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत मरे, अगासीज, डेली आदि
के सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं।
|
|||||