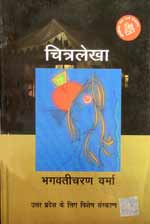|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य निर्धारण की समस्या का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य निर्धारण की समस्या
स्वतन्त्र भारत के संविधान में निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विकास की चर्चा की गई है। अतः सरकार ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इस प्रगति का अभाव माध्यमिक शिक्षा पर अवश्य पड़ा। इसके अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अत: सरकार ने सभी छात्रों के लिये माध्यमिक शिक्षा की सुविधायें देने के लिये प्रयत्न किया। पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक माध्यमिक विद्यालय खोले गये, परन्तु माध्यमिक शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में हम असफल रहे। यह प्रश्न विचारणीय है कि आज की माध्यमिक शिक्षा छात्र-छात्राओं को वह उपयोगी शिक्षा नहीं दे रही है, जिसे पाकर वे आत्म-निर्भर हो जायें और अपनी जीविका कमा सकें।
माध्यमिक शिक्षा पाने के बाद विद्यार्थी के समक्ष केवल निम्नलिखित दो मार्ग रह जाते हैं-
(क) वे अगामी शिक्षा लेने के लिये विश्वविद्यालयों में प्रवेश लें, या (ख) वे रोजगार पाने के लिए इधर-उधर भटकते रहें।
यह अवस्था देश के विकास में बाधक है। अधिकांश विकसित देशों में माध्यमिक शिक्षा को इतना उपयोगी बनाया गया है कि विद्यार्थी उसे पाने के बाद व्यावसायिक दृष्टि से अच्छी तरह आत्म-निर्भर बन जाते हैं परन्तु हमारे देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा बेरोजगारों को जन्म दे रही है। सभी रोजगार पाने के लिये भटकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होने चाहिए कि उच्च शिक्षा-क्षेत्र में अयोग्य छात्रों की भीड़ कम हो, बेरोजगारी न फैले और छात्रों में आत्म-निर्भरता उत्पन्न हो। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली में योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है। अतः माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य ऐसे स्वावलम्बी, कर्त्तव्यनिष्ठ तथा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत चरित्रवान नागरिक तैयार करना है, जो राष्ट्र को समृद्ध व विकसित बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। इसलिये माध्यमिक शिक्षा को धार्मिक, नैतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और चारित्रिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है, जिससे उसके अनुरूप सच्चरित्र व उत्तम नागरिकों का निर्माण किया जा सके।
योग्य नागरिक बनाने का उद्देश्य- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लोकतन्त्रीय स्वरूप को अपनाने वाले नागरिक तैयार किये जाने चाहिये। ये नागरिक राष्ट्रीय समृद्धि में योग देने वाले हो तथा स्वावलम्बी और चरित्रवान हों। विद्यार्थी कर्त्तव्य-परायण, राष्ट्रभक्त मिल-जुलकर एकता से रहने वाले, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक सद्गुणों से पूर्ण हों।
चरित्र-निर्माण के उद्देश्य - वर्तमान माध्यमिक शिक्षा में चरित्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर ध्यान देना आवश्यक है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र पाने योग्य शिक्षा के अवसर जुटाना न होकर बालक को सही अर्थों में चरित्रवान बनाना हो। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। इसे चरित्रवान योग्य नागरिकों की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल पुस्तकीय ज्ञान देने वाली न हो, वरन् इस अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन, राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में उतार कर हम देश व समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। हमारे भावी नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो। वे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार से पूर्ण हों। उन्हें ऐसे पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए कि मौलिक रूप से स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति अपनाये, स्वानुभव अर्जित करें और अर्जित अनुभवों का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में प्रयोग कर सकें। उनमें नैतिकतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता हो।
पाठ्यक्रम के निर्धारण की समस्या-माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यावहारिक और उपयोगी बनायें। यद्यपि हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नताएँ हैं। फिर भी पूरे राष्ट्र के लिये ऐसा समान पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है जो राष्ट्रीय लक्ष्यों और शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक हो सके। भारत सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (All India Board of Secondary Education) ने अपने सुझावों द्वारा कुछ विषयों को अनिवार्य बताकर उन्हें प्रत्येक राज्य में पाठ्यक्रम का अंग बनाने का सुझाव दिया है। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाये, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करता हो, परन्तु साथ-साथ उसमें क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग प्रकार के वर्ग और समूह हों।
पाठ्यक्रम में भाषा-शिक्षण की व्यवस्था को निर्धारित करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। 'हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा 'हिन्दी' है। इसका अध्ययन करना प्रत्येक भारतवासी छात्र के लिये आवश्यक होगा। परन्तु 'अहिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग इसे अन्याय पूर्ण नीति कहकर विरोध करते हैं। यद्यपि अब हम स्वतन्त्र हैं परन्तु अंग्रेजी भाषा के प्रति अब भी हमारा आकर्षण बना हुआ है। दक्षिणी भारत के बहुत से लोग इसी कारण आज भी हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का पक्ष लेते हैं। हमारा देश धर्म प्रयत्न देश है। अतः मूल धर्म ग्रन्थ संस्कृत में होने के कारण लोगों को संस्कृत भाषा के प्रति भी मोह है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह निर्धारित हुआ कि माध्यमिक स्तर पर कम-से-कम तीन भाषायें अवश्य पढ़ाई जायें, यही त्रिभाषा सूत्र (Three Language Formula) कहलाता है। इसमें भाषा का अध्ययन इस प्रकार किया गया है-
1. राष्ट्रीय भाषा हिन्दी या क्षेत्रीय (अहिन्दी क्षेत्रों के लिये)।
2. यदि ऊपर राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी न ली गई हो तो हिन्दी या कोई अन्य भारतीय भाषा या
3. संस्कृत या अन्य भारतीय भाषा (यदि ऊपर न ली गई हो) या पाश्चात्य भाषा।
इस प्रकार की व्यवस्था में छात्र स्थानीय (क्षेत्रीय) भाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय भाषा भी पढ़ेगा और तीसरी भाषा में संस्कृत या अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को पढ़ेगा।
माध्यमिक शिक्षा स्तर पर- पाठ्यक्रम में विषयों की एकरूपता लाने के लिये छात्रों की अभिरुचि (Aptitude), क्षेत्रीय माँग, मातृभाषा (माध्यम के रूप में) परामर्श एवं निर्देशन (Counselling Guidance) की व्यवस्था, तथा पाठ्यक्रम-संचालन की उपयुक्त पद्धति आदि पर ध्यान दिया गया और इन्हें आवश्यक माना गया है। पाठ्यक्रम में निम्न स्तर पर सामान्य विज्ञान (General Science) और सामाजिक अध्ययन (Social Study) को अनिवार्य विषयों में रखा गया। शेष विषयों को छात्रों की आवश्यकता, वैयक्तिक रुचि, अभिरुचि आयु और क्षमता के अनुकूल चुनने की स्वतन्त्रता दी गई। राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में औद्योगिक तथा व्यावसायिक एवं प्राविधिक विषय भी शामिल किये गये। इस प्रकार- निम्न माध्यमिक स्तर पर-उपरोक्त तीन भाषायें, तीन अनिवार्य विषय-सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित तथा कृषि या कोई कलात्मक विषय या कोई वाणिज्यात्मक विषय, संगीत या शारीरिक विकास के विषय को प्रधानता दी गई।
उच्च माध्यमिक स्तर पर- माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अनिवार्य भाषाओं, विषयों के साथ-साथ छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुकूल, विविध वर्ग समूह बनाये गये। इनमें औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Vocational), शिल्प (Craft) आदि विषयों की व्यवस्था करके पाठ्यक्रम को बहु-उद्देशीय बनाने पर विशेष बल दिया गया। प्रश्न 4. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति निर्धारण की समस्या का वर्णन कीजिए। उत्तर- परीक्षा पद्धति की समस्या-वर्तमान समय में प्रचलित परीक्षा पद्धति में बहुत से दोष उत्पन्न हो गये हैं। वर्तमान समय में यह प्रणाली इतनी अनुपयुक्त हो गई है कि इसे छात्र की शैक्षिक उपलब्धि एवं विकास की परख का उचित और वैज्ञानिक साधन नहीं माना जा सकता, परन्तु हम परीक्षा-पद्धति को समाप्त भी नहीं कर सकते। परन्तु इसमें आवश्यक सुधार लाने के लिये सोच-समझकर परिवर्तन अवश्य लाया जा सकता है।
मात्र बाह्य परीक्षाओं (External Examination) को ही बालक की सफलता का मापदण्ड नहीं बनाया जा सकता। हमें छात्रों के कार्य और विकास की अन्तर्परीक्षायें (Internal Examination) एवं परीक्षण (Tests) भी लेने चाहिये। छात्रों की योग्यता की जाँच उनके वर्ष भर के कार्य के आधार पर होनी चाहिये। उनकी प्रगति के मासिक, त्रैमासिक अभिलेख (Records) तैयार हों। उनकी योग्यता की जाँच अंकों (Marks) में न करके ग्रेड्स (Grades) में की जाये। परीक्षा प्रश्नपत्रों में सुधार किया जाये। वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों को भी विषयनिष्ठ या आत्मनिष्ठ (Subjective) प्रश्नों के साथ-साथ पूछा जाये। इस प्रकार परीक्षा-पद्धति में आवश्यक सुधार ला सकते हैं।
प्रबन्ध एवं प्रशासन की समस्या- हमारे देश में तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं- (क) सरकारी विद्यालय, (ख) व्यक्तिगत या गैर-सरकारी विद्यालय, (ग) स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध सरकार द्वारा होता है। व्यक्तिगत (Private) विद्यालयों का प्रबन्ध व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों (Managing Committee) के हाथ में होता है। सरकार इन्हें आर्थिक अनुदान देती है तथा उनके शिक्षकों के वेतनों के भुगतान का दायित्व स्वयं वहन करती है। अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है। स्थानीय संस्थायें माध्यमिक संस्थायें चलाती है, परन्तु उन्हें इस कार्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक (Technical) तथा स्त्री शिक्षा की व्यवस्था सरकार के हाथ में है। इन क्षेत्रों में भी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थायें भी पर्याप्त संख्या में हैं, परन्तु इनकी दशा अच्छी नहीं है। इनकी आर्थिक शैक्षिक, शिक्षक-सम्बन्धी, भवन-सम्बन्धी तथा वातावरण सम्बन्धी व्यवस्थायें अत्यन्त शोचनीय हैं। कहीं ये संस्थायें आवश्यकता से अधिक हैं तो किन्हीं क्षेत्रों में इनका नितान्त अभाव है। कुछ विद्यालय मान्यता के मापदण्डों पर खरे नहीं उतरे हैं।
परन्तु सरकार द्वारा अब इन संस्थाओं के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तो इन संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन भी सरकार ने अपने उत्तरदायित्व में ले लिया है। सरकार धीरे-धीरे अध्यापकों की नियुक्ति पर भी नियन्त्रण कर रही है।
माध्यमिक स्कूलों का प्रशासन भी उपयोगी नहीं है। शिक्षा प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय (Central), मण्डलीय (Regional) तथा जनपदीय (District) इकाइयाँ (Units) हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व निभाती हैं। माध्यमिक विद्यालयों के प्रशासन के लिये प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद् (Board of Secondary Education) होती है। यह परिषद् पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा-व्यवस्था और विद्यालय को मान्यता देने के कार्य करती है। इस कारण माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर दोहरा प्रशासन हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् और शिक्षा विभाग दोनों प्रशासन में भाग लेते हैं। शिक्षा विभाग राज्य के अन्य विभागों से सहयोग लेकर माध्यमिक परिषद् का सहयोग भी प्राप्त करें। दोहरे प्रशासन से माध्यमिक विद्यालय दोहरे नियन्त्रण में आकर अपनी योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। दोनों में सहयोग और तालमेल का होना आवश्यक है। ये एक-दूसरे के काम में साधक हों, बाधक नहीं तभी माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन सही अर्थों में वास्तविक प्रशासन बन सकेगा।
धनाभाव की समस्या- अभी तक शिक्षा-प्रसार में व्यक्तिगत एवं स्वैच्छिक प्रयास ही अधिक हुए हैं। सरकार ने केवल आदर्श (Mode) रूप में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। स्वैच्छिक प्रयास से चलने वाले विद्यालयों को सदैव आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ता है। उनके आय के स्रोत सीमित और अपर्याप्त होते हैं। अधिकांश राज्यों में यद्यपि शिक्षकों के वेतन का भुगतान सरकार द्वारा होता है। परन्तु अभी भी बहुत से विद्यालयों के पास धन के अभाव के कारण उनके पास न तो अच्छे भवन होते हैं और न अच्छी शिक्षण सुविधायें होती हैं। वर्तमान शिक्षा खर्चीली है और अनुपयोगी भी है। उपयोगी विषयों और कार्यक्रमों को ये स्कूल अपने यहाँ धनाभाव के कारण क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा कर लगाकर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार हमारी सरकार भी इन विद्यालयों की दशा सुधारने के लिये शिक्षा-कर जैसी व्यवस्था कर सकती है। दान-राशि को बढ़ाने के लिए दान-राशि को आयकर से मुक्त करके दाता-लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
माध्यमिक विद्यालयों को व्यवस्था के भवन प्रयोगशालायें, वाचनालय, शिक्षण सामग्री तथा कार्यशाला आदि की व्यवस्था करने के लिए धन की पर्याप्त आवश्यकता होती है। सरकार और जनता दोनों मिलकर इस आर्थिक व्यवस्था को अच्छा और सुदृढ़ बना सकते हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न
|
|||||