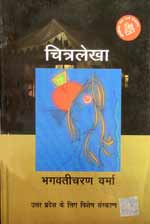|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के उपायों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के उपाय
अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा के लिए हमें वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य, उसकी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। हम उन सबको निम्नलिखित शीर्षकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं -
1. शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य व्यापक हों। आज शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और व्यावसायिक विकास करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना भी होना चाहिए।
2. शिक्षा की पाठ्यचर्या में परिवर्तन - उद्देश्यों के अनुकूल ही पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए पाठ्यचर्या को थोड़ा विस्तृत करना होगा। भूगोल, इतिहास और अन्य सामाजिक विषयों में देश-विदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, देश-विदेश के इतिहास और देश-विदेश के रहन-सहन, खान-पान और उनकी संस्कृतियों का समावेश करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं और संगठनों के विषय में भी बच्चों को बताना आवश्यक है। अतः इन्हें भी पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। इस सबके साथ-साथ उसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सहपाठ्यचारी क्रियाओं को भी स्थान देना होगा, जैसे - अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का मानना, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाना, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर वाद- विवाद कराना और देश-विदेश की सभ्यता एव संस्कृतियों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। इन सबका आधार है भाषा। अपने राष्ट्र को समझने के लिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे राष्ट्रों को समझने के लिए उनकी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चूँकि ये भाषाएँ अनेक हैं इसलिए पाठ्यचर्या में केवल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं को स्थान मिलना चाहिए पर किसी भी स्थिति में इनका अध्ययन अनिवार्य न किया जाये।
3. शिक्षा विधियों में सुधार - अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए बच्चों में स्वतंत्र चिन्तन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और विस्तृत दृष्टिकोण होना आवश्यक है और इन सबका विकास उचित शिक्षण विधियों को विशेष रूप से अपनाना चाहिए जिनमें बच्चों को स्वयं करके, स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर मिलते हैं और बच्चे सामूहिक रूप से एक-दूसरे के सहयोग से समस्त क्रियाओं का संपादन करते हैं।
4. पाठ्य पुस्तकों में सुधार - भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किया जाये। उनमें से ऐसी विषय सामग्री निकाल देनी चाहिए जिससे संकीर्ण राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलता है। उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के जीवन चरित्र एवं घटनाओं आदि का समावेश करना चाहिए। देश-विदेश की प्राकृतिक स्थिति और सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित सामग्री का चुनाव भी किया जाना चाहिए।
5. समान व्यवहार - हमें दूसरे राष्ट्रों के बच्चों और उन राष्ट्रों की वस्तुओं, विशेषकर वहाँ के राष्ट्रध्वज एवं संस्कृति को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छाई को स्वीकार करने और बुराई को त्यागने की प्रवृत्ति का विकास हमें करना ही चाहिए। यह अच्छाई कहीं से भी ली जा सकती है।
6. दैनिक सामूहिक सभा का कार्यक्रम - विद्यालयों का कार्यक्रम 15 मिनट की सामूहिक सभा से आरम्भ होना चाहिए। इस सभा में सर्वप्रथम प्रार्थना और अन्त में राष्ट्रगान होना चाहिए। शेष 10 मिनट में कभी स्वास्थ्य चर्चा, कभी नैतिक शिक्षा, कभी देश-विदेश की संस्कृतियों की चर्चा, कभी भावात्मक एकता, कभी राष्ट्रीय एकता और कभी अंतर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता पर बोलना चाहिए। यदि इन प्रवचनों में हम बच्चों के सामने अपना प्राचीन आदर्श
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्वेत ॥
अर्थात् संसार के सभी व्यक्ति सुखी हों, सभी निरोग हो, सभी को कल्याण का दर्शन हो और कोई दुखी न हो - प्रस्तुत कर सकें तो बच्चे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ेंगे। यह कार्य नारेबाजी से नहीं होगा, इसके पीछे ठोस नैतिक आधार होना आवश्यक है।
7. अंतर्राष्ट्रीय दिवस सह पाठ्यचारी क्रियाओं के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाये जायें। प्रत्येक विद्यालय में संसार के सभी राष्ट्रों के झंडे हों। इन अवसरों पर हमें सभी राष्ट्रों के झंडे फहराने चाहिए और अपने राष्ट्र धुन बजानी चाहिए। प्रातःकालीन सामूहिक सभा में 10 मिनट का समय उस दिन इस कार्य के लिए ही दिया जाना चाहिए।
8. अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के भाषण - आज संसार बहुत छोटा हो गया है. हम किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और अपने विद्यार्थियों के बीच देश-विदेश के नेताओं को उपस्थित कर उनके भाषण कराने चाहिए। इससे बच्चे एक-दूसरे के विचारों से परिचित होने का अवसर प्राप्त करेंगे। यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों पर किया जा सकता है।
9. अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल-कूदों का आयोजन भी करना चाहिए। यूँ तो व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि इस स्तर की प्रतियोगिताओं में जब कोई देश जीतता अथवा हारता है तो पूरे देश में खुशी अथवा शोक मनाया जाता है और इस हार- जीत के फैसले को प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय भावना से देखता है परन्तु यह तो दो भाइयों के बीच होने वाले खेल में भी होता है, इसमें दुर्भावना नहीं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इस भावना से ही तो राष्ट्र तरक्की करते हैं।
10. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवक समारोह मनाये जाने चाहिए और इनमें सब देशों को अपने-अपने देश की सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे बच्चे देश-विदेश की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, वे उनका आदर करने लगते हैं और उनमें अंतर्राष्ट्रीयता का विकास होता है।
11. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ - अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ बहुत सहायक हो सकती हैं जैसे- वेश-भूषा, चित्रकारी, शिल्प, साहित्य, पाठ्य-पुस्तकें, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, वैज्ञानिक आविष्कार आदि की प्रदर्शनियाँ। छोटे-छोटे बच्चे देश-विदेश के बने खिलौनों में बड़ी रुचि लेते हैं, अतः उनके लिए उनकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। इनके माध्यम से बच्चे संसार के भिन्न-भिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृति से परिचित होते हैं और यह सब उनकी ज्ञान परिधि में प्रविष्ट हो जाता है।
12. रेडियो और टेलीविजनों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में स्कूल के समय और उसके बाद भी रेडियो और टेलीविजनों पर अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में सहयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में समाचार पत्र और पत्रिकाएँ भी बड़ा सहयोग दे सकती है। हमें अपनें विद्यालयों में पुस्तकालय एवं वाचनालयों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का साहित्य मँगवाना चाहिए।
13. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों का आदान-प्रदान- इस भावना के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों का आदान-प्रदान होना चाहिए। यह कार्य कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर तो किया ही जा सकता है। जब एक देश के अध्यापक दूसरे देश में जायेंगे तो उनके द्वारा देश-विदेश की संस्कृतियों का प्रसार होगा और इसके द्वारा बच्चों को संसार की सही तस्वीर मिलेगी।
|
|||||