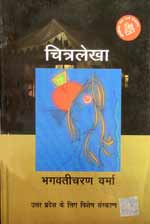|
बी ए - एम ए >> चित्रलेखा चित्रलेखाभगवती चरण वर्मा
|
|
||||||
बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक
प्रश्न- भारत में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए इस सम्बन्ध में गोष्ठियों एवं समितियों के विचारों का भी उल्लेख कीजिए।
अथवा
राष्ट्रीय एकता में कौन-कौन सी बाधायें हैं?
उत्तर-
भारत में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएँ
(Obstacles in the Way of Emotional and National Integration in India)
यह तथ्य सर्वविदित है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम एकजुट होकर लड़ा था। तब हम सबके मन में एक ही विचार था कि हम भारतीय हैं। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष बाद ही हमारे देश में भावात्मक (राष्ट्रीय) एकता में कमी आने लगी। सरकार का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक था। शिक्षा जगत् में भी इस विषय पर गोष्ठियाँ आयोजित होने लगीं और राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारणों और उसके विकास के उपायों पर विचार होने लगा। यहाँ हम कुछ मुख्य गोष्ठियाँ, सम्मेलनों और समितियों के इस सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं -
1. राष्ट्रीय एकता गोष्ठी (1958) - इस गोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था। इसमें अनेक शिक्षाविदों ने भाग लिया। इन लोगों की सम्मिति में राष्ट्रीय एकता में कमी का मुख्य कारण देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव बरतना है।
2. उपकुलपति सम्मेलन (1961) - इस सम्मेलन में कुलपतियों ने देश में क्षेत्र, जाति, धन और भाषा के आधार पर भेदभाव बरतने को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक बताया।
3. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता समिति (1961) - इस समिति का गठन कांग्रेस के भावनगर अधिवेशन में किया गया था। इस समिति की सम्मति में जाति वा धार्मिक संकीर्णता, अशिक्षा पिछड़ापन व्यक्ति और संपत्ति की असुरक्षा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है।
4. मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन (1961) केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर विचार हेतु 31 मई 1961 को राज्यों को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कई केन्द्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने की पर एक दिन में क्या विचार हो पाता। अतः 10 अगस्त को यह सम्मेलन फिर बुलाया गया और इस बार यह 12 अगस्त तक चला। इस बार इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाये। इन्होंने माना कि राष्ट्रीय एकता में कमी आने के मुख्य कारण जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता है, जबकि इन पर काबू नहीं किया जाता राष्ट्रीयता का विकास नहीं किया जा सकता।
5. डॉ. सम्पूर्णानन्द भावात्मक एकता समिति (1961-62 ) - इस समिति का गठन केन्द्रीय सरकार ने 1961 में किया था। इसका कार्य राष्ट्रीय एकता में कमी आने के कारणों का पता लगाना। इन कारणों को दूर करने के उपाय सुझाना और राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका निश्चित करना था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1962 में प्रस्तुत किया। इस समिति के सम्मति में भावात्मक (राष्ट्रीय) एकता के मार्ग में मुख्य बाधक तत्व - जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता युवकों को निराशा और आदर्शों का अभाव है।
6. राष्ट्रीय एकता समिति (1967) - प्रारम्भ से ही हमारी सरकार की नीति रही है - विचार अधिक और काम कम। भारत-पाक युद्ध के बाद केन्द्रीय सरकार ने नये सिरे से राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया और इसमें सभी राजनैतिक दलों के लोग सम्मिलित किये। इसकी पहली बैठक जून 1968 में श्रीनगर में हुई। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने की। इस बैठक में मुख्य रूप में प्रान्तीय और साम्प्रदायिकता पर चर्चा हुई। इस समिति की दूसरी बैठक 1980 में तीसरी बैठक 1984 में हुई। हर बैठक में बढ़ते हुए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता पर चिन्ता व्यक्त की गई। पर किसी ने नहीं कहा कि इसको बढ़ाने का कार्य राजनैतिक दलों और स्वंय सरकार का है। भला अपने को दोषी कौन मानता है।
7. शिक्षा जगत की अन्य गोष्ठियाँ इस बीच शिक्षा जगत में न जाने कितनी गोष्ठियाँ और हुई। इन गोष्ठियों में मुख्य बिन्दु शिक्षा होना स्वाभाविक था। इन गोष्ठियों में भी बढ़ते हुए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता पर चिन्ता व्यक्त की गई परन्तु इसके साथ-साथ इन्होंने इसके लिए वर्तमान शिक्षा को भी दोषी ठहराया। अपने को दोषी मानने का साहस शिक्षाविद ही कर सकते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं।
हमारी अपनी सम्मति
हम मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जातिवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता मुख्य बाधक तत्व हैं परन्तु सोचना अब यह है कि इनको बढ़ावा कौन दे रहा है। हमारी सम्मति में इनको बढ़ावा स्वयं सरकार है और राजनैतिक दल दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या, आर्थिक विषमता और अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं और जैसाकि शिक्षाविद स्वयं स्वीकार करते हैं, उदार शिक्षा की कमी भी इसके लिए उत्तरदायी है। अतः यहाँ इन पर थोडा विचार करना आवश्यक है -
1. जातिवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता - हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, अनेक धार्मिक सम्प्रदाय हैं और यह शासन की दृष्टि से अनेक प्रान्तों में बंटा हुआ है और जहाँ वर्ग हो, वहाँ वर्ग-संघर्ष होना स्वाभाविक है और जहाँ संघर्ष हो वहाँ एकता का प्रश्न ही नहीं उठता पर वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में ये भिन्न-भिन्न जातियाँ, भिन्न-भिन्न भाषाएँ, भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय और भिन्न-भिन्न क्षेत्र (जिनका आधार स्थान नहीं, भाषा और संस्कृति था) ये तो तब भी थे जब हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, और तब देश में राष्ट्रीय एकता अपनी चरम सीमा में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें निरन्तर कमी आती जा रही है और इसका मूल कारण है- हमारी सरकार और राजनैतिक दल।
2. राज्य की भेदभाव पूर्ण नीति - हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धान्त हैं - स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। हमारे संविधान में भी यह घोषणा की गई है कि राज्य स्थान, जाति, लिंग और धर्म आदि किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं बरतेगा, परन्तु अफसोस, हमारा राज्य स्थान, जाति, लिंग और धर्म, सभी के आधार पर भेदभाव बरत रहा है। किस प्रकार, यह आप स्वयं देख समझ रहे हैं। परिणाम यह है कि देश के नागरिकों में समान नागरिक होने का भाव ही उत्पन्न नहीं हो पा रहा जो राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है।
3. वोट की राजनीति भारत में विभिन्न जातियाँ, भाषाएँ और धार्मिक सम्प्रदाय तो पहले से ही थे परन्तु इनके बीच खाई खोदने का काम राजनैतिक दलों ने किया है, वोट की राजनीति ने किया है और यदि हम यह कहें कि वोट की राजनीति ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। इस संदर्भ में पहली बात तो यह है कि हमारे देश में अधिकतर राजनैतिक दलों का निर्माण जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बनते हैं सभी राजनैतिक दल जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर वोट बटोरते हैं। कोई अपने को दलितों का हिमायती कहता है, कोई अपने को पिछड़े वर्ग का हिमायती कहता है और कोई अपने को अल्पसंख्यकों का हिमायती कहता है। इतना ही नहीं अपितु कोई अपने को किसानों के हितों का रक्षक बताता है तो कोई अपने को मजदूरों के हितों का रक्षक बताता है। कोई अपने क्षेत्र के विकास पर वोट मांगता है तो कोई अपनी भाषा के नाम पर वोट मांगता है। राष्ट्रहित की बात सोचने और करने वाले अब दिखाई ही नहीं देते तब आप ही सोचिए कि देश में राष्ट्रीय एकता कैसे हो सकती है।
4. बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी- हमारे देश में जिस तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी के साथ उसमें उत्पादन के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं, परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे राष्ट्र के चरित्र पर प्रभाव पड़ रहा है और चरित्र के अभाव में राष्ट्रीय एकता की बात सोचना व्यर्थ है।
5. आर्थिक विषमता - हमारे देश की जो भी आर्थिक नीति रही, उससे आर्थिक विषमता घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर उठ रहा है परन्तु जिस तेजी से धनी और अधिक धनी हो रहा है उस तेजी से सामान्य जनता का आर्थिक स्तर नहीं उठ रहा है। इस आर्थिक दौड़ में लोग स्वार्थ के आगे राष्ट्र हित की बात नहीं सोच पा रहे जो राष्ट्रीय एकता की पहली शर्त है।
|
|||||