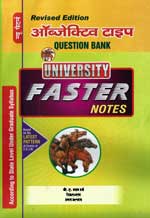|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
प्रश्न- “शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है।' इस कथन की व्याख्या करते हुए इसके कार्य, आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए।
अथवा
शिक्षा के कार्य का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
शिक्षा के कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व
(Functions, Need, Utility and Importance of Education)
शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा व्यष्टि, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। यह मनुष्य को वह सब प्राप्त करने में सहायता करती है जिसके कि वह योग्य होता है और वर्तमान जिसकी वह आकाक्षा करता है। इसके कार्यों को सीमा में नहीं बांधा जा सकता यह मनुष्य के भूत, और भविष्य तीनों से सम्बन्धित होती है। यह उसे भूत से परिचित कराती है, वर्तमान में जीने योग्य बनाती है और भविष्य का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। दार्शनिकों की दृष्टि से यह मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाती है। समाजशास्त्रियों की दृष्टि से यह मनुष्य का समाजीकरण करती है, सामाजिक नियन्त्रण रखती है और सामाजिक परिवर्तन करती है। राजनीतिशास्त्रियों की दृष्टि से यह मनुष्य को राज्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से यह मनुष्य में व्यावसायिक कुशलता का विकास करती है और राष्ट्र का आर्थिक विकास करती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण करती है और वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह मनुष्य की अन्तः शक्तियों का बाह्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है। सामान्य रूप से यह सब ही शिक्षा के कार्य हैं।
शिक्षा के समस्त उद्देश्य अथवा कार्यों को हम निम्नलिखित शीर्षकों और क्रम में संजो सकते हैं।
1. शारीरिक विकास, इन्द्रिय प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों का उदात्तीकरण - जहाँ तक मनुष्य के शरीर की अभिवृत्ति का प्रश्न है, यह उसका नैसर्गिक गुण है आवश्यक भोजन, जल और वायु प्राप्त होने पर वह स्वयं विकसित होती है. परन्तु उसके विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में शिक्षा के तीन कार्य है - पहला - मनुष्य के उचित शारीरिक विकास हेतु उसे उचित आहार- विहार, आचार और विचार का ज्ञान कराना और तद्नुकूल व्यवहार करने की आदत बनाना। दूसरा उसकी उसकी जन्मजात शक्तियों का कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण और तीसरा उदात्तीकरण, हम यह जानते हैं कि 'शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम् अतः शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य का शारीरिक विकास किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य अपनी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है और क्रियाओं का सम्पादन करता है और चूँकि प्रशिक्षण भी होना चाहिए और मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ भी उसकी शारीरिक विशेषताएँ हैं इसलिए शारीरिक विकास में उनका भी विकास होना चाहिए। परन्तु जन्मजात शक्तियों का विकास तो पशु-पक्षियों में भी होता है, मनुष्य में यह विकास व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को सामने रखकर किया जाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इस क्रिया को मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण कहते हैं। इस कार्य द्वारा शिक्षा मनुष्य को मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार (पशुत्व) से सामाजिक व्यवहार (मनुष्यत्व) की ओर प्रवृत्त करती है। जर्मन शिक्षाशास्त्री पेस्टालोंजी अनुसार - "मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास को ही शिक्षा के मानते थे।"
2. भाषा ज्ञान, मानसिक शक्तियों का विकास और ज्ञानवर्द्धन - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह तो कुछ भी करता है अपने शरीर और मन (मस्तिष्क, बुद्धि और विवेक) के द्वारा करता है। अत: उसके शारीरिक विकास के साथ-साथ उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए। शिक्षा यह कार्य भी करती है। यह उसका दूसरा प्रमुख कार्य है। इस क्षेत्र में भी शिक्षा तीन कार्य करती है - पहला - मनुष्य को भाषा ज्ञान कराना। हम जानते हैं कि मानसिक विकास का सीधा सम्बन्ध विचारों से होता है और विचारों का भाषा से। भाषा और विचारों का चोली-दामन का सम्बन्ध है। इसलिए मनुष्य के मानसिक विकास की शुरूआत भाषा ज्ञान से की जाती है। दूसरा उसकी मानसिक शक्तियों (निरीक्षण, स्मृति, कल्पना, तर्क, और विवेक) का विकास करना। इन शक्तियों के विकास के लिए आज बच्चों को स्वयं करके और स्वयं निर्णय निकालने के अवसर दिये जाते हैं और तीसरा उसे विभिन्न वस्तुओं, तथ्यों और क्रियाओं का ज्ञान कराना। इसके लिए बच्चों को विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। उन्हें विभिन्न क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। इस सबके साथ-साथ उन्हें भय से मुक्त कर अभय बनाया जाता है, निराशा से मुक्त कर आशावादी बनाया जाता है और हीनता से मुक्त कर आत्मविश्वासी बनाया जाता है। इसमें बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तू के अनुसार - "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के विकास को ही शिक्षा मानते थे।
3. समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण और उसके सामाजिक परिवर्तन - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। यूँ तो समूह में रहने की प्रवृत्ति अन्य प्राणियों में भी होती है, परन्तु मनुष्य एक विकासशील प्राणी होने के नाते इन सबसे भिन्न होता है। वह एक ओर अपने समाज में समायोजन करता है और दूसरी ओर उसमें परिवर्तन एवं विकास करता है। इस क्षेत्र में भी शिक्षा तीन कार्य करती है - समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। हम जानते हैं कि किसी समाज की कोई भाषा हो, कैसी भी रहन-सहन, खान-पान एवं व्यवहार की विधियाँ हों और कैसे भी रीति- रिवाज हो, उसके सदस्यों को इन्हें सीखना होता है, तभी वे उस समाज में समायोजन कर पाते हैं। इसे समाजशास्त्रीय भाषा में समाजीकरण कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक समाज अपनी भाषा, रहन- सहन, खान-पान एवं व्यवहार की विधियों और रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखना चाहता है और इस कार्य को वह शिक्षा द्वारा करता है। इसे समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक नियन्त्रण कहते है। इस क्षेत्र में शिक्षा का तीसरा कार्य है - सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा मनुष्यों में अपनी भाषा, रहन-सहन, खान-पान एवं व्यवहार और रीति-रिवाजों में अपने अनुभवों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन एवं विकास की क्षमता पैदा करती है और वे इन सबमें निरन्तर परिवर्तन एवं विकास करते हैं। इसे समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस सन्दर्भ में अमरीकी शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी के शब्द उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में "पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है - मृत्यु। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण पर नियंत्रण रखा जाये।'
4. संस्कृति संरक्षण एवं विकास - संस्कृति मानव समाज की विशेषता है। यूँ, संस्कृति सम्प्रत्यय के विषय में विद्वान एक मत नहीं है परन्तु हमारी दृष्टि से किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य समाज विशेष के व्यक्तियों के रहन-सहन एवं खान-पान की विधियों, आचार-विचार, रीति-रिवाज, कला-कौशल, संगीत-नृत्य, भाषा-साहित्य, धर्म-दर्शन, आदर्श-विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जो उसकी अपनी पहचान होते हैं। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को अपनी इस संस्कृति से परिचित है और उन्हें तदनुकूल सोचने और करने की ओर प्रवृत्त करता है और यह कार्य वह शिक्षा द्वारा करता है। इस प्रकार किसी समाज की संस्कृति सुरक्षित रहती है। एक समय था जब कोई समाज अपने आने वाली पीढ़ी में केवल अपनी ही संस्कृति हस्तान्तरित करता था परन्तु आज आवागमन के साधनों ने संसार को बहुत छोटा कर दिया है, आज हम भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं और जाने-अनजाने उनकी संस्कृति को भी सीखते हैं। इतना ही नहीं अपितु आज हम खुले मस्तिष्क से अपनी संस्कृति में विकास भी करते हैं, यह बात दूसरी है कि किसी समाज की संस्कृति में विकास बहुत मन्द गति से होता है।
5. नैतिक एवं चारित्रिक विकास और मूल्य शिक्षा - सामान्य दृष्टि की नैतिकता से तात्पर्य समाज द्वारा निश्चित नियमों व सिद्धान्तों के पालन में होता है और चूँकि भिन्न-भिन्न समाजों के नियम और सिद्धान्त भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिए समाज आधारित नैतिकता में भी भिन्नता होती है। दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ इस नैतिकता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इसके विपरीत धर्म आधारित नैतिकता में स्थायित्व होता है और यदि ध्यानपूर्वक देखें तो संसार के प्रायः सभी धर्मों के नियम एवं सिद्धान्त समान हैं। सभी धर्म मनुष्य को मनुष्य मात्र से प्रेम करने, सत्य बोलने, ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्त्तव्य का पालन करने की शिक्षा देते हैं। हमारी दृष्टि से धर्म आधारित नैतिकता ही सच्ची नैतिकता है। जब कोई मनुष्य इनका पालन दृढ़ता के साथ करता है और कितनी भी विषम परिस्थिति हो, इससे विचलित नहीं होता तो हम कहते हैं कि वह चरित्रवान व्यक्ति है। इस प्रकार नैतिकता एवं चरित्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात अनुभवजन्य है कि जब तक मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होता तब तक न तो वह अपने शरीर और मन की शक्तियों का सदुपयोग कर पाता है, न समाज में समायोजन कर पाता है और न अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा कर पाता है।
6. व्यावसायिक कुशलता का विकास एवं विशेषज्ञों की पूर्ति - संसार के अन्य प्राणियों की आवश्यकताएँ बड़ी सीमित हैं, उन्हें जीने के लिए केवल भोजन और आवास चाहिए और इतना वे प्रकृति से सीधा प्राप्त कर लेते हैं परन्तु मनुष्य ने जैसे-जैसे अपनी सभ्यता का विकास किया वैसे-वैसे उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती गई और आज उसकी आवश्यकताएँ असीमित एवं विविध हैं। शिक्षा उसकी इन असीमित एवं विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे विभिन्न व्यवसायों (कृषि, कपड़ा, निर्माण, भवन निर्माण और बर्तन, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविजन, कार, बस, रेलगाड़ी, जहाज, हवाई जहाज और युद्ध सामग्री आदि के निर्माण) में कुशलता प्रदान करती है। यह समाज अथवा राज्य के लिए कुशल कर्मकार, संगठनकर्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक और सैनिक आदि तैयार करती है। इससे एक ओर तो मनुष्य अपनी रोजी-रोटी कमाता है और दूसरी ओर समाज एवं राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार - "छात्रों को जीविका उपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है - "अर्थ कारिका विद्या।"
7. राष्ट्र के शासन तन्त्र और नागरिकता की शिक्षा - शिक्षा चाहे व्यक्ति के हाथ में रही हो, चाहे समाज के हाथ में रही हो और चाहे राज्य के हाथ में रही हो, उसके द्वारा राज्य अथवा राष्ट्र की शासन प्रणाली का ज्ञान सदैव कराया जाता रहा है। यह बात दूसरी है कि कभी उसके गुण-दोषों का विवेचन करने की स्वतंत्रता रही और कभी उसके गुणों का बखान करने की विवशता रही। आज तो संसार के प्रत्येक राष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का अनिवार्य कर्त्तव्य माना जाता है और हम जानते हैं कि आज संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न शासन प्रणालियाँ है और सभी राष्ट्र अपने-अपने राज्य की शासन प्रणालियों को उपयुक्तम मानते हैं और वे अपने नागरिकों को इसके स्वरूप एवं गुणों से परिचित कराते हैं और यह कार्य वे शिक्षा द्वारा करते हैं।
8. राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति - हम जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक समाज और राष्ट्र की कुछ आकांक्षाएँ होती हैं और इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना होता है। शिक्षा किसी समाज अथवा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति में उसकी सहायता करती है। उदाहरणार्थ आज हमारे देश के सामने पिछडेपन, निर्धनता, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित पर्यावरण, साम्प्रदायिक और अलगाववाद की समस्याएँ है और इन समस्याओं के समाधान हेतु हमने जन शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की शिक्षा की व्यवस्था की है। इसमें दो मत नहीं कि कोई भी समाज अथवा राष्ट्र अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति शिक्षा की सहायता से ही कर सकता है।
9. आध्यात्मिक चेतना का विकास - हमारी दृष्टि से यह शिक्षा का सर्वोच्च कार्य है। यह बात दूसरी है कि आज कुछ राज्यों द्वारा संचालित शिक्षा में इसके लिए प्रावधान है और कुछ में नहीं है और जिन राज्यों की शिक्षा में इसके लिए प्रावधान है, वह भी प्रायः धर्म विशेष की शिक्षा के रूप में है, आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर तो भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। संसार के अधिकतर लोगों का विश्वास है मनुष्य चाहे जितनी भौतिक उपलब्धियाँ कर ले और चाहे जितना सुधार कर ले अपने जीवन की कला में परन्तु वह वास्तविक सुख और शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता, इसके लिए तो उसका आध्यात्मिक विकास होना आवश्यक होता है। शिक्षा यह कार्य भी करती है, कहीं औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में और कहीं केवल अनौपचारिक रूप में। बुद्ध, महावीर, ईसा, मुहम्मद साहब और गुरु नानक आदि। शिक्षकों से हमें ऐसी ही शिक्षा मिली है। आज भी संसार में आध्यात्मिक शिक्षा देने वालों का अभाव नहीं है। देश-देश, नगर-नगर और गाँव-गाँव में ऐसे व्यक्ति मिल जायेंगे। डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों में- "शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है, न सांसारिक एकता अपितु व्यक्ति को यह अनुभूति कराना है कि उसके पास बुद्धि से भी परे का एक तत्व है, जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो।'
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।