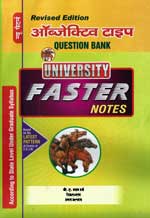|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
प्रश्न- उच्च शिक्षा के मार्ग में कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं? इनके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
उच्च शिक्षा का प्रसार हमारे देश में इसी एक तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि आज हमारे देश में 160 विश्वविद्यालय हैं।
इन विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा का प्रसार करने में निम्न कठिनाइयाँ आती हैं-
नये विश्वविद्यालय आज हमारे देश में 160 विश्वविद्यालय हैं परन्तु आज भी कभी-कभी नये विश्वविद्यालय की माँग उभरती है। यह एक विचारपूर्ण तथ्य है कि क्या हमें और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है? हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 1 : 40 है जबकि इंग्लैण्ड तथा अमेरिका जैसे देश में यह अनुपात क्रमश: 1 : 12 तथा 1 : 3 है। इस तथ्य के साथ हमें यह भी देखना है कि इन राष्ट्रों के मुकाबले में हमारी जनसंख्या भी तीन या चार गुनी है। यदि सर्वेक्षण को आधार बनाया जाये तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि हमें सिंगिल फैक्लटी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता अधिक है। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाओं का मूलभूत ढाँचा पहले से ही विद्यमान है वहाँ पर इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। जमशेदपुर में खनिज विकास, सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा, कानपुर तथा अहमदाबाद के क्षेत्रों में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तथा रूड़की में इंजीनियरिंग आदि से सम्बन्धित यूनिवर्सिटी की स्थापना हो सकती है। वास्तव में, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ उनके आर्थिक नियोजन की भी आवश्यकता है। बिना पूर्ण आर्थिक नियोजन के ये विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकते हैं।
सरकार तथा विश्वविद्यालय - हमारे संविधान में कहा गया है कि- “शिक्षा राज्य का विषय है। संविधान निर्मात्री समिति ने राज्य को उसके क्षेत्र में उच्च शिक्षा करने की व्यवस्था पर जोर दिया है। कुछ लोगों का ख्याल था कि उच्च शिक्षा केन्द्र का विषय होना चाहिए। राज्यों को माध्यमिक शिक्षा तक का उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए।"
विश्वविद्यालय आयोग (सन् 1948 ) इस पक्ष में नहीं था कि उच्च शिक्षा को केन्द्र को सौंपा जाए। इसके दो प्रमुख कारण थे-
1. स्टीरियोटाइप शिक्षा का होना।
2. राज्य सरकार माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ले।
इससे केन्द्र व राज्य के मध्य गम्भीर असन्तुलन होगा।
राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय
भारतीय विश्वविद्यालय दो प्रकार से राज्य पर निर्भर रहते हैं-
1. विश्वविद्यालयों का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा हुआ है तथा विश्वविद्यालय अपनी व्यवस्था तथा अपने विधान के लिए राज्य सरकार पर आश्रित रहते हैं।
2. ये विश्वविद्यालय राज्यों से आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक अनुदान सहायता प्राप्त करते हैं। इसका परिणाम विधायकों पर निर्भर होता है।
विश्वविद्यालयों की सम्प्रभुता - पिछले कुछ समय से इस प्रकार की घटनाएँ प्रकाश में आई हैं जिससे विश्वविद्यालयों की सम्प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों की नीतियों व व्यवस्था में हस्तक्षेप करा जा सकता है, इससे विश्वविद्यालय की सम्प्रभुता तथा कर्मचारियों का स्वाभिमान भी क्षतिग्रस्त होता है।
उपकुलपति (वाइस चांसलर) को राज्यपाल (चासंलर), मुख्यमन्त्री तथा यहाँ कि राज्य के मन्त्रियों तक के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में 14 जून, 1958 को एक एक्ट पारित हुआ जिसके निर्देशन में एक यूनिवर्सिटी एक्ट की स्थापना हुई जो विश्वविद्यालय को परामर्श देने का कार्य करती है। इस एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय की सम्प्रभुता प्रजातन्त्र में शिक्षा तथा शिक्षा में प्रजातन्त्र है।
विश्वविद्यालय के कार्य
विश्वविद्यालय के चार प्रमुख कार्य होते हैं-
(1) शिक्षा- विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य शिक्षा प्रदान करना है। विश्वविद्यालय, संस्थान- कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा को प्रदान करते हैं। बेरोजगारी की समस्या के कारण आज छात्रों की भीड़ विश्वविद्यालय की तरफ इस उम्मीद में उमड़ रही है। कि शायद कोई अच्छा पाठ्यक्रम उन्हें किसी रोजगार को दिलाने में सहायक हो। इसी कारण की वजह से प्रातः कालीन तथा सायंकालीन कक्षायें, डाक द्वारा शिक्षण आदि का प्रचार हो रहा है। इसी कारण से आजकल छात्रों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत काफी कम हो रहा है। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि- "सार्वजनिक फण्ड का दुरुपयोग प्रतिवर्ष हो रहा है और हालत दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है, इसे एक ओर धन का नाश तथा दूसरी ओर छात्रों व अभिभावकों के श्रम तथा शक्ति का अपव्यय एवं आकांक्षाओं पर तुषारापात हो रहा है। " शिक्षा के पूर्ण विकास के लिए विश्वविद्यालयों में सुविधाओं का होना आवश्यक है।
(2) अनुसन्धान- विश्वविद्यालय का दूसरा प्रमुख कार्य छात्रों को अनुसन्धान कार्य की ओर अग्रसर करना है। हमारे देश में मौलिक बौद्धिक अनुसन्धानों का अभाव रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसन्धान के विषय में निम्न आवश्यकता है-
1. बहुत से विश्वविद्यालय व कॉलेज स्नातकोत्तर विष को पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ तो कर देते हैं परन्तु उनके पास न तो उचित साधन होते हैं और न ही योग्य शिक्षक होते हैं। इस कारण से इस स्तर पर शिक्षा का स्तर गिर जाता है। जिन विद्यार्थियों को किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश नहीं मिल पाता है वे इस प्रकार के संस्थान में प्रवेश ले लेते हैं। इससे शिक्षा के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
2. विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर कक्षायें चलाने से पहले सभी सम्भावनाओं पर पूर्ण विचार करना चाहिए।
3. स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य व अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए।
4. अनुसन्धान के लिए रिसर्च सेन्टर्स की स्थापना की जानी चाहिए।
(3) सम्बद्धता - भारत के विश्वविद्यालय का एक अन्य प्रमुख कार्य सम्बद्धता होता है। हमारे विश्वविद्यालय 40 के लगभग कॉलेजों को सम्बद्ध करते हैं इसलिए यू. जी. सी. शिक्षा के लिए कॉलेजों के स्तर को ऊँचा करने पर विचार कर रही है।
(4) प्रसार - विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यों में प्रसार भी है। प्रसार में दो कार्यक्रम प्रमुख हैं-
(i) प्रौढ़ शिक्षा-इसके लिए शिक्षा को प्रचलित रूप प्रदान किया जाये। विद्यार्थियों को नियमित कक्षा अध्ययन करना चाहिए तथा विशेषज्ञों को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
(ii) सामुदायिक सेवा - विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रति रुचि को उत्पन्न करने के लिए सामुदायिक केन्द्र खोलने चाहिए।
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।