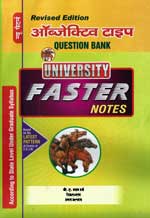|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
21
उच्च शिक्षा
(Higher Education)
प्रश्न- विश्वविद्यालयी सम्प्रभुता से क्या तात्पर्य है? विश्वविद्यालयी सम्प्रभुता की क्या समस्यायें हैं?
अथवा
शिक्षा आयोग (1964-66) ने विश्वविद्यालयी सम्प्रभुता को किस प्रकार परिभाषित किया है? इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों द्वारा किन प्रमुख समस्याओं का अनुभव किया जा रहा है?
उत्तर-
विश्वविद्यालयी सम्प्रभुता से तात्पर्य
विश्वविद्यालय सम्प्रभुता से अभिप्राय विश्वविद्यालयों को कार्य, प्रवेश अनुसन्धान तथा प्रशासन सम्बन्धी स्वाधीनता से है। वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की प्रभुसत्ता पर अनेक राजनीतिक नियन्त्रण हैं।
आयोग ने विश्वविद्यालय की प्रभुसत्ता के तीन क्षेत्र बताये हैं-
1. विद्यार्थियों का चयन।
2. अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति।
3. पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण विधियों का निर्धारण और अनुसन्धान के क्षेत्र तथा समस्याओं का
वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की प्रभुसत्ता पर राजनीति छा गई है। इसके परिणामस्वरूप विद्यालय अखाड़े बन गये हैं। जातिवाद तथा क्षेत्रवाद आज विद्यालयों की पहचान बन गया है और अध्यापक तथा छात्र, दोनों ही आतंकित हो गये।
यह प्रभुसत्ता तीन स्तरों पर है-
1. विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्वायत्तता, अर्थात् समग्र रूप से विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में विभागों, कॉलेजों, अध्यापकों और छात्र की स्वायत्तता।
2. समग्रतः विश्वविद्यालय तन्त्र के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय विशेष की स्वायत्तता, अर्थात् किसी अन्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय विशेष की स्वायत्तता।
3. विश्वविद्यालय तन्त्र से बाहर की एजेन्सियों और प्रभावों-जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सन्दर्भ समग्रतः विश्वविद्यालय तन्त्र की स्वायत्तता।
प्राय: यह दिखाई देता है कि विश्वविद्यालयों पर प्रशासकों का प्रभुत्व है और यहीं पर स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। आयोग ने यह स्वीकार किया है कि अच्छे विचार प्रायः छोटे अधिकारियों के मस्तिष्क की उपज होते हैं और उन्हें मान मिलना ही चाहिये।
राधाकृष्णन कमीशन के विचार
विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में अनेक कमियों को देखा व उन पर विचार किया तो पाया कि उनका कारण तो विश्वविद्यालयों में प्रभुसत्ता का अभाव था।
आयोग ने सम्प्रभुता के निर्माण के लिये ये सुझाव दिये-
1. विश्वविद्यालयों को समवर्ती सूची में रखा जाये।
2. केन्द्र सरकार इन बातों हेतु विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध स्थापित करे- (i) धन, (ii) विशेष अध्ययन की सुविधाओं में समन्वय, (iii) राष्ट्रीय नीतियाँ, (iv) कुशल प्रशासन, (v) विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालायें, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों आदि को जोड़ने वाली कड़ी।
3. विश्वविद्यालयों को अनुदान देने वाली केन्द्रीय अनुदान आयोग की स्थापना हो।
4. सरकारी कॉलेजों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि कॉलेज में परिवर्तित किया जाये।
5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में विजिटर, कुलपति, उप-कुलपति, सीनेटर्स (120), कार्यकारी परिषद् हो। शैक्षणिक परिषद् तथा संकाय भी हों।
सम्प्रभुता पर कुछ विचार-
(1) एस. एन. मुकर्जी के शब्दों में-"हाल ही के कार्यों में विश्वविद्यालयों में सम्प्रभुता पर काफी चर्चा रही है। सरकार ने शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति विकसित कर ली है, ऐसा अनुभव किया जाने लगा है। इस प्रकार के भी प्रमाण हैं कि राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। "
(2) एस. पी. अय्यर के अनुसार-" भारतीय विश्वविद्यालय राज्यों की देन है, पर राज्य विधान सभा या संघीय सभा द्वारा अस्तित्व में आता है। इसकी रचना एवं कार्यों को विस्तार के साथ स्वरूप प्रदान करती है। यद्यपि वह स्वक्षेत्र संस्था के रूप में गठित की जाती है। राज्य सरकार यद्यपि आश्वासन के वर्षों में अनेक उदाहरण ऐसे आये हैं कि सरकार विश्वविद्यालय की प्रभुसत्ता का हनन करने में एक्ट में संशोधन करने में भी नहीं चुकी है।"
(3) डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर - "मैं सम्प्रभुता नहीं चाहता कि जैसा वह कही जाती है। यदि सत्य कहा जाये, जूते पहनने वाला भी जानता है कि वह कहाँ काट रहा है। यह किसी भी रूप में सम्प्रभुता नहीं है।
अनेक अवसरों पर शिक्षा मन्त्रालय से निर्देश प्राप्त होते हैं सेकेट्री हमें यह बताते हैं कि हमें यह लागू करना चाहिये, वह लागू करना चाहिये। ऐसे सन्देश हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम पालन करें तो हम अपने मूलभूत विचारों को सही आकार न दे पायेंगे तथा एक सरकारी कर्मचारी के समान केवल आदेशों का पालन ही करते रहेंगे।
सम्प्रभुता एक मिथक है- वर्तमान समय में जब सम्प्रभुता की चर्चा होती है तो उसका व्यावहारिक रूप विकृत हो उठता है। विश्वविद्यालयों पर राज्य का अंकुश है। महाविद्यालयों पर राज्य, विश्वविद्यालय एवं प्रबन्ध तन्त्र का नियन्त्रण है। आज सम्प्रभुता केवल दिखाने की वस्तु रह गई है। महाविद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्र में केवल भवन साधन व्यवस्था का दायित्व रह गया है। प्रबन्ध तन्त्र न तो नियुक्ति कर सकता है और न भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। इसी प्रकार प्रवेश, नवीन पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने में सरकार की आज्ञा का इन्तजार करना पड़ता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ ज्ञान का विस्तार द्रुत गति से होना चाहिये, शासकीय नियन्त्रण के कारण सम्प्रभुता शासकीय प्रभुसत्ता में परिवर्तित हो रही है।
आज आवश्यक है कि विश्वविद्यालय की सम्प्रभुता बनाने के लिये समुदाय का सहयोग लिया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री मनुष्य को बौद्धिक नेतृत्व एवं रचनात्मक कार्यों के लिये तैयार करे। विश्वविद्यालयों को परिवर्तनशील समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिये समय की चुनौती को स्वीकार करना चाहिये तभी इसकी प्रभुसत्ता अक्षुण्ण रह सकती है।
वित्तीय समस्या
सबसे प्रमुख समस्या के रूप में वित्त की समस्या है। राज्य की शासन प्रणाली, उसकी शिक्षा नीति तथा आर्थिक नीति का विश्वविद्यालय की वित्त नीति पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। विश्वविद्यालय के 1.50% व्यय राजकोष से, 2. शुल्क से, 3. स्थानीय परिषदों से चलते हैं। विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध कॉलेज सीधे ही विश्वविद्यालयों से अनुदान राशि प्राप्त नहीं करते हैं अपितु राज्य के शिक्षण विभाग से ही उन्हें यह धन प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में राधाकृष्णनन आयोग ने बताया कि निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदान राशि का प्रयोग किया जाना चाहिए-
1. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में भवन-निर्माण के लिए।
2. साधनों को प्राप्त करने के लिए।
3. पुस्तकालय को चलाने के लिए।
4. छात्रावास को चलाने के लिए।
5. शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन, प्रोविडेण्ट फण्ड, पेन्शन आदि के लिए।
6. छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने तथा फैलाशिप के लिए।
7. यात्रा छात्रवृत्ति तथा अध्ययन अवकाश के लिए।
8. स्नातकोत्तर कार्य एवं अनुशासन अनुदान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा।
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।