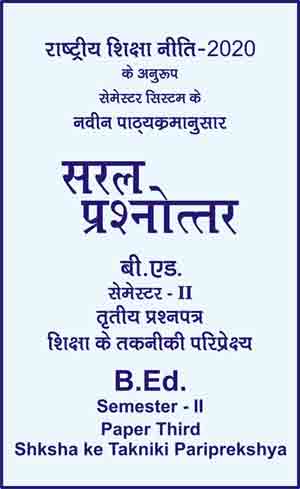|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्यसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय-7 शिक्षण की विधियाँ एवं युक्तियाँ : व्याख्यान, प्रदर्शन, वर्णन, चित्रण, समस्या - समाधान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन एवं परिचर्चा विधि
Methods and Strategies of Teaching : Lecture, Demonstration, Narration, Illustration, Problem Solving, Project, Brain Stroming and Discussion Methods)
प्रश्न- शिक्षण की क्या-क्या विधियाँ हैं? किसी एक विधि का वर्णन कीजिए।
अथवा
शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन-कौन-सी हैं? व्याख्यान विधि या भाषण विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए।
अथवा
शिक्षण की विधियों का अर्थ लिखिए।
अथवा
शिक्षण की व्याख्यान विधि की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
शिक्षण की विधियाँ
(Methods of Teaching)
"शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणामस्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं।" इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप छात्र कुछ ज्ञानार्जन करता है। शिक्षण विधि के प्रक्रिया होने के कारण इसमें कई सोपान (Steps) होते हैं, जिन्हें सुव्यवस्थित करना शिक्षण का कार्य है।
शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं-
1. पाठ्य-पुस्तक विधि (Text Book Method)
2. व्याख्यान विधि अथवा भाषण विधि ( Lecture Method)
3. समस्या-समाधान विधि (Problem Solving Method)
4. कहानी पद्धति (Story Telling Method)
5. आगमन - निगमन विधि (Inductive Deductive Method)
6. वाद-विवाद पद्धति (Discussion Method)
7. योजना विधि (Project Method)
8. प्रयोगशाला विधि (Laboratory Method)
9. निरीक्षित अध्ययन विधि (Supervised Study Method)
10. समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि (Socialized Recitation Method)
11. स्रोत विधि (Source Method)
12. इकाई विधि (Unit Method)।
व्याख्यान विधि अथवा भाषण विधि
(Lecture Method)
शिक्षण में व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। आज भी भारतीय विद्यालयों में इस विधि ने महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है। व्याख्यान का तात्पर्य पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। इसमें शिक्षक अपने मुख से बात कहकर पढ़ाता है। बाइनिंग व बाइनिंग इसको कथन विधि (Telling Method) के नाम से पुकारते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। इस विधि द्वारा शिक्षक गहन एवं सूक्ष्म विषय-वस्तु को सरल तथा सुबोध बना सकता है। शिक्षक इसके प्रयोग में व्याख्यान के साथ-साथ स्वयं प्रश्नों द्वारा पाठ का विकास करता चलता है तथा छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके विषय-वस्तु की विवेचना करता है।
प्रयोग (Application) - अब प्रश्न यह है कि शिक्षण में यह पद्धति कब प्रयुक्त की जाये ? इस विषय में यह कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग निम्नलिखित अवसरों पर करना चाहिए-
1. इसका प्रयोग लगभग प्रत्येक प्रकरण या विषय में छात्रों के अध्ययन को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।
2. व्याख्यान पद्धति का प्रयोग बालकों के समय की बचत के लिए भी किया जाना चाहिए।
3. इसका प्रयोग किसी बड़ी इकाई या लम्बे प्रकरण का पुनअवलोकन करने के लिए किया जाना चाहिए।
4. किसी नवीन पाठ की प्रस्तावना से परिचित कराने के लिए भी व्याख्यान पद्धति का उपयोग हो सकता है।
5. इस पद्धति का प्रयोग किसी विषय या प्रकरण का सारांश देने के लिए भी किया जा सकता है।
6. छात्रों में पाठ या विषय के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए।
इस पद्धति के प्रयोग में शिक्षक को परम्परागत ढंग को नहीं अपनाना चाहिए वरन् उसे व्याख्या के साथ विचारोत्तेजक, विकासात्मक एवं बोध प्रश्नों का सहारा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे छात्रों की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्तियों हेतु विकास की वाद-विवाद पद्धति को भी अपनाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों से पाठ का स्वाभाविक एवं तर्कसम्मत विकास होता है।
उदाहरणार्थ, यदि छात्र को उत्पत्ति के भेदों को पढ़ाना है तो विषय का विकास निम्नलिखित ढंग से करना लाभप्रद होगा-
अध्यापक - मिट्टी हमें कहाँ से प्राप्त होती है?
छात्र - भूमि से।
अध्यापक - भूमि किसकी देन है?
छात्र - प्रकृति की।
अध्यापक - भूमि का क्या अर्थ है?
छात्र - निरुत्तर।
अध्यापक - कथन अथवा व्याख्यान।
भूमि के अन्तर्गत सभी प्राकृतिक साधनों, खनिजों तथा पदार्थों का समावेश होता है।
व्याख्यान विधि की उपयोगिता एवं लाभ
(Utility and Advantages of Lecture Method)
व्याख्यान विधि की उपयोगिता एवं लाभ को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है-
1. छात्रों को प्रेरित करने में सहायक - शिक्षण कार्य में अध्यापकों को सर्वप्रथम छात्रों को प्रेरित करना होता है। व्याख्यान विधि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन के विभिन्न प्रकरणों, जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ, महापुरुषों की उपलब्धियाँ, विभिन्न आन्दोलन, भौगोलिक तथ्य एवं परिवर्तन आदि का सरल एवं सुबोध शब्दों में वर्णन करने से छात्र अवश्य ही प्रेरित होते हैं।
2. शिक्षक तथा शिक्षार्थी के सम्पर्क को सरल बनाने में उपयोगी - शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिये शिक्षक तथा शिक्षार्थी में सम्पर्क स्थापित होना अति आवश्यक है। व्याख्यान या भाषण विधि इस सम्पर्क को सरल बनाती है। इस विधि में अध्यापक जब विद्यार्थियों के समक्ष बोलना आरम्भ करता है तो उसके वाणी के उतार-चढ़ाव, उसके शारीरिक संचालन तथा उसकी प्रभावशाली भाषा से विद्यार्थी शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं और स्वतः ही शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य सुविधाजनक सम्पर्क स्थापित हो जाता है।
3. स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण साधन - व्याख्यान अथवा भाषण विधि विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में भूमिका निभाती है। इसमें भाषण समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को प्रश्न करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इस विधि में पहले अध यापक अपने भाषण के दौरान विविध पहलुओं की व्याख्या करता हुआ विद्यार्थियों को समझाता है और यदि फिर भी विद्यार्थियों के मन में कुछ शंकायें रह जायें तो अध्यापक उनको पुनः बताकर दूर करता है।
4. समय और शक्ति की बचत में उपयोगी - विषय की कई बातें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आतीं। विद्यार्थियों को उन्हें स्वतः समझने के लिये कहा जाये तो वे अन्य कई साधनों से उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि विद्यार्थियों द्वारा स्वतः समझने से उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास होगा, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश विद्यार्थी तो इध र-उधर भटकने में अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाते रहते हैं। उनका समय और शक्ति बचाने * तथा उनका उचित मार्गदर्शन करने के लिये व्याख्यान या भाषण विधि अत्यन्त उपयोगी है।
5. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी - भाषण विधि जहाँ सामान्य विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन के कई प्रकरण स्पष्ट रूप से समझने में सहायता प्रदान करती है, वहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ज्ञान अभिवृद्धि के लिये भी प्रेरित करती है। अपना भाषण तैयार करने में अध्यापक कई पुस्तकों व अन्य साधनों से सहायता प्राप्त करता है। अपने भाषण में उल्लेख करने से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में उन पुस्तकों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है और ज्ञान अभिवृद्धि के लिये उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अतः प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये यह विधि अत्यन्त उपयोगी है।
|
|||||