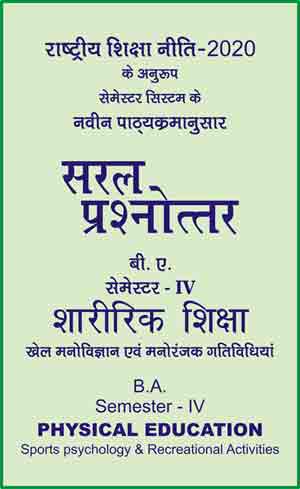|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 5
व्यक्तित्व
(Personality)
प्रश्न- व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिये।
अथवा
व्यक्तित्व से आपका क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व के आयाम का वर्णन कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
अथवा
व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर-
व्यक्तित्व का अर्थ
व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के 'परसोना' से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। नाटकों में चेहरे पर पात्र एक मुखौटा पहनते थे जो नाटक के पात्र की चारित्रिक विशेषताओं के दर्शन कराता था। 'व्यक्तित्व' क्या है? इसके बारे में अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग-अलग मत है। 'व्यक्तित्व' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'पर्सनैलिटी' शब्द का ही हिन्दी अनुवाद है। 'पर्सनैलिटी' शब्द लैटिन भाषा के 'परसोना' से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है- 'मुखौटा' या 'नकली चेहरा। प्राचीन काल में तथा एक आम या अशिक्षित व्यक्ति के लिए 'व्यक्तित्व' से अभिप्राय शारीरिक रचना, रंगरूप, वेषभूषा इत्यादि से था। बाहरी गुणों द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता था। लेकिन व्यक्तित्व का अर्थ समझने के लिए या व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिये अनेक कारक या पक्ष अपना-अपना योगदान देते हैं।
गिलफोर्ड के अनुसार - निम्नलिखित चार प्रतिकारकों के कारण ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है-
(i) सामाजिक अनुक्रिया - व्यक्ति को सामाजिक अनुक्रिया का प्रभाव माना गया है। एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का जो प्रभाव पड़ता है, उसे ही व्यक्तित्व कहा गया है। इस दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति 'व्यक्तित्वपूर्ण' माना जायेगा।
(ii) सर्वव्यापी तत्व - इस विचार के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का योग माना जाता है।
(iii) संगठन पर बल - इस मत के अनुसार व्यक्तित्व किसी एक तत्व या शक्ति की उपज या परिणाम नहीं है। यह मत अनेक तत्वों के संगठन पर बल देता है।
(iv) सम्पूर्ण मत - इस मत के अनुसार व्यक्तित्व सम्पूर्ण व्यक्तित्व है।
आधुनिक सन्दर्भ में व्यक्तित्व एक अत्यंत व्यापक शब्द है तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ इसके परम्परागत शाब्दिक अर्थ से पर्याप्त भिन्न है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से व्यक्तित्व अत्यंत जटिल, भ्रामक तथा अस्पष्ट प्रकृति वाला एक ऐसा प्रत्यय है, जिसकी सर्वमान्य एवं पूर्णतया यथार्थ एवं सुस्पष्ट परिभाषा देना न केवल कठिन बल्कि लगभग असंभव सा कार्य है। मनोविज्ञान के साहित्य में व्यक्तित्व शब्द की अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं तथा उनमें पर्याप्त भिन्नताएँ पाई जाती हैं। व्यक्तित्व की ये सभी परिभाषाएँ किसी एक मत पर सहमत नहीं हो पाती हैं। वास्तव में व्यक्तित्व एक ऐसी अपरोक्ष विशेषता है, जिसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग-अलग ढंग से देखा तथा परिभाषित किया है-
(1) गिलफोर्ड के अनुसार - 'व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है।'
(2) वुडवर्थ के शब्दों में - 'व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है।'
(3) डेशील के अनुसार - 'व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है, जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है।'
(4) ड्रेवर के शब्दों में - 'व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान-प्रदान में व्यक्त करता है।'
(5) बिग तथा हण्ट के शब्दों में - 'व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमान इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है।'
(6) आलपोर्ट ने सन् 1937 में - व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण व वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष निकाला कि 'व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। आलपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गयी व्यक्तित्व की इस परिभाषा को मनोविज्ञान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इस परिभाषा के ऊपर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि वह व्यक्तित्व के संबंध में निम्न तीन प्रमुख बातों की ओर संकेत करती है -
(i) व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है।
(ii) व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं।
(iii) व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है।
व्यक्तित्व की प्रकृति के संगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व किसी एक गुण या गुणों के अलग-अलग समूहों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, वरन् सभी गुणों के एक मिले-जुले या समन्वित रूप से अभिव्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व गुणों का समग्र रूप . है । व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष बताता है कि व्यक्तित्व कोई जड़ या स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि इसमें एक प्रकार की परिवर्तनशीलता तथा नम्यता होती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व कोई स्थायी विशेषता न होकर, एक परिवर्तनशील विशेषता है। परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति तरह-तरह से समायोजन करता रहता है जिसके प्रभाव से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होते रहते हैं। परन्तु व्यक्तित्व के गत्यात्मक रूप का यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्तित्व तेजी से बदलता रहता है तथा आज कोई व्यक्तित्व है तो कल कोई दूसरा व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व काफी लम्बे अंतराल में अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अत्यंत मंद गति से गतिशील होता है। व्यक्ति के तात्कालिक गुण ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही-सही प्रदर्शन करते हैं।
व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है अर्थात् इसमें न केवल शारीरिक गुण वरन् मनोवैज्ञानिक गुण भी निहित रहते हैं। व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर उसके कुल व्यक्तित्व की रचना करते हैं।
इस प्रकार से व्यक्तित्व के प्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, रंगरूप, चाल-ढाल, वेषभूषा, वाणी जैसे अनेक शारीरिक गुण तथा मैत्रीभाव, परोपकार, समाज सेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र जैसे अनेकानेक मनोवैज्ञानिक गुण समाहित रहते हैं। केवल शारीरिक गुणों या केवल मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में कुछ कहना, व्यक्तित्व के अधूरे पक्ष को प्रस्तुत करना ही है।
वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने में उसका व्यक्तित्व भूमिका अदा करता है। वास्तव में वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के दौरान ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण के साथ एक अनूठे ढंग से समायोजन करने का प्रयास करता है। समायोजन का यह अनूठा ढंग ही उस व्यक्ति की अनोखी पहचान का परिचायक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है।
इस प्रकार आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को गतिशील माना है तथा इसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताओं का मिश्रण माना है। व्यवहार द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व गतिशील इसलिये है कि वह समय-समय पर वातावरण की अन्तः क्रियाओं द्वारा स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करता है।
व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक
मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इन कारकों का सम्बन्ध शारीरिक रचना, वंशानुक्रम तथा वातावरण से होता है। व्यक्तित्व को कोई एक ही कारक प्रभावित नहीं करता। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विभिन्न कारक किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये इन्हें हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
(1) जैविक या वंशानुक्रम सम्बन्धी कारक,
(2) वातावरण सम्बन्धी कारक,
(3) मनोवैज्ञानिक कारक।
(1) जैविक या वंशानुक्रम सम्बन्धी - कारक इन कारकों का सम्बन्ध व्यक्ति के जैविक या वंशानुक्रम पक्ष से होता है। ये कारक जन्मजात होते हैं। यही जन्मजात कारक व्यक्तित्व को एक अलग ही स्वरूप प्रदान करते हैं। इन जन्मजात कारकों के निष्क्रिय होने से व्यक्तित्व विघटित हो सकता है। अतः इन कारकों का अपना ही महत्व है। ये कारक निम्नलिखित हैं-
(i) शारीरिक संरचना - किसी भी व्यक्ति के शरीर की रचना वंशानुक्रम पर आधारित होती है। शरीर की रचना के अंतर्गत रंग, कद, भार, शारीरिक दोष, शारीरिक स्वास्थ्य आदि शामिल किये जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का रंग, रूप, कद, भार इत्यादि जन्मजात होते हैं। किसी भी शरीर की सुंदर संरचना सभी ओर से प्रशंसनीय रहती है। यही प्रशंसा व्यक्ति के आत्मविश्वास की आधारशिला है। इसके विपरीत सुन्दर शारीरिक रचना के अभाव में व्यक्ति में हीन भावना घर करने लगती है तथा संवेगात्मक अस्थिरता को जन्म देती है। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति में सामाजिक अस्थिरता भी आ सकती है। इस प्रकार की रचना व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करती है।
(ii) लिंग - भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में यदि देखा जाये तो व्यक्तित्व पर 'लिंग' का भी बहुत प्रभाव देखने में आया है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों पर कई पाबन्दियाँ लगा दी जाती हैं और परिणामस्वरूप उनके व्यक्तित्व की जन्मजात शक्तियाँ दब जाती थीं तथा व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आता था। इसके विपरीत लड़कों को स्वतंत्रता में रखकर उनके व्यक्तित्व को विकसित होने के पूरे अवसर प्रदान किये जाते थे। आज के आधुनिक युग में स्थिति कुछ बदली अवश्य हैं, लेकिन बहुत कम। आज भी लड़की के पैदा होने पर खुशी का प्रदर्शन नहीं होता और लड़के के जन्म पर समारोह किये जाते हैं। लड़की की शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता तथा लड़के की शिक्षा पर लाखों रुपये बहा दिये जाते हैं।
(iii) बुद्धि - बुद्धि को जन्मजात माना गया है। बुद्धि व्यक्तित्व का एक आवश्यक तत्व है। यदि किसी व्यक्ति का आकर्षक शरीर, रंग गोरा और ऊँचा कद है, लेकिन बुद्धि का स्तर निम्न है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका व्यक्तित्व उत्तम नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं, कद छोटा है तथा रंग काला है, लेकिन बुद्धि का स्तर बहुत ऊँचा है तो उसका व्यक्तित्व स्वीकार्य होगा तथा समाज में प्रशंशनीय होगा। बुद्धि युक्त व्यक्तित्व समाज में स्वयं को ठीक ढंग से समायोजित भी कर लेगा तथा समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार भी कर लेगा। लेकिन निम्न बुद्धि वाला व्यक्तित्व न तो समाज में उचित ढंग से स्वयं को समायोजित कर पायेगा और न ही समाज की आशाओं पर खरा उतरेगा। समाज के अन्य सदस्य भी बुद्धिमान व्यक्तित्व के साथ सम्पर्क रखने में गर्व का अनुभव करेंगे। बुद्धिहीन व्यक्ति से सभी लोग दूर-दूर ही रहेंगे, जिससे वह व्यक्ति में हीन भावना जागृत होने का भय रहता है।
(iv) अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ - अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ हारमोन छोड़ती हैं। थाइराइड, पैराथाइराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, एडरनल आदि अन्तःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा छोड़े जाने वाले हारमोन की मात्रा आवश्यकता से कम या अधिक होने पर शरीर का समुचित विकास नहीं हो पाता जिससे सम्पूर्ण व्यक्तित्व परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रभावित होता है।
(2) वातावरण सम्बन्धी कारक - मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार हमारे कुछ व्यवहार जन्मजात होते हैं तथा कुछ व्यवहारों को वातावरण से अर्जित किया जाता है। अतः वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वैसे भी जन्म से ही व्यक्ति एक निश्चित वातावरण में रहता है। जिसको जैसा वातावरण मिलेगा, उसकी वैसी ही विशेषताएँ विकसित होंगी। वातावरण भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है, जैसे-
(i) सामाजिक वातावरण - सामाजिक वातावरण का बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। डलर्ड के अनुसार, "मनुष्य का व्यक्तित्व समाज में वातावरण से गुंथा हुआ होता है। " लारेंस के अनुसार, "संस्कृति वह आधारभूमि है, जिससे व्यक्तित्व विकसित होता है।"
हम सामाजिक वातावरण में रहकर ही वहाँ की माया, रीति-रिवाज, खान-पान की विधि, व्यवहार की विधि आदि अर्जित करते हैं। इस प्रकार, वास्तव में समाज ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गैरेट के अनुसार 'जन्म के समय ही बच्चे का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें वह रहता है, निर्मित और परिवर्तित किया जाता है।'
(ii) सांस्कृतिक वातावरण - मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में उसकी सभ्यता तथा रहन-सहन के ढंग का भी विशेष योगदान रहता है। व्यक्तित्व पर सभ्यता की अमिट छाप रहती है। वैसे भी व्यक्तित्व को संस्कृति का दर्पण कहा गया है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएँ, रीति-रिवाज, रहन-सहन की विधियाँ, धार्मिक विश्वास इत्यादि शामिल होते हैं। अतः जिस संस्कृति में व्यक्ति रहता है, उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास होगा।
(iii) भौगोलिक या भौतिक वातावरण - व्यक्तित्व के विकास में भौगोलिक अथवा भौतिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान की जलवायु ठंडी होती है, वहाँ के लोग गोरे, सुन्दर, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। लेकिन गर्म जलवायु में रहने वाले लोग काले आलसी तथा मंदबुद्धि होते हैं।
(iv) पारिवारिक वातावरण - व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से परिवार का वातावरण भी एक शक्तिशाली कारक माना गया है। व्यक्तित्व के निर्माण में पारिवारिक जीवन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवार का बालक पर नियंत्रण ही उसके व्यक्तित्व के विकास को दिशा प्रदान करता है। यदि नियंत्रण अधिक है तो भी यह हानिकारक है और यदि कम है तो भी बालक गलत दिशा की ओर बढ़ सकता है। घर का वातावरण निम्नलिखित कारकों से मिलकर बनता है
(a) माता-पिता का बच्चे के प्रति दृष्टिकोण - घर में सभी बच्चों के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण क्या है? उनका बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है? तथा माता-पिता की बच्चों के प्रति निष्पक्षता इत्यादि बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।
(b) माता-पिता की योग्यताएँ - घर में माता-पिता की शिक्षा, उनके संवेगात्मक और सामाजिक गुण, उनकी अपनी रुचियाँ, अभिरुचियाँ तथा उनका चरित्र इत्यादि बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं।
(c) परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व और व्यवहार - घर में रहने वाले सभी सदस्यों का व्यक्तित्व और उनका व्यवहार विकसित हो रहे बच्चों को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। बच्चा घर के हर सदस्य के व्यवहार को बड़ी बारीकी से देखता है तथा उसका अनुकरण करता है। कई बार घर के किसी सदस्य को वह अपना गुरु आदर्श भी मान लेता है।
(v) स्कूल का वातावरण - परिवार के पश्चात् बच्चा स्कूल में अधिकतर समय व्यतीत करता है। अतः स्कूल का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ना आवश्यक है। स्कूल में रहकर अनुशासन, नैतिक मूल्यों आदि से बच्चों का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावित होता है। जो बातें बच्चे स्कूल में रहकर सीखते हैं, उन बातों को हम घर पर भी नहीं सिखा पाते। इसी प्रकार स्कूल में सहगामी क्रियाएँ बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में विशेष योगदान करती हैं। अतः जो स्कूल बच्चों को अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं वहाँ पर उनका व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है। स्कूल में बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति, मनोरंजन के साधन, खेलों की व्यवस्था, उच्च आदर्श, नाटक, पुस्तकालय आदि सभी कुछ बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपलब्ध होता है।
(vi) आस-पड़ोस परिवार - तथा स्कूल की भाँति व्यक्तित्व आस-पड़ोस के प्रभाव से भी अछूता नहीं रह सकता। बच्चे के आस-पड़ोस में रहने वाले लोग सुशिक्षित हैं तथा सभ्य हैं तो उस पड़ोस में पनप रहे अन्य बच्चों का व्यक्तित्व अवश्य प्रभावित होगा। यह माना जाता है कि बच्चों में बुरी आदतों का विकास आस-पड़ोस से ही होता है। यही कारण है कि एक अच्छे पड़ोसी का होना अति आवश्यक है।
(3) मनोवैज्ञानिक कारक - व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में मनोवैज्ञानिक कारक भी पीछे नहीं रहते। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित हैं-
(i) इच्छा शक्ति - इच्छा शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। संवेगात्मक संतुलन के लिये सुदृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से अभिप्राय है कि जब व्यक्ति कुछ भी करने की ठान लेते हैं, उसे करके या प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति सदा असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आत्म-विश्वास का भी अभाव रहता है। अतः सुदृढ़ इच्छा-शक्ति का होना एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है।
(ii) आकांक्षा स्तर एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा - व्यक्ति की आकांक्षाओं का स्तर और उसकी उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपलब्धि के लिये अर्थात् कुछ प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित रहना एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। यदि उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर बहुत निम्न है तो वह व्यक्ति निकम्मा, सुस्त तथा आलसी व्यक्तियों के वर्ग में आता है। दूसरी ओर, जिनमें आकांक्षा का स्तर ऊँचा होगा, उनमें उपलब्धि- अभिप्रेरणा का स्तर भी अधिक रहेगा। ऐसे व्यक्ति सदा कर्म पर अधिक विश्वास करते हैं, न कि भाग्य पर।
(iii) रुचियाँ एवं दृष्टिकोण - व्यक्ति की रुचियाँ और दृष्टिकोण उसके व्यवहार करने के तरीकों तथा व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालते हैं। हमारे हर कार्य तथा व्यवहार में रुचि का कुछ न कुछ अंश अवश्य होता है। जिन चीजों के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उनमें हमारी रुचि होती है तथा जिनके प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण होता है उनमें हमारी रुचि नहीं होती। अतः हमारा व्यवहार इन दृष्टिकोणों और रुचियों पर निर्भर करता है।
(iv) बुद्धि तथा मानसिक विकास - व्यक्तित्व के निर्धारण में उसकी बुद्धि और मानसिक विकास का बहुत अधिक हाथ होता है। उसका व्यवहार उसकी मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है तथा व्यक्तित्व उसके व्यवहार से जुड़ा रहता है। व्यक्ति का सम्पूर्ण समायोजन, अधिगम प्रक्रिया तथा सीखने में सफलता, ज्ञान को अर्जित करना तथा कौशल सीखने, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को हल करने की योग्यता, व्यक्तियों और परिस्थितियों से तालमेल रखने का कौशल आदि व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। व्यक्ति का व्यवहार वही बनता है, जो उसकी बुद्धि और मानसिक क्षमता द्वारा बनाया जाता है।
(v) संवेगात्मक विशेषताएँ - व्यक्ति की संवेगात्मक विशेषताएँ तथा उसका स्वभाव उसके व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं। सकारात्मक संवेग तथा नकारात्मक संवेगों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। एक क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव एक शान्त व्यक्ति से भिन्न होगा। इसी प्रकार सबके हित की बात सोचने वाले व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्तित्व भी अलग प्रकार का ही होगा। संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही संतुलित होता है।
(vi) अन्य मनोवैज्ञानिक कारक - उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जैसे अर्जित रुचियाँ, चरित्र, तर्क, चिंतन, कल्पना सम्बन्धी क्षमताएँ, समायोजन सम्बन्धी योग्यताएँ इत्यदि।
|
|||||