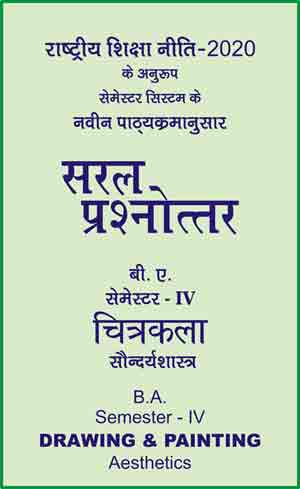|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला बीए सेमेस्टर-4 चित्रकलासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 7
भारतीय कला में सौन्दर्यशास्त्र की अवधारणा
(Concept of Aesthetics in Indian Art)
प्रश्न- सौन्दर्यशास्त्र की भारतीय परम्परा के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर-
सौन्दर्यशास्त्र की भारतीय परम्परा - भारत में पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्र की प्रमुख अवधारणा ब्यूटी के लिए सौन्दर्य को स्थिर कर दिया गया परन्तु पश्चिमी सौन्दर्य के विचारक्रम को समझाने के लिए निरन्तर नवीन प्रयोग एवं निरन्तर नवीन शब्दों को प्रयुक्त किया गया याकोबी ने रस के लिए जर्मन शब्द स्टिमंग का प्रयोग किया। कुछ विज्ञान गेशमेक तथा कुछ सेवर का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में टेस्ट, ऐलिश, एस्थेटिक, इमोशन इत्यादि शब्द मिलते हैं। रस सौन्दर्य विरोधी तत्व नहीं है। रसवादी आचार्यों ने भी रस के अन्तर्गत किसी न किसी रूप में सौन्दर्यबोधक तत्व को समाविष्ट किया है। आनन्दवर्धन ने रस को जानने के लिए तत्व को लावण्य कहा है। पण्डितराज जगन्नाथ ने रस को रमणीयता का वाहक कहा है। संस्कृत काव्य परम्परा में सौन्दर्य शब्द का सम्बन्ध अलंकार एवं रीतियों माना गया। एस संज्ञा में कलागत सौन्दर्य के साथ ही उसकी अनुभूति का सौन्दर्य भी निहित हैं। भारतीय दार्शनिकों ने भौतिक सौन्दर्य पर वार्शनिक विवेचन नहीं दिये। धर्म ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारत में धार्मिक एवं सौन्दर्यानुभूति एक ही स्पष्ट रूप से दिखाई दी। भारतीय दृष्टि से सौन्दर्य सार्वभौमिक है जिसकी अनुभूति अलौकिक है। सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से पाश्चात्य सौन्दर्य दृष्टिकोण स्थूल रहा तथा पूर्वी दृष्टिकोण सूक्ष्म। पाश्चात्य दर्शन की भाँति पूर्वी दर्शन में सौन्दर्य के भौतिक स्वरूप को लेकर कभी भी चिन्तन, मनन व विवेचन नहीं हुआ।
उत्सव व विकास - सौन्दर्यशास्त्र की भारतीय परम्परा के अन्तर्गत प्रागैतिहासिक गुफा चित्र, भित्ति चित्र, प्राचीन साहित्य, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक काल, मौर्य, शुंग, सप्त वाहन, कुषाण, गुप्तकाल, मध्य-काल एवं आधुनिक काल तक कला व सौन्दर्य की समृद्ध परम्परा एक नदी की भाँति बह रही है। सौन्दर्य को अनुभूति की वैयक्तिकता की परिधि में नहीं बाँधी जा सकती। प्रत्येक युग में भावना की एकता ही प्रबल होती है किन्तु तत्व समान होते हैं। आदिम मानव के मन में स्वतन्त्र, प्रचण्ड तूफानों, अवध गति से प्रवाहित करते पशुओं ने मर्यादाहीनता और स्वच्छन्दता के भाव उत्पन्न किये और इसी बन्धन विहीनता में आदिम मानव ने सौन्दर्य अनुभूति का आनन्द लिया। उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद व सुचारु पूर्वक बना सके। इसी से कला व सौन्दर्य की भावना उत्पन्न हुई। उसके जीवन की कोमलतम भावनाएँ तथा संघर्षपूर्ण जीवन के क्षणों को अनगढ़ पत्थरों पर उकेरा। भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता-संस्कृति हड़प्पा संस्कृति भी यहीं से भारतीय कला का प्रारम्भ होता है। इस संस्कृति का विस्तार 4000-1800 ई. पू. के मध्य हुआ था। विभिन्न सुविधाओं से युक्त आवास, अन्न भण्डार, स्नानागार आदि से प्राप्त अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि हड़प्पा संस्कृति में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पर थी। इस समय का मानव कला शिल्प में निपुण था। इस युग में चित्रण कला, मूर्ति - निर्माण - कला और संगीत कला पर्याप्त उन्नत थी। मिट्टी के बर्तनों पर सुन्दर अलंकरण व विविध आकृतियों द्वारा सजावट चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्रों का निर्माण भी होता था। तैयार किये गये वस्त्रों पर अनेक प्रकार के अलंकरण एवं आकृतियाँ बनाई (काढ़ी) जाती थीं। छपाई का भी प्रचलन रहा। मिट्टी, चूना पत्थर तथा कांस्य मूर्तियों का निर्माण भी होता था। इसका आश्चर्यजनक उदाहरण है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। यह मूर्ति तत्कालीन मानव के सौन्दर्यबोध की परिचायक हैं। मुद्राओं पर मानवाकृतियाँ व पशु आकृतियाँ लिपि के साथ अंकित मिलती है। तत्पश्चात् वैदिक काल (10000 ई.पू. से 6000 ई. पू.) का प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्ययन से उपलब्ध स्रोतों में पुरातत्व व पुरातन साहित्य महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राचीनता (पुरातत्व) दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो साहित्य की दृष्टि से भारतीय कला व संस्कृति का परिपक्व रूप हमें वेदों में दृष्टव्य है। इन प्राचीनतम ग्रन्थों में भारतीय आर्यों की सभ्यता, संस्कृति, जीवन व धर्म का परिचय दृष्टिगत है क्योंकि चिन्तन, दर्शन एवं साक्षात्कार के क्षणों में जो ज्ञान - रश्मियाँ वैदिक ऋषियों के हृदय में उतरीं उन्हें शब्दों व प्रतीकों के माध्यम से वेद मंत्रों व सूक्तियों में बाँधा गया। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेदों की संख्या चार है जिनकी सामग्री का सम्पादन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने ऋक, यजुष, साम, अथर्व की संहिताओं के रूप में किया। वैदिक साहित्य का विकास क्रम वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में दृष्टिगत होता है। सर्व प्राचीन ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर कलात्मक सौन्दर्य का उल्लेख हुआ है। रूप निर्माण का वर्णन भी मिलता है। निवास स्थान काष्ठ शिल्प के अद्वितीय उदाहरण थे जिनको अलंकरणों से सज्जित किया जाता था। उस समय स्त्रियाँ भी विद्वान थीं। वे रंगाई, कढ़ाई व बुनाई इत्यादि कलाओं में निपुण थीं। वस्त्राभूषणों की रुचि तथा अंग लेप द्वारा सौन्दर्य को बढ़ाया जाता था। नाविक, धनुषकार, रंगरेज, संगतकार, बुनकर, संगीतकार, शिल्पकार और चित्रकार जैसे पेशेवरों ने विभिन्न कलाओं को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों, सूत्र -ग्रन्थों तथा वेदांगों की रचना हुई। इसके अन्तर्गत दस्तकारी, स्वर्ण रजत आभूषणों का निर्माण, सिक्कों तथा गृह उद्योगों का वर्णन मिलता है। गृह निर्माण की कला का विकास हुआ, जिसके सभी मूल तत्वों का उल्लेख है। जैसे नींव, कोठे, सभा, पंखे, अन्तःपुर द्वार, आलिन्द, ऊर्ध्वछन्द, सूत्रमापन, अध: छन्द, स्तम्भ, छत इत्यादि। उस समय चित्रकला अलंकरण के रूप में दृष्टव्य थी। घर को रमणीक व अलंकृत बनाया जाता था। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है, इस चित्र को यज्ञ के समक्ष लटकाया जाता था। यज्ञ की समाप्ति पर लपेट दिया जाता था। चौखटों पर देवियाँ ऊषा तथा रात्रि की प्रतीक बनाई गईं। अथर्ववेद में ऐसे अलंकृत घरों की उपमा अलंकृत हथिनी से दी गई है। आज ये सभी उदाहरण प्राप्त नहीं हैं मात्र साहित्यिक उल्लेख ही इसका प्रमाण है। वस्तुतः वैदिक ऋषियों ने सौन्दर्य को परम सत्ता के गुणों के रूप में देखा और सत्यं शिवं और सुन्दरम् के दर्शन किये। 'ईश', 'केन', 'कंठ' और 'माण्डुक्य' उपनिषदों में सौन्दर्य का रूप सौन्दर्याभिव्यक्ति, सामजस्यपूर्ण, भावपूर्ण तथा अविरल प्रवाह से युक्त है। ऋषियों ने जिस सौन्दर्य का वर्णन किया वह परमतत्व का सौन्दर्य है जिसे उन्होंने मानव व प्रकृति दोनों में देखा। इनके अनुसार परमतत्व बुद्धि से ग्रहण करने पर सत्य, अभ्यास से ग्रहण करने पर शिव तथा मानव व प्रकृति में प्रकाशित होकर सुन्दर हो जाता है। यही सच्चिदानंद रूप है अर्थात् आनन्द ब्रह्म है और सौन्दर्य आनन्द का ही मूर्त रूप है। यह वैदिक काल ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी तक विकसित रहा। उत्तर वैदिक काल में लगभग 8000 ई. पू. से 500 ई. पू. के मध्य महाकाव्यों की रचना हुई जिनमें रामायण, महाभारत व अष्टाध्यायी महत्वपूर्ण है। इसे महाकाव्य काल भी कहा जाता है। महाकाव्य काल में वैदिककालीन सौन्दर्य प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप पर केन्द्रित नहीं रह सका और अनेक प्रकार की राजनैतिक व सामाजिक समस्याओं में उलझा रहा। ऐसा दृष्टव्य है कि आदिम युग का सौन्दर्य प्राकृतिक था तो वैदिक युग का सौन्दर्य दिव्य, महाकाव्य काल में सौन्दर्य का रूप मानव सौन्दर्य में परिलक्षित हुआ। व्याकरण आचार्य पाणिनी की रचना अष्टाध्यायी में पशु-पक्षियों के अंकन की विधि तथा मुद्राओं के प्रचलन का वर्णन मिलता है। इसमें शिल्प का चारु (ललित) और कारू (उद्योग) के अर्थो में प्रयुक्त किया है। रामायण व महाभारत की रचना सैकड़ों वर्षों के कालक्रम में हुई होगी। रामायण में आर्य श्रीराम के द्वारा अनार्य नेता रावण के वध और राज्य की 'क्रौंच कथा' के शोक में ही महाकाव्य काल का मानव सौन्दर्य छिपा है, जिसमें सौन्दर्य व करुणा की आर्द्रता का समन्वय महर्षि वाल्मीकि ने किया है। महर्षि ने बालकाण्ड के छठे सर्ग में अयोध्या वर्णन के साथ अंग राग, केश सज्जा, स्त्रियों के कपोलों पर पत्रावली का श्रृंगार, राजमहलों, रथों व पशुओं की साज-सज्जा का उल्लेख किया है जिससे तत्कालीन समाज में कला के व्यावहारिक रूप व उच्च स्थान की प्रतिष्ठापना होती है। राम को संगीत, वाद्य तथा चित्र आदि का ज्ञाता भी बताया है। अश्वमेघ यज्ञ के समय राम द्वारा सहधर्मिणी सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण करवाने का उल्लेख भी है। यह प्रतिमामय नामक शिल्पी ने बनाई थी। रावण की लंकापुरी में हनुमान द्वारा एक चित्र दीर्घा तथा चित्रित क्रीड़ागृह देखे जाने का वर्णन भी महर्षि ने किया है। रानी कैकेयी के चित्रित भवन व श्रीराम के राजप्रासाद के भित्ति चित्रों के वर्णन से भी तत्कालीन कलाभिरुचि का ज्ञान होता है। बाली व राचण की शव पालकियों एवं पुष्पक विमानों को भी चित्रित किया गया था। उपर्युक्त उदाहरणों से वाल्मीकि के समय में कला के प्रति समाज में निहित उत्कृष्ट अभिरुचि एवं सौन्दर्यबोध का साक्ष्य मिलता है।
महाभारत विश्व का सर्वाधिक बड़ा काव्य ग्रन्थ है। प्रारम्भ में इसमें 8,000 श्लोक थे। कालान्तर में श्लोकों की संख्या बढ़ती गई तथा वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें दो मानव पक्षों का संघर्ष नहीं वरन् एक मानसिक संघर्ष है जिसमें एक ओर प्राकृतिक भोग, पशुत्व की लालसा का प्रतीक है कौरव पक्ष है, तो दूसरी ओर नीति, धर्म व मर्यादा से युक्त पाण्डव पक्ष है। यह भोग व मर्यादा का संघर्ष कृष्ण के शान्त व्यक्तित्व में सौन्दर्यानुभूति प्राप्त करता है। शान्त रस सौन्दर्य चेतना का मुख्य अंश है। महाभारत में उषा-अनिरुद्ध की कथा में देवताओं, महापुरुषों तथा युवराजों के छवि चित्र एक परिचारिका चित्रलेखा द्वारा बनाने का उल्लेख किया गया है। एक अन्य कथा के अन्तर्गत सत्यवान द्वारा भी घोड़े का भित्ति-चित्र अंकित करने का प्रसंग स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है । धर्मराज युधिष्ठिर के सभा भवन में भी भित्ति चित्रण का वर्णन है। यह सज्जा मयसुर नामक चित्रकार ने की थीं। यह सज्जा अनोखी थी इसमें कौरव भ्रमित हो गये हैं तथा द्रौपदी द्वारा परिहास करने पर अपमानित हुए, यहीं से पाण्डव - कौरव युद्ध का प्रारम्भ हुआ जो महाभारत का प्रमुख विषय है। रामायण व महाभारत के पश्चात् पणिनि की अष्टाध्यायी में भी कला का उल्लेख मिलता है। इसमें शिल्प को चारु (ललित) तथा कारु (उद्योग) कहा गया है। पशु-पक्षी, पुष्प, वृक्ष, नदी, पर्वत इत्यादि के सांकेतिक लक्षणों के वर्णन के साथ चित्रित किया गया है एवं उसकी विधि को भी प्रस्तुत किया गया। इसी समय पुराणों को भी लिपिबद्ध किया गया जिसकी संख्या 18 (अठ्ठारह) है। मत्स्यपुराण में भारतीय शिल्प के जनक तथा वास्तुशास्त्र के पुरातन अठ्ठारह आचार्यों की नामावली दी गई। इनमें विश्वकर्मा जी का नाम प्रमुख है। इन्होंने शिल्प- शास्त्र पर अनेक ग्रन्थों को रचा। वस्तुतः वैदिककाल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिल सके। काष्ठ निर्मित भवन, गुहा-चित्र तथा साहित्यिक मूल-प्रमाण प्राकृतिक प्रकोन व परिवर्तन के कारण नष्ट हो गये। समय-समय पर लिखी गई टीकाओं, भाष्य एवं ग्रन्थों के संकलनों से तत्कालीन कला व सौन्दर्य सम्बन्धी तथ्यों के प्रबल साक्ष्य प्राप्त हैं। तीसरा चरण 600 से 200 ई. पू. का है। इस समय भारतीय इतिहास के प्रथम साम्राज्य का उत्थान एवं पतन भी दृष्टव्य है। यह कोल राजनैतिक व सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय भगवान बुद्ध से सम्राट अशोक तक वैदिक धर्म के साथ हिन्दू धर्म के विश्वासों व कर्मकाण्डों, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों का प्रचार व प्रसार हुआ। वैदिक धर्म के कर्मकाण्डों का विरोध हुआ फिर भी इस समय जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र, बौद्ध - पिटकों तथा जातकों में चित्रकला व सौन्दर्य का उल्लेख प्राप्त होता है।
इसी समय वात्स्यायन का कामसूत्र, कला सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रन्ध है। चन्द्रगुप्त मौर्च (921 - 207 ई. पू.) के समय में रचित कारू (उद्योग) शिल्पियों की नामावली दी गई। यह विश्वकोशात्मक तथा अति महत्वपूर्ण रचना है। मौर्यकालीन कला के दर्शन हमें राजगृह के महादुर्ग, जोगीमारा गुफा, लौरियानन्दगढ़ के स्तूप, काष्ट-स्तम्भों, मातृदेवी की मूर्तियों मंजुषाओं, श्री चक्र तथा अशोक स्तम्भों में होते हैं। इसके पश्चात 200 ई. पू. से 800 ई. तक कला व सौन्दर्य से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों की रचना हुई तथा कलाओं का भी पर्याप्त विकास हुआ। भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' शूद्रक का मृच्छकटिक, मानसार महत्त्वपूर्ण है। शुंग - सातवाहन काल (187-76 ई. पू.) में अजन्ता व उदयगिरि की कलात्मक गुफाएँ आदि चित्रकला व मूर्तिकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैन धर्माबलम्बी श्री पालित रचित तरंगवती, गुणालच की बृहत्कथा मंजरी, हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती, अश्वघोष का बुद्धचरित व सौन्दरानन्द आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ भी हैं जिनमें कला सम्बन्धी उल्लेख मिलते। प्रथम शताब्दी ई. में कुषाण शासन काल की गान्धार कला भी उल्लेखनीय है, जो प्रथम शताब्दी में उचित भारत - यमन कला की समन्वयात्मक प्रज्ञा का परिणाम थी। कला की दृष्टि से यह युग नवीन प्रयोगात्मक युग कहा जा सकता है।
प्राचीन काल का अन्तिम चरण 275 ई. से 800 ई. तक रहा। यह समय गुप्तकाल के नाम से जानते हैं। कला की दृष्टि से यह स्वर्णकाल माना गया है। चन्द्रगुप्त (प्रथम), चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) समुद्रगुप्त अदि के समय में कला की चहुँमुखी उन्नति हुई। गुप्त सम्राट साहित्य मर्मज्ञ, कलाकारों के आश्रयदाता तथा स्वयं भी कलाओं में निपुण थे झाँसी के देवगढ़ मन्दिर, कानपुर के भीतरगाँव मंदिर, भुमरा का शिव मन्दिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, परण की विष्णु प्रतिमा, वाराह प्रतिमाएँ, शिव मूर्तियाँ आदि इस युग (गुप्तकाल) चिरस्मरणीय देन रही हैं। अजन्ता व बाघ के गुफा चित्र, भिति चित्रकला अनुपम उदाहरण हैं। अजन्ता के भित्ति चित्रों में भारतीय षडांगों की सुन्दर अभिव्यक्ति है। संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। महाकवि कालिदास के काव्य ग्रन्थ ऋतुसंहारम्, मेघदूतम्, कुमारसम्भवम् रघुवंश तथा नाट्यग्रन्थ के अन्तर्गत विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्, मालविकाग्निमित्र, भारवि का किरातार्जुनीयम, बाणभट्ट की कादम्बरी हर्ष चरित, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कथाएँ, अमर सिंह का अमरकोश, भर्तृहरि का श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, वाक्य प्रदीप, महाभाष्य दीपिका, भवभूति का उत्तर राम भरित, माघ का शिशुपाल वध, अमरू का अमरुशतक, हर्षवर्धन की रत्नावली इत्यादि बेजोड़ साहित्यिक रचनाएँ हैं। युद्धघोष का ललित विस्तार, दण्डी का काव्य दर्शन, सुबन्धु का वासवदत्तम्, विष्णुधर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्रम् उपर्युक्त गुप्तकाल के समय की रचनाएँ हैं।
तत्कालीन साहित्य में राजनैतिक घटनाओं के साथ श्रृंगार, रूपक, हास्य - प्रसंग, दर्शन, कला व सौन्दर्य का विवेचन भी प्राप्त हुआ।
कला की दृष्टि से मध्ययुग अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, इसके अन्तर्गत गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष इत्यादि ग्रन्थों की रचना मध्यकालीन गौरव के प्रतीक हैं। कला सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना दृष्टव्य हैं। इसके अन्तर्गत वास्तु, मूर्ति और चित्र कलाओं के लक्षण, नियम उपनियम, आधार, वर्ण संयोजन, लैप्य कर्मादि का प्रामाणिक और वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। चित्रशास्त्र के सिद्धान्तों का उद्घाटन करने वाले प्रतिनिधि ग्रन्थ मानसार का परवर्ती मध्ययुगीन संकलन, चित्रलक्षणम् का तिब्बती अनुवाद, समरांगण सूत्रधार, मानसोल्लास, अभिलषितार्थ चिन्तामणि, शिल्परत्न, आचार्य माधव विद्यारण्य की पंचदशी का चित्रद्वीप प्रकरण, कामसूत्र की टीका जयमंगला, गुणाढ्य की बृहत्कथामंजरी का संस्करण, कथा सरित्सागर, श्रीहर्ष का नैषधचरित्, जयदेव का प्रसन्नराघव, पद्मपुराण, गीत-गोविन्द, कल्हण की राजतरंगिणी, कंबन की रामायण, जायसी का पद्मावत, केशवदास की रसिकप्रिया, तुलसीदास की रामचरितमानस आदि चिरस्मरणीय एवं हृदयस्पर्शी अनमोल साहित्यिक कृतियाँ हैं जिसमें सौन्दर्यबोध एवं कलाप्रियता स्पष्ट परिलक्षित है। साहित्यशास्त्र सम्बन्धी रचनाओं के अन्तर्गत भामह का काव्यशास्त्र, दण्डी का काव्यदर्शन, उदभट्ट का काव्यालंकार और संग्रह, वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, सद्रभट्ट का शृंगार तिलक, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, भट्टतौस का काव्य कौतुक, राजशेखर की काव्य मीमांसा, क्षेमेन्द्र का औचित्य विचार, भोजराज का श्रृंगार प्रकाश, मम्मट का काव्य प्रकाश तथा अभिनवगुप्त, कुन्तक, भानुदत्त, रूप गोस्वामी, पण्डितराज जगन्नाथ के विचार मध्य काल की अनमोल धरोहर हैं, जिनमें कला व सौन्दर्य सम्बन्धी विचार दृष्टव्य हैं। इस समय जैन व बौद्ध ग्रन्थ भी रचे गये। सचित्र बौद्ध ग्रन्थों में अष्टसाहस्रिका, प्रज्ञापारमिता, पञ्चरक्षा और महामयूरी गण्डव्यूह प्रमुख हैं, जो 9वीं से 12 वीं शताब्दी के मध्य चित्रित हुए। जैन सचित्र पोथियों में कल्पसूत्र, बालगोपाल स्तुति, दुर्गासप्तशती, रतिरहस्य, गीत गोविन्द, वसन्तविलास, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णिका, उत्तराध्ययन सूत्र, औधनियुक्ति, नेमिनाथ चरित, अंगसूत्र, संग्रहणीयसूत्र, सुरसुन्दरी कहा, त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरित तथा पाल सचित्र पौधियों में प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा करनवेव गुहा इत्यादि तत्कालीन कला परम्परा के साक्षात् प्रमाण हैं।
वास्तुकला व मूर्तिकला के श्रेष्ठ उदाहरण एवं भित्ति चित्र भी मध्यकालीन कला की अमूल्य धरोहर हैं जिनमें महाबलिपुरम् वृहदेश्वर मन्दिर संजीर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो, माउंट आबू के जैन मंदिर, नटराज की कांस्य प्रतिमा तथा चोलेश्वर, तिरुपतिपुरम् लेणक्षी व ऐलोरा के भित्ति चित्र प्रमुख हैं। पन्दहवीं शताब्दी के लगभग मुगल साम्राज्य में मुगल व राजस्थानी कला भी बहुत फली फूली। मुगल काल में वास्तुकला के माधाब नमूने मिलते हैं। उदाहरण के लिए शेरशाह का मकबरा, हुमायूँ का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, सिकन्दरा, आगरा का लाल किला, ताज महल, दिल्ली की जामा मस्जिद में लाल किला आदि। इसी समय उर्दू-फारसी ग्रन्थ बाबरनामा, हुमायूँ नामा, अकबरनामा, आईने अकबरी की रचना भी हुई। भारतीय ग्रन्थों में महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवहीता, पंचतंत्र इत्यादि का फारसी अनुवाद भी हुआ तथा चित्रित भी करवाया। राजस्थानी व पहाड़ी चित्र शैलियाँ भी चरमोत्कर्ष पर पहुंची जिनमें नायक नायिका भेव बारहमासा, रसिकप्रिया, रागमाला, बल्लभ सम्प्रदाय, वैष्णव व शेष मतों पर चित्रण हुआ। सदियों के कालक्रम में भारतीय सौन्दर्यशास्त्रीय परम्परा के विकास की यह एक संक्षिप्त रूपरेखा है। इन हजारों वर्षों में उस महान कला, संस्कृति तथा दर्शन का निर्माण हुआ जिसमें विश्वास व धर्म, दर्शनशास्त्र, काव्यशास्त्र, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला, नृत्यकला आदि कलाओं की अनेक धाराएँ विकसित हुई। भारतीय कला का आधार ही धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा दृष्टव्य है। यहाँ कलाकार पहले दार्शनिक है तत्पश्चात् कलाकार एवं सौन्दर्यदृष्टां है। उन्नीसवीं शती से कला, साहित्य, संगीत, नाटक, काव्य आदि में नवीन पद्धतियों व रूपों का विकास हुआ। आधुनिक काल में रवीन्द्रनाथ टैगोर, ई. बी. हेबेल, आनन्द कुमार स्वामी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ. कांतिचन्द्र पाण्डेय, डॉ. नगेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, सरमोनियर विलियम्स, पर्सी ब्राउन आदि ने कला व सौन्दर्य के गूढतम रहस्यों के मर्म को पहचानने तथा परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इक्कीसवीं शताब्दी में कला और सौन्दर्य में नवीन सौन्दर्य दृष्टि की आवश्यकता है। आज की कला समसामयिक संघर्षों, जटिलताओं, नवीन अन्वेषणों, रहस्यों, मशीनी व वैज्ञानिक युग से प्रभावित होकर नवीन परिवेश में दृष्टव्य है।
|
|||||